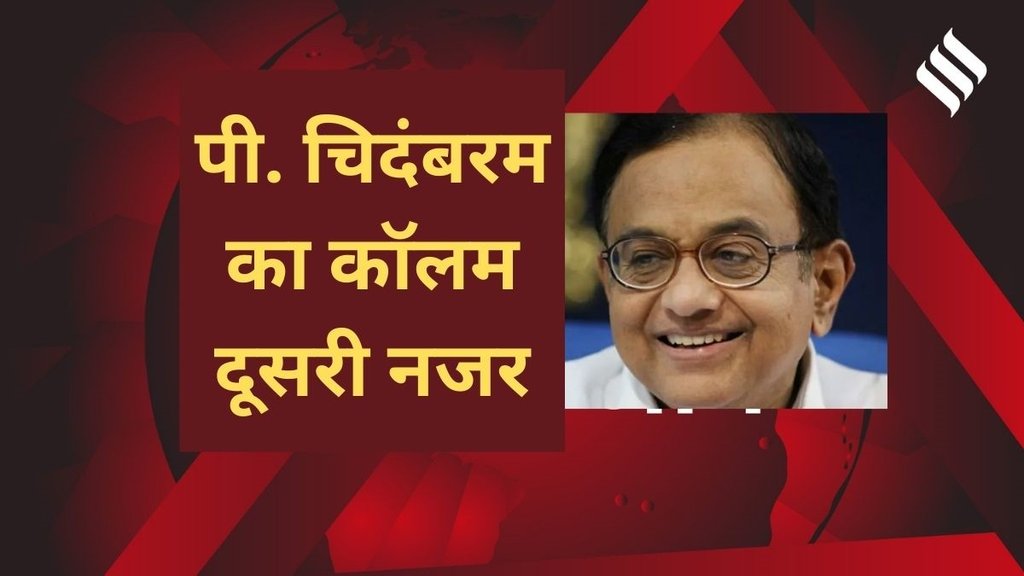P. Chidambaram Election Lessons: एक उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना कठिन काम होता है, उसमें एक उतार-चढ़ाव भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। किसी उम्मीदवार की ओर से चुनाव की जिम्मेदारी संभालना मुश्किल और जोखिमभरा काम होता है। एक राजनीतिक दल की ओर से राज्य चुनाव की निगरानी करना और उसका प्रभारी होना एक जटिल काम है, जिसमें कई अलग-अलग काम करने होते हैं। चुनाव एक निर्णायक फुटबाल मैच की तरह है, जिसमें एक कोच विजेता होता है और प्रतिद्वंद्वी को हार का मुंह देखना पड़ता है।
एक पार्टी या तो चुनाव जीतती है या हारती है। जब किसी राजनीतिक दल के हारे हुए चुनावों की संख्या जीते गए चुनावों की संख्या से अधिक हो जाए, तो वह उसके लिए थोड़ा ठहर कर चिंतन करने का समय होता है। मेरी कहानी 1984 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी से शुरू होती है। मैंने आठ लोकसभा चुनाव लड़े और सात जीते। मैंने अपने चुनावों से पहले और बाद में, कई चुनाव कराए हैं। मैं अब भी अपने जिले में चुनावों पर व्यापक निगरानी रखता हूं।
समय बदल गया है
एक समय था, जब चुनाव जीतने के लिए चेहरा, वादे या हाव-भाव ही काफी होता था। अब नहीं। एक समय था, जब किसी उम्मीदवार को किसी जाति के नेता या नेताओं का समर्थन मिल जाता था, जो उस जाति के बहुलांश वोट पा जाने के लिए पर्याप्त होता था। अब नहीं। एक समय था, जब घोषणापत्र अप्रासंगिक हुआ करता था। अब नहीं। एक समय था, जब राजनीतिक दलों ने ‘नैरेटिव’ शब्द की खोज नहीं की थी। यह शब्द, अपनी अनेक बारीकियों के साथ, आधुनिक समय के चुनावों में प्रमुख शब्द है।
मेगाफोन, माइक्रोफोन, पोस्टर, पर्चे, झंडे और तोरण, जो चुनावों में गोला-बारूद हुआ करते थे, अब पुराने पड़ चुके हैं। अब सोशल मीडिया, टेलीविजन विज्ञापन, फर्जी खबरें और ‘पैकेज’ नामक एक अपमानजनक प्रथा, जिसे आमतौर पर ‘पेड न्यूज’ के रूप में जाना जाता है, नए हथियार और गोला-बारूद हैं। शुक्र है कि कुछ अखबार अपना ईमान बचाए हुए हैं। पर, मुझे डर है कि अगले दस वर्षों में अखबार, चुनावों में अप्रासंगिक हो जाएंगे।
कुछ स्थिरांक
मैं पिछले पचास वर्षों से चुनावी परिदृश्य में आए नाटकीय बदलावों का गवाह रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें स्थिर बनी हुई हैं और हमेशा बनी रहेंगी, हालांकि उनमें सुधार होता रहेगा। एक राजनीतिक दल के लिए कुछ स्थिरांक इस प्रकार हैं: शहर, जिला और अधीनस्थ समितियां: किसी भी पार्टी के लिए राष्ट्रीय समिति पर्याप्त नहीं है, जो तीन महीने में एक बार मिल सकती है। शहर, जिला, ब्लाक, वार्ड और गांव की समितियां जरूरी हैं, जिनका दिल चौबीसों घंटे धड़कता रहता है। आप उस राजनीतिक दल के बारे में क्या कहेंगे, जिसने कई वर्षों से शहर, जिला या अधीनस्थ समितियों का गठन या नियुक्ति नहीं की? मैं उसके बारे में यही कह सकता हूं कि उस राज्य में राजनीतिक दल सिर्फ एक अवधारणात्मक विचार के रूप में मौजूद है।
समावेशी नीतियां और व्यवहार: हालांकि लगभग सभी राजनीतिक दल सदस्यता और पार्टी के कार्यकारी निकायों में प्रतिनिधित्व में समावेशिता का प्रचार करते हैं और आमतौर पर इसके लिए गतिविधियां भी चलाते हैं, पर उम्मीदवारों का चयन करते वक्त वे चूक जाते हैं। ‘जीतने की क्षमता’ की आड़ में, वे अक्सर प्रतिद्वंद्वी गुट या किसी खास जाति के उम्मीदवारों को बाहर कर देते हैं। यह पहले से मान लेना कि कोई खास जाति पार्टी का समर्थन करेगी या कोई खास जाति प्रतिद्वंद्वी पार्टी का समर्थन करेगी, उम्मीदवारों के चयन में एक जाति के पक्ष में झुकाव पैदा करेगा और दूसरी जाति को हाशिए पर धकेल देगा। मेरा अनुभव है कि चुनावों में जाति की पकड़ लगातार काफी कमजोर हुई है। जब महिलाओं की बात आती है, तो व्यावहारिक रूप से हर सीट पर ‘जीतने की संभावना’ के भ्रामक तर्क पर पुरुष उम्मीदवार के पक्ष में पूर्वाग्रह बना लिया जाता है।
अनुशासन बनाना: चुनाव के समय हर पार्टी में अनुशासन भंग हो जाता है। उम्मीदवार के खिलाफ काम करना आम बात है। बागी उम्मीदवार, जिनमें से कुछ प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा लगाए गए होते हैं, नए और बढ़ते हुए खतरे होते हैं। बागी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या- कभी-कभी आधिकारिक उम्मीदवार को तीसरे या चौथे स्थान पर धकेल देती है। आमतौर पर इससे साबित होता है कि ‘बागी’ पार्टी कार्यकर्ताओं का पसंदीदा उम्मीदवार था। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि, एक राज्य विधानसभा चुनाव में, एक राजनीतिक दल ने बागी उम्मीदवारों की उपस्थिति के कारण सत्रह सीटें तक खो दी।
बूथ समितियां: कुछ राजनीतिक दलों के पास सक्रिय बूथ समितियां हैं। इनमें द्रमुक और एआइडीएमके अग्रणी थे। हाल ही में, आरएसएस के समर्थन से, भाजपा ने द्रविड़ दलों की नकल करने की कोशिश की और कुछ हद तक सफल भी हुई। बूथ समितियां अकेले चुनाव के अंतिम चरण में वोटों के लिए प्रचार और मतदान के दिन मतदाताओं को लामबंद कर सकती हैं। बूथ समितियों को तैनात करने में विफल रहने वाली पार्टी संभावित समर्थकों के वोट खो देगी।
चुनाव प्रबंधन: ऐसा व्यक्ति, जिसने कभी चुनाव न लड़ा हो या जिसने शायद ही कभी चुनाव जीता हो, वह सबसे खराब चुनाव प्रभारी होगा। चुनाव प्रभारी को मतदान की तारीख से छह महीने पहले राज्य में शारीरिक रूप से उपस्थित रहने के लिए तैयार होना चाहिए; तकनीकी रूप से जानकार होना चाहिए; किसी भी जाति या लिंग के पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए; और उसमें विद्रोहियों को शांत करने का अधिकार और क्षमता होनी चाहिए। पार्टियों में कुछ नेता ऐसे होते हैं, जो कार्यक्रम में फिट बैठते हैं, लेकिन कई बहुत छोटे पड़ जाते हैं। एक सब कुछ जानने वाला प्रभारी, उस प्रभारी से बदतर साबित होता है, जो कुछ कुछ नहीं जानता।
धन: धन महत्त्वपूर्ण है, लेकिन वह निर्णायक कारक नहीं है। पैसे बांटना पूरी तरह धन की बर्बादी है, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार भी पैसे बांटेंगे। पैसे का बेहतर इस्तेमाल सोशल मीडिया पर खर्च करने और बूथ समितियों के पास आखिरी दिन बूथ प्रबंधन के लिए थोड़ा पैसा खर्च करने में होगा। अधिकतर उम्मीदवार दावा करते हैं कि चुनाव के दिन से पहले ही उनका सारा बजट खत्म हो गया है।
आखिरी सबक: अगर किसी राजनीतिक दल ने चुनावों से सबक नहीं सीखा है, तो वह जीतने लायक चुनाव भी हार सकता है।