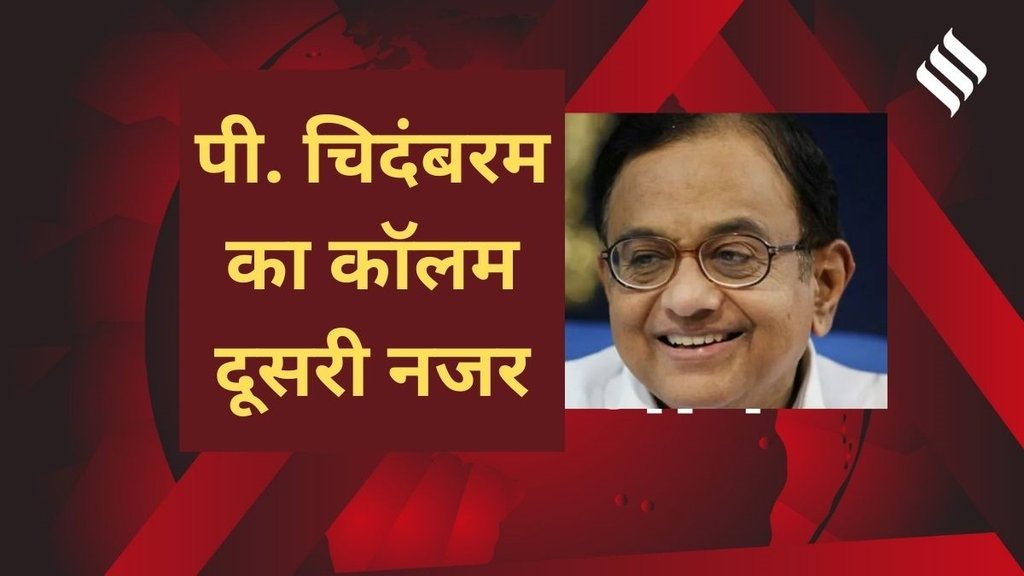इसी दो अप्रैल, 2025 को और उसके बाद आने वाले दिनों में हम जान जाएंगे कि दुनिया आधुनिक ‘पाइड पाइपर’ की धुन पर नाचेगी या नहीं। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य लक्षित देशों से आयातित वस्तुओं पर दंडात्मक शुल्क लगाता है, तो यह विश्व व्यापार संगठन यानी डब्लूटीओ नियमों, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों और सम्मेलनों का उल्लंघन होगा। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कानून की परवाह नहीं है, चाहे वह अमेरिकी हो या कोई और। वे खुद एक कानून हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ‘लक्षित’ देशों की पहचान की है और उन देशों से आयातित चुनिंदा वस्तुओं पर वे शुल्क लगाने का इरादा रखते हैं। भारत इस सूची में है।
शुल्क एक बाधा है, जिसका उद्देश्य विदेशी वस्तुओं को घरेलू बाजार में प्रवेश करने और घरेलू वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने से रोकना है। शुल्क (यानी सीमा शुल्क) के अलावा अन्य शुल्क भी हैं, जैसे डंपिंग-रोधी शुल्क और सुरक्षा शुल्क। इन्हें विशेष परिस्थितियों में लगाया जाता है, लेकिन इन्हें घरेलू स्तर पर लागू किया जाता है, जिसे केवल घरेलू न्यायालयों में ही चुनौती दी जा सकती है और आमतौर पर विदेशी निर्यातक के खिलाफ इसका घरेलू उद्योग के पक्ष में झुकाव होता है। इसके अलावा, गुणवत्ता मानकों, पैकेजिंग मानदंडों, पर्यावरण दिशा-निर्देशों आदि की आड़ में गैर-शुल्क बाधाएं हैं। इस स्वहित को एक नाम मिला- संरक्षणवाद।
देशभक्ति नहीं, संरक्षणवाद
संरक्षणवाद ‘आत्मनिर्भरता’ या ‘आत्मनिर्भरता’ प्राप्त करने के ‘शस्त्रागार’ का हिस्सा था। संरक्षणवाद को देशभक्ति के साथ भ्रमित किया गया। आधुनिक आर्थिक सिद्धांत और अनुभवजन्य साक्ष्य ने ‘आत्मनिर्भरता’ के सिद्धांत को खारिज कर दिया है। आत्मनिर्भरता एक मिथक है। कोई भी देश उन सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकता है जो उसके लोग चाहते हैं और उपभोग करते हैं। एक संरक्षणवादी देश कमतर विकास, कम निवेश, घटिया सामान, सीमित विकल्प और खराब ग्राहक सेवाओं की पीड़ा का सामना करेगा। पिछले पचास वर्षों के इतिहास ने निर्णायक रूप से स्थापित किया है कि एक खुली अर्थव्यवस्था और मुक्त व्यापार- संरक्षणवाद नहीं- आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। दुनिया के सबसे अमीर देश वे हैं, जो व्यापार और प्रतिस्पर्धा के लिए खुले हैं।
भारत ने लगभग चालीस वर्षों तक संरक्षणवाद को अपनाए रखा। आयात पर बहुत अधिक प्रतिबंध लगाए गए। नतीजतन, निर्यात भी बाधित हुआ। हमारे पास वाणिज्य मंत्रालय में एक विभाग था, आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के रूप में नामित एक प्राधिकरण के तहत अधिकारियों की एक सेना थी। किसी ने भी यह स्पष्ट प्रश्न नहीं उठाया कि ‘हम समझते हैं कि आप आयात के मुख्य नियंत्रक क्यों हैं, लेकिन कृपया बताएं कि आप निर्यात के मुख्य नियंत्रक क्यों हैं?’ एक ऐसे देश में निर्यात को नियंत्रित करने की विडंबना किसी को समझ में नहीं आई, जिसे विदेशी मुद्रा की सख्त जरूरत थी।
सत्ता परिवर्तन
1991 में वित्त मंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह का आगमन हुआ। उनकी आर्थिक नीतियों ने संरक्षणवाद को खत्म करने और अर्थव्यवस्था को खोलने का मार्ग प्रशस्त किया। 1991-92 में घोषित नई विदेश व्यापार नीति ने भयावह लाल किताब को फाड़ दिया और घोषणा की कि भारत मुक्त व्यापार के लिए खुला है। संरक्षणवाद को औपचारिक रूप से त्याग दिया गया, प्रतिबंधात्मक नियमों और विनियमों को समाप्त कर दिया गया, शुल्कों को धीरे-धीरे कम किया गया और भारतीय निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा के लिए सामने लाया गया। अर्थव्यवस्था को खोलने के अल्पकालिक और दीर्घकालिक लाभ बहुत अधिक थे।
India-US Tarrif: ट्रंप ने की PM मोदी की तारीफ, बोले- टैरिफ पर अच्छी तरह काम करेंगे भारत और अमेरिका
जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो भारत ने दिशा उलट दी और संरक्षणवाद को फिर से अपना लिया। आत्मनिर्भरता को एक आकर्षक नाम मिला- आत्मनिर्भर। सरकार यह पहचानने में विफल रही कि दुनिया बदल गई है: देशों ने अपने ‘तुलनात्मक फायदों’ की खोज की और अपने लाभों का दायरा बड़ा किया। ‘आपूर्ति शृंखला’ का आविष्कार किया गया। मोबाइल फोन जैसा उत्पाद एक देश में नहीं, बल्कि कई देशों में ‘बनाया’ गया था। ‘मेड इन जर्मनी’ या ‘मेड इन जापान’ के विपरीत, कई उत्पाद ‘मेड इन द वर्ल्ड’ थे। ‘आत्मनिर्भर’ के कारण त्यागे गए नियम, विनियम, लाइसेंस, अनुमति, प्रतिबंध और सबसे महत्त्वपूर्ण बात, शुल्कों को फिर से लागू किया गया।
विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, भारत का सामान्य औसत अंतिम बाध्य शुल्क 50.8 फीसद है। एमएफएन के साथ, व्यापार भारित औसत शुल्क 12.0 फीसद है। ये दो संख्याएं इस बात के माप हैं कि भारत कितना ‘संरक्षणवादी’ है।
वैध बनाम संकीर्ण हित
दूसरी ओर, भारत के पास किसी भी अन्य देश की तरह वैध हित हैं, जिनकी रक्षा करना उसका दायित्व है, जैसे कि कृषि, मछली पकड़ना, खनन, हथकरघा, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यवसाय। वे संरक्षण के हकदार हैं, क्योंकि लाखों लोगों के जीवन और आजीविका उन पर निर्भर हैं। दुनिया इन वैध हितों के प्रति असंवेदनशील नहीं है।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पहला हमला किया है। उन्होंने अल्युमीनियम और स्टील के आयात पर शुल्क से शुरुआत की, पीछे हट गए और एक नई तारीख तय की। 26 मार्च को उन्होंने आटोमोबाइल और आटो पार्ट पर उच्च शुल्क लगाया। मुझे संदेह है कि ट्रंप एक स्नाइपर या निशानेबाज की तरह काम करेंगे जो एक समय में एक लक्ष्य को चुनता है और उसे मार गिराता है।
भारत की प्रतिक्रिया अब तक संकोच से भरी और प्रतिक्रियात्मक रही है। सरकार ने 2025-26 के बजट में शुल्क कटौती की घोषणा की। ट्रंप प्रभावित नहीं हुए। नरेंद्र मोदी ने खुशामद करने की कोशिश की, ट्रंप संतुष्ट नहीं हुए। जब वित्त विधेयक पारित हुआ तो डिजिटल सेवा कर (‘गूगल टैक्स’) वापस ले लिया गया। अधिक रियायतों पर चर्चा चल रही है। यह एक असंतोषजनक दृष्टिकोण है। इसके बजाय, आपसी चिंता के सभी शुल्क मुद्दों पर व्यापक चर्चा और सहमति होनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी रुक गए हैं, लेकिन यह अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वे जीतेंगे या नहीं।
भारत को अपनी लड़ाई में मित्र देशों के समर्थन की जरूरत है, जैसे अन्य देशों को अपनी लड़ाई में भारत के समर्थन की आवश्यकता है। कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय देश संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किए गए शुल्क युद्ध में भारत के सबसे अच्छे सहयोगी हैं। अधिक बुद्धिमानी का रास्ता यह लगता है कि इन देशों को एक समूह बनाने के लिए राजी किया जाए और अमेरिका पर दबाव डाला जाए कि वह इन देशों के समूह के साथ बातचीत करे तथा एक व्यापक समझौते पर पहुंचे, जो यह सुनिश्चित करे कि विश्व की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिले और वह कायम रहे।