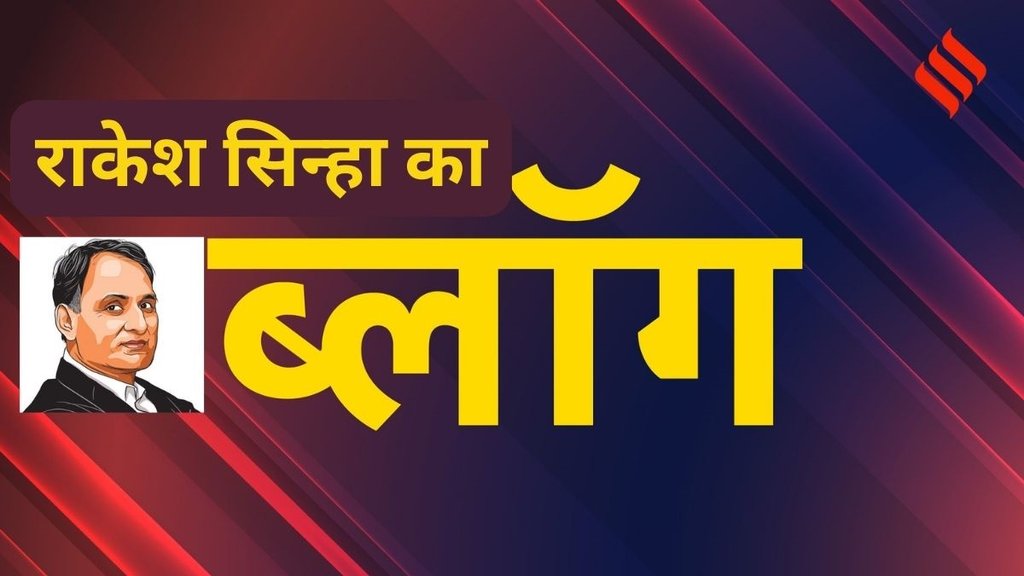राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का विजयादशमी भाषण कई अर्थों में महत्त्वपूर्ण है। पहला, यह प्रचलित संवाद की सतही हो चुकी संस्कृति से भिन्न है। समकालीन राष्ट्रीय जीवन में संवाद का स्तर सिर्फ भाषा नहीं, तथ्य और तर्क के स्तरों पर भी गिरता जा रहा है। गंभीर प्रश्नों को सहज तरीके से उठाया जा रहा है। दूसरा, संघ क्यों बढ़ता जा रहा है, इसका भी उत्तर इसमें मिलता है। भागवत ने इतिहास के चार नायकों- महारानी दुर्गावती, स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्संग अभियान के अनुकूल चंद्र ठाकुर और बिरसा मुंडा को लोगों की जीवंत स्मृति में लाने का काम किया है।
नायकों के विचार संघ के लिए महत्वपूर्ण
ऐसा नहीं है कि भारत के लोग इन नायकों से अपरिचित हैं। पर उनका दर्शन और कर्तृत्व स्मृति पटल में ओझल होता जा रहा है। ऐसे नायकों के विचार संघ के सामाजिक-सांस्कृतिक दर्शन के कितने नजदीक हैं, यह महत्त्व का विषय नहीं होता है। इतिहास के पन्नों में सिमटे पात्रों और घटनाओं को नई पीढ़ी के सामने सिर्फ पाठ्य पुस्तकों द्वारा नहीं लाया जा सकता है। देश में दूसरा कौन सामाजिक-राजनीतिक संगठन है, जिसकी रुचि इन बातों में है?
राष्ट्र के अतीत को वर्तमान से जोड़ना किसी जीवंत समाज की विशिष्टता होनी चाहिए। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, अपने ही संस्थापकों को भूल चुकी है। वामपंथी कुलीनों को मार्क्स, माओ के पुनर्पाठ से फुर्सत नहीं है। विरासत को आत्मसात करना संघ की ताकत बन गई है। भाषण में षड्यंत्रकारी ताकतों, जिन्हें ‘डीप स्टेट’ कहा जाता है, को चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें वे भी हैं जो संविधान की भाषा और प्रावधानों का उपयोग कर संविधानेतर कार्य कर असंतोष को अराजकता में रूपांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति का एक बड़ा वर्ग अपनी राजनीति की अनुकूलता के लिए उन ताकतों को वैधानिकता देता है। राष्ट्र की बुनियाद पर खतरे से लोकशक्ति द्वारा ही लड़ा जा सकता है। देश में गांधीवादी, आंबेडकरवादी सहित अनेक विचारों के लोग हैं। पर उन बातों पर उनकी चौंकाने वाली चुप्पी, अरुचि या आलस्य तीनों दिखाई पड़ती है।
संघ का नाम आते ही ‘अल्पसंख्यक’ विरोध सामने आ जाता है
यों तो पूरी दूनिया तकनीक के विस्तार के कुछ दुष्परिणामों को जूझ रही है। भारत अपवाद नहीं है। उदाहरण के लिए इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी या अश्लील फिल्मों के चार मंच पर 2020 में प्रति माह 1100 करोड़ लोग पहुंचे, जो तमाम सोशल मीडिया के मंचों से अधिक है। यह हमें कहां ले जाएगा? हमारी मानसिकता और आचरण पर क्या प्रभाव डालेगी यह, एक गंभीर सवाल है। संघ इस विषय पर अपनी बेचैनी दिखा रहा है। ऐसी बेचैनी व्यक्तिगत स्तर पर तो लोगों में है, पर संगठनों के स्तर पर नहीं है। संघ का नाम आते ही ‘अल्पसंख्यक’ विरोध सामने आ जाता है। संघ विरोधी ऐसी छवि गढ़ने में सफल हुए हैं।
भागवत के भाषण में एक नई दृष्टि आई है। उन्होंने समुदायों के लोगों के बीच दोस्ती की बात कही है। यह विवादास्पद दुविधा से समाज को बाहर निकालने का एक मंत्र है। अनेक संप्रदायों, पूजा पद्धतियों के देश में विविधता की जड़ हमारे स्वभाव में आ गई है। ये विविधताएं संविधान सभा से नहीं, सांस्कृतिक चेतना से उपजती हैं। जिस समाज में ऐसा स्वभाव नहीं है, वहां न्यूनतम विविधता बनाए रखने के लिए भी संविधान के प्रावधानों और बहुमत वाले समुदाय के दया भाव की जरूरत होती है। लेकिन विविधता को अलगाव, जातीय-सांप्रदायिक, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में बदलने का भी प्रयास हो रहा है। विभिन्न समुदायों के लोगों का साथ रहना, परस्पर सहयोग करना, साझा प्रयास और साझी विरासत के प्रति समर्पण ही दोस्ती का आयाम है। यह परंपरागत समुदायों के बीच संवाद से भिन्न है। ऐसा संवाद राष्ट्र को काल्पनिक रूप से विभाजित कर मोल-तोल को प्रोत्साहित करता है।
एक नए सांस्कृतिक अभियान द्वारा सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को समाप्त करने की आवश्यकता है। यह कार्य दुष्कर इसलिए है कि वोट बैंक की राजनीति देश में मानसिक विभाजन को निरंतर बढ़ा रही है। साझा आर्थिक गतिविधियों के भी प्रभावित होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। किसे लाभ होगा, किसे हानि होगी, यह अंकगणित सत्तावादी राजनीति का हिस्सा है। विपक्ष का बड़ा वर्ग अल्पसंख्यकवाद को अपना दर्शन मानता है। पर उसके प्रतिकार में ‘हिंदू खतरे में है’ का नारा भी अनुचित है। स्वतंत्रता पूर्व महासभा का यही स्वभाव था। राष्ट्रीय जीवन को अखंडित रूप में देखना अब चुनौती नहीं बननी चाहिए। समाज को स्वविवेक से खड़ा होना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्थिति बिगड़ने में देर नहीं लगती है। एक-दूसरे के पर्व-त्योहारों, घर-दलानों पर व्यापक तौर से पहुंचना ही उसका आयाम है।
भागवत के भाषण का यह पक्ष कुछ लोगों और समुदायों के लिए दुविधा का कारण बन सकता है, पर वे कुछ लोग राष्ट्र के भाग्य निर्माता नहीं हैं। व्यक्ति, समुदाय, पूजा पद्धतियां, परंपराएं आती-जाती रहती हैं, पर राष्ट्र की आयु, असीमित होती है। संघ ने इससे अपने आपको जोड़ा है। इसलिए इसके पास जितनी जिम्मेदारी पच्चीस लोगों के साथ 1925 में स्थापना के समय थी, उससे कई गुना अधिक चुनौती पच्चीस करोड़ लोगों के समर्थन के बाद सौवें वर्ष में है। ऐसी जिम्मेदारी की भावना ने ही संघ को विभाजन, आंतरिक सत्ता प्रतिस्पर्धा और निराशावाद से बचाया है।
आधुनिक दुनिया में यह अपवाद की तरह है। रूस में बोल्शेविक पार्टी बनी थी, जो बाद में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी कहलाई। इसके वैचारिक रूप से संकल्पित बुद्धिजीवी-नेता, लेनिन, मारटोव, ट्राटस्की और प्लेखानोव एक साथ नहीं रह पाए। बिखरे और एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी, आलोचक बन गए। संघ के आलोचकों को अपना फलक बदलना होगा, अन्यथा वे विध्वंसात्मकता के पैरोकार बने रहेंगे। नुकसान संघ को कम, राष्ट्रीय जीवन को अधिक होगा। ऐसे ही विभाजन के कारण पंथनिरपेक्षता की जननी भारत को पंथनिरपेक्षता के लिए ‘अग्नि परीक्षा’ बार-बार देनी पड़ती है।