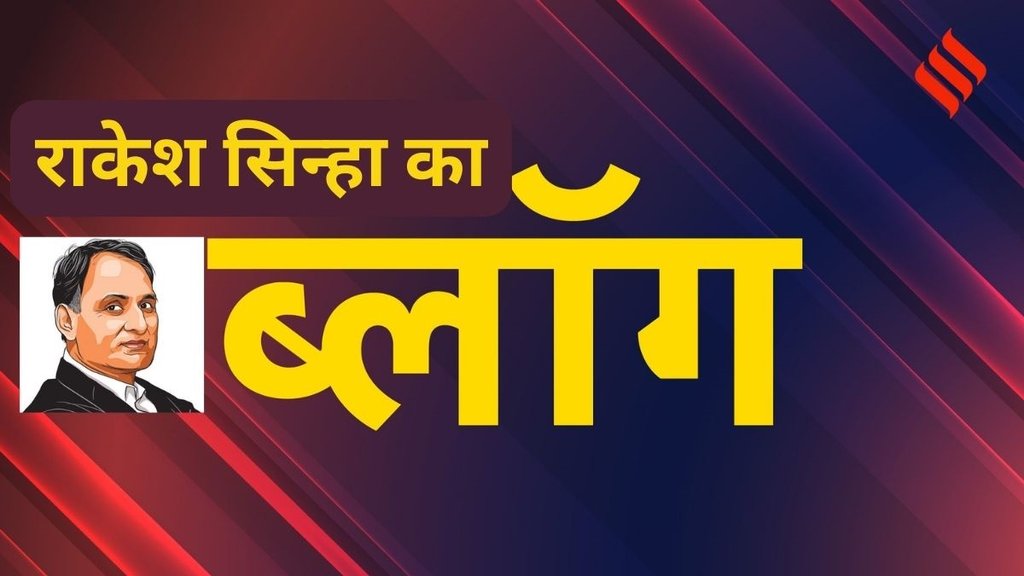दुनिया के एक सौ निन्यानबे देशों में संविधान है, लेकिन इस पर विवाद सिर्फ भारत में है। रोचक बात है कि इस विवाद का कोई सिर-पैर नहीं है। विवाद को समझने के लिए भारत के संसद में भी दो दिनों की बहस 13 और 14 दिसंबर को हुई। पर क्या विवाद सुलझा? पूर्वाग्रह से चीजें सुलझती नहीं, बल्कि और उलझती हैं। देश के लोगों के लिए कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था में हुई बहस से क्या हासिल हुआ? इतना जरूर हुआ कि संवैधानिक चेतना का सूचकांक बढ़ा। संवाद के तीन प्रमुख स्वरूप होते है।
पहला वाद है। इसमें पक्ष-विपक्ष सत्य जानने की कोशिश करता है। तथ्य और तर्क का उद्देश्य किसी निष्कर्ष तक पहुंचना होता है। दूसरा ‘जलपा’ है। इसमें शोरगुल कर अपनी बात या तर्क को सामने वाले पर आरोपित करना होता है। सत्य जानने का मकसद नहीं होता है। तीसरा है वितंडावाद। इसमें वितंडा करने वाला इस बात को प्रमुखता देता है कि सामने वाला गलत है। ऐसा करने में वह कभी-कभी उन तर्कों या तथ्यों का सहारा लेता है, जिस पर वह स्वयं विश्वास नहीं करता है। ऐसे बहस करने वाले का उद्देश्य सामने वाले को चुप कराने का होता है।
समकालीन विमर्श की प्रकृति क्या है, यह हम सब समझ सकते हैं। विडंबना यह है कि जिस देश में स्वाध्याय, सत्संग और शास्त्रार्थ की परंपरा का मिसाल हो, वही संकट से जूझ रहा है। पहले ही निष्कर्ष निकालकर हम विमर्श का हिस्सा बनते हैं। ऐसे में रचनात्मकता की कल्पना कैसे की जा सकती है?
संविधान को कोई पवित्र ग्रंथ मानना इसके साथ ही अन्याय है। यह शुद्ध रूप से हमारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के संचालन का एक संदर्भ ग्रंथ है, जो समय और आवश्यकता के अनुसार बदलाव को आमंत्रित करता है। इसकी प्रस्तावना अपने निचोड़ में हमारे राष्ट्रीय जीवन के आदर्श और उद्देश्य, दोनों को प्रतिबिंबित करता है। भारत का संविधान बनाते समय संविधान सभा ने भारत को अन्य देशों से भिन्न देखा। इसका कारण है। वे जिस राष्ट्र-राज्य का संविधान बना रहे थे, उसका एक सभ्यताई इतिहास रहा है। इसीलिए संविधान की मूल प्रति में सभ्यता और संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाले बाईस चित्रों को सांकेतिक तरीके से रेखांकित किया गया था।
संसद के रूप में संविधान सभा काम करती थी। इसका कार्यकाल समाप्त होने पर विदाई भाषण में अध्यक्ष मावलंकर ने 5 मार्च, 1952 में कहा था कि ‘(संविधान के) पृष्ठों को सुप्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस द्वारा प्राचीन काल के भारतीय जीवन के उपयुक्त दृश्यों द्वारा सजाया गया है। अंग्रेजी संस्करण तैयार है… हिंदी संस्करण का कार्य चल रहा है।’ पर जब सदस्यों के हाथ संविधान की प्रति आई तो उसमें कोई चित्र नहीं था। यह रहस्य बना हुआ है कि किसके आदेश से राम-सीता के पुष्पक विमान की सवारी, शिव के तांडव, कृष्ण की गीता का उपदेश देते हुए, भगवान बुद्ध, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस आदि दृश्यों को हटा दिया गया। संविधान ही नहीं, इस सभ्यता के साथ स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी जालसाजी है।
स्वशासन आते ही ‘स्वतंत्रता’ के प्रति शासकों का दृष्टिकोण बदल गया। पहला विधेयक संविधान लागू होने के सिर्फ पंद्रह माह बाद लाया गया। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता को कम किया गया। गृहमंत्री राजाजी के पास कहने के लिए एक भी ठोस बात नहीं थी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। वे अजीब तर्क देते रहे, उसमें एक है- स्कूल में शिक्षक के पास बेंत (छड़ी) होती है, जिसका उपयोग वह करना नहीं चाहता है। इसके उलट अमेरिका में संविधान लागू होने के बाद तीन साल बाद जो पहला संशोधन आया, उसने व्यक्ति, अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता के दायरे को बढ़ाने का काम किया। भारत का विपक्ष इन तथ्यों को या तो जानना नहीं चाहता है या जानकर भी उससे अनजान बना रहता है। असत्य के रास्ते चलकर, स्वार्थ के अनुसार तर्क गढ़कर कभी विमर्श जीता नहीं जा सकता है।
सन 2014 के बाद संविधान को बदलने की साजिश का आरोप कितना तथ्यात्मक या भ्रामक है, इसकी पड़ताल करना आवश्यक है। संविधान सभा ने अपनी आदर्शवादी सोच, इच्छा और अपने उद्देश्यों को राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों में रखा है। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता, भ्रातृत्व, सौहार्द, सांस्कृतिक समृद्धि है। 2014 से पहले इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कानूनों को प्रधानता दी। इसी का परिणाम तीन तलाक पर कानून का बनाया जाना है। पीढ़ियों से पितृसत्ता का दमन, अराजक व्यवहार सह रही मुसलिम महिलाओं को सशक्त बनाना संविधान का मान बढ़ाना है या उसे कलंकित करना है? इस देश में दस से बारह करोड़ वे लोग हैं, जिनके पास ‘स्थायी पता’ नहीं है। उन्हें साम्राज्यवादियों ने ‘अपराधी जनजाति’ घोषित कर रखा था। उनकी सुध सबसे पहले 2018 में ली गई, जब उनके लिए कल्याणकारी बोर्ड का निर्माण हुआ।
संविधान कोई राजनीतिक ‘नैरेटिव’ नहीं है। यह अपने आप में साधन और साध्य दोनों होता है। इसकी सार्थकता तब होती है, जब गणतंत्र सामान्य लोगों को आत्मविश्वास और सम्मान देता है। मोदी-युग ने पद्म सम्मान द्वारा इसे साबित किया है। केरल में लक्ष्मी कुट्टी नाम की एक गरीब महिला अनाम रहकर दुर्लभ औषधीय पौधों को बचाने का असमान्य कार्य कर रही थीं। उन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब ऐसे ही लोग ढूंढ़े जाते हैं। गणतंत्र को कुलीनता से मुक्त करना संविधान की सिद्धि ही माना जा सकता है।
संविधान तो आंसू इस बात पर बहा रहा है कि सामंतवाद, अस्पृश्यता, जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद जैसी बातें राजनीति की सारथी बनी हुई हैं। इन्हें कैसे समाप्त किया जाए, यह चिंता का विषय होना चाहिए। पर अपने सारथी को कौन मारना चाहेगा? मंजिल तक तो यही ले जाता है! कभी-कभी विषाक्त प्रश्नों का समाधान न तो सर्वोच्च न्यायालय कर पाता है, न ही संसद। उसे जनता करती है। भारत का संविधान इसकी भी इजाजत देता है। जब तक लोक संवाद और लोक शक्ति राजनीतिक साये में रहती है, राजनीति संविधान को अपने मकसद से देखती रहेगी।