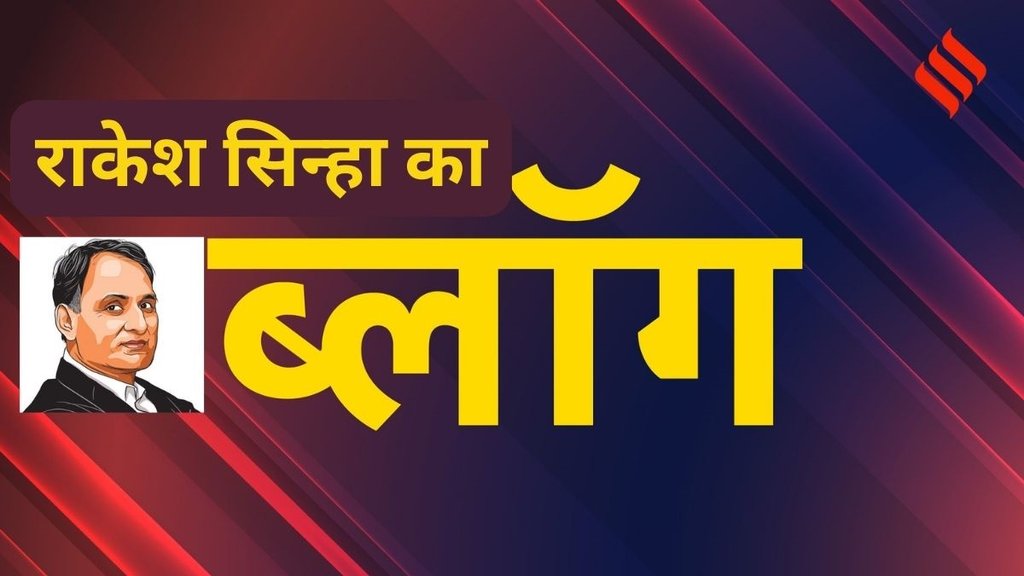कुछ दिनों पूर्व एक साहित्यिक पत्रिका का ग्राहक बना। इसका प्रकाशन बिहार के ग्रामीण अंचल नौबतपुर से होता है। यह देश के सुदूर क्षेत्रों में छपने वाली उन हजारों लघु पत्र-पत्रिकाओं में से एक है, जिनके सामने लेख संग्रह से लेकर छपाई के लिए धन एकत्रित करने की चुनौती बनी रहती है। मगर बौद्धिकता के प्रति आग्रह उन्हें थकने या निराश होने नहीं देता है। हालांकि संपन्न घरानों के साथ यह बात लागू नहीं होती है। अन्यथा राष्ट्रीय स्तर की अनेक उपयोगी और लोकप्रिय पत्र-पत्रिकाओं पर ताला नहीं लग जाता। संपन्न घरानों को यह आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं लगता। वे इसे तेल साबुन से अधिक नहीं देख पाते। सामान्य और संपन्न का यह अंतर चार्वाक के पुनरागमन की सूचना दे रहा है। शिक्षा और संस्कृति भी इससे प्रभावित हो रही है। इसी का परिणाम बौद्धिक जगत का बाजारीकरण है। इससे न अमेरिका बचा हुआ है न ही इथियोपिया।
कन्याकुमारी से कुशीनगर के बौद्धिकों से चुनौती
भारत में चार्वाक को चुनौती बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों या विश्वविद्यालयों से नहीं, बल्कि कन्याकुमारी से कुशीनगर के बौद्धिकों से मिल रही है। वे समाज के प्रबोधन को अपनी स्वाभाविक और नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं। इसीलिए धन की तंगी के बावजूद ‘कांवर’ पत्रिका बंद होने नहीं दी गई। इस पर ‘अनियमित प्रकाशित होने वाली पत्रिका’ लिखा रहता है।
चार्वाक चमक-दमक, विलासिता और शरीर केंद्रित जीवन को सब कुछ मानता है। यह जब-जब आया, समाज के औसत मानसिक स्तर का सूचकांक शून्य हो गया। चार्वाकी संस्कृति ही भौतिक पराकाष्ठा पर पहुंचे रोमन साम्राज्य के अंत का कारण बना, जिसे इतिहासकार गिब्बन ने बखूबी ‘द हिस्ट्री आफ द डिक्लाइन एंड फाल आफ द रोमन एम्पायर’ में बताया है। फ्रांस में अठारहवीं शताब्दी में सामान्य लोगों ने चार्वाकी संस्कृति के सामाजिक-राजनीतिक परिणामों से ऊब कर इस पर हमला बोला था। इसलिए थामस कार्लाइल की रचना ‘द फ्रेंच रिवोल्यूशन- ए हिस्ट्री’ कभी पुरानी नहीं पड़ेगी। उपनिषद् मानव-विवेक, बुद्धि और आलोचनात्मक दृष्टि की सत्ता स्थापित करता है। इसीलिए इसकी प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी।
आत्मविश्वास के साथ और बिना ग्लानि के बताया जाता है
जब-जब चिंतन सृजन कमजोर पड़ता है, मानव मन हल्केपन का शिकार होता है। कुछ दशकों में कितना परिवर्तन हुआ, यह दिखाई पड़ रहा है। हम जाने-अनजाने भौतिक उपलब्धियों की होड़ में दौड़ रहे हैं। गंभीर बाते पढ़ने-सुनने और समझने की क्षमता साझा रूप से खोते जा रहे हैं। सामाजिक विज्ञान नवउदारवाद के ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी की तरह है। मानव मन को तकनीकी के माध्यम से संतुष्ट करने की कोशिश चल रही है। अब तो खर्चीली शादियां या अन्य ऐसे ही उपक्रमों को रोजमर्रा की जिंदगी में वंचित भी सम्मान देने लगे हैं। नींद की दवा या शस्त्रों का बाजार अगले बीस साल बाद कितना बढ़ेगा, यह आत्मविश्वास के साथ और बिना ग्लानि के बताया जाता है।
बौद्धिकता के कमजोर होने का दूसरा बड़ा उदाहरण तकनीकी से उपार्जित सोशल मीडिया पर हमारा व्यवहार है, जो उत्तेजना, प्रतिशोध, ओछा व्यंग्य और बिना सिर-पैर की सूचनाओं से भरा होता है। सामान्य लोग ‘अच्छी खबर’ की प्रतीक्षा में हैं। यह साहित्यकार और समाजशास्त्री ही अपनी रचनाओं से दे सकते हैं। कैरिअरवादी कभी भी बौद्धिक मार्गदर्शक नहीं बनते हैं। जब यह जुनून बनता है, तभी प्रभावी होता है। गोपाल गणेश आगरकर एक प्रतिबद्ध समाज सुधारक और खुले मन वाले चिंतक थे। उनका अपनी मां को लिखा गया पत्र इस बात की पुष्टि करता है। वे निर्धनता में पले-बढ़े थे।
आज की ताजी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां यहां देखें…
उन्होंने लिखा, ‘प्रिय मां, मैं जानता हूं कि आप आशा कर रही होंगी कि आपके पुत्र ने उच्च विद्यालय की परीक्षा पास कर ली है और वह अधिकारी बनेगा, जिससे आप अच्छी जिंदगी जी सकेगी। लेकिन स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि मैं उतना ही अर्जित करूंगा, जिससे जीवन चल सके। शेष समय समाज के अच्छे के लिए लगाऊंगा।’
वे ऐसे अकेले नहीं हैं। पूरी दुनिया के अधिकांश बौद्धिकों का यही रास्ता रहा है। प्रतिकूलता बौद्धिकों की जीवनसंगी जैसी होती है। यह प्रकृति की योजना में ही निहित होता है। ऐसी ही अग्नि परीक्षा से निकले लोगों की रचनाएं पीढ़ियों की मानसिक उन्नति का साधन बनती हैं। कार्लाइल की रोचक कहानी है। उन्होंने फ्रांस की क्रांति पर तीन खंडों में पुस्तक तैयार की। अपने मित्र राजनीतिक वैज्ञानिक जेएस मिल को दस्तावेज पढ़ने को दिया। 1935 में एक दिन मध्यरात्रि को मिल कार्लाइल को सूचना देने पहुंचे कि उनके घर की नौकरानी ने दस्तावेज को रद्दी कागज समझकर जला दिया।
यह किसी लेखक के लिए कितना बड़ा प्रतिघात है, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। पर उन्होंने हार नहीं मानी। फिर नए सिरे से तीनों खंड तैयार किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ‘गीता रहस्य’ की रचना की। उसके छपने से पहले अंग्रेज अधिकारी इसकी जांच-पड़ताल करने ले गए। काफी समय तक दस्तावेज वापस नहीं आया। इस पर तिलक निराशा में नहीं डूबे। उन्होंने कहा था- ‘लिखा हुआ नोटबुक तो उनके पास है, पर लिखी गई बात मेरे मस्तिष्क में है। मैं फिर लिखूंगा।’ समकालीन दुनिया में ऐसे जुनूनी मानो लुप्त हो गए हों।
भारत में चार्वाक की राह आसान नहीं है। यहां बौद्धिक प्रवाह सदैव विकेंद्रित रहा है और रहेगा। चार्वाकी संस्कृति स्वभाव से केंद्रीकृत होती है। यथार्थ है कि विकेंद्रीकृत चीजों से लड़ना आसान नहीं होता है। यहां समाज का हर वर्ग अपने-अपने तरीके से बौद्धिकता का सृजन कर रहा है। इसीलिए आज साहित्यकारों और समाजशास्त्रियों से अधिक प्रवचनकर्ता अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में स्वाध्याय, स्वचिंतन और आध्यात्मिक प्रेरणा से दिया गया प्रवचन सामूहिक समझ और दृष्टि को सर्वहिताय बनाने की कोशिश है।
विश्वविद्यालयों और ‘थिंक टैंक’ की परिधियों में बंद लोग उन्हें सुनना भी अपने प्रति धृष्टता मानते हैं। फिर वे उसका मूल्य क्या समझ सकेंगे? समर्थ रामदास जैसे संतों ने ऐसे ही प्रवचन से लोगों को स्वाभिमान से जीने के लिए सुदृढ़ किया था। बौद्धिक वर्ग अपनी जिम्मेदारी को ख्वाब और खैरात की चाहत से नहीं, साधना और प्रतिबद्धता से निभा सकता है। यही चार्वाक के पुनरागमन को रोक सकता है।