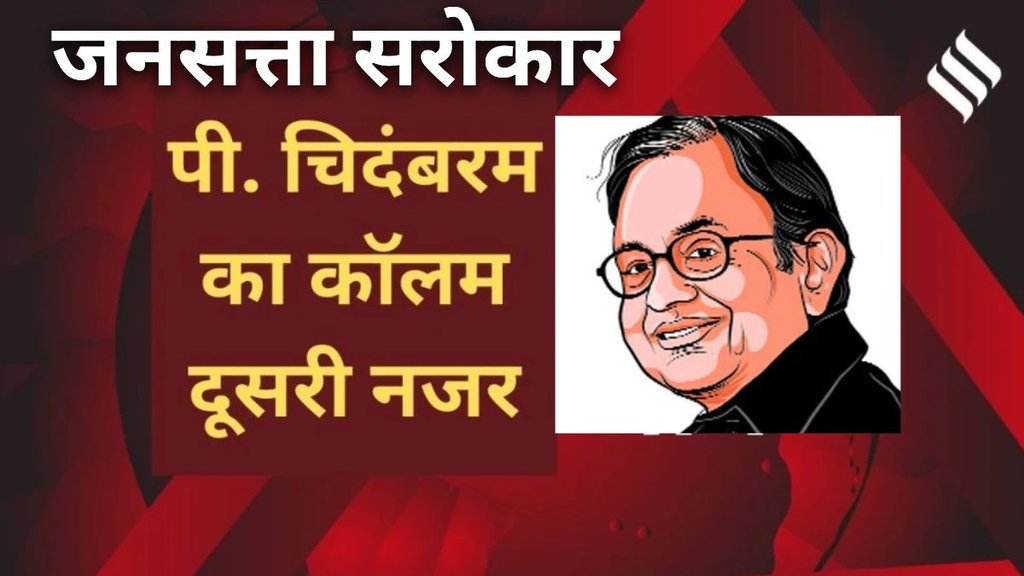अगर केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 के अनुसार चलती है और दक्षिणी राज्य जनसंख्या के आधार पर पुनर्निर्धारण के अपने विरोध पर अड़े रहते हैं, तो यह एक अप्रतिरोधी शक्ति का एक अचल वस्तु के साथ संघर्ष का मामला होगा। इससे कलह और विध्वंश बढ़ता जाएगा। क्या हमारे पास सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का विवेक है?
भारतीय संविधान में बयालीसवें संशोधन के बाद, परिसीमन की तलवार, 1977 से ही राज्यों की गर्दन पर लटकी हुई है। संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 में स्पष्ट भाषा में कहा गया है कि: वे ‘एक नागरिक, एक वोट’ के सिद्धांत को अंगीकार करते हैं। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के सदस्यों की संख्या तय कर दी गई है, जिसके मुताबिक इसमें राज्यों से चुने जाने वाले कुल 530 से अधिक और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाने वाले 20 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। वर्तमान संख्या राज्यों के लिए 530 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 13 है।
उप-अनुच्छेद (2) (ए) में लिखा है: ‘प्रत्येक राज्य को लोकसभा में उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में सीटें आबंटित की जाएंगी और जहां तक संभव हो सकेगा, सभी राज्यों के लिए यही नियम समान होगा।’ ‘जनसंख्या’ शब्द का अर्थ पिछली जनगणना में निर्धारित जनसंख्या है, पर शर्त यह है कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक राज्यों की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार ही मान्य होगी। अनुच्छेद 81 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद किसी राज्य को आबंटित सीटों की संख्या का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, लेकिन 2026 के बाद की जनगणना तक इस प्रक्रिया को रोक दिया गया था। इसलिए, विभिन्न राज्यों को आबंटित सीटों की संख्या को 1971 की तरह स्थिर रखा गया, जो ‘एक नागरिक, एक वोट’ के सिद्धांत का उल्लंघन है।
लोकतंत्र और संघवाद
इसमें कोई दो राय नहीं कि ‘एक नागरिक, एक वोट’ लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है, लेकिन अमेरिकी लोगों ने 1776 में महसूस किया, यह संघवाद के सिद्धांत के विपरीत है। उन्होंने इसका एक समाधान निकाला, जो पिछले ढाई सौ वर्षों में उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ है। उन्होंने समय-समय पर प्रतिनिधि सभा में पचास राज्यों में से प्रत्येक को राज्य की जनसंख्या के आधार पर आबंटित सीटों का पुनर्निर्धारण किया, लेकिन सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व (2 सदस्य) दिया। अमेरिका की तरह भारत भी एक लोकतंत्र और संघ है। हमने 1971 में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व के नुकसानों को देखा, लेकिन उसका समाधान खोजने के बजाय हमने इसे 2026 तक टाल दिया।
आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। 2021 के बाद से किसी न किसी बहाने जनगणना का काम टाला जाता रहा है। 2026 के बाद जनगणना का मतलब है कि परिसीमन करना होगा; हर राज्य को आबंटित सीटों की संख्या का पुनर्निर्धारण होगा; और कुछ राज्यों को जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए पुरस्कृत किया जाएगा और कुछ राज्यों को 2.0 या उससे कम की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) प्राप्त करने के लिए दंडित किया जाएगा। ‘एक नागरिक, एक वोट’ की असमानता आपके सिर पर वार करेगी।
घटाना और बढ़ाना
अगर लोकसभा में सीटों की कुल संख्या 530+13 पर स्थिर कर दी जाती है और अनुच्छेद 81 और 82 के अनुसार परिसीमन और पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो दक्षिणी राज्य (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना) बुरी तरह हार जाएंगे। उनकी कुल संख्या 129 से घटकर 103 रह जाने का अनुमान है। राज्यों के लिए लोकसभा में सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए जनसंख्या के अनुपात के सिद्धांत को लागू करने का कोई भी तरीका उन राज्यों को ‘दंडित’ करेगा, जिन्होंने प्रजनन दर कम और अपनी जनसंख्या को स्थिर करने में अच्छा प्रदर्शन किया है- जो पचास से अधिक वर्षों से एक राष्ट्रीय लक्ष्य था और अब भी है। आज, दक्षिणी राज्यों की लोकसभा में 129/543 के बराबर आवाज है, और यह पर्याप्त मुखर नहीं है। अगर यह हिस्सा 103/543 हो जाता है, तो दक्षिणी राज्यों की आवाज और कम हो जाएगी।
यह वादा कि दक्षिणी राज्यों की सीटों की संख्या कम नहीं की जाएगी, एक खोखला वादा है। कृपया ध्यान दें कि ऐसा कोई वादा नहीं है कि सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों- उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्यप्रदेश की सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं की जाएगी। अगर सीटों के पुनर्निर्धारण के माध्यम से ‘कोई कमी नहीं’ और ‘वृद्धि’ दोनों को लागू किया जाना है, तो ऐसा करने का एकमात्र तरीका लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करना है। ऐसी स्थिति की आशंका- और उसके लिए योजना बनाते हुए- लोकसभा के नए कक्ष को 888 सदस्यों के बैठने के लिए चतुराई से डिजाइन किया गया है। अगर सीटों के पुनर्निर्धारण के लिए वह रास्ता अख्तियार किया जाता है, तो दक्षिणी राज्यों की आवाज काफी कम हो जाएगी- 129/543 (23.76 फीसद) से 129/888 सीटें (14.53 फीसद) तक।
किसी भी तरह, ‘एक नागरिक, एक वोट’ के सिद्धांत का पालन करने के लिए यह बहुत बड़ी कीमत है। प्रजनन दर कम और जनसंख्या को स्थिर करने के लिए भी यह एक अस्वीकार्य कीमत है। चुनिंदा राज्यों की वर्तमान कुल प्रजनन दर (स्रोत: एनएचएफएस-5) इसका किस्सा बयान करती है :
निम्न उच्च
आंध्र प्रदेश 1.70 बिहार 3.0
कर्नाटक 1.70 उत्तर प्रदेश 2.35
केरल 1.80 मध्यप्रदेश 2.0
तमिलनाडु 1.80 राजस्थान 2.0
तेलंगाना 1.82
खोने और पाने वाले
लोकसभा में राज्य की आवाज के संदर्भ में, कम टीएफआर वाले राज्यों को नुकसान उठाने होंगे और उच्च टीएफआर वाले राज्य लाभ में होंगे। राज्यसभा की सदस्यता पहले से ही अधिक आबादी वाले राज्यों के पक्ष में है।
अगर केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 के अनुसार चलती है और दक्षिणी राज्य जनसंख्या के आधार पर पुनर्निर्धारण के अपने विरोध पर अड़े रहते हैं, तो यह एक अप्रतिरोधी शक्ति का एक अचल वस्तु के साथ संघर्ष का मामला होगा। इससे कलह और विध्वंस बढ़ता जाएगा। क्या हमारे पास सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का विवेक है?