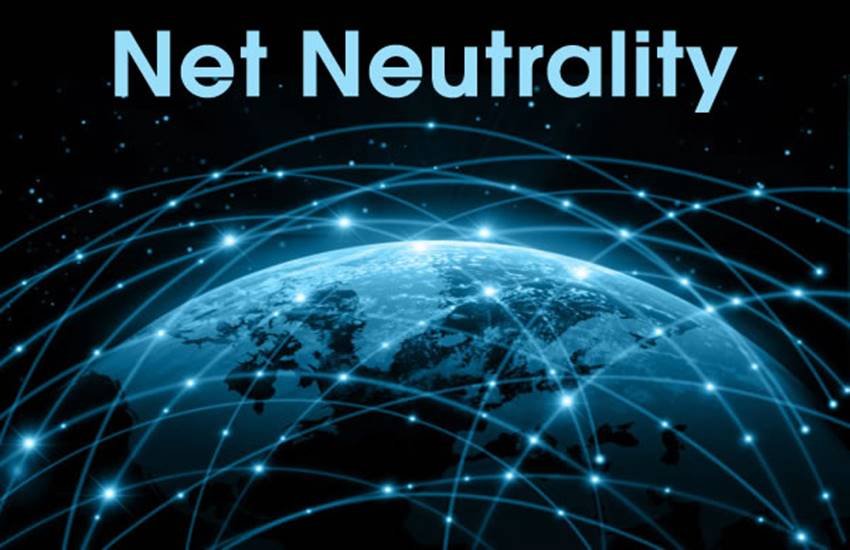कितनी तेजी से कोई विचार, शब्द या पद पूरे देश में फैल जा सकता है! तकनीक उद्योग को नजदीक से जानने वाले एक छोटे-से समूह और अकादमिक दायरे तक सीमित रहा ‘नेट निरपेक्षता’ पद देखते-देखते कुछ ही हफ्तों में आम चलन में आ गया। इस पद का अर्थ है कि इंटरनेट को अपनी सारी सामग्री के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, इस बात की परवाह किए बगैर कि कथ्य की प्रकृति क्या है या उपयोगकर्ता कौन है।
ऐसा लग रहा था मानो कोई चुनाव हो। 9 दिसंबर 2015 से 8 फरवरी 2016 के बीच खूब जोर-शोर से प्रचार अभियान चला। दो पक्ष थे। एक मायने में मतदान भी हुआ, जिसमें लोगों से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा पेश किए गए परामर्श-पत्र पर राय मांगी गई। केवल चुनाव चिह्न नदारद थे। दोनों पक्षों में एक के लिए दुबका हुआ बाघ और एक के लिए छिपा हुआ ड्रैगन उपयुक्त चुनाव निशान हो सकते थे।
छिपे ड्रैगन का तर्क था कि सेवा प्रदाताओं को इस बात की इजाजत होनी चाहिए कि वे कुछ निश्चित वेबसाइटों तक मुफ्त पहुंच मुहैया कराएं तथा अन्य सामग्री के लिए अलग-अलग दरें वसूल सकें। इस पक्ष का चेहरा फेसबुक और इसके संस्थापक जुकरबर्ग थे। दुबके हुए बाघ ने नेट निरपेक्षता की वकालत की। इस पक्ष में कोई उतना पहचाना हुआ चेहरा नहीं था, पर इस पाले में थे ‘नैस्कॉम’, बहुत-से उत्साही व्यक्ति और इंटरनेट को बचाने की अपील करता हैशटैग (सेव द इंटरनेट)। सरकार खामोश खिलाड़ी थी, पर कुछ हद तक चौकन्नी भी।
नेट निरपेक्षता की जीत
अगर नागरिक मुहिम न होती, तो नेट निरपेक्षता पर ट्राई की ओर से पेश किए गए परामर्श-पत्र का नतीजा भिन्न भी हो सकता था। ट्राई और सरकार ने पिछले साल काफी भ्रम का माहौल बना दिया था। परामर्श-पत्र ने शीर्षस्थ सेवाओं को मिश्रित संकेत दिए थे। शुरू में सरकार ने नेट निरपेक्षता की रक्षा करने की कोई प्रतिबद्धता जाहिर नहीं की थी। जब एक विभागीय समिति ने नेट निरपक्षता का पक्ष लिया, तो संचार मंत्रालय ने उसे पूरी तरह अपना दृष्टिकोण नहीं माना था। फिर भी, जब ट्राई ने आठ फरवरी को नियमन के नियमों की घोषणा की, तो जीत नेट निरपेक्षता की हुई।
नियमन के नियम निरपवाद हैं। कोई भी सेवा प्रदाता जानकारी मुहैया कराने वाली सेवाओं के लिए कथ्य के आधार पर विभेदकारी या अलग-अलग शुल्क नहीं वसूल सकेगा, न ही विभेदकारी दरों की पेशकश करने वाले व्यक्ति से करार कर सकेगा। केवल आपातकालीन सेवाओं तथा बंद इलेक्ट्रॉनिक संचार नेटवर्क से जुड़ी सूचनाओं को अपवाद के खाने में रखा गया है।
प्रतिद्वंद्विता का तर्क
सामान्य कायदों के मुताबिक इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। 1980 के दशक के शुरू में इंटरनेट के पथप्रदर्शकों ने एक सख्त फैसला लिया कि हर किसी को सामान्य प्रोटोकॉल को मानना होगा, नहीं तो उसे इंटरनेट से बाहर होने का जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उस फरमान ने इंटरनेट की मुक्त प्रकृति की रचना की और इसकी तीव्र वृद्धि की आधारशिला रखी। अगर सेवा प्रदाता इंटरनेट पर मौजूद सामग्री को एक टुकड़े या पैकेज के रूप में पेश करते हैं, तो इंटरनेट के बुनियादी सिद्धांत की क्षति होती है, साथ ही यह उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने की अतिक्रमणकारी कोशिश भी मानी जाएगी। यह बात वैसे उपभोक्ता की बाबत और भी लागू होती है जिसने पहले इंटरनेट का इस्तेमाल न किया हो।
दूसरी तरफ, जो लोग सेवा प्रदाताओं को पैकेज तथा सामग्री के हिसाब से अलग-अलग दरें वसूलने का हक देने के हिमायती हैं, ‘मुक्त बाजार’ की दलील देते हैं: उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक सेवा मुहैया कराने दिया जाए, प्रतिद्वंद्विता से सब ठीक हो जाएगा। वे यह भी दलील देते हैं कि इंटरनेट तक मुफ्त पहुंच उन लोगों के लिए भी इस सुविधा के दरवाजे खोलेगी, जिनकी पहुंच अभी तक नहीं है। प्रत्येक तीन भारतीय में से दो अभी इसी श्रेणी में आते हैं। वे अमेरिका तथा यूरोप के बहुतेरे देशों का उदाहरण देते हैं जिन्होंने अलग-अलग शुल्क वसूलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा रखी है; वे उन देशों का भी हवाला देते हैं जिन्होंने अभी नियमन का कोई फैसला नहीं लिया है।
बहस अभी जारी है
मोटे तौर पर मैं ट्राई के फैसले को सही मानता हूं। फिर भी यह बात मुझे परेशान करती है कि नियमन के नियम इतने निश्चयात्मक और सख्त हैं कि नवाचार तथा प्रयोग की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। अमेरिका और यूरोप के कुछ देश अलग-अलग मामले में नियमन का अलग-अलग मॉडल अंगीकार करते या खारिज करते हैं।
ट्राई ने सब पर समान रूप से जो पाबंदी लगाई है उसका पूरा परिणाम महीनों, शायद बरसों बाद सामने आए, और मैं उम्मीद करता है कि जन-हित में अपवादों की गुंजाइश बनाने की खातिर ट्राई नियमन में उचित संशोधन करेगा। न तो नेट निरपेक्षता कोई नारा है, और न ही नियमन; वे बारीक संतुलन की मांग करते हैं।
नियमन में जिस विभेदकारी शुक्ल निर्धारण की बात उठाई गई है, नेट निरपेक्षता उससे कहीं व्यापक विषय है। भारत को इस पर संसदीय मंजूरी से कानून बनाने की जरूरत पड़ सकती है। नेट निरपेक्षता पर बहस और नीति निर्माण की प्रक्रिया समाप्त होने की फिलहाल दूर तक कोई संभावना नहीं दिखती।