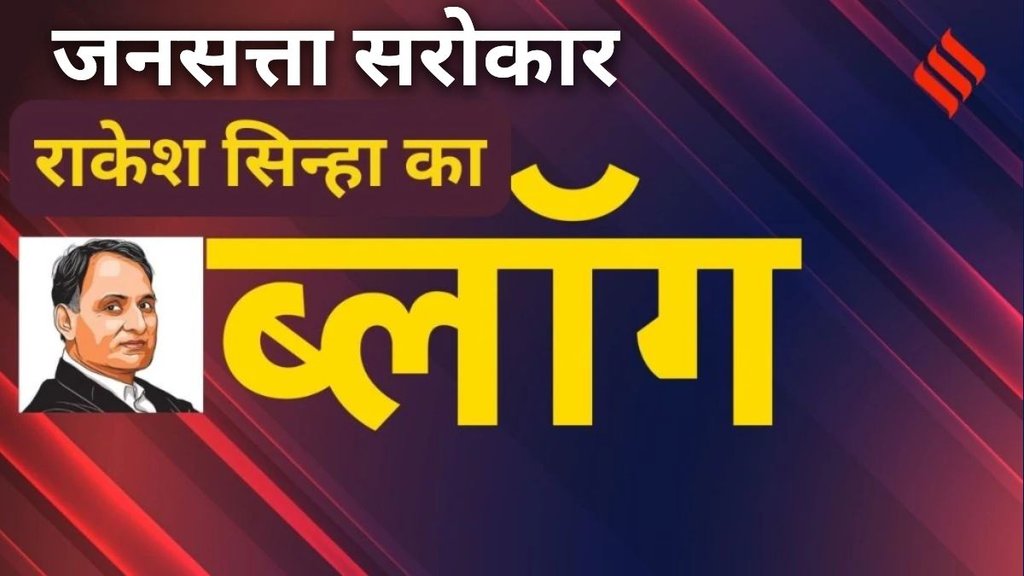जाति जनगणना पर कुछ वर्षों से विवाद अनावश्यक था। विपक्ष की मान्यता थी कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के अंत:करण में इसके प्रति विरोध है। केंद्र सरकार ने बाजी पलट दी। इस जनगणना के पीछे विपक्ष का तर्क है कि जातियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व असंतुलित है, जिसे इसी से ठीक किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद सर्वसमावेशी विकास के नारे और हकीकत के बीच के अंतर को अपना निशाना बनाया। नतीजतन, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला। इस निर्णय पर जितना विमर्श नीति आयोग और भाजपा ‘थिंक टैंक’ को करना था, वह नहीं हो पाया।
नीति आयोग और योजना आयोग के बीच एक अंतर सामने आता है। योजना आयोग शोधपरक तथ्यात्मक जानकारियों के साथ-साथ केंद्र सरकार की निर्णायक नीतियों को शैक्षणिक संस्थाओं, बौद्धिकों के माध्यम से जमीन तक पहुंचाता था। अगर नीति आयोग ओबीसी कमीशन जैसे दूरगामी और सकारात्मक प्रभाव वाले निर्णय को योजना आयोग की तर्ज पर व्यापक विमर्श से जोड़ पाता तो जमीनी स्तर पर सामाजिक-आर्थिक न्याय की तस्वीर धुंधली नहीं रहती।
पीएम मोदी की नीतियां अन्य प्रधानमंत्रियों से अधिक प्रगतिशील रही है
सोशल मीडिया पर निर्णय के सूत्रवाक्य की पुनरावृत्ति करते रहना इसका विकल्प नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां, कार्यक्रम और उनका सामाजिक दर्शन स्वतंत्र भारत के अन्य प्रधानमंत्रियों से अधिक प्रगतिशील हैं। किसान, मजदूर, हाशिये के लोग दर्जनों योजनाओं के केंद्र में रहे हैं। आयुष्मान, आवास, शौचालय, जन औषधि केंद्र जैसी योजनाओं की लंबी सूची है।
कार्यक्रम का प्रचार तो हुआ, पर उसके पीछे के दर्शन को लोगों तक पहुंचाने में असमर्थता बनी रही। कार्यक्रम का प्रभाव तात्कालिक होता है, दर्शन का असर दीर्घकालिक होता है। कार्यक्रम संदर्भ की भौतिक परिस्थितियों में बदलाव लाता है, जबकि दर्शन लोगों की सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है। पार्टी ‘थिंक टैंक’ कार्यक्रम केंद्रित बनी रही।
मुकेश भारद्वाज का कॉलम बेबाक बोल: बंटेंगे तो बचेंगे?
दर्शन की व्याख्या की जिम्मेदारी विपक्ष के पीछे खड़ी बुद्धिजीवियों पर छोड़ दी गई। इसीलिए आधारहीन आरोपों, जैसे भाजपा संविधान बदल देगी, दलित-आदिवासी के मौलिक अधिकारों पर प्रहार हो रहा है आदि का सामना करने में सरकार और पार्टी को उर्जा लगानी पड़ती है।
जाति जनगणना पर भी कुछ ऐसा ही विपक्ष द्वारा किया गया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो यह कहकर कि इसे कराने में कोई परहेज नहीं है, विपक्ष को चुप कर दिया। आज विपक्ष को सरकार की घोषणा का स्वागत करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। लोकतंत्र में जनगणना का विशेष महत्त्व है। यह जानकारियों को सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं, यथार्थ और प्रवृत्तियों को पारदर्शी तरीके से सामने लाता है। इससे हम उस हकीकत को जान और समझ पाते हैं, जो आंखों से ओझल रहता है। यह हमारी सोच को स्वत:स्फूर्त परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है।
1921 की जनगणना ने यह दिखाया था कि एक वर्ष से नीचे की आयु की 597, एक से दो वर्ष के बीच 494 बच्चियां विधवा थीं। इस तरह के आंकड़ों ने समाज को झकझोरा और समाज की चेतना में बाल विवाह और विधवा विवाह के प्रति नई जागृति आई थी। लोकतंत्र की खूबसूरती खुलापन है। इसका अर्थ है हकीकत से अपरिचित नहीं रहना। जब यह सामने आता है तब हम अपने पूर्वाग्रहों से भी मुक्त होते हैं। बुनियादी परिवर्तन की परिभाषा भी बदल जाती है। जनगणना में ब्रिटिश राज में जितनी बौद्धिकता का सदुपयोग होता था, वह स्वतंत्र भारत में नहीं हुआ। साम्राज्य के सर्वोत्तम मस्तिष्क इस प्रकिया से जुड़े होते थे।
1891, 1901, 1911 और 1931 के जनगणना आयुक्त क्रमश: जेए बेन्स, एचएच रोज्ली, इए गेट और जेएच हटन प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ-साथ शैक्षणिक योग्यता और योगदानों के लिए जाने जाते थे। प्रदेशों में नियुक्त जनगणना अधीक्षक भी प्रशासनिक अधिकारी के साथ-साथ भारतीय विषयों में रुचि लेनेवाले विशेषज्ञ होते थे। लेकिन स्वतंत्र भारत में हुई सात जनगणनाओं को लेकर सवाल उठे कि जनगणना सिर्फ भौतिक परिस्थितियों तक सिमट गया है। जबकि इसका उद्देश्य समाज के नैतिक और भौतिक दोनों स्थितियों का मूल्यांकन होता है।
जाति जनगणना को इसी दायरे में देखना चाहिए। दुर्भाग्य से इसे ध्रुवीकरण का विषय बनाने की कोशिश हुई। इसका कारण समझना कठिन नहीं है। सिर्फ इसी तक सीमित नहीं है। हमने लोकतंत्र को राजनीतिक दलों का अखाड़ा मान लिया है। फिर तो जनतंत्र राजनीतिक अखाड़े के नियमों से ही चलेगा। जो आज चल रहा है। पिछले कई दशकों से बौद्धिक संस्थाएं, सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन, बुद्धिजीवी रंगकर्मी, राजनीतिक दलों के साये में चले गए हैं।
परिणामत: जन परिष्कार, जन चेतना और जन विवेकशीलता का कार्य पचास-साठ के दशक के बाद प्राय: बंद हो गया। वर्धा और पवनार जैसे आश्रम पर्यटक स्थल बन कर रह गए। शेष सभी एनजीओ बनते चले गए। फिर भी हम चेतना, विवेकशीलता और परिष्कार की खोज कर रहे हैं। बिना उचित दिशा में परिश्रम किए हम सही परिणाम चाहते हैं। यह कभी संभव नहीं हुआ।
आंबेडकर के ‘सामाजिक लोकतंत्र’ को हम सबने भाषणों का विषय बनाकर रखा था। परिणामत: राजनीति को ध्रुवीकरण का खुला अवसर मिला। जातीय कटुता और जातीय राजनीति यथार्थ बन गया। ‘हम भारत के लोग’ का लक्ष्य अखाड़ेबाजी से हासिल नहीं हो सकता है। लेकिन समकालीन भारत में तो जातिविहीनता की बात करना राजनीतिक अपराध और वैचारिक रूप से अप्रासंगिक बनता जा रहा है।
लोकतंत्र की सफलता और समृद्धि जातीय, सांप्रदायिक, क्षेत्रीय और नस्लीय सोच को खत्म करने में है। जातिविहीन बनना और बनाना ही नैतिक उपलब्धि होगी। जाति जनगणना सर्वसमावेशी विकास के साथ-साथ सामूहिक चेतना के परिष्कार का भी साधन बने, यही लक्ष्य इसकी लोकतांत्रिक सार्थकता साबित करेगा।