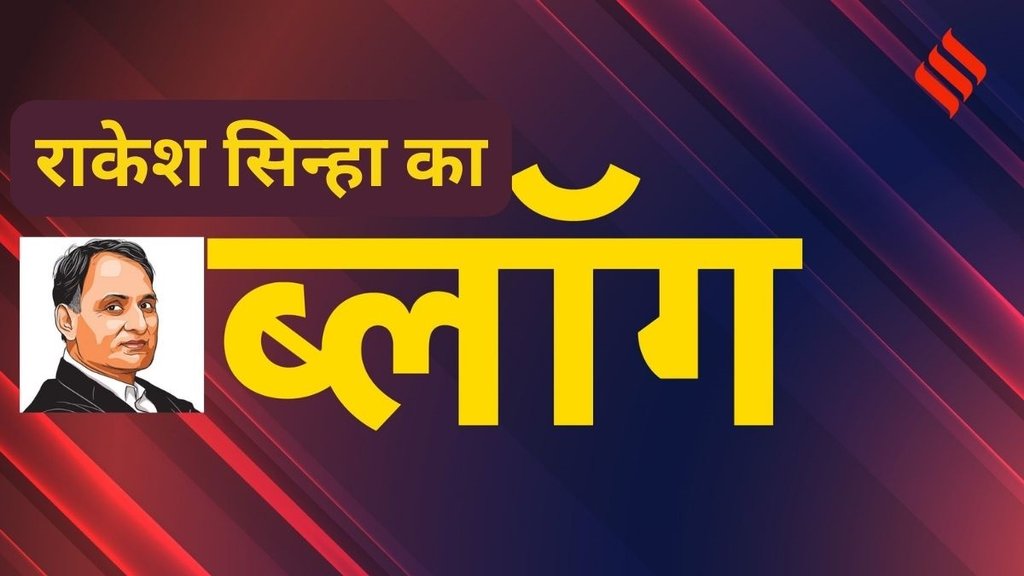खुले आसमान के नीचे जमीन पर चाय पीने की एक जगह दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कालेज में थी। यह अत्यंत ही आकर्षक स्थान जय सिंह का ढाबा था। यह एक ‘लघु सभागार’ की तरह था। छात्र समूहों में राजनीति से लेकर सिनेमा, स्थानीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय मसलों पर तर्क-वितर्क होते रहते थे। यह अकेला उदाहरण नहीं है। देश के प्राय: सभी विश्वविद्यालयों और शहरों/ महानगरों में ऐसे कुछ चिह्नित स्थान होते थे। अभी भी कुछ बचे हुए हैं। छोटे बजट में बड़ी बातें होती थीं। कोलकता, पुणे, चेन्नई, बंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ‘लघु सभागर’ आपको मिल जाता था। पर अब वे समाप्ति की ओर हैं। जय सिंह के ढाबे का जो हश्र हुआ, वही सबके साथ हो रहा है।
हमारा व्यवहार हमारी वाणी और वार्तालाप भी औपचारिकता के करीब रहता है
ये सभी भौतिकता की बलि चढ़ रहे हैं। उनके स्थान पर चाय-काफी की महंगी दुकानें खुल रही हैं, जहां अच्छी आरामदेह कुर्सियां, वातानुकूलित कमरे, अंग्रेजी बोलने वाले चाय परोसक होते हैं। बजट बड़ा है, तो बात भी स्वकेंद्रित ही होगी। हंसने-बोलने, समय बिताने की जगह अच्छी है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। पहली स्थिति में सब कुछ अनौपचारिक है। मन-मस्तिष्क भौतिकता में कैद नहीं है। पर दूसरी स्थिति में हम मात्र उपभोक्ता हैं। हमारा व्यवहार हमारी वाणी और वार्तालाप भी औपचारिकता के करीब रहता है।
चकाचौंध की संस्कृति जब पैर पसारती है, तब हम उसके गुलाम हो जाते हैं। वह हमारी मौलिकता छीन लेती है। उसे हम अपने ही जीवन के अनुभवों से कुछ हद तक समझ सकते हैं। हम सामूहिकता से दूर होकर व्यक्तिवादी बनते जाते हैं। जीवन में जीने के साधनों में साझीदारी घटती जाती है। अपनी संतुष्टि के लिए नए-नए उपक्रमों की तलाश में लगे रहते हैं।
हमारा समाज अनौपचारिक प्रकृति, प्रवृत्ति और प्रवाह वाला है
यह संकट सिर्फ भारत का नहीं है। पूरी दुनिया में नई आर्थिक संस्कृति ने अपना दुष्प्रभाव डाला है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भौतिक प्रगति गलत है। पर सवाल सीधा है। यह प्रगति हमारी मानसिक उन्नति, सामाजिक सरोकार और साझापन को बढ़ाता या हमें अपने आचरण को उसके अनुकूल ढालने के लिए बाध्य करता है। हमारा समाज अनौपचारिक प्रकृति, प्रवृत्ति और प्रवाह वाला है। इसे जितना औपचारिकता के सांचे में ढालेंगे, व्याकुलता बढ़ेगी, परंपरागत संस्थाएं चरमराएंगी और सामाजिक प्राणी की जगह हम उपभोक्ताओं की भीड़ बनते चले जाएंगे।
विश्वविद्यालय माल की तरह, पुस्तकालय क्लब की तरह और परिसर बाजार की तरह बन जाए तो चेतना का सृजन बाजार की संस्कृति के अधीन हो जाता है। यह सब नियोजन वे करते हैं, जो बड़े माल, पुल, सड़क, ‘आडिटोरियम’ या सभागार बनाते हैं। उस प्रक्रिया से छात्रों-शिक्षकों को नहीं जोड़ा जाता है। ठीक उसी प्रकार शहर के नियोजन में लोगों की मूल प्रकृति पर विचार नहीं किया जाता है। नवउदारवाद इसी का नाम है। सवाल उठता है कि हम चूक कहां रहे हैं? इसी का निदान हमारी मौलिकता बचा सकती है। मनुष्य स्वभाव से विकेंद्रीकरण के साये में रहना चाहता है। यह छोटे-छोटे समूह, लघु परंपराओं और उत्सवों में प्रकट होता है। भारत का स्वभाव रहा है। इसी को भारत के विमर्श में विविधता कहा जाता है।
केंद्रीकरण इस स्वभाव पर सीधा हमला होता है। सुकरात और चाणक्य, दोनों के सामने भौतिकता का विकल्प था, पर वे सादगी पसंद थे। महलों की जगह कुटिया में रहते थे। वे याद किए जाते हैं, पर उस काल के धन्नासेठों, भौतिकवादियों का नाम खोजने पर भी नहीं मिल पाता है।
विचार का केंद्र वैभव से दूर होता है, क्योंकि वैभव भी उसी विचार के तहत विमर्श का हिस्सा होता है। ऐसे केंद्र मूल प्रश्नों पर अनौपचारिक-औपचारिक निरंतर विमर्श करते हैं। इस प्रक्रिया का लक्ष्य चेतना सृजन है। नवउदारवाद इससे भयभीत रहता है। उसे ‘कार्य संस्कृति’ वाला मनुष्य चाहिए जो पुस्तकालय से लेकर माल तक लाभ हानि की चौहद्दी में रहे। जबसे हमने केंद्रीकृत बातों के प्रति समर्पण किया है, तबसे समाज की आंतरिक ऊर्जा का क्षरण शुरू हो गया है। बहुत पीछे याज्ञवल्क्य या शंकराचार्य के युग में जाने की जरूरत नहीं है। साठ-सत्तर के दशक में छोटी-छोटी पत्र-पत्रिकाएं निकलती थीं। सीमित लेखकों और सीमित पाठकों के ये बौद्धिक औजार व्यापक परिणाम देते थे।
लोकवाणी, क्रांतिनाद, मुक्ति संग्राम, तरुण क्रांति खूब पढ़ा जाता था। लोग स्वयं या समूह के योगदान से कुछ प्रकाशन करते थे, जो मन को आंदोलित करता रहता था। जयप्रकाश नारायण का ‘एवरीमैन’, शंकर पिल्लै का ‘शंकर वीकली’, राजमोहन गांधी का ‘हिम्मत’, पीलू मोदी का ‘मार्च आफ द नेशन’, मीनू मसानी का ‘फ्रीडम फर्स्ट’, एडी गोरवाला का ‘ओपिनियन’, रमेश धापर का ‘सेमिनार’, जार्ज फर्नाडिज का ‘प्रतिपक्ष’, ये कुछ प्रकाशन थे। सैकड़ों में प्रसारण था। लाभ-हानि के उद्देश्य से वे नहीं चलते थे। आर्थिक प्रगति के दौर में लोग प्रशिक्षित होते रहते थे। ये सभी जय सिंह के ढाबे की तरह ही अपने-अपने तरीके से खुला मंच थे।
जब पेट भरने को पैसा नहीं था, तब लोग विचार सृजन करते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जमीन पर विचार के सिपाहियों ने राष्ट्रवाद की उर्वरा भूमि सृजित की थी। चंदा कर पत्रिकाएं निकलती थीं। ‘हिंदी प्रदीप’ के संपादक बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था- ‘ग्राहकगण, आपलोग भी इस पत्र का आयुष्य चाहते हों तो द्रव्य से सहायता कीजिए- अगर आपलोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो इतिश्री हो गई है।’ सुंदरलाल का कर्मयोगी नौ महीने अस्तित्व में रहा, तीन संपादकों को जेल जाना पड़ा। इलाहाबाद का ‘स्वराज्य’, गोरखपुर का ‘स्वदेश’, तिलक का ‘केसरी’, विचार प्रवाह के माध्यम थे। इनकी संख्या सैकड़ों में थी।
विपन्नता में वैचारिक संपन्नता थी। आज संपन्नता में वैचारिक विपन्नता है। इसी वैचारिक विपन्नता की लपट और न फैले, दिल्ली स्कूल आफ इकोनामिक्स के छात्र चिंतित हैं। चाय के खोखेकी जगह कहीं चकाचौंध वाली कैंटीन न खुल जाए। अगर चेतना सृजन की प्रक्रिया राजनीतिक अखाड़ेबाजी तक सीमित हो जाएगी, तब गंभीर प्रश्न और गंभीर विचार का लुप्त होना स्वाभाविक ही है। वही प्रश्न: हम क्या कर रहे हैं? हम विचार सृजन और विचार प्रवाह में पूर्व के विकेंद्रीकृत स्वभाव को फिर से जगाएं। यही रास्ता नव बौद्धिकता का मार्ग प्रशस्त करेगा।