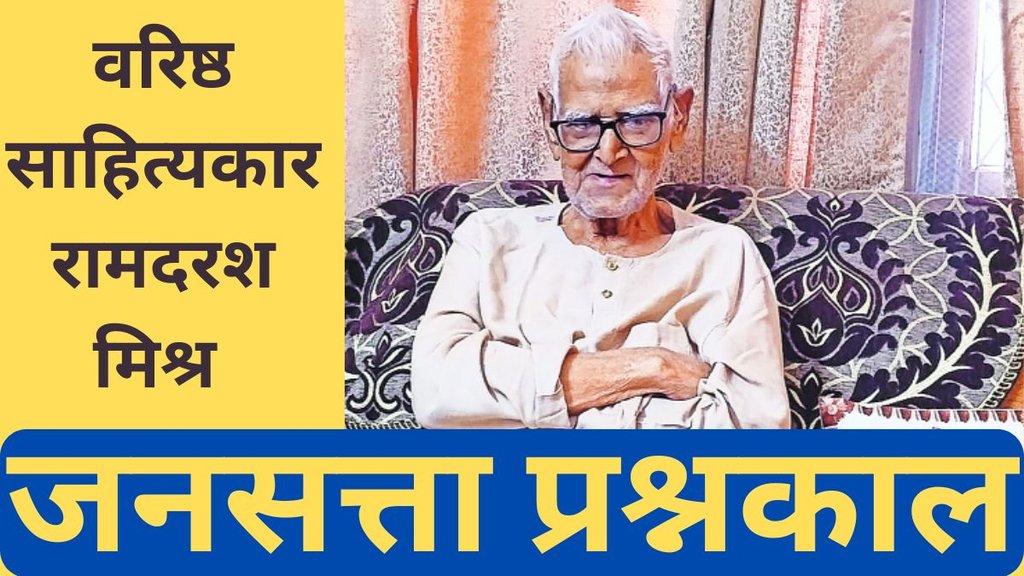वरिष्ठ साहित्यकार रामदरश मिश्र का कहना है कि वे अपने समय की उपज हैं और कभी किसी वाद के बंधन में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि साहित्यिक संवेदना अपने अनुभवों से हासिल होती है, आयातित संवेदनाओं का साहित्य कभी नहीं टिकता। अपनी मुख्य विधा कविता को मानते हुए आज के समय के बारे में कहते हैं कि आज कविता कम और उसका आभास ज्यादा हो रहा है। कवियों को अपनी रचनाओं की अस्वीकृति असहज करती है। आज की राजनीति को कविता की जरूरत नहीं है। साथ ही कहा कि आलोचना की दुनिया अभी भी कुछ गुटों में सीमित है और अच्छे समीक्षकों के पास संरक्षक नहीं हैं। दिल्ली में रामदरश मिश्र के साथ कार्यकारी संपादक मुकेश भारद्वाज की विस्तृत बातचीत के चुनिंदा अंश।
एक शतायु साहित्यकार के समक्ष साक्षात्कार के लिए बैठना एक सदी के अनुभव से साक्षात्कार है। आपको लेखन के सत्य, शिव और सुंदर जैसे जीवन के लिए शुभकामना। शुरुआत आप ही करें, अपने बारे में बात कर।
रामदरश मिश्र: आपका आभार, आप यहां आए। पिछले दिनों से इस सुंदर अनुभव से गुजरते हुए आनंदित हूं। लोग पूछते हैं कि आपकी लंबी उम्र का राज क्या है? मैं कहता हूं कि जो मेरा निर्माता है वास्तव में वही जानता होगा। मेरी भूमिका इतनी है कि दस साल वाराणसी में रहकर भी पान खाना नहीं सीखा। किसी तरह का नशा नहीं किया। मैं महत्त्वाकांक्षी नहीं हूं। महत्त्वाकांक्षा आदमी को मारती है। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला इसमें कभी नहीं उलझा। खान-पान को लेकर बाजार से संबंध नहीं रखा। इसके साथ ही मेरे आसपास के नम्र और संवेदनशील संबंधों ने मुझे हर तरह से स्वस्थ रखा। मेरे 99 वर्ष पूरे होते ही हर तरफ कार्यक्रम हुए, संगोष्ठियां हुईं।
अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में बताएं।
रामदरश मिश्र: मैं कविता के साथ पैदा हुआ था। जब मैं दर्जा दो में था तभी पाठ्य पुस्तकें पढ़ कर, लोकगीत सुनकर इच्छा होती थी कविता लिखने की। कुछ पंक्तियां लिखीं, लेकिन यह उतना आसान नहीं था। मैंने पहली कविता कांग्रेस के शुरू किए आंदोलन पर लिखी। मेरा सौभाग्य है कि मेरी कविता की शुरुआत देश के लिए काम करने वाली संस्था से हुई, देश प्रेम से हुई। समय के साथ चलना मुझे अच्छा लगता है। सहज भाव से। यानी समय अपनी छाप छोड़ता रहता है मुझ पर। मैं किसी दल का नहीं, किसी वाद का नहीं सिर्फ समय का हूं। 1945 में वाराणसी गया। मेरी कविता पर छायावाद का प्रभाव था। त्रिलोचन ने मेरी कविताओं पर कहा कि छायावाद की भाषा जा चुकी है। पहले मुझे बुरा लगा कि मैं इतनी कोमल भाषा में लिख रहा हूं और ये उसे अस्वीकार रहे हैं। धीरे-धीरे मुझे लगा कि वे सही कह रहे हैं और मुझमें परिवर्तन आता गया। 1951 में गीत छपा था और 1962 में मेरा संग्रह आया। मेरी कविता यात्रा समकालीन रूप में चलती रही। मुझ पर समय का प्रभाव आता गया। इसलिए मेरा हर संग्रह एक-दूसरे से कुछ अलग दिखाई देता है। आज तक मैं कविता के साथ चलता रहा, अभी भी चल रहा हूं। मैं मानता हूं कि कविता मेरी केंद्रीय विधा है। मैंने कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण लिखे। रेणु के ‘मैला आंचल’ की तरह मेरे लेखन में गांव था। जब ‘मैला आंचल’ आया तो पाया कि एक साथ पूरे गांव पर कथा हो सकती है। मेरे कई उपन्यास आते गए। मेरा लेखन आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं गांव से आया, लेकिन गांव छूटा नहीं। मेरी अपेक्षा यही रही कि मैं आम लोगों के मोहल्ले में रहूं। आभिजात्य वर्ग से लगाव नहीं रहा। गांव ने मुझे सादगी और प्रकृति का विशाल अनुभव संसार दिया। गांव एक जमीन भर नहीं है, गांव एक दृष्टि है। पंत की पंक्तियां हैं, ‘देख रहा हूं विश्व को आज मैं ग्रामीण नयन से’। लेखन के नयन को गांव से लिया। मेरे गजल की पंक्ति है-‘मेरे प्यारे गांव ये तेरी कैसी अद्भुत माया है/तुझको छोड़ चला तो देखा तू भी साथ चला आया है।’
आप और आपकी कविता समय के साथ बदलते रहे। क्या आपको लगता है कि वर्तमान दौर की कविता समय के साथ चल रही है?
रामदरश मिश्र: मैं अपने समय की कविता से परिचित हूं और उसकी उपज हूं। हमारे समय की कविता में आम आदमी और सामाजिक दुख-दर्द है। नए लेखन से जुड़ाव नहीं महसूस कर पा रहा हूं। मंच की आभा में कविता खो सी जाती है। कविता पढ़ते वक्त शारीरिक भंगिमाओं पर इतना जोर दिया जाता है कि शाब्दिक भाव खो जाते हैं। आज कविताएं कम हैं, कविताओं का आभास ज्यादा है। सांगठनिक मूल्यबोध नहीं दिखता। अब कविता लिखी जाती है और सीधे पढ़ी जाती है। पहले किसी कवि की कविताएं लौटा दी जाती थीं तो उसे लगता था कि हां उसमें परिपक्वता की कमी है तो उस पर और काम करते थे। अस्वीकृति कवि को असहज नहीं करती थी। अभी के समय से मैं बहुत हर्षित नहीं हूं। लेकिन, कविता की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। कविता तो हर समय में होती है।
साहित्य बनाम साहित्यिक संस्थाओं पर हमेशा बहस होती रही है। साहित्यकारों को बनाने-बिगाड़ने में इनकी अहम भूमिका रही है। क्या आपको लगता है कि आज ये संस्थाएं सही रूप से अपना काम कर पा रही हैं?
रामदरश मिश्र: किसी संस्था से आपका निजी संबंध है तो वह आपका सम्मान कर सकती है, आपके बारे में गोष्ठी कर सकती है। अगर निजी संबंध नहीं हैं तो आपके काम को नजरअंदाज कर सकती है। लेकिन संस्थाओं की भूमिका सीमित है। कमजोर व्यक्ति को कवि बना कर खड़ा कर देंगे तो कितनी देर ठहर पाएगा? ठहरेगी तो कविता ही। नए कवि देखते हैं कि हमारे ऊपर कौन है, उससे संबंध बनाने से क्या मिल सकता है और उसी के बनाए मार्ग पर चलने लगते हैं। लेकिन सही रास्ता वह है जो आप खुद बनाते हैं। आपकी निजता का रास्ता ही सही रास्ता है। प्रसाद, प्रेमचंद इसलिए हुए कि अपने अनुभव के लेखन का रास्ता चुना। आपके सवाल के जवाब में मेरी कविता की पंक्तियां शायद कुछ इस तरह हैं-रास्ता चिकना था, हरा भरा था/लेकिन अपना नहीं था। इसलिए जब जब इस पर चला/फिसल कर गिर पड़ा/अपना रास्ता बीहड़ है, सुनसान है/तपाता है हैरान करता है/लेकिन गिराता नहीं खड़ा करता है। बार-बार मांजता है/ बड़ा करता है…। अपना रास्ता बनाना आसान नहीं होता है। जो कवि अपना रास्ता बनाकर चलते हैं वही जिंदा रहते हैं। दूसरों के बनाए रास्ते पर चलने वालों के लिए आगे की राह बंद हो जाती है।
आपने कहा कि आपकी पहली कविता देश प्रेम यानी कांग्रेस पर थी, क्योंकि उस समय का राजनीतिक माहौल ऐसा था। आजादी की लड़ाई का वह दौर और आज का दौर, क्या आपको लगता है कि कविता की कोई राजनीतिक भूमिका रह गई है?
रामदरश मिश्र: आज के नेताओं का साहित्य से कोई संबंध नहीं रह गया। स्वाधीनता आंदोलन में मैथलीशरण गुप्त से लेकर माखनलाल तक राजनीति से जुड़े हुए थे। उनकी कविता ही उनकी राजनीति थी। कविता हमारी संवेदना को सघन करती है। संवेदना जब आहत होती है तो कविता उसे जगाती है। इस मायने में समाज से लेकर राजनीति को कविता की बड़ी आवश्यकता है। लाल किले में कवि सम्मेलन था। दिनकर जी वहां उपस्थित थे मंच पर। नेहरू जी पहुंचे तो सीढ़ी से फिसलने लगे। दिनकर ने उनका हाथ पकड़ कर कहा-नेहरू जी राजनीति जब भी फिसलेगी तो कविता उसका हाथ पकड़ लेगी। नेता भी कवियों को सम्मान देते थे। बाबू जगजीवन राम जी के एक गांव का लड़का मेरा शिष्य था। उसने कहा कि बाबूजी बुला रहे हैं आप चलिए। मैंने कहा, उनसे मेरा क्या काम? काफी आग्रह पर मैं गया। कमरे में कई लोग उनका इंतजार कर रहे थे। लड़के ने जाकर कहा कि मिश्र जी आए हैं तो बाबू जगजीवन राम दौड़े हुए आए। मुझे गले लगाया और अंदर ले गए। वहां बैठे हुए नेता देखने लगे कि ये कौन आया। पंत जी से राष्ट्रपति मिलना चाहते थे। लोग उन्हें खोजते हुए गए और कहा कि राष्ट्रपति आपसे मिलना चाहते हैं। पंत जी ने कहा कि मैं खुद कवितापति हूं। राजेंद्र बाबू खुद मिलने गए पंत जी से। यह कविता की ताकत थी। आज नेताओं को कविता से कोई लगाव नहीं।
क्योंकि कवि के पास वोट नहीं है?
रामदरश मिश्र: कवि और कविता की समझ के लिए संवेदनशीलता होनी चाहिए। एक बार मैं लखनऊ गया। मेरे उपन्यास पर भोजपुरी फिल्म बन रही थी। उसके लिए मुझे मंच पर बुलाया गया। मेरे आगे आकर एक राजनेता खड़े हो गए। मैंने सोचा, देखो ये मेरा सम्मान हो रहा है कि मुझे पीछे खड़ा कर दिया। मैं चुपके से नीचे आ गया। यही आज की राजनीति है। भाजपा के एक सज्जन नेता मुझे दिनकर पर एक कार्यक्रम में ले गए। वहां प्रधानमंत्री थे। मैंने दिनकर पर बोला और बताया कि मेरा गुजरात से जुड़ाव रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की कोई तवज्जो मुझे नहीं मिली। अटल बिहारी वाजपेयी की बात सुनिए। एक कार्यक्रम में वाजपेयी जी आए हुए थे। किसी ने उनसे मेरा परिचय कराया कि ये रामदरश मिश्र हैं। वाजपेयी जी ने तपाक से बोला कि अरे भई मैं इनका पाठक हूं। मैं इन्हें पढ़ता हूं। उन्होंने प्रकाशक की तरफ देखते हुए मजाक किया कि इन्हें कुछ पैसे-वैसे देते भी हैं या नहीं?
प्रकाशक का मुद्दा आपने अच्छा उठाया। अंग्रेजी की लेखिका अरुंधति राय पर जब विदेशी फंड लेने के आरोप लग रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मेरे किताबों की इतनी रायल्टी मिलती है कि मुझे किसी फंड की जरूरत नहीं होती है। क्या हिंदी का लेखक कभी इतना सक्षम हो पाएगा? हिंदी के लेखकों और प्रकाशकों के रिश्ते को आप कैसे देखते हैं।
रामदरश मिश्र: मुझे याद है कि रूस में किसी से पूछा गया था कि आप क्या करते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि मैं लिखता हूं। यानी उन देशों में आप लेखन से जीवनयापन कर सकते हैं। यहां अंग्रेजी में लिख कर विदेश के पाठकों को संतुष्ट करते हैं। यहां के भी अंग्रेजी के पाठक खरीदते ही हैं। लेकिन उस लेखन में देश नहीं होता है, राष्ट्र नहीं होता है। जर्मनी के एक अधिकारी थे, काफी अच्छी हिंदी जानते थे। मैं नाम भूल रहा हूं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के लेखकों के सम्मेलन में बुलाया गया है। मैं भी उनके साथ चला गया। उनका भाषण आज भी नहीं भूलता हूं। उन्होंने कहा कि आप लोग जो लिखते हैं, उसमें देश नहीं होता है। आपके पाठक यहां नहीं हैं, इसलिए आप लिखेंगे तो उनके अनुसार लिखेंगे। लोगों ने पूछा कि कैसे? उन्होंने कहा कि आप लिखेंगे हनुमान तो आपके पाठक समझ नहीं पाएंगे। फिर आप लिखेंगे राम के भक्त। जब आपने अपने पात्र का विस्तार कर दिया तो फिर वह कविता नहीं रह गई। कविता का ध्येय खत्म हो गया। लेकिन, यह बात सही है कि अंग्रेजी के लेखक की तुलना में हिंदी के लेखकों की हालत खराब है।
हिंदी के लेखकों की हालत खराब है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हिंदी में किताबें खूब छप रही हैं, खूब बिक रही हैं। रायल्टी से ज्यादा पैसे लेखकों को पुरस्कार से मिल जाते हैं। फिर लेखन में पैसा क्यों नहीं आ पा रहा?
रामदरश मिश्र: हिंदी में दो प्रमुख प्रकाशक हैं, एक रायल्टी कुछ ठीक देता है दूसरा औने-पौने (दोनों प्रकाशन संस्थान दो सगे भाई चलाते हैं) भेज देता है। पहले कुछ और लोग देते थे जो अब बिल्कुल चुप हो गए हैं। बाकी लोग तो बस किताबें छाप रहे हैं। हम लोग तो नौकरी में थे, और अब पेंशन मिलती है तो हमारा काम चल जाता है।
जो रायल्टी मिल रही है क्या आप उसे समुचित मानते हैं? आपने कहा कि अंग्रेजी का लेखक अपने लेखन से ही जीवनयापन कर लेता है।
रामदरश मिश्र: हिंदी के लेखकों को किसी अच्छे प्रकाशक ने पंद्रह हजार या बीस हजार की रायल्टी दे दी तो उसे ही महानता समझी जाती है। अब तो मेरी खूब किताबें छपी हैं। लेकिन, जब मैं गुजरात से यहां आया तो था यहां के लिए अपरिचित था। मेरा उपन्यास ‘जल टूटता हुआ’ पूरा हो गया था। लेकिन कोई भी छापने को तैयार नहीं था। बनारस के एक प्रकाशक ने उसे रख लिया। उपन्यास पूरा हुआ 1964 में और छपा 1969 में। धर्मवीर भारती को भेजा तो उन्हें भी दुख हुआ कि इसे छपने में इतनी देर हो गई। 1964 में ही छप जाता तो उसी वक्त इसकी चर्चा हो जाती। हिंदी के लेखकों की यही परेशानी होती है कि आपकी रचना की गुणवत्ता नहीं आपको जानता कौन है इस आधार पर किताब छपती है।
हिंदी साहित्य में आलोचकों की भी भूमिका किसी को बनाने और बिगाड़ने में होती है। वर्तमान हिंदी आलोचना को आप कैसे देखते हैं?
रामदरश मिश्र: बड़ी विसंगत स्थिति है आलोचना की। दल बने हुए हैं। मुख्यतया वामपंथियों का प्रधान दल है। उसके कवि एक-दूसरे को पसंद करते हैं, तारीफ करते हैं। उस दल के जो आलोचक हैं, वे भी उन्हीं कवियों तक सीमित रहते हैं। आलोचना की एक ठहरी हुई दुनिया है। नामवर जी, मैनेजेर पांडेय जी आलोचक रहे हैं। सवाल समीक्षा का है तो बहुत लोग पुस्तकों की समीक्षाएं लिख रहे हैं जिन्हें तकनीकी रूप से आलोचक नहीं माना जाता है। इन समीक्षकों के पास अच्छे संरक्षक नहीं हैं। नामवर जी पहले अच्छी कविताएं लिखते थे, छोड़ दी। मैनेजर पांडेय भी कविता लिखते थे छोड़ दी। ये लोग आलोचक बनने के लिए और सब कुछ छोड़ देते हैं। वामपंथियों ने कभी मुझे नहीं पूछा। मैं भी चार-पांच साल तक मार्क्सवादी रहा था। फिर मुझे लगा, यह एक बंधन है। लेखक के लिए बंधन उचित नहीं है। ये लोग वही चीज देखते हैं जो मार्क्सवाद के अनुकूल है। नामवर जी ने ईश्वर का नाम लिया तो हंगामा मच गया। मैनेजर पांडेय गांव गए, पत्नी के साथ पूजा पर बैठे तो हंगामा मच गया। लेखक को बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। अभी आलोचना के क्षेत्र में उथल-पुथल है।
आलोचना की तरह साहित्यिक संस्थाओं में भी गुटबाजी के आरोप हैं। क्या इससे साहित्य का नुकसान हुआ है?
रामदरश मिश्र: हर जगह यह गुटबाजी छाई रही। मेरे कई अच्छे उपन्यास आए, चर्चा में रहे, लेकिन मैं नेपथ्य में रहा। साहित्य अकादेमी खास गोलबंदी से मुक्त हुआ तो अब उन लोगों को भी सम्मान मिल रहा है, जिन्हें पहले मिलना चाहिए था। मुझे अकादेमी सम्मान मिला था तो उस वक्त उदय प्रकाश ने सम्मान वापसी की मुहिम चला दी। आरोप लगाया कि भाजपा छाई हुई है। यह तो बदतमीजी है। पहले आप सम्मान लेकर चर्चा में बने और अब सम्मान वापस कर सम्मान पाना चाहते हैं। साहित्य की दुनिया को सीमित कर दिया गया था।
साहित्य और संख्या का क्या संबंध है? बहुत सारे लेखक कहते हैं कि सौ किताबें लिख दी, कुछ छोड़ा नहीं। क्या संख्या से कोई अच्छा लेखक बन सकता है?
रामदरश मिश्र: साहित्य का संबंध सिर्फ संवेदना से है। संवेदना संख्यात्मक नहीं होती। अनुभव के बिना लेखन सघन नहीं होता है।
जीवन के इस पड़ाव पर ऐसा क्या लग रहा जो बहुत अच्छा हुआ, और क्या कुछ छूट जाने का मलाल भी है?
रामदरश मिश्र: मैंने योजना बना कर कोई चीज नहीं लिखी। मेरे अनुभव ही लेखन का रूप लेते गए। गांव का संघर्ष, शहर का संघर्ष, मैंने यह नहीं सोचा कि यह संघर्ष नहीं हो। अब थकान होती है। बेटी कहती है आप डायरी लिखा कीजिए। मेरे लिए सबका अपना महत्त्व है। काफी कुछ लिख लिया, काफी कुछ कह लिया। अब लोग आकर कहते हैं बधाई आपको यह सम्मान मिला। अच्छा हुआ सब वृद्धावस्था में जाकर मिला। अमूमन मजमे जवानी में लगते हैं और यह समय अकेलेपन का होता है। लेकिन मेरी वृद्धावस्था रौनक से भर गई है। इतनी अच्छी संतान। सौभाग्य है कि परिवार और समाज से इतना सुख मिल रहा है।
नए लेखकों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
रामदरश मिश्र: यही कहना चाहता हूं कि लेखक वही है जो अपना रास्ता खुद बनाता है। अपने अनुभव पर अनुसंधान करें।
प्रस्तुति : मृणाल वल्लरी