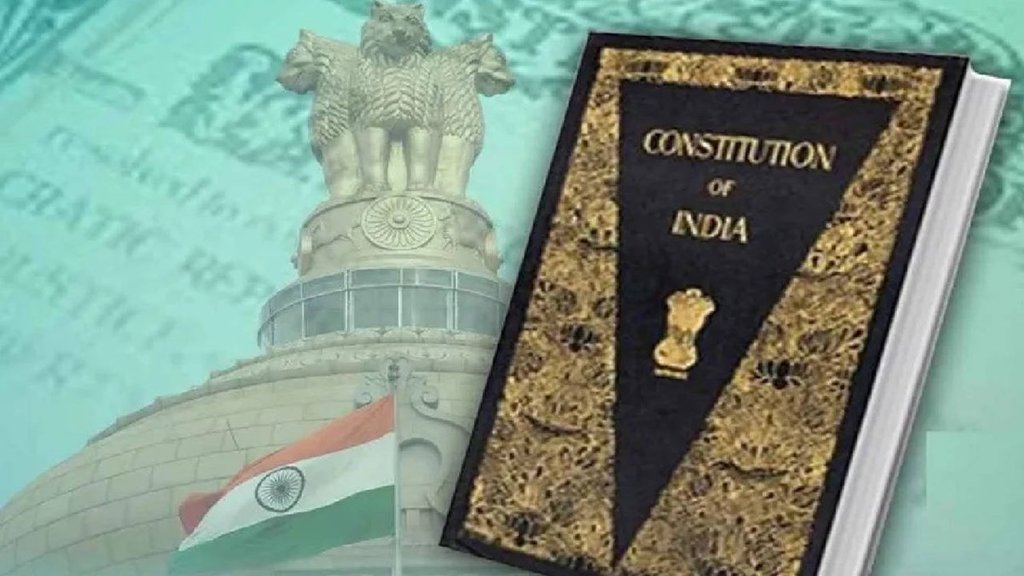आम चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक देश में अस्सी वर्ष आयुवर्ग के लगभग 1.328 करोड़ लोग हैं। यानी उन्होंने 1952 का आम चुनाव देखा है, और अब अठारहवां न केवल देखेंगे, बल्कि उसमें मतदान भी करेंगे। वे स्कूलों में ‘विज्ञान युग’ पर निबंध लिखते थे, और अब कृत्रिम मेधा से रूबरू हो रहे हैं। इन्होंने जो परिवर्तन देखे और उसकी गति को झेला है, उसकी कल्पना करना भी नई पीढ़ी के लिए मुश्किल होगा। ये उस युवा वर्ग के बचे हुए लोग हैं, जिनको विश्वास था कि अगले कुछ वर्षों में छुआछूत तथा जातिगत विभेद समाप्त हो जाएंगे, सामाजिक सद्भाव और पांथिक समरसता तेजी से बढ़ेगी!
1964 में यानी साठ साल पहले किशोरलाल मश्रुवाला द्वारा संपादित पुस्तक ‘गांधी-विचार-दोहन’ आई थी। वह गांधी, सुभाष, नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लोहिया, कृपलानी जैसे लोगों का समय था। सत्ता के बड़े पदों पर रहने वाले भी पद से हटकर कैसा सामान्य जीवन व्यतीत करते थे, यह भी इस पीढ़ी ने देखा था। लोग भूल नहीं सकते जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत होकर पटना गए, तो वे सदाकत आश्रम में किन परिस्थितियों में रहे। उनके पास अपना कोई घर नहीं था, बैंक खाते में कुछ सौ रुपए थे।
वे जीवन पर्यंत सरकार द्वारा उपलब्ध बड़े सरकारी बंगले में सुख-सुविधाओं के लिए अधिकृत नहीं थे। मूलत: गुजराती में लिखे गांधी विचारों का हिंदी अनुवाद पंडित काशीनाथ त्रिवेदी ने किया था। त्रिवेदी जी से 1976 में भोपाल में भेंट हुई थी। जीवन भर केवल दो धोती, दो कुर्ते रखने का व्रत निभाने वाले काशीनाथ जी राजनीतिक परिदृश्य में हो रहे परिवर्तनों से सहज नहीं हो पा रहे थे। अनेक बार वे पूछते थे कि ‘लोग गांधी से दूर क्यों होते जा रहे हैं।’
उस समय गांधीजी का एक चित्र सरकारी दफ्तरों में अभयदान मुद्रा में लगा रहता था। सुविधा शुल्क उगाहने के अभ्यस्त सरकारी कर्मचारी उसकी ओर इशारा करते हुए अपना मन्तव्य स्पष्ट कर देते थे। एक मुहावरा ‘मजबूरी का नाम महात्मा गांधी’ भी तेजी से फैला था। अब अनेक राज्यों के सरकारी दफ्तरों में गांधीजी का चित्र आधिकारिक तौर पर हटा दिया गया है। इस परिवर्तन की ओर ध्यान कम ही गया है। इस आम चुनाव के समय काशीनाथ जी या उनके समय के सर्वस्व-समर्पित गांधी के अनुयायी सारे वातावरण को देखते, तो उनको कैसा लगता?
दलगत राजनीति करने वाले राजनेताओं को अपना समय किन-किन कार्यों में लगाना पड़ता है, यह किसके हित में लगाया जाता है तथा लोकसेवा के लिए उनके पास क्या कोई समय बचता है? विभिन्न दलों से जुड़े ‘लोकसेवकों’ के आपसी संबंध अब कैसे और किस स्तर के बचे हैं? क्या वे कभी भी देशहित के किसी भी पक्ष पर सहमति व्यक्त कर पाते हैं?
राममनोहर लोहिया संसद से लेकर सड़क तक पंडित नेहरू की जबर्दस्त आलोचना करते थे, उनके ऊपर होने वाले खर्च का पैसे-पैसे का हिसाब जनता को समझाते थे। कोई तल्खी न उनके बीच में थी, न ही इन दोनों को सुनने वालों के बीच में कभी रही थी। लोग दोनों को प्यार करते थे, दोनों को सुनना चाहते थे। मगर अपनी राय स्वयं बनाते थे। राजनेताओं के मध्य व्यावहारिक रूप में संवाद की संस्कृति थी।
गांधी का मत था कि ‘लोकसेवक की जीविका का पैमाना दूसरे सेवकों से भिन्न होगा’। विचार करके देखिए कि इस दर्शन में क्या कई चुनाव जीत चुके लोगों का हर कार्य-अवधि की अलग से पेंशन लेना समा सकता है? ये ‘लोकसेवक’ जब किसी मुद्दे पर अपनी असहमति प्रकट करने के लिए संसद की गांधी प्रतिमा के समक्ष एकत्रित होकर या राजघाट जाकर प्रदर्शन करते हैं, तब यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि वे गांधी का सम्मान कर रहे हैं, या कुछ और।
गांधी के समक्ष ये कैसे खड़े हो पाएंगे, क्योंकि गांधी तो चाहते थे कि ‘‘लोकसेवक नम्रता की पराकाष्ठा दिखाएं- शून्य बन कर रहें। वे दूसरे वैतनिक सेवकों तथा अन्य व्यवसायों के अलावा सेवा का काम करने वाले लोगों की तुलना में अपने को श्रेष्ठ न समझें और उनसे श्रेष्ठ बनकर रहने का प्रयत्न न करें।’’
देश, और देश के भविष्य के प्रति असीम लगाव और चिंता उन लोगों के मन-मस्तिष्क में भी प्राथमिकता से बनी रहती है, जो राजनीति से दूर हैं, लेकिन अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठापूर्वक सजग हैं। आम चुनाव के समय ऐसे लोगों की चर्चा में कुछ बिंदु लगातार उभरते हैं: क्या चुनाव-खर्च इसी तरह बढ़ता रहेगा; क्या पक्ष-विपक्ष के मध्य लगातार बढ़ रही तल्खी निर्बाध रूप में शालीनता, पारस्परिक सम्मान, और सद्भाव पर और अधिक हावी होती रहेगी; क्या देश में राजनीति करने के लिए इसकी संस्कृति, सभ्यता और धार्मिक आस्था पर प्रहार कर सफलता पाने के प्रयास बंद नहीं होंगे?
क्या चुनाव संवाद के स्थान पर विवाद को ही बढ़ाते रहेंगे? सामान्य जन अब इस तथ्य का अभ्यस्त हो गया है कि चुनाव परिणाम आने के बाद उसकी खोज-खबर लेने न जीतने वाला आएगा, न ही हारने वाला। सारी भीड़ पांच साल के लिए छंट जाएगी।