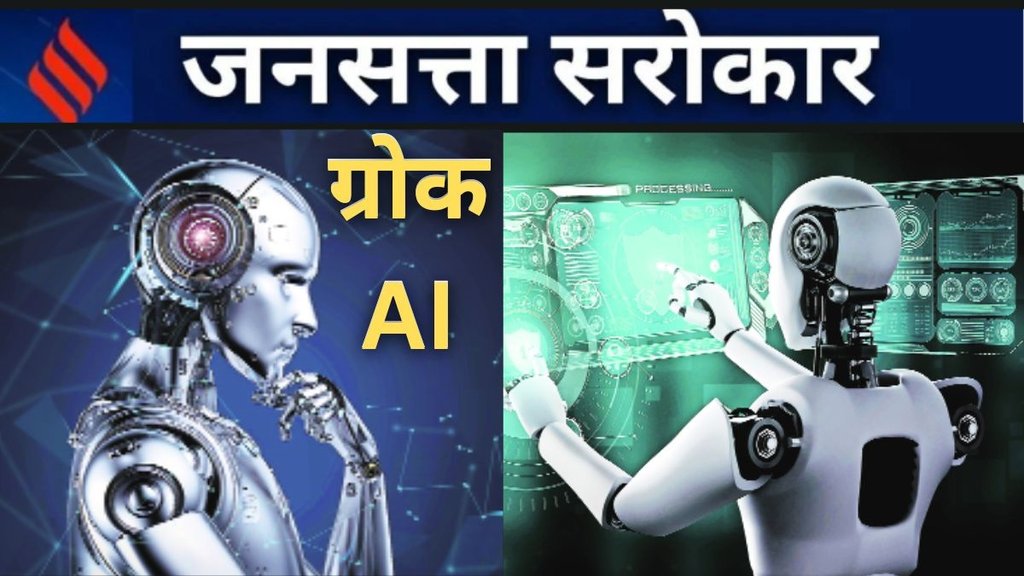Grok AI: कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआइ के एक औजार के तौर पर ग्रोक के आने के पहले से इस मसले पर बहस शुरू हो चुकी थी कि विज्ञान और तकनीक का यह आविष्कार समूची दुनिया और मनुष्य के लिए कितना और किस स्तर पर उपयोगी साबित होगा। ग्रोक के आने के बाद हुआ बस यह है कि चारों तरफ चर्चा इसके विस्तार और भावी स्वरूप पर होने लगी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एआइ के रूप में दुनिया जिस संसाधन को रोजमर्रा का हिस्सा बनाने जा रही है, उसकी उपयोगिता कई क्षेत्रों में साबित हो गई है, लेकिन इसके साथ ही इसके खमियाजे किस शक्ल में सामने आएंगे, इस पर भी बहस जोर पकड़ रही है।
Future of AI: ग्रोक के सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध होते ही सोशल मीडिया पर इसके साथ जिस तरह के सवाल-जवाब सामने आए, उसने एक नया सवाल यह उठाया है कि इससे निकले जवाब का तंत्र कहां से और कैसे संचालित होता है और क्या इसके जवाब पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। मसलन, कुछ उदाहरण ऐसे भी देखे गए, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में ग्रोक ने एक ही सवाल एक से ज्यादा तरीके से किए जाने पर जवाब अलग-अलग और काफी हद तक विरोधाभासी भी दिए। ऐसे में प्रश्न करने वाले के सामने क्या यह दुविधा खड़ी नहीं होगी कि वह किस जवाब को सही माने? ग्रोक फिलहाल अन्य चैटबाट या एआइ प्रणाली से थोड़ा अलग इसलिए है कि यह सवाल का जवाब देते हुए कई बार हल्का-फुल्का मजाक का छौंक लगाता है।
संवेदनशीलता के लिहाज से दूसरे चैटबाट से ग्रोक कई मायनों में अलग है
इसके अलावा, कई चैटबाट कुछ संवेदनशील विषयों पर या तो स्पष्ट नहीं बोल पाते या फिर जवाब नहीं देते, ग्रोक उनके बारे में भी खुल कर बात कर रहा है। बाकी चैटबाट के मुकाबले ग्रोक को ज्यादा प्रचार और विस्तार मिलने का एक कारण यह भी है कि इसमें कुछ भी पूछने के लिए किसी अलग ऐप का उपयोग नहीं करना पड़ता या बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि कभी ट्विटर के नाम से काम करने वाले मौजूदा एक्स के टिप्पणियों वाले हिस्से पर ही ग्रोक को संबोधित करके सवाल पूछा जाता है और वह वहीं जवाब दे देता है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिस रूप में सुर्खियों में है, उस एआइ को भाषा माडल के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि एआइ की संरचना और उसकी कार्यविधि के बारे में जिन लोगों को बुनियादी जानकारी है, वे इस बात को समझ पाएंगे कि ग्रोक या एआइ का कोई भी मंच किसी सवाल का वही जवाब देगा, जिसे खोज सकने की उसकी सीमा होगी, सवाल के जवाब में इंटरनेट के संजाल पर उसकी उपलब्धता होगी। लेकिन क्या अब यह भी संभव है कि एक ही मसले पर अलग-अलग विचारों की उपलब्धता के विस्तार की दुनिया में एआइ भी विभ्रम का शिकार हो सकती है? अगर नहीं, तो एक ही प्रश्न के उत्तर में विरोधाभासी जवाब सामने आने की वजह क्या हो सकती है? संभव है कि आने वाले वक्त में एआइ इसके भी निदान से युक्त हो।
एआई की सामग्री का सही-गलत मनुष्य के विवेक पर निर्भर है
जाहिर है, इंटरनेट की दुनिया में कहीं भी अगर कोई सामग्री है, तो उसे छान कर ही कोई एआइ अपना जवाब तैयार करता है। मगर उसके सही या गलत होने या उस पर नए सिरे से विचार करने का मामला आखिर मनुष्य के विवेक पर ही निर्भर है।
इसके समांतर यह भी सच है कि सभ्यता के विकास क्रम में मनुष्य ने जितनी यात्रा की है, उसमें विज्ञान का साथ एक सबसे अहम कड़ी के रूप में कायम रहा है। यह अलग बात है कि अब इस बात का विश्लेषण होने लगा है कि एक समय विज्ञान के जिस उपादान ने मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने, नई दुनिया गढ़ने में मददगार की भूमिका निभाई, उसमें से कौन बाद में या आगे चल कर मनुष्य के हित में या फिर कई स्तर पर मानव सभ्यता के प्रतिकूल साबित हुआ।
यहां यह तर्क जरूर दिया जा सकता है कि विज्ञान ने जो तकनीकी दुनिया की दी, उसके उपयोग पर निर्भर है कि वह मनुष्य और दुनिया के लिए क्या साबित होता है। यह सही भी है। मगर यहीं यह सवाल भी उभरता है कि कोई खास तकनीक अगर अपने सामान्य उपयोग या प्रयोग में दुनिया के एक छोटे-से हिस्से के लिए फायदेमंद और ज्यादातर लोगों के लिए या तो अनुपयोगी या फिर नुकसानदेह साबित हो तो उसे किस कसौटी पर आंका जाएगा। इसी क्रम में मौजूदा दौर में एआइ के जितने भी स्वरूप हमारे सामने आए हैं, वे बहस के बीच हैं और उनकी उपयोगिता के साथ-साथ आने वाले वर्षों में उनके असर का मूल्यांकन होने लगा है। यों एक तकनीकी के स्तर पर एआइ का दायरा बहुत बड़ा है और यह केवल प्रश्न-उत्तर के एक मंच तक सीमित नहीं है और इसका विस्तार बहुत सारी नई मशीनों के भीतर भी है, जो मनुष्य के श्रम का विकल्प बन रही हैं।
मगर फिलहाल बहस में एआइ का वह हिस्सा है, जो कोई प्रश्न करने पर उसका उत्तर देता है। हाल में सुर्खियों में आया ग्रोक उसी की एक कड़ी है। इससे पहले इस क्षेत्र में चैट-जीपीटी और मेटा से लेकर कुछ समय पहले बाजार में उतरे डीपसीक और माइक्रोसाफ्ट के कोपायलट ने इस मुद्दे पर एआइ के बहुस्तरीय और बहुआयामी पहलुओं को सामने रखा है और उस पर बात शुरू हो चुकी है। अब तक जिस रूप में इससे काम लिया जा रहा है, उसमें इसकी उपयोगिता का आकलन इस स्तर पर भी हो रहा है कि भविष्य में इसका सिरा कहां जाएगा।
दरअसल, ग्रोक, डीपसीक, मेटा, जेमिनी, कोपायलट या चैट-जीपीटी आदि को बातचीत के मशीनी अवतार की तरह देखा जा सकता है। इस तरह के चैटबाट से कोई सवाल पूछा जाता है तो कई बार कुछ तकनीकी या तथ्यगत संदर्भ को यह काफी सटीकता के साथ जवाब के तौर पर पेश करता है, लेकिन ऐसा भी आम है कि कुछ पूछने पर यह उस प्रश्न का संदर्भ आधा-अधूरा समझता है और उसी में एक सामान्य विश्लेषण का छौंक लगा कर पेश कर देता है। इसके कई जवाब में सामान्य से बेहतर समझ दिखती है, जिसका कारण यह हो सकता है कि यह इंटरनेट पर मौजूद डेटा की विस्तृत दुनिया के सहारे काम करने के लिए प्रशिक्षित होता है।
हालांकि एआइ चैटबाट के संदर्भ में यह बात जोर देकर कही जा रही है कि ये मंच केवल रटे-रटाए जवाब नहीं देते, बल्कि इनके सोचने-समझने की शक्ति भी असीमित है। लेकिन एआइ को लेकर यह धारणा किस हद तक सही है? अब तक इसका जो स्वरूप सामने आया है, इसके काम करने की जो शैली और नतीजे देखे गए हैं, उससे तो यही लगता है कि इस तरह के यंत्रों को जितना सोचने लायक बनाया गया है, उससे ज्यादा इसकी उपयोगिता लोगों को नियंत्रित करने में हो सकती है।
सच यह है कि फिलहाल डिजिटल दुनिया के संजाल, मुश्किलों और चुनौतियों को समझ पाना अभी पूरी तरह संभव नहीं हो सका है। विचित्र यह है कि इस हकीकत के बावजूद कृत्रिम मेधा के संदर्भ में ही दुनिया के भविष्य में इसकी भूमिका की व्याख्या की जा रही है। जिस कसौटी पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मनुष्य के विचार-संसार और जीवन-गतिविधियों के क्षेत्र में बहुत ज्यादा संभावनाओं वाला होने के बारे में दावे किए जा रहे हैं, उसी के समांतर आने वाले वक्त में मनुष्य की भूमिका के सिमटने से आगे सभ्यता पर संकट की भी आशंका जाहिर की जा रही है।
जाहिर है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव इस पर निर्भर करेगा कि इस तकनीक के उपयोगकर्ता के तौर पर मनुष्य अपने विवेक को कितना बचा पाता है और इसके उपयोग को कितना मानव सभ्यता के हित में सुनिश्चित किया जा सकेगा। अगर किन्हीं हालात में आगे चल कर तकनीक ही मनुष्य को नियंत्रित करने लगे, तो उसके बाद की दुनिया के बारे में सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। वैसी स्थिति में मनुष्य की समूची सभ्यता के सामने जो खतरा पैदा होगा, उससे निपटने क्या इतना आसान होगा? उससे कौन निपटेगा? उसके बाद के नतीजे और उसके बाद की दुनिया कैसी होगी?
जनसत्ता सरोकार: मोबाइल की दुनिया में सिमटतीं संवेदनाएं, तकनीक के बढ़ते जाल में खोता इंसान
इस संदर्भ में निकोलस नेग्रोपोंटे की यह राय गौरतलब है कि प्रौद्योगिकी सिर्फ एक उपकरण नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति भी है जो हमारे स्वभाव को भी बदल रही है। हमारे पास दो विकल्प हैं। या तो हम अपनी प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करेंगे या यह हमें नियंत्रित करेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में सबसे ज्यादा चिंता इस बात पर जताई जा रही है कि इसके कारण दुनिया भर में बड़े पैमाने पर नौकरियां जाएंगी और इसका बहुत ज्यादा नकारात्मक असर बड़ी आबादी पर पड़ेगा। जिस दौर में दुनिया के बहुत सारे देश पहले ही बेरोजगारी के संकट से जूझ रहे हैं, वैसे में अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता सचमुच भारी पैमाने पर नौकरियों को प्रभावित करता है, इंसानी मेहनत और मानव संसाधन के रूप में उनके काम करने का विकल्प बनता है, तो दुनिया किस तरह के भविष्य का सामना करेगी? चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की खोज और जीवाश्म ईंधन को बदलने के साथ-साथ अन्य कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में शोध के लिहाज से इसकी अहमियत अब छिपी नहीं है।
हालांकि इस क्षेत्र में नए हुनर से लैस होने वाले लोगों के लिए एआइ से संबंधित नई नौकरियों का विकल्प खुलने की भी बात कही जा रही है, लेकिन इसकी वजह से जो लोग रोजगार से वंचित होंगे, बेकार लोगों की एक व्यापक दुनिया खड़ी होगी, उसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या किसी योजना पर विचार किया जा रहा है? या फिर बेकार या अनुपयोगी घोषित किए गए लोग दुनिया के सामने एक नई चुनौती बनेंगे?
इसकी वजह से कुछ अन्य क्षेत्रों में जिस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं, वे भी छिपी नहीं रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआइ का सहारा लेकर असली लगने वाली फर्जी खबरें जिस तरह एक बड़ी आबादी को प्रभावित करती हैं, उससे कई बार जटिल स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा, एआइ की मदद से ऐसी तस्वीरें और वीडियो बना लिए जाते हैं, जो फर्जी होते हैं, लेकिन असली होने का आभास देते हैं। ऐसे में आपराधिक मानसिकता वाले लोग इसका उपयोग गलत तरीके से या फिर भयादोहन तक के लिए कर रहे हैं। इसी तकनीक के सहारे डिजिटल ठगी का ऐसा संजाल खड़ा हो गया है, जो आज साइबर अपराधों की दुनिया को एक नया रूप दे रहा है और उससे निपटना सरकारों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है।
इसमें कोई शक नहीं कि तमाम सवालों और आशंकाओं को बावजूद इस आधुनिक तकनीकी के रास्ते को रोक देना शायद अब संभव नहीं है, लेकिन मनुष्य के विवेक के सामने यह चुनौती जरूर है कि अगर एआइ सब कुछ को हस्तगत करने की राह पर है, तो इसके विकास को कम से कम इस स्तर तक नियंत्रित किया जाए, जब इस संसाधन का इस्तेमाल करने वाली कंपनियां और पूरी मानव जाति इसके सकारात्मक प्रभाव और उससे उपजी मुश्किलों और चुनौतियों से आसानी से निपट पाने को लेकर हर तरह से आश्वस्त हो जाए। स्टीफन हाकिंग जैसे वैज्ञानिक भी मानवता को कृत्रिम मेधा से भावी खतरे को लेकर काफी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं।

इसके समांतर दुनिया भर के कई देशों में शिक्षा के क्षेत्र में एआइ को बढ़ावा देने की कोशिशें चल रही हैं, वहीं इसका विरोध भी हो रहा है। कुछ वर्ष पहले जब कोरोना महामारी फैली थी और लोगों का घर से बाहर निकलना भी बाधित हुआ था, पूर्णबंदी की वजह से स्कूल-कालेज भी बंद किए गए थे, उस समय आनलाइन पढ़ाई को जरिया बनाया गया था। इस बात का आकलन अभी आना बाकी है कि उस दौरान बच्चों की पढ़ाई से लेकर मनोविज्ञान तक पर कितना और कैसा असर पड़ा था। उस दौरान बहुत सारे देशों में स्कूल-कालेज ने पढ़ाई के लिए जो आनलाइन तरीका अपनाया था, उस पर यूनेस्को ने भी सवाल उठाए थे।
यह कहा गया कि तकनीकी समाधानों का हड़बड़ी में लागू किया जाना एक त्रासदी थी… इससे असमानता बढ़ी और पढ़ाई के नतीजे खराब हुए। यह बेवजह नहीं है कि कुछ देशों में शिक्षण के क्षेत्र में एआइ के उपयोग को लेकर नए सिरे से विचार किया जा रहा है और इसके प्रयोग को हतोत्साहित किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर स्वीडन में अब स्कूली बच्चों को डिजिटल यंत्रों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। छपी हुई किताबें, उनसे सीधे पढ़ाई, हस्तलेखन को बढ़ावा दिया जा रहा है और टैबलेट देखने, उस पर टाइप करने और आनलाइन शोध-अनुसंधान को कम करने को कहा जा रहा है।
इसकी रफ्तार और इसके असर को देखते हुए इस बात का आकलन शुरू हो गया है कि आने वाले सौ वर्षों में दुनिया कैसी होगी। समाज से लेकर राजनीति और हर स्तर पर जिस तरह एआइ अपने पांव पसार रहा है, उसमें यह मानव जीव के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लोकतंत्र की व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या होगा, लोकतांत्रिक मानी जाने वाली संस्थाओं के काम करने का स्वरूप कैसा होगा, नैतिक मूल्यों पर इसका क्या असर पड़ेगा, परिवार, समाज किस रूप में बना रहेगा, रिश्तों और भावनात्मक संबंधों का स्वरूप क्या होगा। आने वाले वक्त में सभी स्तर पर इस तरह के सवाल दुनिया के सामने चुनौती बनेंगे।