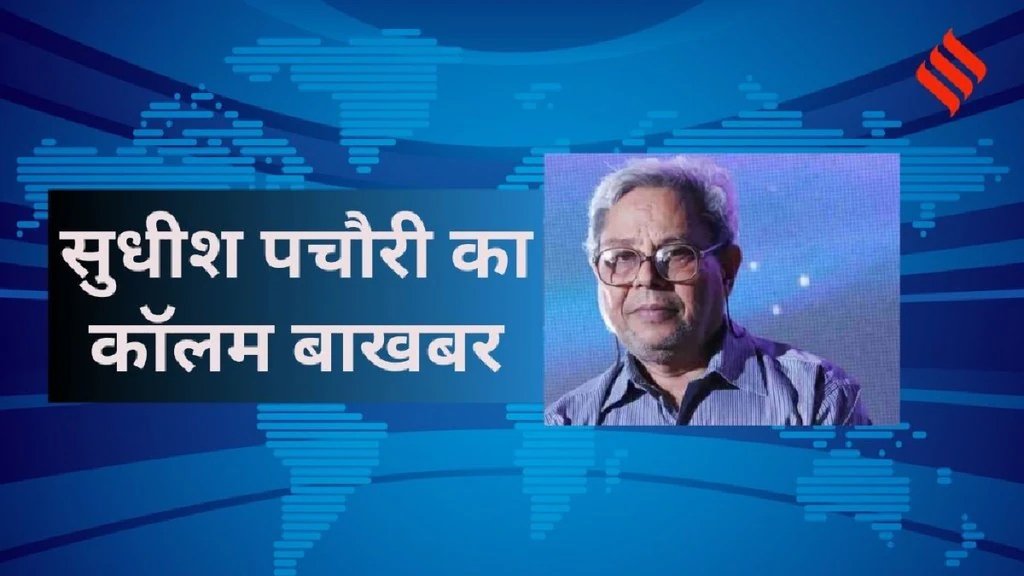इधर राष्ट्रीय शोक रहा, उधर चैनलों में क्लेश-कलह रहा। एक पक्ष का आरोप रहा कि सात दिन का राष्ट्रीय शोक, फिर भी वे विदेश गए तो दूसरे पक्ष का प्रत्यारोप रहा कि अंतिम दर्शनों और अंत्येष्टि के दौरान भी अपमान किया गया! न उनके परिजनों को सीट दी गई न किसी और को सीट दी गई… लेकिन वे सब सीटों पर बैठे रहे। फिर बहसों में आई एक आवाज कि बताइए, एक शाम एक ‘बिल’ को सरेआम फाड़कर किसने किसका ‘अपमान’ किया था! किस-किस पूर्व महामहिमों को उनके निधन के बाद उनको कायदे से अंतिम विदाई तक न दी गई?
यह शिकायत भी रही कि ‘जहां अंत्येष्टि, वहीं समाधि की नीति के अनुसार वहीं जगह दी जानी चाहिए थी। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? जवाब आया कि ऐसे सारे आरोप गलत हैं! सब कुछ कायदे से किया गया है… एक कमेटी समाधि की जगह की तलाश रही है… जल्दी ही जगह दे दी जाएगी। इस तरह, लड़ाई-झगड़े भी चलते रहे और शोक भी चलता रहा। चैनलों के कई दिन-रात चर्चा-कुचर्चा में बीते। फिर एक दिन शोक भी किनारे हुआ, सिर्फ ‘सम्मान बरक्स अपमान’ की ‘बतबढ़’ रह गई। और इस सबके बीच ‘जिन मानस ते देवता, करत न लागै बार’ जैसे भाव भी उमड़ते-घुमड़ते दिखते रहे! यही अपनी संस्कृति है। जब तक बंदा जिंदा रहता है, तब तक ‘घर की मुर्गी दाल बराबर’ होती है, लेकिन सिधारते ही उसमें ‘देवत्व’ देखा जाने लगता है।
सभी अहसानमंद भक्त और इन भक्तों के नए देवता। फिर ऐसे भक्तों की घुड़की भी बनी रहती है जो कहती है कि हमारे देवता तो तुम्हारे भी देवता। मानो कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा। और अगर कोई न माने तो वह तो गया! पिछले कुछ ही दिनों में इस तरह दो-दो देवता हमें मिले! एक अपेक्षाकृत ‘सर्वमान्य’ से रहे, दूसरे ‘प्राइवेट लिमिटेड’ से रहे। ‘शोक की होड़’ और ‘अहसानमंदी की होड़’ के इन दिनों में सबसे अधिक पुण्य का काम है: ‘देव निर्माण’।
इधर बनाना उधर भूल जाना। फिर कुछ दिन बाद नए देवता का पधारना और फिर भूल जाना और फिर जरूरत पड़ने पर उसकी खुदाई करने लगना और फिर उस या इस नए देवता का पधारना। इन दिनों उत्तर प्रदेश के संभल और उसके आसपास जहां भी फावड़ा चलता है, वहीं कोई पुराना मंदिर, पुराना कुआं, पुरानी बावड़ी और मंदिर के प्रतीक चिह्न निकल पडते हैं। इसी बीच ‘मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा’ के इस दौर में अचानक कुछ ‘बाबाओं’ की ‘बम-बम’ भी सुनाई पड़ती है। और इस ‘महाविज्ञापित हाइप’ से संचालित ‘महाकुंभ’ के घर बैठे नित्य दर्शन पाकर चैनलों के दर्शक भी धन्य-धन्य होते नजर आते हैं।
बहसों के ‘दो पाटों के बीच’ में फंसे कई एंकर जितना कहते कि ‘जो चला गया, उस पर राजनीति न करें’, वक्ता-प्रवक्ता सभी उतने ही जोर-शोर से राजनीति करते दिखते। इन दिनों सभी एक दूसरे को जरा-जरा-सी बात पर नीचा करने के चक्कर में नजर आते हैं। ऐसी ही एक बहस में एक पत्रकार ने इस ‘कलह संस्कृति’ को ‘आउटरेज की राजनीति’ का नाम दिया। हिंदी में आप इसे ‘खुंदकी राजनीति’ या ‘क्षोभ की राजनीति’ यानी ‘चिर संचित गुस्से की राजनीति’ कह सकते हैं। एक ने कहा भी कि यह ‘न जीत पाने की निराशा की राजनीति’ है, लेकिन हम कहेंगे कि यह है ‘खिसियानपट्टी’ की राजनीति या ‘चिढ़ की राजनीति’ है।
इन दिनों अनेक वक्ता-प्रवक्ता इतने क्षुब्ध नजर आते हैं कि अगर किसी ने किसी के महामहिम को ‘हलो’ किया तो गया, न किया तो गया। कोई किसी से मिलने गया तो ‘देसी चिह्न शास्त्री’ शुरू कि उसके ‘मिलने’ को न देखो, मेरी व्याख्या को देखो। हुआ यों कि एक दिन ज्यों ही पंजाबी के गायक दिलजीत दोसांझ जब प्रधानमंत्री से मिलने गए तो तो काला सूट, काली पगड़ी, काली टाई पहनकर गए। इसे देख एक कथित चिह्नशास्त्री बने विपक्षी प्रवक्ता ने तुरंत दोसांझ के ‘काले सूट पगड़ी’ को ‘विरोध’ का रंग बताया. जबकि वह बंदा अपने बयानों में प्रधानमंत्री की तारीफ ही करता नजर आया।
बहरहाल, दिल्ली के ‘चुनावी दंगल’ में एक दिन एक नए ‘हिंदुत्व’ की ‘एंट्री’ ने पुराने हिंदुत्ववादियों तक को चौंका दिया। इस ‘नए हिंदुत्व’ ने जैसे ही दिल्ली के सभी पुजारियों व ग्रंथियों को अठारह हजार रुपए महीने की ‘सम्मान राशि’ देने का वादा किया, वैसे ही विवाद शुरू होकर चैनलों में छा गया। मजे की बात यह कि जिस वक्त पुजारियों, ग्रंथियों को सम्मान राशि देने की घोषणा की जा रही थी, उसी वक्त दिल्ली स्थित सैकड़ों मस्जिदों के इमाम मांग कर रहे थे कि पिछले अठारह महीने से हमें दिल्ली सरकार ने वेतन नहीं दिया, पहले वह तो दे!