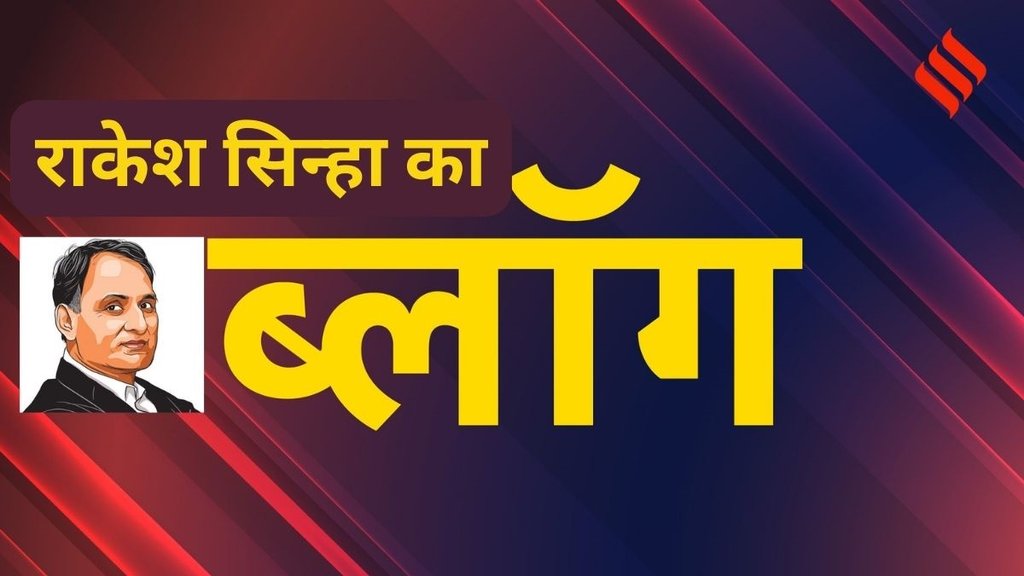राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने धार्मिक स्थलों के विवाद को बेलगाम होने से रोकने का संदेश दिया है। इसे किसी संदर्भ में देखना अनुचित ही नहीं, एक गंभीर हस्तक्षेप के प्रति अन्याय है। जब भी दो टूक बातें कही जाती हैं, तब सहमति और असहमति का स्वर उठना अस्वाभाविक नहीं होता है। विशेषकर वैचारिक बेरोजगारों के लिए अपने होने का अहसास करने का स्वर्णिम अवसर होता है। पर तात्कालिकता से ग्रस्त प्रतिक्रिया बहस का हिस्सा नहीं बनती है। किसी वैचारिक हस्तक्षेप की ताकत इस बात से परखी जाती है कि उसका जटिल प्रश्नों पर कितना प्रभाव पड़ता है। भागवत के कथन ने सभी प्रकार के लोगों को अपनी-अपनी दृष्टि से मंथन करने के लिए प्रेरित एवं बाध्य किया है। धार्मिक स्थलों पर विवाद के जरिए उन्होंने राष्ट्रीयता, संस्कृति और पंथनिरपेक्षता को बहस के केंद्र में ला दिया है। हिंदुत्व की परिधि में जरूर विमर्श हो रहा है, पर इसका फलक एकपक्षीय नहीं है। यह रचनात्मक परिणाम की संभावना को दिखाता है।
भागवत के भाषण का निचोड़ अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक अवधारणाओं का अंत करना है। संविधान सभा में इसके उपाध्यक्ष रहे डा एचसी मुखर्जी ने इसी प्रश्न को सदस्यों के सामने रखते हुए कहा था कि अगर हम ‘एक राष्ट्र और एक जन’ का निर्माण करना चाहते हैं तो किसी भी समुदाय को धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक नहीं मान सकते हैं। वे स्वयं इसाई मतावलंबी थे। उपनिवेशवादी राजनीतिक दर्शन इतना हावी था कि उनकी बात अनसुनी कर दी गई। संघ अपने सौ वर्षों की यात्रा में इसी राजनीतिक संस्कृति के विरुद्ध लड़ता रहा है। नेहरूवादी राज्य हिंदू बनाम अल्पसंख्यक से उपजने वाले प्रश्नों से धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करता रहा। इसने इसे भानुमती का कुनबा बना दिया था।
संघ का संविधान सभा में भले ही प्रतिनिधित्व नहीं था, पर इसके विचार की छाया वहां विद्यमान थी। संविधान सभा में लोकनाथ मिश्र ने ‘सेकुलर स्टेट’ के प्रयोग को छलावा माना। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जीवन के प्राचीन इतिहास की उपेक्षा करने का उपकरण बन जाएगा। स्वतंत्रता के बाद ठीक वही हुआ। प्राचीन काल की वही और उतनी ही बातों को चयनित किया गया जो अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों को निराश नहीं करे। हमारा प्राचीन काल का इतिहास और हमारी उपलब्धि सामान्य ज्ञान की पुस्तकों और परीक्षाओं तक सिमट कर रह गया।
इस विस्मृति को समाप्त करना आसान नहीं था। इसका ठोस कारण है। पाठ्यक्रमों, राज्य द्वारा पोषित संस्थाओं, प्रचार माध्यमों के साथ अधिकांश राजनीतिक दलों और बुद्धिजीवियों द्वारा राष्ट्रीयता और पंथनिरपेक्षता की एकपक्षीय तस्वीर पेश की जाती रही है। दूसरी तरफ संघ पर छवि का संकट थोपा जाता रहा है। पर राष्ट्र निर्माण के ध्येय से किया गया कार्य सदैव अपराजेय रहता है। संघ अलग-अलग कालखंडों में अलग-अलग तरीकों से विचार का प्रयोग करता रहा है। संघ की स्थापना के समय एक भिन्न प्रकार की चुनौती थी। बीसवीं शताब्दी में ‘हिंदू’ शब्द बहुत से लोगों के लिए ग्लानि का प्रतीक था और इसका अभिप्राय सामाजिक दृष्टिकोण से संकुचित था। इस बात को सबसे पहले कर्नल यूएन मुखर्जी ने अपनी पुस्तक ‘डॉईंग रेस’ (1909) में उठाया था। तब थोड़ी हलचल हुई थी। कुलीनों तक बात सिमट गई। इस प्रश्न को संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार ने गंभीरता से लिया।
वे समझते थे कि हिंदुत्व राजनीतिक अवधारणा बनकर या भाषणों या प्रचार से कभी सामाजिक-सांस्कृतिक विसंगतियों, जो जातीय कटुता, अस्पृश्यता, भाषायी संघर्ष आदि रूप में विद्यमान था, को समाप्त नहीं कर सकता है। तात्कालिक या भावनात्मक कारणों से संगठित हो जाना सामाजिक एकता और सद्भाव का सूचक नहीं है। विविधताओं को संरक्षित रखते हुए उसे प्रतिस्पर्द्धी नहीं बनने देना तभी संभव है जब हिंदुओं में राष्ट्रवाद का संचार होगा। इन्हीं बातों ने संघ और हिंदू महासभा की राह अलग-अलग कर दी। जिस देश में आक्रांताओं द्वारा विध्वंस के इतिहास का मौखिक विवरण मौजूद हो, वहां कुछ लोगों के मन में प्रतिकार और प्रतिरोध का भाव पैदा होना अस्वाभाविक नहीं है। हिंदू महासभा के अंत के बाद यह वर्ग संघ में महासभा तलाशना चाहता है। यही स्वर सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर निर्णायक क्षणों में दिखाई पड़ता है। 1930 और 1940 के दशकों में भी कुलीन और प्रतिष्ठित हिंदू नेताओं को सार्वजनिक आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था। मुखर और मौन लक्ष्यों का अंतर समझना कठिन होता है। संघ मौन लक्ष्य लेकर चलता रहा है।
मोहन भागवत की पहल ने मार्क्सवादी-नेहरूवादी और अल्पसंख्यकों, दोनों को जड़ता से निकलने का स्पष्ट संदेश दिया है। कोई रचनात्मक पहल दूसरे पक्ष के लिए उनकी यथास्थितिवाद बनाए रखने के लिए समर्थन नहीं होता है। भागवत ने सभ्यताई-सांस्कृतिक पक्ष से जुड़ने के लिए आत्मालोचन का अवसर दिया है। चिंतन इसी प्रश्न पर होना चाहिए। इसमें मुसलिम-इसाई मध्यम वर्ग और आध्यात्मिक नेताओं की पहल अपेक्षित होता है। यह असंभव नहीं है। एक छोटा देश अल्बानिया इसका उदाहरण है। वहां साठ फीसद मुसलिम और तीस फीसद ईसाई हैं। शेष में रुढ़िवादी और नास्तिक है। उनके पास न प्राचीन सभ्यता की, न ही संस्कृति की पूंजी है। पर स्थानीयता ने सामुदायिक जीवन विकसित किया है। सौहार्द और धर्मनिरपेक्षता उसका अभिन्न अंग है। इसे वे राष्ट्रीय भाव कहते हैं।
भारत के पास सभ्यता और संस्कृति का विविधतापूर्ण इतिहास है, जिसे स्वीकार करना ही संवैधानिक भारत के साथ सांस्कृतिक भारत का हिस्सा बनना है। यही सभ्यताई भाव कहा जाएगा, जैसे अल्पसंख्यक मोहम्मद अली जिन्ना से जोड़कर नहीं देखते हैं, वैसे ही आक्रांताओं के चरित्र से जुड़ना भी लांछन की तरह है। यही से राष्ट्रीयता और पंथनिरपेक्षता पुन: परिभाषित होता है। भागवत के कथन की आलोचना अपने को उदार मानने वाले ‘जयपुर डायलाग’ से हुआ। ऐसे लोग उसी युग से प्रेरणा ले रहे हैं, जिसमे संघ और हिंदुत्व अवांछनीय था। अब वैचारिक लड़ाई का स्वरूप भूतकाल से भिन्न है। यह लड़ाई जड़ता और जीवंतता के बीच है।