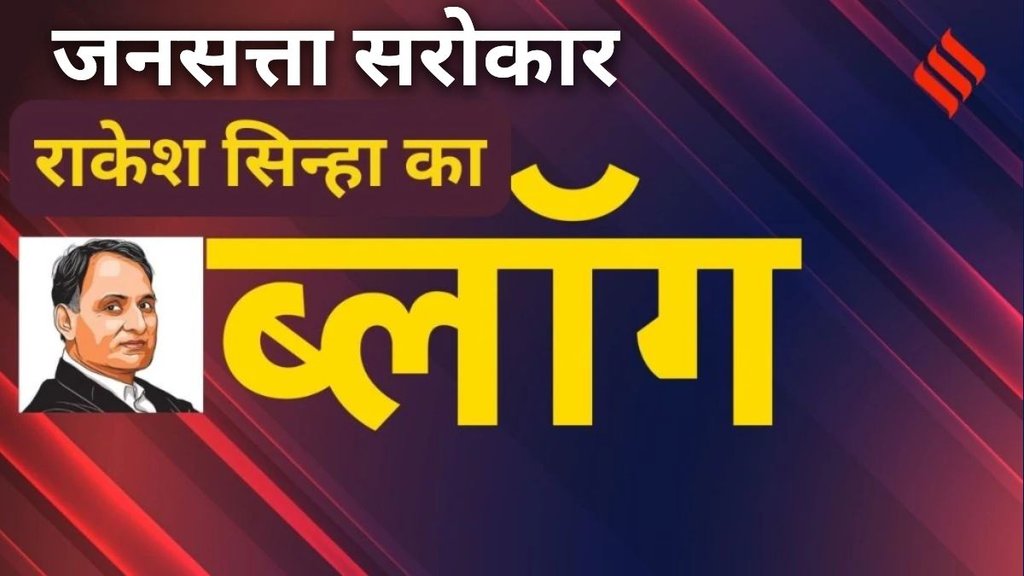राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सौवां वर्ष एक अवसर है, राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित करने वाले विषयों पर खुलकर चर्चा करने का। इनमें पंथनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और संस्कृति का भारतीय पक्ष प्रमुख है। इन प्रश्नों का बार-बार विमर्श के क्षितिज पर उभरकर आने का कारण भी संघ ही रहा है। पर यह संघ के प्रति अतिशय प्रेम और अतिशय द्वेष के कारण सांकेतिक बनकर रह गया। बौद्धिक फलक पर संघ के विरोध का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन संघ इससे कभी परेशान नहीं हुआ। इसके पीछे बौद्धिकता की उपेक्षा करने की मानसिकता न होकर एक दर्शन रहा है।
आधुनिक विश्व में दो लोगों ने ‘संस्कृति’ को बुनियादी परिवर्तन का सबसे बड़ा जीवंत उपकरण माना है। इनमें एक जर्मनी के जोहान गाटफ्रीड वान हर्डर (1944-1803) हैं। वे अपनी रचनाओं द्वारा जर्मनी के ‘स्व’ को जागृत करते रहे। दूसरे, संघ के संस्थापक डा केशव बलिराम हेडगेवार हैं। दोनों में एक विशिष्ट समानता और स्पष्ट अंतर भी है। दोनों ने सामान्य जनों को अपना कर्मक्षेत्र बनाया। विशिष्ट मानकर समाज को निर्देशित करने का भ्रम पालने या दावा करने वालों से दूर रहे। हर्डर की लेखनी और हेडगेवार की दृष्टि ने क्रमश: जर्मनी और भारत में सबसे अधिक प्रभाव छोड़ा है। पर जहां हर्डर की प्रासंगिकता समय के साथ सिमटती गई, वहीं हेडगेवार की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। इसका कारण है।
हर्डर ने जर्मनी की संस्कृति को ‘पवित्रता’ और ‘नस्लीय चेतना’ से जोड़ने का काम किया। इसके विपरीत हेडगेवार ने ‘हिंदू चेतना’ को ‘पवित्रता’, ‘नस्लीय भाव’, ‘पराएपन’ जैसी संकीर्णताओं से मुक्त रखा। इसीलिए संघ अतीत की घटनाओं को देखने में ‘स्मृति’ और ‘विस्मृति’, दोनों का उपयोग करता है। हिंदू अस्तित्व के साथ-साथ हिंदू का सर्वसमावेशी स्वरूप हेडगेवार के व्यावहारिक आदर्श का हिस्सा था। यह संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के व्याख्यानों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।
संघ ऐतिहासिक अनिवार्यता बन गया है। इसका कारण क्या है? लोगों की सामूहिक उपचेतना में उपस्थित हिंदू सभ्यता को पुनर्स्थापित करने वाला यह एकमात्र संगठन है। निरंतर आक्रामकता के कारण सभ्यता में बिखराव हुआ। खंडित सभ्यता भारतीय राष्ट्र के रूप में है। वह भी गंभीर आंतरिक चुनौतियों से मुक्त नहीं है। संघ ने उससे लड़ने की ताकत और लोगों का विश्वास दोनों अर्जित किया है। अखंडित सभ्यता की पुनर्प्राप्ति से ही भारत को भारतवर्ष बनाना होगा। इसलिए तात्कालिक राजनीति या बौद्धिक आलोचनाओं से संघ बहुत प्रभावित नहीं होता है। यही इसकी संजीवनी है।
हिंदू सभ्यता के बिखराव का दर्द संघ से पूर्व भी महसूस किया गया, लेकिन वह व्यक्तिगत अनुभूति और सीमित प्रभाव के साथ में इतिहास का हिस्सा बनकर रह गया। बंगाल में नबागोपाल मित्रा ने 1867 में ‘हिंदू मेला’ की शुरुआत की थी, जिसे राजनारायण बोस (1826-1899) ने व्यापक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी रूप देने का काम किया। रामानंद चटर्जी ने मासिक पत्रिका ‘माडर्न रिव्यू’ तो राजा रवि वर्मा (1848-1906) ने चित्रकारी के जरिए उस हिंदू सांस्कृतिक चेतना को उभारने का काम किया। पंजाब में लाला लालचंद ने ‘पंजाबी’ समाचार पत्र में छद्म नाम से संपादक के नाम इक्कीस पत्रों के द्वारा तो यूएन मुखर्जी ने ‘बंगाली’ सामाचार पत्र में इकतीस लेखों की शृंखला से हिंदू अस्तित्व और अस्मिता को झकझोरने का काम किया था। पर सभी शिक्षित वर्ग तक सीमित रहे।
संघ द्वारा हिंदू चेतना जागृति सिर्फ बाह्य चुनौतियों के आधार पर नहीं है। इसने सामाजिक बदलाव को, चाहे अस्पृश्यता हो या जातीय संकीर्णता, पहली प्राथमिकता देने का काम किया है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अनाम योगदानकर्ता बन गया। इसका एक अच्छा उदाहरण डा हेडगेवार के जीवन से है। प्रसिद्ध लेखक दामोदर पंत ने हेडगेवार से उनकी जीवनी लिखने की पेशकश की तो उनका उत्तर था- ‘मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उन लोगों की श्रेणी में आऊं, जिनकी जीवनी लिखी जाती है। अगर आप ऐसा प्रयास नहीं करेंगे, तब मैं आपके प्रति अभारी रहूंगा।’
प्रासंगिक काम कर स्वयं को अपने जीवन काल में अप्रासंगिक बनाकर रखना ही उनका मूल मंत्र था। नैतिक सामर्थ्य की जगह भौतिक सामर्थ्य और प्रसिद्धि की लालसा ही चिंतकों, समाज सुधारकों और सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाओं के निष्प्रभावी होने और प्रेरणा देने की क्षमता खो देने का कारण बनता है। 1929 में कांग्रेस के नेता तेजराम ने मध्यप्रांत की हनुमान व्यायामशाला के वार्षिक समारोह में कहा था कि ‘संघ व्यायामशाला से भिन्न है। बल्कि यह मानसिक और नैतिक शक्ति का प्रतिबिंब है।’
आजादी से पूर्व बुद्धिजीवी संघ को निकट से आकर देखकर अपनी राय बनाते थे। इसलिए उनकी आलोचनाओं में भी रचनात्मकता और वजन होता था। 1934 में मध्यप्रांत की विधान परिषद में संघ पर लगे प्रतिबंध पर हुई बहस में मुसलिम नेता एमएस रहमान द्वारा संघ की प्रशंसा करने में न तो स्वार्थपूर्ति, न ही किसी विवशता का परिणाम था। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, द्वारका प्रसाद मिश्र, जमुनालाल बजाज, सुभाष बोस, जय प्रकाश नारायण आदि सब ने संघ की झंकार देखने में अपने व्यक्तित्व या दर्शन का अवमूल्यन नहीं माना। समकालीन बुद्धिजीवियों और राजनेता इस स्वस्थ परंपरा से पूरी तरह कटे हुए हैं।
संघ के शताब्दी वर्ष के संदर्भ में 1940 की घटना उल्लेखनीय है। हेडगेवार का निधन 21 जून, 1940 को हुआ। किसी बड़े आंदोलन के जन्मदाता पर सबसे अधिक लिखा जाता है, पर हेडगेवार पर सबसे कम लिखा और बोला गया। किसी भी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि सभाओं का दौर अपेक्षित होता है। पर बंगाल, महाराष्ट्र और मध्यप्रांत के बुद्धिजीवियों ने इसे बौद्धिक संवाद का अवसर बना दिया। अखबारों में उनके वैचारिक पक्ष पर संपादकीय और लेखों का सिलसिला महीनों तक चलता रहा। उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले सामाचार पत्रों ‘केसरी’, ‘मराठा’, ‘महाराष्ट्र’, ‘काल’, ‘माडर्न रिव्यू’ के साथ-साथ वैचारिक विरोध रखने वाले ‘मातृभूमि’, ‘नवाकाल’ आदि में वैचारिक प्रश्नों पर गंभीर विमर्श हुआ।
2025 में क्या हम गंभीर विमर्श के लिए तत्पर हैं जो आरोप-प्रत्यारोप और पूर्वाग्रह की व्याधियों से मुक्त हो? अन्यथा ‘प्रेम’ और ‘द्वेष’ की आड़ में अनपेक्षित ताकतें और अनियंत्रित बहसें चलती रहेंगी।