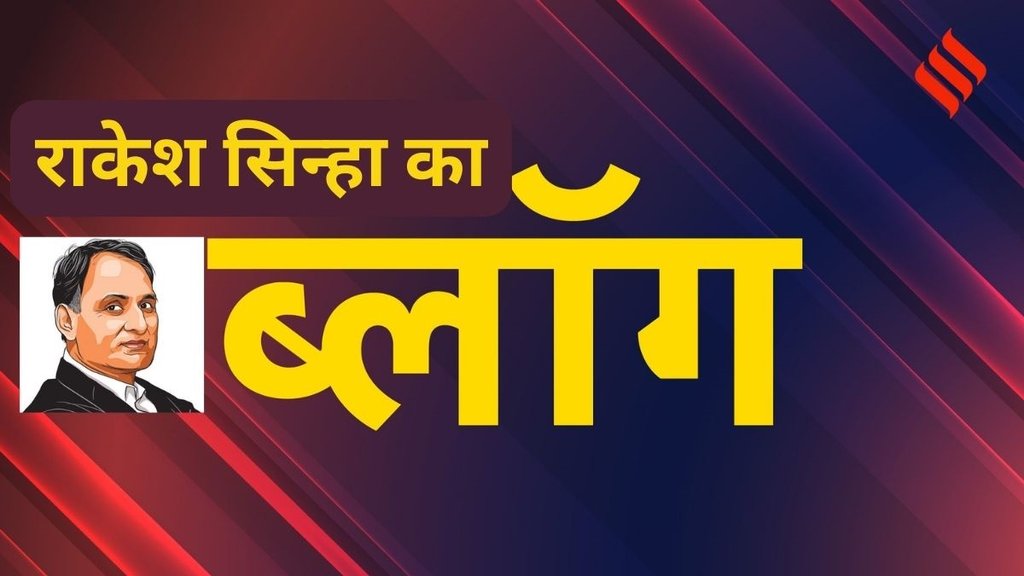महापुरुषों की जयंतियां अवसर की तरह होती हैं। उनके जीवन के संघर्ष और संदेश दोनों को याद करना हमारे मन-मस्तिष्क की खुराक बन सकती है। पर जब हम स्वेच्छा से ही मरीज बनकर रहना चाहते हैं, तब न दवा की चिंता होती है, न ही उसकी जरूरत। समकालीन समाज की यही त्रासदी है। इसे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के बहाने समझ सकते हैं। कुछ परिष्कार का भी प्रयास कर सकते हैं। हमारी कर्मशीलता में सच का अंश और साहस कितना है, इसे हम उनके व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के आईने में चाहें तो देख सकते हैं। दिनकर की लेखनी भूत व वर्तमान के प्रसंगों द्वारा भविष्य की बुनियाद तैयार करती है।
दिनकर के संपूर्ण साहित्य का सार ‘प्राकृतिक न्याय’ के लिए संघर्ष और संकल्प है
ऐसे व्यक्तित्व के धनी वे सभी होते हैं जो इस बात की चिंता करते हैं कि हम क्या विरासत छोड़ जाएंगे! दुनिया में ऐसी चेतना के लेखक और राजनेता रहे हैं। 1930 में अर्थशास्त्री किंस ने भविष्य को सामने रखकर एक लेख लिखा था ‘इकोनोमिक पासिबिलिटिज फार आवर ग्रैंड चिल्ड्रेन’, मार्टिन लूथर किंग (जूनियर) का 1963 का लिंकन मेमोरियल भाषण ‘आई हैव ए ड्रीम’ और 1931 में कृष्णचंद्र भट्टाचार्य का आशुतोष मेमोरियल भाषण ‘विचारों में स्वराज’ इसके कुछ ज्वलंत उदाहरण हैं। दिनकर कवि और राजनेता दोनों थे। उन्होंने समकालीन राजनीतिक प्रक्रिया से मुंह नहीं मोड़ा। माखनलाल चतुर्वेदी और फणीश्वरनाथ रेणु, अफ्रीकी उपन्यासकार न्गुगी वा थ्योंगो, अल्जीरिया के फ्रैंज फैनन और रूस के गोर्की इसी श्रेणी में आते हैं। दिनकर के संपूर्ण साहित्य का सार ‘प्राकृतिक न्याय’ के लिए संघर्ष और संकल्प है।
साधारणतया खलनायकों को मुख्य पात्र बनाकर साहित्य सृजन या फिल्मों का निर्माण नहीं होता है। पर दिनकर अपवाद हैं। कर्ण को लेकर उन्होंने संकीर्णता, भेदभाव और अन्याय के विरुद्ध आवाज बनने का प्रभावी संदेश दिया है। राजनीति से उनका संबंध संसद सदस्य होने की वजह से था। पर न कभी लेखनी कमजोर हुई, न जुबान लड़खड़ाई। एक साहित्यकार या समाजशास्त्री जब समाज की चिंता करता है, तब उसके जीवन में अनेक अदृश्य अड़चनें आती हैं, जिनका वह शिव की तरह विषपान करता है। उसका अनुपात जितना होता है, उसके शब्दों की ताकत उतनी ही अधिक होती है। सत्तर के दशक में अभिव्यक्ति की आजादी और संस्थाओं का सूचकांक गिर रहा था।
रेणु ने ‘सिंहासन खाली करो कि जनता आती है’ का पाठ जेपी की सभा में की
लोगों की निगाह जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व की ओर थी। दिनकर और रेणु दोनों उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में लगे थे। दिनकर ने जेपी को अपनी आयु देने की प्रार्थना करते हुए कहा था, ‘देश को आपकी जरूरत है’। व्यवस्था विरोधी आंदोलन जब 1974 में शुरू हुआ, तब दिनकर दुनिया में नहीं थे, पर वे संघर्ष के दौर में कभी अनुपस्थित नहीं रहे। रेणु ने उनकी कविता ‘सिंहासन खाली करो कि जनता आती है’ का पाठ जेपी की सभा में कर हर नौजवान को दिनकर बना दिया। इस तरह की निडर प्रतिभाएं ही बौद्धिक विमर्श का नेतृत्व करती हैं। उनका नाम मूल्य और विचार का पर्याय बन जाता है।
समकालीन भारत में या पूरी दुनिया में विमर्श पर ग्रहण लगा हुआ है। ऊल-जलूल बोलने वाले सामाजिक-राजनीतिक बहस को जन्म देते हैं। सबसे आश्चर्य की बात है कि वे लज्जित भी नहीं होते हैं। यही गिरावट की सबसे प्रामाणिक सूचना है। समाज उनकी भाषा और भाव-भंगिमा को सहन करती है, यह चेतना शून्यता का संकेत है। गलती न समाज की है, न ही ऊटपटांग बोलने वाले लोगों की। जब बौद्धिक नेतृत्व कमजोर हो जाता है, तब ऐसी ही परिस्थितियों से समाज को गुजरना पड़ता है।
बौद्धिकता कलम या जुबान की जादूगरी नहीं है। यह त्याग, निडरता, चेतनामूलक जीवन को प्रसारित करती है। दिनकर की कविता ‘कलम, आज उनकी जय बोल’ उनके सामने नतमस्तक होने की बात करती है, जो दधीचि की तरह अपने समाज के लिए अपने जीवन का होम कर देते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने 1921-22 (असहयोग आंदोलन) में विलासपुर की जेल से ‘पुष्प की अभिलाषा’ लिखकर ऐसा ही संदेश दिया था। रेणु ने जेपी पर हमले पर रोष जाहिर कर चार नवंबर 1974 को ‘पद्मश्री’ को ‘पापश्री’ कहकर लौटा दिया था। दिनकर, चतुर्वेदी, रेणु की मन की स्वायत्तता उन सबकी विलक्षणता थी। यही उन्हें कालजयी बना देती है। उन सब लोगों ने आलोचनात्मक दृष्टि को कभी मुरझाने नहीं दिया।
दुनिया के सभी भागों में इसका समांतर मिलता है। न्गुगी की अंग्रेजी में अंतिम रचना ‘पेटल्स आफ ब्लड’ थी। उन्होंने साम्राज्यवाद को एक आधिपत्य ही नहीं, मानसिक दासता मानकर अफ्रीकी समाज को नई रोशनी दिखाई। वे 1977 से अपनी भाषा गिकुयी में लिखने लगे और अपनी पुस्तक ‘डिक्लोनाइजिंग द माइंड’ द्वारा उपनिवेशवाद से पीड़ित दुनिया के लोगों को राह दिखाई। वैसे ही श्वेतों के जुल्म को फ्रैंज फेनो ने ‘रेचेड आफ द अर्थ’ और ‘ब्लैक स्किन, वाइट मास्क्स’ में सधे शब्दों में रखा है। मानवीय सम्मान और सामाजिक आर्थिक समानता की पक्षधरता ऐसे सभी कालजयी लेखकों की बुनियादी सोच का हिस्सा होती है।
समर्पण सदैव अनाथ होता है। उसका परिणाम जरूर उनकी जय-जयकार करने वालों की जमात पैदा करता है। कुछ उनकी राह के राही बनते हैं, शेष नया कर्मकांड बनाकर चलते हैं। दिनकर एक साधक की तरह समाज साधना करते रहे। वे कभी शहरी या महानगरीय नहीं बने। ऐसे बौद्धिक अपने-अपने स्थान पर अपनी भाषा में संदेश देते हैं। सबका आशय नवमानव का निर्माण होता है। वैश्विकता उन सबकी पात्रता को पीढ़ियों के लिए उपयोगी बना देती है।
अपनी ख्याति और व्यस्तता के बावजूद दिनकर ने अपने जन्म स्थान सिमरिया (बेगूसराय) को नहीं छोड़ा। इसलिए समाज की मानसिकता को पढ़ना उनके लिए आसान था। जब उन्होंने दिल्ली को ‘रेशमी नगर’ कहकर संबोधित किया तो उसका आशय आम और खास के बीच बढ़ती दूरी थी। दिनकर ने विषमता, भेदभाव, आधिपत्यवाद, आर्थिक बेचैनी जैसे प्रश्नों को संबोधित किया जो किसी एक काल या भूगोल की समस्या नहीं होकर सार्वकालिक और वैश्विक है।
जब इस प्रकार के नेतृत्व के लिए समाज का बुद्धिजीवी संकल्पित होता है तो ऊल-जलूलवादी विमर्श का स्वत: पतन हो जाता है। दिनकर की रचनाएं चेतना के स्वर और विवेकवाद, दोनों की बुनियाद को मजबूत करती है। ऐसा करने में न दिनकर, न ही फ्रैंज फेनन तटस्थ थे। दिनकर के ये शब्द खूब उद्धृत होते हैं- ‘जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध।’