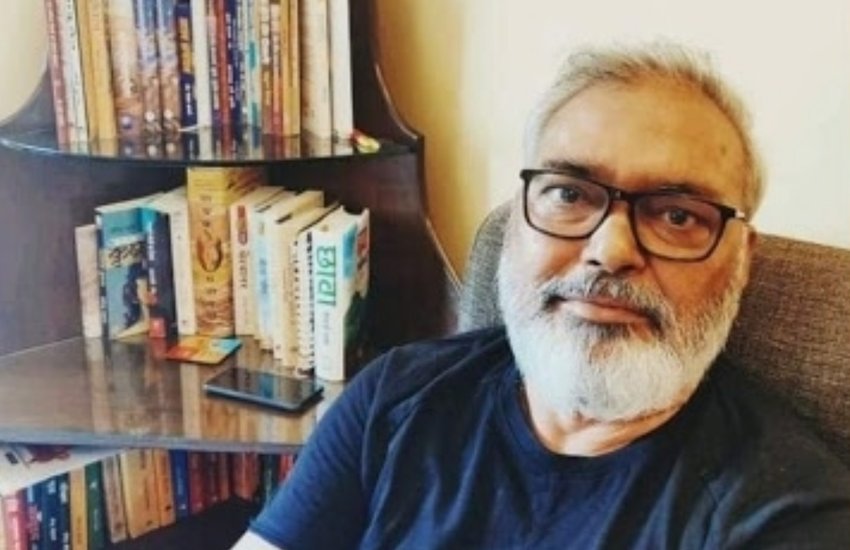किसी शहर का ‘शहर’ होना ही बड़ी बात होती है, लेकिन अगर शहर वाकई ‘बड़ा’ हो, तो यह उसकी संपन्नता का सूचक माना जाता है। यहां महत्व भौगोलिक आकार का नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक मजबूती का है। दरअसल, शहर बड़ा इसलिए होता है, क्योंकि उसमें समाज के हर तबके के लोगों के बेहतर जीवन-यापन, संयमित आचार-व्यवहार, मजबूत सांस्कृतिक आजादी आदि की पर्याप्त गुंजाइश होती है। दुनिया के विशाल देशों में शुमार भारत में भी दिल्ली, मुंबई, कोलकता, चेन्नई, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे कई बड़े शहर हैं। इनमें से कुछ शहर तो पिछले कुछ वर्षों में ही विकास की सीढ़ियां छलांग कर ‘बड़े’ हुए हैं। लेकिन, कई राज्यों की राजधानी, जिन्हें शहर का दर्जा हासिल है, को देखने से वह जिला मुख्यालय जैसे भी नहीं लगते हैं। यह बात बिहार की राजधानी पटना पर पूरी तरह चरितार्थ नही होती है। पटना आने के बाद किसी के मन में यह गुमान नहीं होता कि वाकई यह किसी गरीब राज्य की राजधानी है । सुंदर सपाट सड़कें , बड़ी बड़ी मल्टीस्टोरी बिल्डिंग, लंबी लंबी कारें – कहां से है गरीब बिहार।
दरअसल, अन्य राज्यों के शहर इसलिए विकसित हुए, क्योंकि वहां विकास की ललक देखी गई। उन राज्यों में जिस किसी भी पार्टी की सरकार बनी, उसका मकसद राज्य का विकास करना रहा। उन राज्यों की सरकार विकास को लेकर सदैव जागरूक रही। ऐसे में वहां के शहर भी विकसित होते गए। वहां की सरकारों को अपने राज्य, वहां की जनता से प्रेम है, एक अपनापन है, इसलिए उनका सदैव प्रयास यही रहा कि उनके राज्य की सड़कें अच्छी हों, बिजली की कमी न रहें, अपराध न हो और विश्व के सभी उद्योगपति उनके राज्य में उद्यम लगाकर युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी को दूर करें। लेकिन, इस तरह के प्रयास बिहार के किसी सरकार ने किया हो, इसका कोई इतिहास नहीं मिलता। संभवत: इसीलिए बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य गिना जाता है। तभी तो जदयू सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने संसद में पूछा था कि नीति आयोग की 2020-21 की रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बताया गया है। अगर यह सही है तो बिहार के पिछड़ेपन की वजह क्या है? उन्होंने यह भी पूछा था कि बिहार का पिछड़ापन दूर करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से हो रही है, उस पर केंद्र कब विचार करेगा? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में ललन सिंह के सवाल पर दिए अपने लिखित जवाब में बताया कि आखिर बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है।
नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कई पैमानों पर बिहार देश में सबसे पिछड़ा राज्य साबित हुआ है। सरकार ने कहा कि नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्यों की भारत सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 के मुताबिक बिहार का समग्र स्कोर सभी राज्यों में सबसे कम है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार को 100 में से महज 52 नंबर मिले हैं, जो देश के सभी राज्यों से कम है। बिहार के कम स्कोर के लिए गरीबी, 15 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए खराब शिक्षा, मोबाइल और इंटरनेट का कम इस्तेमाल भी मानक था। बिहार में 33.74% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। अगर वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करें तो यह 52.5 प्रतिशत हो जाता है। राज्य में केवल 12.3 % परिवार के लोग हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में हैं। पांच वर्ष के कम उम्र के 42 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं। 15 वर्ष से ऊपर के लोगों की साक्षरता 64.7 फीसदी है। बिहार में सबसे कम मोबाइल का इस्तेमाल होता है। 100 लोगों में महज 50.65 लोग ही मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी केवल 39.99% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। बिहार के पिछड़ेपन को लेकर कई अनुसंधानकर्ताओं ने कई सुझाव दिए हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि सरकार को कृषि पर जोर देना होगा, शहरीकरण को तेज करने की चुनौती स्वीकार करनी होगी, आधारभूत सुविधाओं का विकास करना होगा, राजस्व का आधार बढ़ाना होगा, मानव संसाधन पर ध्यान, शासन में सुधार, सिविल सोसायटी की महत्वपूर्ण भूमिका तय करनी होगी तथा बेहतर शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण करना होगा।
जहां तक बात विशेष राज्य का दर्जा देने की है, तो अपने पिछले कार्यकाल में मुखमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष दर्जा देने को लेकर मुद्दा बनाया था, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के संबंध में भी केंद्र ने ठोस जवाब दिया है। केंद्र ने कहा है कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार अब विशेष राज्य और सामान्य राज्य को मिलने वाले टैक्स शेयर के बंटवारे में कोई फर्क नहीं रह गया है। लिहाजा, बिहार को केंद्र के राजस्व में अब 32 के बजाय 42 फीसद हिस्सा मिल रहा है। योजनाओं को लागू करने के लिए यह ज्यादा माकूल समय है। वित्त आयोग की सिफारिश के बाद सामान्य कैटेगरी और विशेष कैटेगरी के राज्य में कोई अंतर नहीं रह गया है।
वास्तविकता से कोसों दूर जहां तक मैंने समझा, बिहार के वाह्याडंबरों की तो अच्छी मार्केटिंग हो रही है, लेकिन राज्य के अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर इसकी पुष्टि की जा सकती है कि सच क्या है? सहरसा जिले के बघवा पंचायत को ही देखिए। बाढ़ पीड़ित इस इलाके में आपको उफनाती नदी में नाव चलाते सात से पंद्रह साल की उम्र के लड़के—लड़कियां दिख जाएंगे। मवेशियों को चारा खिलाना है तो जान जोखिम में डालकर नाव चलाना ही पड़ेगा। इसी पंचायत के रघुबीर पासवान की मानें तो यह यहां के लिए आम बात है। और सरकार का हाल यह है कि बगल के जिलों में सरकार ने आर्थिक सहायता राशि तो बांट दी, लेकिन इस बाढ़ पीड़ित इलाके की सुध नहीं ली। यह तो पंचायत की बात है, लेकिन उन लोगों की हालत का भी अंदाजा लगाइए जो बाढ़ प्रभावित होने के कारण अपना घर—बार छोड़कर, जान को दांव पर लगाकर परिवार एवं मवेशियों के साथ हाईवे पर जीवन गुजारने को मजबूर हैं और उन्हें सरकार की ओर से एक दाना तक नसीब नहीं हो रहा है।
यह बिल्कुल ठीक है कि बिहार की सड़कें अब अच्छी बन गई हैं, बिजली निर्बाध रूप से उपलब्ध हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कोढ़ में खाज यह कि अपराध में कोई कमी नहीं आई है। स्थानीय लोगों की मानें तो नरसंहार यहां के लिए कोई विशेष बात नहीं है, यह तो होता ही रहता है। छोटी-मोटी घटना को वह महत्व नहीं देते, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। ऐसे में जीवन गुजारने के लिए यदि अपराध कोई करता है, तो यह उसकी मजबूरी है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह ठीक है कि हमारा देश आजादी से अब तक कम संसाधनों के बावजूद विकसित हुआ है, लेकिन देश के कोने-कोने में यह विकास पहुंचा हो, ऐसा नहीं हुआ।
ऐसे में फिर जदयू सांसद का सवाल मुंह उठा कर सामने आ जाता है, क्योंकि जब अच्छी सड़कें हैं, बिजली कभी जाती नहीं है, तो फिर किस बात की कमी है और सरकार के प्रति इतनी नाराजगी क्यों है? इसका जवाब और भी मार्मिक था। लोगों का कहना है, यह सड़कें शहर में रहने वाले संपन्न लोगों के लिए हैं, जो चमचमाती कारों से गुजरते हैं। बिजली भी उन्हीं के लिए है, जो मकानों में रहते हैं और एसी, फ्रिज जैसे उपकरण चलाते हैं। लेकिन लाखों ऐसे लोग, जिन्होंने बाढ़ की विभीषिका में अपना सब कुछ गंवा दिया हो, उनके लिए सड़कें एवं बिजली का क्या और कितना महत्व हो सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है। इन्हें तो बस पेट भर खाना और शरीर ढकने के लिए वस्त्र, मवेशियों के लिए चारा चाहिए, जो नहीं मिल रहा है।
हालांकि, सरकार इन्हीं तबके के वोट से बनी है, इस कठोर सच से इनकार करना किसी के लिए भी संभव नहीं हो सकता। प्रश्न यह जटिल है कि बाढ़ से विस्थापितों को पुनर्स्थापित कैसे किया जाए? यह यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर किसी आमजन को नहीं मालूम। हो सकता है, सरकार कोई योजना बना रही हो, लेकिन वह कब तक कार्यान्वित होगी, यह भी बड़ा सवाल है। बदहाली और कंगाली का हल तो सरकार को ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि जीवन रक्षा का दायित्व तो उसी का है।