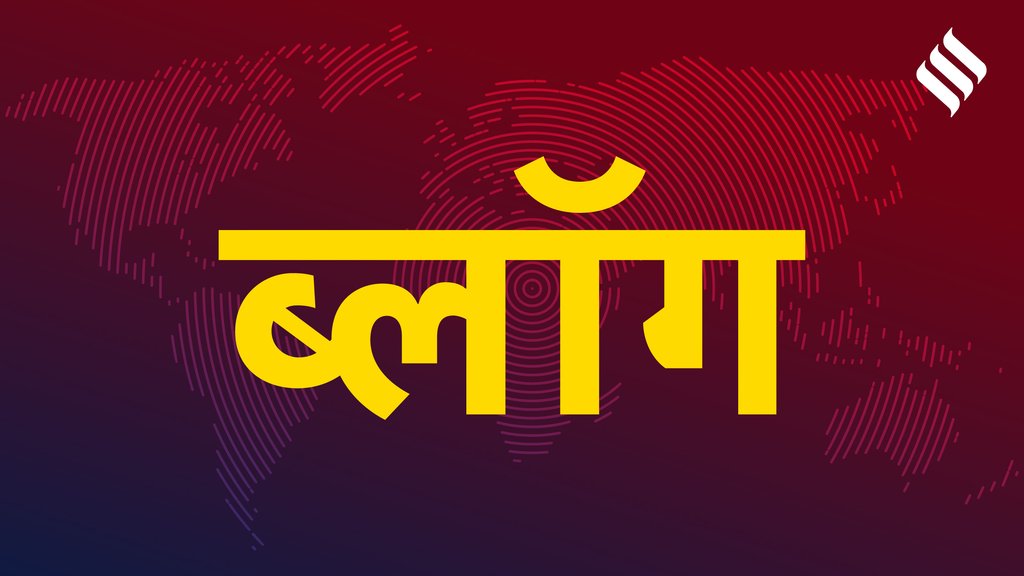देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर गंभीर वायु प्रदूषण का सामना कर रही है। खांसते-हांफते नागरिकों को रस्मी तौर पर राहत देने के लिए सरकार ने कुछ पाबंदियां लागू कर दी हैं। जैसे ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का चौथे चरण वाला प्रतिबंध पिछले दिनों लगाया गया। नर्सरी से बाहरवीं तक के लिए स्कूल बंद कर उनकी आनलाइन कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए गए। केंद्र, दिल्ली सरकार और नगर निगम के दफ्तरों के समय में थोड़ी तब्दीली की गई, ताकि कर्मचारियों के आवागमन के कारण सड़क पर यातायात और उससे होने वाले प्रदूषण में कुछ कमी आ सके। मगर हमारे देश का हर नागरिक भलीभांति परिचित है कि इन सारी पाबंदियों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ये सारी पाबंदियां और सरकारों के दृढ़ निश्चय अंदर से खोखले हैं। मौसम बदलने के साथ प्रदूषण में नरमी आते ही ये सारी प्रतिज्ञाएं और प्रतिबंध हवा हो जाते हैं। जनता एक बार फिर प्रदूषण के सामने असहाय छोड़ दी जाती है।
सोशल मीडिया पर लोगों ने चिंता जताई कि आखिर यमुना कब साफ होगी
हाल में, छठ पर्व के दौरान हर साल की तरह झाग में लिपटी हुई यमुना नदी की तस्वीरें छाई रहीं। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने तस्वीरें देख कर चिंता जताई कि आखिर यमुना कब साफ होगी। कब उसका जल आचमन लायक होगा। उधर, छठ से पहले ही अदालत ने चेता दिया था कि यमुना की हालत ऐसी नहीं है कि उसमें उतर कर पूजा की जाए या उसमें डुबकी लगाई जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसका उदाहरण भी दिया कि एक व्यक्ति ने हाल में यमुना में डुबकी लगाई थी और उन्हें दो दिन अस्पताल के सघन चिकित्सा कक्ष में बिताने पड़े।
सवाल है कि प्रदूषण की मार झेलती जनता का दुख-दर्द देख कर सरकारें, अदालतें और तमाम संगठन प्रयास करते दिख रहे हैं, लेकिन बात चाहे पानी की हो, हवा की हो या जमीन की। उनसे जुड़ा प्रदूषण घटने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। यमुना की सफाई में बीते दशकों में करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। दिल्ली की हवा को दुरुस्त करने के लिए प्रतिबंध लगाने के अलावा स्माग टावरों की स्थापना हो चुकी है। पड़ोसी राज्यों में पराली (खेती के अवशेष) जलाने पर रोक के फरमान कई बार जारी हो चुके हैं। मगर कोई उपाय कारगर नहीं हो रहा है।
प्रदूषण रोकने को लेकर कोई भी राजनीतिक दल चिंतित नहीं दिखता है
असल में, इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहली मुख्य वजह यह है कि पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा हमारी राजनीतिक चिंतन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है या यह मसला राजनीतिक क्षितिज से पूरी तरह गायब ही है। जाति, धर्म और कथित विकास के नाम पर राजनीति करने वाले दल पर्यावरण की सार-संभाल और प्रदूषण की रोकथाम के मुद्दों की न तो कोई चर्चा करते हैं और न ही इनसे जुड़े वादों को अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल करते हैं। चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव।
राष्ट्रीय दलों की ओर शायद ही कोई ऐसा आश्वासन या वादा सामने आया हो, जिसमें प्रदूषण खत्म करने और नागरिकों को साफ हवा-पानी देने की बात कही गई हो। दिल्ली जैसी जगहों पर चार चरणों में पाबंदियां लगाने और छूट देने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन विभिन्न चरणों में होने वाले चुनावों के दौरान राजनीतिक दल प्रदूषण से राहत दिलाने की कोई घोषणा नहीं करते हैं, जिसकी आज ज्यादा जरूरत है। कोई नेता या उसका दल यह एलान करते दिखाई नहीं देता कि अगर वे सत्ता में आए तो जल संकट, प्रदूषण और कचरे की बढ़ती समस्या से कैसे निजात दिलाएंगे। साफ हवा-पानी का बंदोबस्त कैसे करेंगे।
लोकसभा चुनावों के दौरान पश्चिम बंगाल के कुछ दलों ने पर्यावरण संतुलन कायम करने की मांग को संविधान के छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की थी। इसके पीछे पर्यटक स्थल दार्जिलिंग की बिगड़ती आबोहवा थी। एक रपट में दावा किया गया है कि दार्जिलिंग और नजदीकी जगहों पर पर्यटकों की बढ़ती भीड़ ने प्रदूषण को खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया है, जिससे स्थानीय लोग परेशानी महसूस करने लगे हैं। पर्यटकों की जरूरतों के अनुरूप रिहाइश के लिए होटलों और आवागमन के लिए सड़कों के निर्माण ने इलाके की हरियाली और जंगलों को लील लिया है। स्थानीय लोग पेड़ों के लगातार सफाए के असर को महसूस कर रहे हैं। वे बढ़ती गर्मी और आबोहवा में खतरनाक परिवर्तनों का निरंतर अहसास कर रहे हैं। यही कारण है कि पर्यावरण सुधार की जनता की इस मांग ने वहां एक राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया।
राजनीतिक पटल पर पर्यावरण की आवाज को मुखर करने के पीछे लद्दाख क्षेत्र में प्रख्यात पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का आंदोलन भी है। उन्होंने बिगड़ते पर्यावरण का हवाला देकर लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग के साथ इसी साल 21 दिन तक भूख हड़ताल की थी। उनका मत है कि वे छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की मांग कर इस इलाके के पर्यावरण को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। उसके अनुसार छठी अनुसूची स्थानीय संस्कृति को बचाने के लिए रक्षा कवच का काम करती है।
लद्दाख और दार्जिलिंग से पर्यावरण सुधार और संरक्षण की राजनीतिक मांग उठना राजनीतिक क्षेत्र में एक सार्थक बदलाव का संकेत देता है, लेकिन अफसोस है कि ऐसी पहलकदमियां बहुत सीमित हैं। बंगलुरु भीषण जल संकट से जूझ रहा है, लेकिन कोई राजनीतिक दल इस संकट से उबरने का मुद्दा अपने घोषणापत्र में शामिल करने का जोखिम नहीं ले सका है। महाराष्ट्र और बुंदेलखंड के कई इलाके भयानक सूखे की मार झेलते हैं, लेकिन किसी दल या नेता में यह साहस नहीं दिखा है कि उन्होंने अपने चुनावी वादों में कभी इसका कोई उल्लेख किया हो। झारखंड विधानसभा के चुनाव के दौरान वहां अवैध खनन और वनों की कटाई से लेकर झरिया, धनबाद और रांची के प्रदूषण का जिक्र भूले से भी किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया।
सवाल है कि क्या पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का कोई राजनीतिक महत्त्व नहीं होता। क्या इन विषयों और मुद्दों की वैसी अहमियत नहीं है जो असल में नागरिकों की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव ला सकें। इससे स्पष्ट है कि हमारे देश में पर्यावरण की चुनौतियों और इनसे संबंधित माहौल को राजनीतिक विमर्श का विषय नहीं माना जाता है। यह जरूर है कि सत्तारूढ़ दल वैज्ञानिक उपलब्धियों को अपने चुनावी अभियानों का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन वे न तो भावी वैज्ञानिक कार्यक्रमों या पर्यावरण सुधार की योजनाओं का ठोस खाका अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल करते हैं और न ही कोई उनसे इन कार्यों से जुड़ी लागत और पर्यावरणीय प्रभावों की जानकारी मांगता है।
हालांकि यहां एक समस्या पर्यावरण संबंधी जागरूकता की कमी का भी है। जाति और धर्म के नाम पर वोट डालने वाली जनता में अभी यह समझ बनना शेष है कि उनका जीवन स्तर राष्ट्र और समाज के चौतरफा उन्नयन से सुधर सकता है। इससे लगता है कि विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण का सारा लेना-देना सिर्फ शोध संस्थाओं, संबंधित मंत्रालयों और विश्वविद्यालयों से है न कि देश के विकास का दम भरने वाली राजनीति से। इसलिए यदि भारत को विकसित राष्ट्र की पांत में शामिल होना है, तो राजनेताओं से विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण से जुड़े मसलों पर सवाल करना जरूरी है।