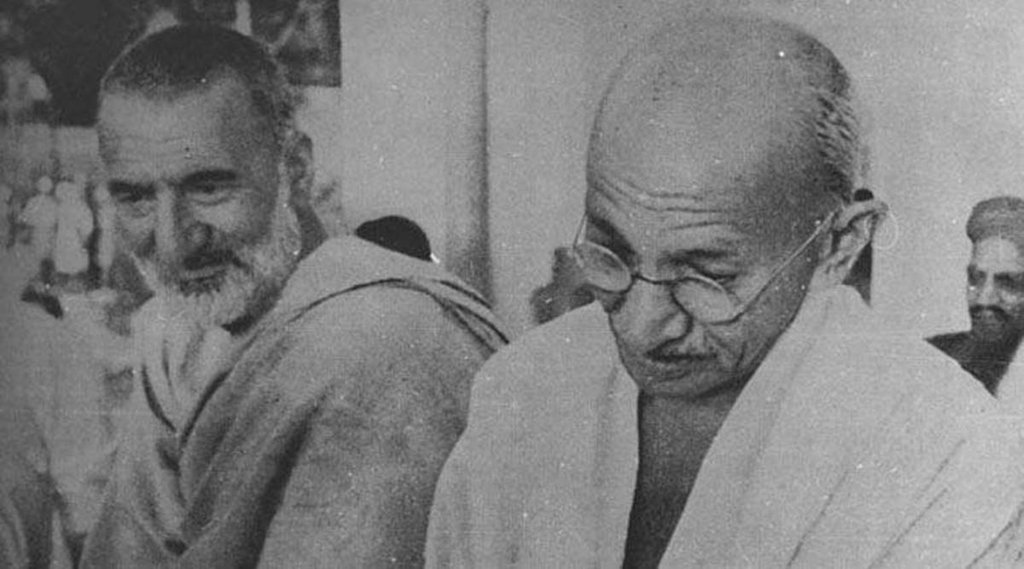नवनीत शर्मा
गांधी हर दौर में उन संदर्भों के लिए याद किए जाएंगे, जिनके लिए वे मर-मिटे। हालांकि उन्हें बतौर ‘आदर्श’ याद किया जाए, ऐसा गांधी नहीं चाहते थे, क्योंकि वे स्वयं को आदर्श स्वरूप नहीं देखते थे। लेकिन वे खुद को एक मुक्कमल इंसान बनने की कवायद में जरूर देखते थे। उन्होंने जिस धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना गढ़ी, वह ‘धर्म’ के विरुद्ध न होकर ‘सर्व धर्म समभाव’ होने की थी।
नोआखली के प्रकरण में जब एक क्षुब्ध हिंदू ने अपने आक्रोश को जाहिर किया कि उसके एकमात्र लड़के को मुसलमानों ने मार डाला, तब गांधी कहते हैं कि अब उसे अपने ही लड़के के हमउम्र मुसलमान बच्चे को ढूंढ़ना चाहिए और उसका लालन-पालन अपने धर्मानुसार न कर, उसके मां-बाप के धर्मानुसार करना चाहिए। उनकी मशहूर उक्ति ‘आंख के बदले आंख एक दिन पूरी दुनिया को अंधा बना देगी’, धर्मनिरपेक्षता और धर्मांधता के भेद का सबसे बेहतरीन अंतर बताती है।
आज आधुनिक समाज में अधिसंख्य लोग उदारवादी मान्यता के चलते कहीं परदा और कहीं पगड़ी का विरोध करते हैं। जबकि गांधी उसके पहनने वालों और उनमें आस्था रखने वालों के अधिकार के हिमायती थे। वे इस अधिकार के संरक्षण को ही लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता मानते थे। वे शाकाहारी थे, पर जब बादशाह खान के बच्चे उनसे मिलते थे तो वे उनके लिए सामिष व्यंजनों का प्रबंध भी करवाते थे।
इसलिए गांधी की जरूरत आज के भारतीय समाज को अधिक है, क्योंकि वे जिस जात-पात के विरुद्ध थे, वह आज भी सैकड़ों महिलाओं के सिर पर मैला उठवा रही है। दलित बच्चे स्कूल में अभी भी कहीं कक्षा के हाशिये पर दिख जाते हैं। रोजाना धर्म और जाति के नाम पर हिंसा की जाती है।
तीस जनवरी को रस्मी तौर पर राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करके, बकौल हरिवंशराय बच्चन, हम उनके फकीरी ठाट को ठेंगा दिखाते हुए आगे बढ़ चलते हैं। सीखना और गांधी से सीखना जटिल काम है। आनलाइन सीखना और गांधी की नई तालीम शायद ही कभी सुमेलित हो। नई तालीम का तालिब, कंप्यूटर और डाटा के चक्रव्यूह में आत्महत्या नहीं करेगा।
नई तालीम सबको डाटा भले ही न उपलब्ध करवा पाती, पर आटा सबके लिए पर्याप्त होता। गांधी की मनुष्य और मनुजता में आस्था को हम अब मानो जंजीर से गिलास को प्याऊ के साथ जकड़ कर सुरक्षित रखना चाहते हैं। एक ही जैसे नागरिक, एक ही जैसा ज्ञान और एक ही सत्य हमें सुरक्षा का भान देते हैं। भिन्नता, बहुलता हमें आतंकित न भी करे तो हमारी आस्था को ठेस पहुंचाती है और ठेस पहुंचाने वाले को जेल।
गांधी भिन्नता को उत्सवकारी मानते थे और एकरूपता को सौंदर्यहीन। लेकिन ऐसा लगता है कि भिन्नता या अनेकता में एकता के गांधीवादी नारे को अब एक ही मत की एकता ने विस्थापित कर दिया है। गांधी के तीनों बंदर एक ही सत्य सुनें, बोलें और देखें, ऐसा अपेक्षित आदर्श भारतीय नागरिक बनाने में हम जुटे हैं। गांधी इसे ही सहजता से मानते तो शायद चौरी-चौरा से विचलित होकर आंदोलन वापस न लेते। गांधी ने एक ही ‘तानाशाह’ की बात को सुनने का मंत्र दिया था और वह ‘तानाशाह’ कोई मंत्री या हाकिम न होकर ‘अंतरात्मा की आवाज’ का होना था।
इसी अंतरात्मा की खोज अब हम आनलाइन करने में जुटे हैं। गांधी ने कहा था कि ‘जब संदेह में घिरने लगे, अहम हावी होने लगे तो जो सबसे गरीब व्यक्ति देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और विचार करो…!’ पर विचारने का काम तो हमने अब ‘गूगल’ की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुपुर्द कर दिया है। तीनों बंदरों की तरह हमने ‘बुरा’ की पहचान करने की जिम्मेवारी इंटरनेट के विवेक पर छोड़ दिया है और सब कुछ ग्रहण करते जा रहे हैं। देखने, सुनने और बोलने के किसी भी भिन्न प्रयास को ‘राष्ट्र-विरोधी’ करार दिया जा सकता है।
शायद गांधी ने यह नहीं सोचा होगा कि बंदरों में पाए जाने वाले ‘संज्ञानात्मक लचीलेपन’ को परे धकेल कर हम ‘अच्छे-बुरे’ की सुनिश्चित श्रेणियां बना लेंगे और उन्हीं खांचों में दुनिया को ढालने का प्रयास करेंगे। इस ‘अच्छे-बुरे’ के लचीलेपन और सार्वभौमिकता के कारण ही गांधी ने कहा- ‘पाप से घृणा करो, पापी से नहीं’।
गांधी के ‘करो या मरो’ के नारे को हमने सोशल मीडिया के मंच तक सीमित कर दिया है। सभी आक्रोश, सारी क्रांति और सारा सर्वोदय अब ‘डाउनलोड’ की रफ्तार का मोहताज है। सिकुड़ता और ठिठुरता हुआ गणतंत्र ‘माउस क्लिक’ में है। इसलिए यह विद्रूप इस मजाहिया अंदाज में कहा जाता है कि अगर चौथा बंदर होता तो वह न देखता, न सुनता, न बोलता, बस हाथ में फोन लिए फेसबुक या व्हाट्सऐप में लीन रहता।
गांधी जिस विनोदी भाव में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि वे बादशाह से मिलने लंगोट में ही क्यों चले गए, वह गौरतलब है। उन्होंने कहा कि बादशाह ने दोनों के लिए पर्याप्त कपड़े पहन रखे थे। उनका यह उत्तर उस असमानता, भेदभाव और अन्याय को इंगित करने के लिए था जो आज भी व्याप्त है और अधिक गहराया भी है।
इसी असमानता, भेदभाव और अन्याय की अवधारणाओं के चलते लोग हिंसा पर उतारू होते हैं। गांधीवाद और गांधीगीरी की हार मनुजता की हार है। उम्मीद की हार है और अजन्मे शांतिपूर्ण, समतामूलक, न्यायप्रिय समाज की हार है। तीस जनवरी शायद हमें बंदर से इंसान बनने को भले ही न प्रेरित करे, पर इस विकास क्रम को हम उलटने न दें, इसके बारे में जरूर चेताती है।