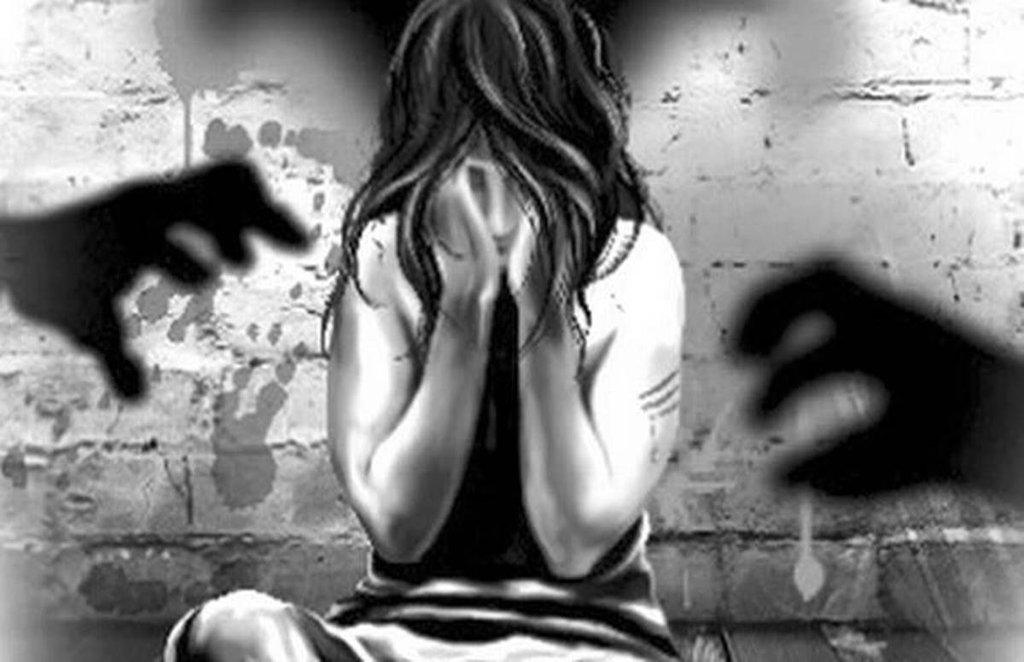हाल में एक अनचाही खबर कुछ समय के लिए सुर्खियों में थी- ‘चौथी बार बिटिया के जन्म पर पिता ने आत्महत्या की!’ बरबस मैं बचपन की स्मृतियों में चली गई और प्रचार का एक गीत कौंध गया, जिसका स्वरूप आज भी मेरे जेहन में जस का तस है- ‘नन्ही मेरी बिटिया होगी, लाडली मेरी रानी, रात भर जगाएगी वो, मैं सुनाऊंगी कहानी!’
जब बहुत छोटी थी, तब दूरदर्शन पर एक प्रचार का यह एक अंश था, जिसमें एक गर्भवती महिला अपने भावी बच्चे के लिए सपने बुनती है और लोरी गाती है। फिर कुछ होता है और उभरा पेट सपाट हो जाता है। पृष्ठभूमि में गीत चलता है, पर अबकी बोल थोड़े बदले होते हैं- ‘नन्ही मेरी बिटिया होती, लाडली मेरी रानी, रात भर जगाती मुझको, मैं सुनाती…’ और इसके बाद एक लंबा उच्छ्वास और फिर एक शब्द ‘कहानी!’
कहते हैं, जो बातें बचपन में मन में घर कर जाएं, वे आसानी से नहीं निकलतीं और ताउम्र उसका असर हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व पर दिखाई देता है। अमूमन ऐसी बातें नकारात्मक ही होती हैं, सो मन से निकाल देना ही हितकर होता है। पर बढ़ती उम्र के साथ अगर वही या वैसी ही बातें या घटनाएं दोहराई जाती रहें तो उस गिरह को भला कोई कैसे खोले? गांठ और भी कसती चली जाती है, जब नए कलेवर के साथ वे बातें प्रत्यक्ष होती हैं। एक ऐसा ही प्रभाव इस प्रचार ने मुझ पर छोड़ा था।
तब अबोध थी तो गीत आकर्षक लगता था। इसे जैसे प्रस्तुत किया गया था, वह भी अपनी ओर खींचता था। पर न गाने में बदलाव का अर्थ पता था और न ही यह कि बीच में कुछ क्या होता है, जिसके बाद गर्भवती स्त्री उदास हो जाती है। मां से पूछती तो मां क्या ही जवाब देती! अभी तो उनकी चिरैया ही इतनी नन्ही थी कि छांव से बाहर जाने नहीं देतीं। फिर इतने बड़े झंझावात का सत्य क्या ही बताती भला! थोड़ी और बड़ी हुई तब थोड़ा-थोड़ा समझ आने लगा था।
वह प्रचार अब भी टीवी पर आता था। पर अब सारी बातें समझ आती थीं। पड़ोस में रहने वाली एक महिला को मैं चाची कहती थी। उनका पेट भी फूल कर ऐसे ही पिचक गया था। उनकी पहले से चार बेटियां थीं और एक बेटा। मोहल्ले की बुजुर्ग अम्मा लोग एक दिन चर्चा कर रही थीं- ‘एक आंख को आंख नहीं कहते! आंखें तो दो ही सही और भली!’ वहां पड़ोस की उस चाची की सास भी थीं। फिर कुछ महीनों बाद वही दृश्य दिखा।
मैं समझ गई थी कि बेटे आंख होते हैं और बेटियां? बेटियां खर-पतवार! कोई नई फसल नहीं लगानी तब तक पनपने दिया! जब मन किया उखाड़ दिया। कुछ भी हो, खर-पतवार कभी भी गेहूं और धान नहीं बन सकते ना! आज से बीस-बाईस साल पहले और आज के दौर में कन्याभ्रूण हत्या को लेकर क्या परिवर्तन आया है? संख्याएं तो नित-नित बढ़ ही रही हैं। पिता की आत्महत्या ने तो एकदम से बेटियों को और भी दोयम दर्जे का साबित कर दिया।
क्या लड़कियां इतनी ‘अभागी’ होती हैं? या समाज के ढुलमुल रवैये ने उनको जिम्मेदारी की जगह बोझ समझा? दहेज के लिए एक ओर धन जुटाता बाप जितना लाचार होता है, वहीं लड़कियों के सिर पर परिवार के इज्जत का टोकरा रखता समाज अनजाने ही उनको अवांछनीय बना देता है।
यह सच है कि सुखद बदलाव का साक्षी भी समाज बन रहा है। मगर ऐसे उदाहरण अंतरिक्ष के ब्लैक होल में समा जाने वाले किसी क्षुद्र ग्रह की तरह अर्थहीन जैसे लगते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक 2017-2030 के बीच देश में अड़सठ लाख अजन्मी बेटियों को कोख में ही मार दिया जा चुका होगा। हम ऐसी निकृष्ट सोच को भला कैसे स्वीकार लेते हैं।
भारत के ही पड़ोसी देश नेपाल में लिंग परीक्षण वैध है। एक बार वहां की लड़कियों पर भी नजर दौड़ाई जाए। कितनी उन्मुक्त, निडर और बेबाक होती हैं। हम यह सब अपने ही पड़ोसी से क्यों नहीं सीखते? देवी के रूप में हम मातृशक्ति को प्रणाम करते हैं, लेकिन अपने आसपास बहन, बेटी, पत्नी, मां, मित्र, सहकर्मी आदि के रूप में हम उसी स्त्री रूप को सम्मान नहीं दे पाते हैं।
मस्त मलंग लड़कियां जो दुपट्टे की कोर से खेलती हों, बालों की लटों को बेफिक्री से उड़ाती हों, आजाद पंछी की तरह उड़ती हो, भाई जितना पढ़ती हो, भाई जैसा भोजन करती हो, भाई न भी हो तो तानों के बिना हो। ऐसी लड़कियां कितनी हैं? उस पिता ने अपने प्राण ले लिए।
पर मैं उस मां से… उस बेटी से कहना चाहती हूं कि इसमें आपका दोष रत्ती भर भी नहीं है। आप लोगों को समाज के तानों को नजरअंदाज करके एक ऐसे जीवन को गले लगाना है जो समानता और जिजीविषा से भरी हो। और यह प्रण जरूर लेना है कि अपने जीवन में इस असमानता को लाद कर नहीं चलना है। यही प्रण आज हर स्त्री को लेना होगा। तभी इस रोग से मुक्ति है।