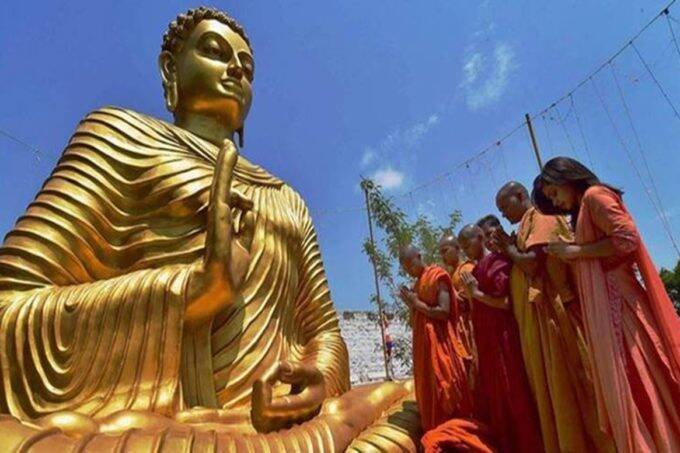महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जिस इंसान का दिमाग आलस्य से परिपूर्ण है, वह अपना हित नहीं समझ सकता तो फिर वह दूसरों का हित कैसे समझेगा। आलस्य ऐसा रोग है जो इंसान के तन-मन-धन का सर्वनाश करता है। आलस्य का शिकार व्यक्ति रोगों की चपेट में आ जाता है। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा नकारात्मकता से घिरा रहता है। आलस्य का शिकार व्यक्ति मेहनत करने से कतराता है। विद्यार्थियों और युवा वर्ग के लिए तो आलस्य एक श्राप की तरह सिद्ध हो सकता है। अगर कोई विद्यार्थी आलस्य नहीं त्यागता है तो वह पढ़ाई में पिछड़ जाता है, परीक्षा में असफल भी हो जाता है। इस कारण वह अपना कॅरियर नहीं बना पाता।
आलसी लोग अपने आलसपन के कारण अपने कामों को टालते हैं या फिर देरी से करते हैं। वे कभी सर्दी के मौसम में ठंड का बहाना बना कर तो कभी गर्मी के मौसम में गर्मी का बहाना बना कर अपना काम टालते रहते हैं। जबकि कुदरत कभी आलस नहीं करती। लेकिन कुदरत की कृति होने के बावजूद कुछ लोग आलस-प्रिय होते हैं। आलस्य के कारण बहुत से दुर्गुण इंसान में आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति खुद के लिए ही नहीं, बल्कि देश और समाज के लिए भी खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अगर हमारे वैज्ञानिकों ने आलस्य किया होता तो आज हमें नई तकनीकी न मिली होती। देशभक्तों ने आलस्य किया होता तो हमें आजादी न मिली होती। आज भी हमारे देश के सैनिक न तो झुलसाने वाली गर्मी की परवाह करते हैं, न कंपकंपाती ठंड की परवाह करते हैं और न ही आंधी-तूफान की परवाह करते हैं।
’राजेश कुमार चौहान, जलंधर, पंजाब</p>
न्याय का कठघरा
कौन कहता है कि आज से पांच दशक पहले लिखी गई पुस्तक वर्तमान से संदर्भित नहीं हो सकती है? जॉर्ज आॅरवेल की लिखी ‘एनिमल फॉर्म’ और ‘1984’ आज भी प्रासंगिक लगती है। राजनीतिक दलों की बड़ी-बड़ी बयानबाजी बस यों ही उपक्रम में सुर्खियां बटोरते हैं, जिनसे राजनीतिक दलों को लाभ मिलता है। लेकिन जहां मानव अधिकार, नागरिक अधिकार, मनुष्यता, सामूहिक जिम्मेदारी और संवेदना का प्रश्न उठता है या जिन प्रश्नों से उनके वोट बैंक के खिसकने का डर रहता है, वहां इन दलों की सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो जाती हैं और लगता है जैसे उनकी सारी संवेदनाएं लुप्त हो गई हैं।
हम चीन को हर पल या यों कहें कि हर समय गलत मानते हुए उसके हर ऊधम पर खुलेआम प्रतिकार भी करते दिखते हैं, लेकिन चीन के अच्छे गुणों को सीखने के लिए हम सब कभी कोई मजबूत कसरत नहीं करते हैं। हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था काफी चुस्त और दुरुस्त है और यहां न्यायिक व्यवस्था में कोई भी बाहरी-आंतरिक हस्तक्षेप भी ‘शून्य’ है। भारत की सुप्रीम न्यायिक व्यवस्था ने ऐसे कई उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं, जहां न्याय मिला है, पर फादर स्टेन स्वामी की मौत ने एक प्रश्न चिह्न खड़ा कर दिया है। प्रश्न सिर्फ जमानत का था कि जिंदा रहते उन्हें जमानत मिलनी चाहिए थी या नहीं। यह मौत हमारी व्यवस्था पर एक सवालिया निशान लगा कर गया है। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।
’अशोक, पटना, बिहार