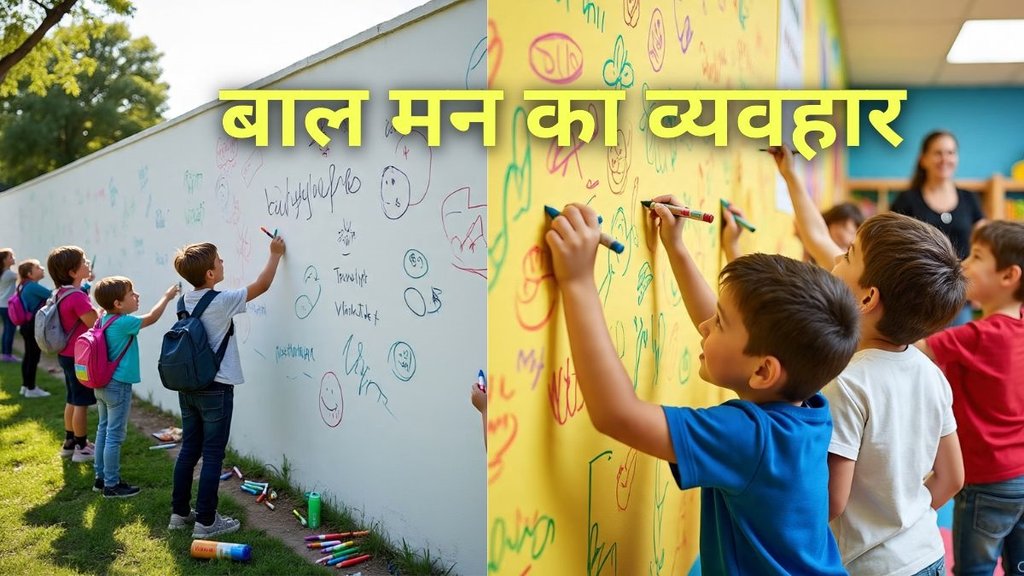विप्रम
शिक्षक जब स्कूल की कक्षा के श्यामपट्ट यानी ब्लैक-बोर्ड पर लिख रहे होते हैं तब अक्सर देखा जाता है कि कुछ बच्चे अपने तरीके से अपने सामने मेज पर कलम से कोई चित्र उकेर रहे होते हैं। कुछ विद्यार्थी अपने मन से कुछ भी लिख रहे होते हैं, कोई स्केच वाली कलम से अपने आगे बैठे सहपाठी की कमीज पर कुछ लिख देता है, तो कोई कापी से पन्ना निकाल हवाईजहाज बना कर उड़ाता दिखता है। इसी तरह की कुछ और नटखट कारगुजारियां करते हुए कई स्कूली बच्चों को देखा जा सकता है।
कई बार स्कूल के शौचालय की दीवारों पर भी भद्दी चित्रकारी देखने को मिलती है। कुछ अच्छे तो कई खराब टिप्पणियां भी उकेरी हुई होती हैं। यही हाल अक्सर रेलगाड़ियों, बसों या सरकारी सार्वजनिक स्थलों पर भी देखने को मिलता है। ऐसा लिखने वाले बढ़ती उम्र के बच्चों के भीतर शायद किसी तरह की हिचक नहीं होती और ये इसके असर के बारे में अंदाजा नहीं लगा पाते।
सार्वजनिक जगहों पर निजी जज़्बात, बोल नहीं पाए, तो दीवारों पर लिख दिया
ऐसे कारनामे यहीं नहीं रुकते, बल्कि कुछ ऐतिहासिक इमारतों की दीवारों-दरवाजों पर भी लिखे या चित्र रूप में इस विचित्र मनोवृत्ति का प्रदर्शन दिख जाता है। ये कभी बेमानी होते हैं तो कभी अश्लीलता की हद भी पार कर जाते हैं। ऐसा लगता है कि इस तरह की हरकत करने वालों को अपने मन की कुंठा निकालनी होती है या किसी तरह अपनी बात दूसरे तक तुरंत पहुंचानी होती है, तो इन्हें इससे सरल और सहज माध्यम कोई और नहीं सूझता। यों भी, जो किसी के सामने नहीं कहा जा सकता या सामने आने पर कहने की हिम्मत नहीं होती, उसे इस तरह पेश कर देना इन्हें बेहतर लगता है। किसी पर्यटन स्थल या किसी ऐतिहासिक इमारत पर प्रेम संदेश या दिल की आकृति को चीरते हुए तीर कई लोगों ने देखा होगा।
ऐसी जगहों पर कुछ सामान्य और सूचनात्मक शब्दों को भी मिटा या बिगाड़ दिया जाता है। इस तरह की हरकत करने वालों को कई बार रचनात्मकता के दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन सच यह है कि इस तरह से अपनी कुंठा या मानसिकता का प्रदर्शन किसी भी तरह से सराहनीय नहीं हो सकता, क्योंकि इससे दूसरों को असहजता होती है, उन्हें बुरा लगता है। इसके अलावा, इस तरह की कुंठा बाद में और ज्यादा विकृत होती जाती है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली बन जाती है। पर्यटन स्थलों या ऐतिहासिक इमारतों पर नाहक ही कुछ लिखना उसे क्षति पहुंचाना भी होता है। इसे दंडनीय भी माना जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं।
देखा जाए तो रचनात्मकता मानव मन में बहुत छोटी उम्र से आने लगती है। बच्चे जब रेत में घर-घर खेल रहे होते हैं, तो अपने घरौंदे बना कर खुश होते हैं। कई बार वे किसी और का घरौंदा तोड़ कर भी खुश होते हैं। अबोध बच्चे नहीं जानते दूसरे का दुख या दूसरे बच्चों के घर टूटने का मतलब, लेकिन उसी दौर में जब उनका घर कोई अन्य बच्चा तोड़ देता है तो वहां दुख का सामाजिक प्रशिक्षण होता है।
बढ़ती उम्र के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो खुद को छोटी उम्र का बच्चा नहीं समझते। मगर ज्यादा उम्र वाले बड़े बच्चे उन्हें अपने साथ नहीं बिठाते। ऐसे में ये बीच उम्र के बच्चे या किशोर अपने में कुछ अधिक ही खोए से रहते हैं। मन ही मन जो उद्गार उमड़ते हैं, उन्हें प्रकट कर देना चाहते हैं, पर समझ नहीं पाते कि वे अपनी बात किससे कहें, कैसे और कब कहें। खुद में खोए हुए बच्चे कुछ न कुछ नया करने की सोचते हैं। बिना किसी को कुछ बताए कभी-कभी अचानक ही एक अजूबा-सा दिखा देना चाहते हैं।
इस प्रवृत्ति के बच्चों के लिए मनोचिकित्सक कहते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ घुलना-मिलना बहुत जरूरी होता है। इनके मन को सकारात्मक सोच से मापते हुए इनकी खुशियों का खयाल रखा जाना चाहिए, वरना ये भटक सकते हैं। बिना बताए इनके स्कूली बस्ते को देखते रहना चाहिए। ऐसे बच्चों से दोस्ताना व्यवहार सबसे कारगर दवा का काम करती है। मगर सबसे बड़ी समस्या आज स्मार्टफोन हो चुका है, जिसकी सार्थक उपयोगिता पर भी प्रश्नचिह्न लग रहा है।
हमारे दिमाग को पसंद नहीं है विरोधाभास, हर बार खुद को सही ठहराना कर देना चाहिए बंद
बढ़ती उम्र के बच्चों का एक रूप और देखने को मिल सकता है। चूंकि इनकी कुछ जरूरतें उम्र के विकास से संबंधित भी हो जाती हैं, जिन्हें ये घर में बताना ठीक नहीं समझते, बल्कि संकोच कर जाते हैं। ऐसे में अगर इन्हें जीवन को लेकर सही प्रशिक्षण नहीं मिले, तो इनके गलत दिशा ग्रहण लेने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा, संगति की वजह से इनके भीतर कुछ ऐसी जरूरतें भी विकसित हो जाती हैं, जो इनके भावी जीवन के लिए सकारात्मक नतीजा देने वाली नहीं होतीं।
एक बच्चे के उदाहरण से समझा जा सकता है, जो घरेलू सामान लाने खुशी-खुशी दुकान पर जाता था। मगर जो भी सामान वह लाता, उसकी मात्रा कुछ कम होती। बाद में उसकी मां ने इस पर गौर किया और दुकानदार से जाकर इसकी पुष्टि की, तब समझ में आया और उसने अपने बच्चे से बात की। दरअसल, सामान में कमी करने से जो पैसे बचते, उसे वह बच्चा अपने लिए सही-गलत कोई चीज खरीदता था।
जाहिर है, यह बच्चे के जीवन के लिए चिंतित करने वाली बात थी। सवाल है कि उसे सामान में कटौती करके अपने लिए पैसा निकालने की आदत क्यों और कैसे पड़ी। अभिभावक उसके साथ कैसे पेश आकर यह रोक सकते थे? यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन और व्यवहार के प्रति बच्चे का साधारण गणित बड़ा ही रोचक होता है। अगर बच्चे की उलट मन:स्थितियों का समाधान समय पर रोचक तरीके और मैत्री भाव के साथ किया जाए तो कोई समस्या बनती ही नहीं।