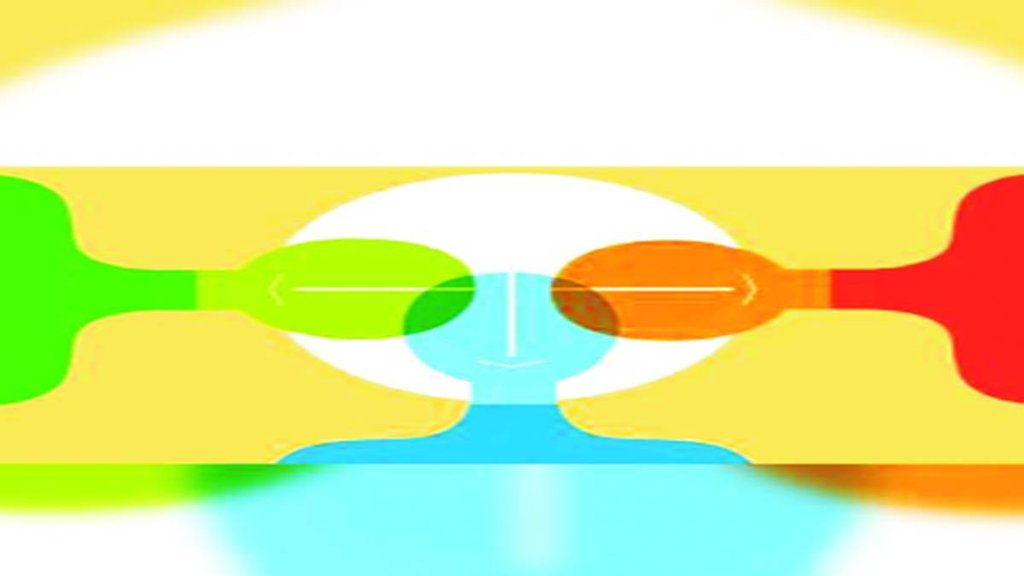रूपा
हर जीव स्वतंत्र पैदा होता है और सदा स्वतंत्र रहना चाहता है। मनुष्य के बारे में यह कथन और भी प्रबल रूप में सही ठहरता है। इसलिए कि उसमें सोचने-समझने, निर्णय कर सकने की क्षमता होती है। हर कोई अपने ढंग से जीना चाहता है। अपने बारे में स्वयं निर्णय करना चाहता है। किसी थोपे हुए निर्णय को स्वीकार करने में उसे असहजता महसूस होती है। बच्चे तक दूसरे के निर्णय थोपने पर विद्रोही हो उठते हैं। मगर मनुष्य चूंकि एक इकाई भर नहीं है, उसे दूसरे लोगों के साथ रहना होता है, वह दूसरों के साथ के बिना रह नहीं सकता। इसलिए उसे उस समूह, अपने वर्ग, अपने समाज और अंतत: देश के नियम-कायदों का पालन करना ही होता है। यहीं मनुष्य की स्वतंत्रता की सीमारेखा तय होती है। स्वतंत्र होने और स्वच्छंद होने में फर्क तय होता है।
विचारों का खंडन-मंडन बुरी बात नहीं है
फिर भी प्राय: लोगों की इच्छा, और शक्ति अर्जित करने के बाद जिद, यही होती है कि वे जैसा चीजों को देखना चाहते हैं, जिस तरह जीवन को जीना उचित मानते हैं, उसी तरह दूसरे भी अपनी जीवन-शैली बना लें। अपने विचारों पर व्यक्ति तब तक अडिग रहता है, जब तक कि उसके विरोध में उसका कोई अकाट्य तर्क न प्रस्तुत हो जाए। दुनिया की तमाम विचार-पद्धतियां इसी तरह बनती और टिकी रहती हैं, फिर उनके विरोध में, समांतर या फिर उन्हें आगे बढ़ाती हुई विचार-पद्धतियां पनपती रहती हैं। दुनिया के तमाम दर्शन इसी तरह जीवन और जगत की व्याख्या करते, एक दूसरे के चिंतन को खारिज करते, आगे बढ़ाते हुए विकसित हुए हैं। किसी के विचारों का खंडन-मंडन बुरी बात नहीं है। स्वस्थ वैचारिक बहसों से ही जीवन के नए सूत्र विकसते हैं।
मगर झगड़ा तब शुरू हो जाता है, जब कोई अपने विचार, अपने सिद्धांत, अपनी धारा को ही श्रेष्ठ मानने की जिद पर अड़ जाता है। वह तमाम दूसरे विचारों या धाराओं को मिटा कर केवल अपने विचारों या धारा को स्थापित करने पर तुल जाता है। ऐसी जिद की वजह से सभ्यता के बहुत सारे निशान उपद्रव की भेंट चढ़ गए। उनके सारे निशान मिट गए। दुनिया की तमाम सभ्यताओं में किसी की जिद के चलते ऐसे उपद्रव हुए। अभी तक होते रहते हैं। भारत में बुद्ध-विचारों को इसी जिद के चलते उखाड़ फेंकने के प्रयास हुए। हालांकि वे विचार अब एक धर्म के रूप में दुनिया के कई देशों में जड़ें जमा चुके हैं, पर वे अपनी जमीन से उखड़ गए। चार्वाक की चिंतनधारा तो समूल नष्ट कर दी गई। हालांकि चार्वाक जिस तरह जीवन को देखते थे, उस तरह आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग, चार्वाक का महिमामंडन किए बगैर भी, जीवन जीने का प्रयास करते हैं। उन्हें वही जीवन-शैली पसंद आती है। वे खुल कर दूसरी पद्धतियों की निंदा भी करते हैं।
मगर हकीकत यह है कि जीवन के सारे सूत्र किसी एक पद्धति में आज तक समाहित नहीं हो पाए। जीवन जीने का सही ढंग कोई एक चिंतन पद्धति नहीं बता सकी। दरअसल, मनुष्य अपनी जीवन-शैली का चुनाव अपने समय और समाज की स्थितियों के मुताबिक करता है। इस चुनाव के पीछे दोनों कारक हो सकते हैं- भौतिकवादी भी और आध्यात्मिक भी। कोई सिर्फ इस जगत को अंतिम सत्य मान कर जीवन जीने का तरीका अपना सकता है, तो कोई इस जगत को असार संसार मान कर पारलौकिक शक्तियों से जुड़ने की राह चुन सकता है।
मगर इन दोनों रास्तों की बनावट भी सब जगह एक जैसी नहीं होती। उनमें भी भेद है। जो इस लोक को सत्य मानता है, उसके तो भटकाव का कोई अंत नहीं। जो परलोक की चिंता करता है, उसके भी रंग अनेक हैं। भटकाव की संभावनाएं वहां भी कम नहीं। इस तरह झगड़े की गुंजाइश वहां भी खूब है। परलोक की चिंता करने वालों के झगड़े भी उन झगड़ों से अलग नहीं, बल्कि अधिक भयावह हैं, जो इस लोक को संपूर्ण रूप में प्राप्त करने को व्याकुल हैं।
कबीर ने कहा- संतो, घर में झगरा भारी। यह घर, यह संसार, झगड़ों से मुक्त नहीं। बड़े झगड़े हैं यहां। शांति सब चाहते हैं, पर अशांति का वरण भी स्वयं करते हैं। संत हों या असंत, झगड़ा सबके बीच है। उनके जीवन के बाहर भी, भीतर भी। तमाम तप, साधना करने के बाद भी तपस्वियों को झगड़े से मुक्त नहीं देखा जाता। इस लोक पर विजय प्राप्त करने को भागते लोगों के धतकरम तो पूछो मत। इन दोनों के बीच तीसरे किस्म के लोग भी हैं और बड़ी संख्या में वही हैं, जो मानते हैं कि इस लोक और परलोक दोनों पर विजय प्राप्त करना जरूरी है।
यहीं से जीवन में संतुलन के सूत्र बनते हैं। कर्म और धर्म के बीच सेतु बनता है। नैतिक और अनैतिक की पहचान की कसौटी तय होती है। ऐसे लोग परंपरा से चली आ रही जीवन-पद्धति को पकड़ कर चलने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही लोगों को समाज का असल तत्त्व माना जाता है। सच्चे सामाजिक ऐसे ही लोग माने जाते हैं। जो समाज की परवाह किए बिना स्वच्छंद जीवन जीना चाहते हैं, नैतिकता जैसी बातों में भरोसा नहीं करते, वे तो असामाजिक हैं ही। जिन्होंने समाज को त्याग दिया, परलोक की चिंता में निकल पड़े, वे भी समाज का हिस्सा कहां रह पाते हैं।
मगर जिन्हें हम सच्चे सामाजिक कहते हैं, झगड़े उनके बीच भी कम नहीं हैं। तमाम अदालतों में उनकी जिद और अपने को सही ठहराने की कोशिशों की नालिशें ठुंकी पड़ी हैं। वे तो नीति, धर्म, सामाजिक समरसता आदि के रक्षक दिखते हैं, पर जीवन-शैली में जहां कहीं अपनी पसंद में व्यतिरेक आया कि उनका संतुलन बिगड़ जाता है। पति का पत्नी के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, भाई का भाई के प्रति स्वभाव में असंतुलन प्रकट हो जाता है। तब उनके सीखे-समझे तमाम सिद्धांत, चिंतन, संयम और साधनाएं कपूर की तरह उड़ जाती हैं। बस जिद अडिग खड़ी मिलती है। यह जिद छूट जाए, तो बहुत सारे झगड़े भी खत्म हो जाएं। ल्ल