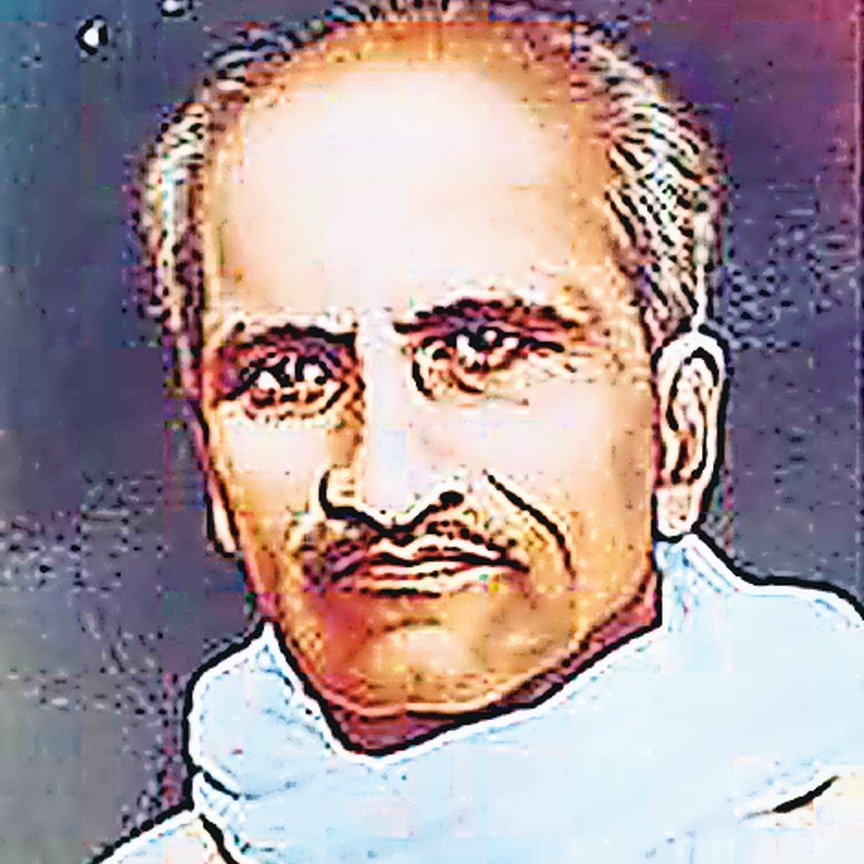बीसवीं सदी के इतिहास में भारत जिन प्रतिभाओं के बूते दाखिल हुआ, वे ज्ञान और संस्कृति की विभिन्न धाराओं से जुड़े थे। कमाल यह कि इन प्रतिभाओं ने उस दौर में अपने कृतित्व का उजास फैलाया जब देश गुलाम था। इस लिहाज से साहित्य और खासतौर पर हिंदी साहित्य की बात करें तो इसके इतिहास के कई गौरवशाली सर्ग इसी दौरान रचे गए। पराधीनता के बीच भारतीय प्रतिभाएं जब अक्षर उद्यम में जुटी थीं तो जाहिर तौर पर उनके सामने सबसे बड़ा सवाल अपने और देश के स्वाभिमान का था।
वे अपनी परंपरा, इतिहास और स्मृतियों से ऊर्जा बटोरते हुए स्वाधीन भारत का सवेरा आंजने में जुटे थे। वृंदावनलाल वर्मा हिंदी के ऐसे ही एक बड़े साहित्यकार हैं जिन्होंने उस दौर में खासतौर पर ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यासों के जरिए भारतीय चेतना और चरित्र को गौरवशाली बोध का अहसास कराया। प्रतिभाओं की तुलना ठीक नहीं होती तब भी यह उल्लेख दिलचस्प है कि उनके विपुल साहित्य को देखते हुए उन्हें हिंदी का वाल्टर स्काट कहा जाता है।
वृंदावनलाल वर्मा का जन्म नौ जनवरी, 1889 को उत्तर प्रदेश में झांसी के मऊरानीपुर में एक ठेठ कायस्थ परिवार में हुआ था। पिता का नाम अयोध्या प्रसाद था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भिन्न-भिन्न स्थानों पर हुई। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कानून की परीक्षा पास की और झांसी में ही वकालत करने लगे। इसके साथ ही उनका लेखन कार्य भी चलता रहा। वे प्रेम को जीवन का सबसे आवश्यक अंग मानने के साथ जुनून की सीमा तक सामाजिक कार्य करने वाले साधक भी थे। उन्होंने वकालत के माध्यम से कमाई सारी पूंजी समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को पुनर्वासित करने में लगा दी।
1909 में वृंदावनलाल वर्मा जी का ‘सेनापति ऊदल’ नामक नाटक छपा, जिसे सरकार ने जब्त कर लिया। 1920 तक वे छोटी-छोटी कहानियां लिखते रहे। उन्होंने 1921 से निबंध लिखना प्रारंभ किया। स्काट के उपन्यासों का उन्होंने स्वेच्छापूर्वक अध्ययन किया और उससे खासे प्रभावित हुए। ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा उन्हें स्काट से ही मिली।
भारत के साथ विदेशी साहित्य खासतौर पर उपन्यासों का उन्होंने भरपूर अध्ययन किया। वृंदावनलाल जी ने 1927 में ‘गढ़ कुंडार’ दो महीने में लिखा। उसी दौरान उन्होंने ‘लगन’, ‘संगम’, ‘प्रत्यागत’, ‘कुण्डली चक्र’, ‘प्रेम की भेंट’ तथा ‘हृदय की हिलोर’ भी लिखा। 1930 में ‘विराट की पद्मिनी’ लिखने के बाद कई साल तक उनका लेखन स्थगित रहा।
1946 में उनका प्रसिद्ध उपन्यास ‘झांसी की रानी’ प्रकाशित हुआ। इसके साथ जुड़ी उनकी यशस्विता आज भी पहले की तरह बहाल है। इसके बाद उन्होंने ‘कचनार’, ‘मृगनयनी’, ‘टूटे कांटें’, ‘अहिल्याबाई’, ‘भुवन विक्रम’, ‘अचल मेरा कोई’ आदि उपन्यासों और ‘हंसमयूर’, ‘पूर्व की ओर’, ‘ललित विक्रम’, ‘राखी की लाज’ आदि नाटकों का प्रणयन किया। ‘दबे पांव’, ‘शरणागत’, ‘कलाकार का दंड’ आदि कहानी संग्रह भी इस दौरान आए।
साहित्यिक सेवाओं के लिए वृंदावनलाल जी आगरा विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि से सम्मानित किए गए। 1965 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा। ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बीच भारतीय नायकत्व को उन्होंने जिस तरह अक्षर सम्मोहन के साथ लोगों के सामने रखा उसने पराधीनता के दिनों में लोगों को नैतिक साहस से तो भरा ही, वह आज भी हमारे सामने अक्षर प्रेरणा की तरह है।