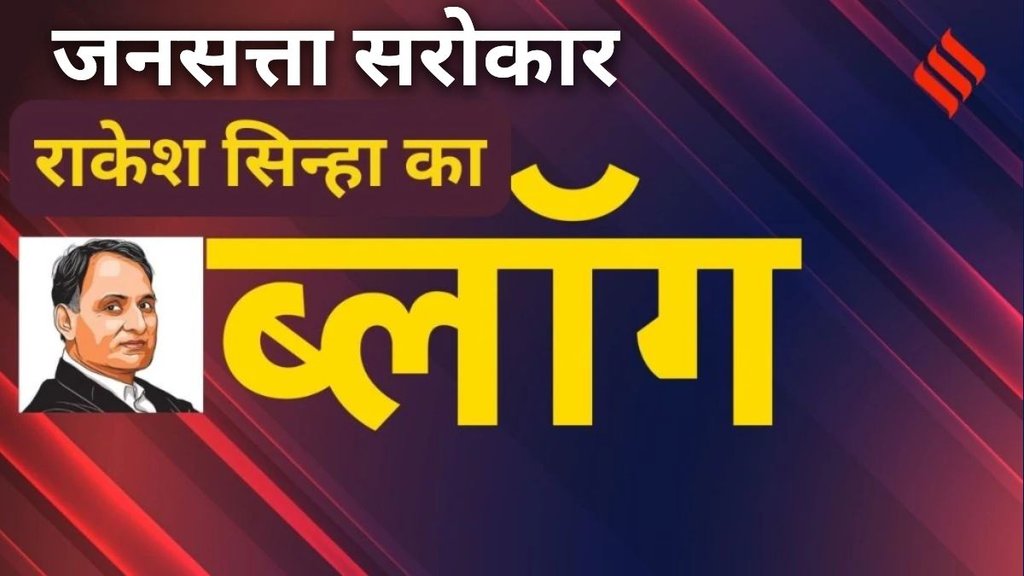केंद्र सरकार द्वारा वक्फ में सुधार को लेकर मुसलिम नेतृत्व और विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया को बड़े फलक पर देखने की जरूरत है। वे इसे मुसलिम संप्रदाय पर आघात मान रहे हैं। वक्फ कानून में हुए संशोधन के तीन महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। पहला, इसके प्रबंधन से निहित स्वार्थी तत्त्वों को बाहर कर इसे अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाना। गैर-मुसलमानों को इसमें जोड़ने पर जो आपत्ति कर रहे हैं, वे भूल रहे हैं कि यह प्रबंधन धार्मिक नहीं, सिविल प्रशासन का हिस्सा होता है।
1995 में वक्फ संशोधन विधेयक पर बोलते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद सैयद मोसुदल हुसैन ने कहा था कि गैर-मुसलमानों को इसमें नहीं जोड़ना सेकुलर मूल्यों के खिलाफ होगा। दूसरा, 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति का उसके उद्देश्यों के आईने में सदुपयोग सुनिश्चित करना। 2011 में शास्वत समिति ने बताया था कि इन संपत्तियों से बारह हजार करोड़ रुपए अनुमानित वार्षिक आमदनी की जगह मात्र 163 करोड़ रुपए ही आता है।
2013 में वक्फ कानून में संशोधन कर वक्फ बोर्ड को असीमित और अनियंत्रित ताकत दिया गया था
तीसरा, 2013 में वक्फ कानून में संशोधन कर वक्फ बोर्ड को असीमित और अनियंत्रित ताकत दिया गया था। किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। केरल में 400 एकड़ का मुनम्बम गांव और तमिलनाडु में 480 एकड़ में फैले थिरुचेंथुरई गांव को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। यह सूची लंबी है। मोदी सरकार ने ‘वक्फ वीटो’ को समाप्त कर दिया। वास्तव में भारत में अलग से वक्फ कानून होना ही नहीं चाहिए। मुसलिम वक्फ विधेयक 1954 पर जब संसद में बहस हुई थी, तब सदस्यों ने इसको संविधान की भावना के प्रतिकूल माना था। तब नेहरू सरकार ने ‘प्राइवेट मेम्बर बिल’ को समर्थन कर वक्फ अधिनियम बनाया था।
जनसत्ता सरोकार: संघ का शताब्दी वर्ष, अतीत, आलोचना और अनदेखे पहलू
राज्यसभा में 23 अप्रैल 1954 को केबी लाल ने चेताया था, ‘ऐसा कर हम राष्ट्र को सिर्फ विघटित करने और (धार्मिक समुदायों का) अलग अस्तित्व बनाए रखने का रास्ता प्रशस्त कर रहे है।’ ऐसा मानने वाले वे अकेले नहीं थे। राजगोपाल नायडु, एचवी सक्सेना, सीता परमानंद, एसएस मोरे, पीवी काने, मोहनलाल सक्सेना, राघवाचारी सहित दर्जनों सांसदों की राय थी कि सभी धर्मों के ट्रस्टों के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। इसका प्रतिमान देश के पास पहले से मौजूद था। बंबई पब्लिक (चैरिटेबल) ट्रस्ट एक्ट, 1950 के अंतर्गत सभी समुदायों, हिंदू, मुसलिम, ईसाई, पारसी, जैन आदि के ट्रस्टों का सुचारु संचालन होता था। तब कानून मंत्री चारुचंद्र विश्वास ने सदन से कहा था कि वे भविष्य में ऐसा कानून लाएंगे, जिसके अंतर्गत सभी धर्मों के ट्रस्टों का प्रबंधन हो सके।
पर हुआ उसका उल्टा। 1960 में ‘रिलीजियस ट्रस्ट बिल’ आया, जिसका दायरा हिंदू ट्रस्टों तक सीमित था। तब जम्मू-कश्मीर के लोकसभा सदस्य एएम तारीक ने व्यंग्यात्मक लहजे में इसे हिंदू ट्रस्ट बिल कहकर पूछा, ‘मुसलमानों और अन्य समुदायों के ट्रस्टों को इस कानून के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है? क्या हम इस देश के नहीं हैं? और क्या कुप्रबंधन सिर्फ हिंदू ट्रस्टों में होता है?’
अरविंद घोषाल, महावीर त्यागी, एमएस अणे, महावीर त्यागी सहित दर्जनों सदस्य उनसे सहमत थे। तब उप कानून मंत्री मार्तंड हजरनवीस ने जो कहा, वह गैर-मुसलिमों की अस्मिता पर सीधा प्रहार था- ‘बाकी समुदायों को भी हम मुसलमानों के प्रबोधन के स्तर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। समुदायों के बीच दूरियों को कम करने का प्रयास ही पंथ निरपेक्षता को आगे बढ़ाता है। हिंदू मंदिरों से प्राप्त धन के उपयोग में संप्रदाय बाधक नहीं बनता है। इसीलिए 23 अप्रैल, 1954 को राज्यसभा में मुसलिम वक्फ विधेयक पर चर्चा के दौरान वीके डांगे ने पूछा था- ‘क्या मैं जान सकता हूं कि वक्फ से जो आमदनी होगी, उसका उपयोग मानवता के लिए होगा या मुसलमानों के लिए?’ आज परिस्थिति हम सबके सामने है।
सामुदायिक विकास को सांप्रदायिकता का मुखौटा नहीं बनाना चाहिए। केंद्र की सरकार ने मुसलिम समाज में सुधार के लिए तीन तलाक या वक्फ जैसे प्रश्नों पर जो कदम उठाया है, वह सांप्रदायिक हठ को समाप्त करने जैसा है। पंथनिरपेक्षता का संवर्धन समुदायों की सांस्कृतिक चेतना पर निर्भर करता है। यह नहीं भूलना चाहिए कि पंथनिरपेक्षता सिर्फ दो समुदायों के बीच समझ या एकता तक सीमित नहीं है।
हिंदू समाज ने सुधार के प्रश्न पर औपनिवेशिक काल में उपनिवेशवादी शासकों की भी मदद लेने में भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी। सती प्रथा के प्रश्न पर राजा राम मोहन राय ने गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बेंटिक की प्रशंसा की थी। 1829 में इस पर कानून बना। ठीक उसी प्रकार विधवा विवाह के प्रश्न पर ईश्वरचंद विद्यासागर ने अभियान चलाया था और गवर्नर जेनरल केनिंग और डलहौजी के सहयोग से 1856 में इस पर कानून बना। थोड़े लोग जो दोनों अवसरों पर इसे इसाई हस्तक्षेप बताकर सुधार रोकना चाहते थे, वे न सिर्फ अस्वीकृत हुए, इतिहास के कूड़ेदान में चले गए। सांस्कृतिक चेतना सामाजिक समझ विकसित करने का मार्ग होता है और यह समुदायों की विशिष्ट चेतना का विरोधाभासी नहीं होता है। लेकिन अगर किसी समुदाय की विशिष्ट चेतना सुधार और आधुनिकता को धर्म पर खतरा कहने लगे, तब सांप्रदायिक चेतना फासीवाद बन जाती है।
तभी केबी लाल ने राज्यसभा में कहा था कि ‘आप चाहे जितनी भी ऊंची आवाज में कहते रहें कि हम सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन यह बढ़ती ही जाएगी। आप इसे कभी खत्म नहीं कर सकते है।’ वक्फ में सुधार निश्चित रूप से एक महत्त्वपूर्ण कदम है, पर संविधान तभी मुस्कुराएगा, जब सभी समुदायों के ट्रस्टों के लिए एक ‘पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट’ बन पाएगा।