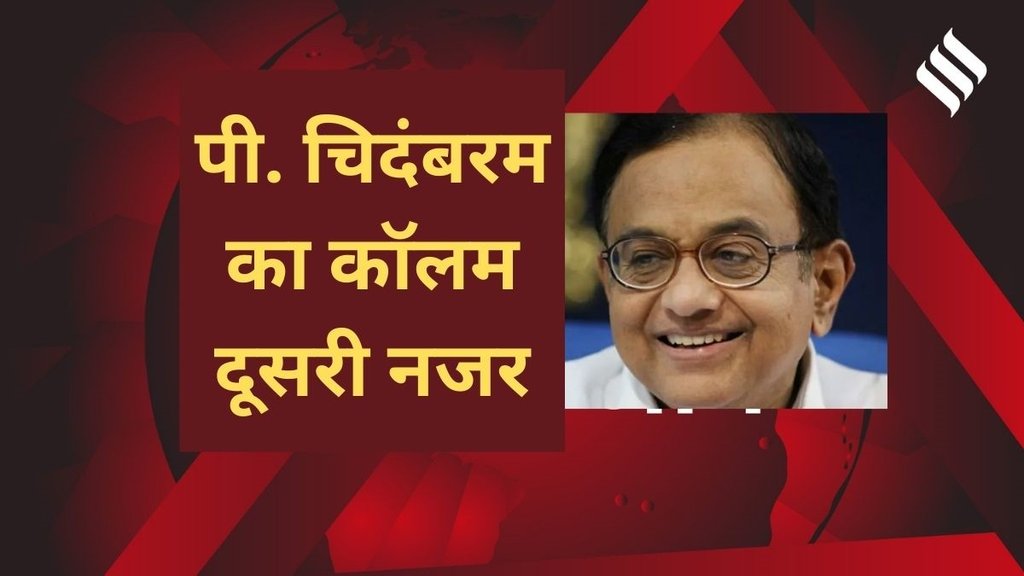व्यावहारिक रूप से सभी सरकारें अधिक से अधिक ताकत हासिल करना चाहती हैं और खुद को अधिक नियंत्रण-शक्ति और अधिक अधिकार देने के लिए कानून बनाती हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि शासकों को लगता है कि केवल उन्हें पता है कि देश और लोगों के हित में क्या है। यही मनोग्रंथि कुछ व्यक्तियों में भी होती है। इसे ‘सेवियर’ (या मसीहा) मनोग्रंथि कहा जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथि है, जिसके चलते किसी व्यक्ति में यह विश्वास भर जाता है कि उसे सारी समस्याओं को ‘ठीक’ करना चाहिए और लोगों को ‘बचाना’ चाहिए। यह ग्रंथि जब अपने चरम पर पहुंच जाती है, तो उसे भ्रम पैदा हो सकता है कि वह जैविक रूप से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि ‘भगवान ने उसे भेजा है’।
सात जनवरी, 2025 को अखबारों के अंदर के पन्नों पर एक छपी खबर थी, जिसका शीर्षक था ‘यूजीसी ने कुलपतियों की नियुक्ति संबंधी नियमों में किया बदलाव’। उसकी विषय-वस्तु विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की चयन प्रक्रिया पर केंद्रित थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इससे संबंधित नियम-कायदों का मसविदा जारी किया है और उन पर लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।
हवा में प्रावधान
मौजूदा वक्त में, राज्यों के विश्वविद्यालयों में राज्यपाल को एक या उससे अधिक विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाया जाता है, जो उनके स्थापना संबंधी अधिनियमों की परिपालन प्रणाली को देखने के लिए अधिकृत होता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्थापना संबंधी अधिनियमों में राष्ट्रपति विजिटर होते हैं। राज्यपाल प्राय: लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में रह चुके, सेवानिवृत्त राजनीतिक नेता, विशिष्ट या प्रतिष्ठित नागरिक होते हैं। राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप काम करेंगे। अभी यूजीसी ने जिस नियम-कायदे पर सुझाव मांगे हैं, वह खोज-सह-चयन समिति के प्रावधान से संबंधित है, जिसमें राज्यपाल, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय की सीनेट और विश्वविद्यालय परिषद में से एक-एक नामित व्यक्ति शामिल होगा। पहले खोज-सह-चयन समिति वैविध्यपूर्ण और लोकतांत्रिक हुआ करती थी। हालांकि अंतिम चयन कुलाधिपति/ राज्यपाल द्वारा किया जाता था, पहले राज्यपाल आमतौर पर राज्य सरकार की ‘सहायता और सलाह’ पर यह काम करते थे। मगर दुर्भाग्य से यह प्रथा पिछले एक दशक में दफ्न हो गई और राज्यपालों ने अपने विवेक से कुलपतियों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी है।
अब वक्त बदल गया है- पहले से चीजें बदतर हुई हैं। मौजूदा निजाम में, इस पद पर राजनीतिक नियुक्तियां की जाती हैं और उन्हीं लोगों को उनकी वफादारी के लिए पुरस्कृत करने के मकसद से राज्यपाल बनाया जाता है, जो आरएसएस/ भाजपा की विचारधारा से जुड़े या भरोसेमंद सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। विपक्ष शासित राज्यों में, राज्यपाल को केंद्र सरकार के वायसराय के रूप में कार्य करने और राज्य सरकार पर शिकंजा कसने का निर्देश दिया जाता है। दरअसल, राज्यों में दोहरी शासन प्रणाली है: एक निर्वाचित सरकार की और दूसरी अनिर्वाचित राज्यपाल की। भारत के संविधान में वर्णित ‘सहायता और सलाह’ के प्रावधान को हवा में उड़ा दिया गया है।
बढ़ता दोहरा शासन
इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि किस तरह राज्यपाल, राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण के पूरे या कुछ हिस्सों को विधानसभा में पढ़ने से इनकार कर देते हैं। राज्यपाल को सार्वजनिक रूप से राज्य सरकार, खासकर मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए देखा जाता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री को दरकिनार करते हुए मुख्य सचिव या पुलिस प्रमुख को बुलाते और उन्हें निर्देश जारी करते हैं। राज्यपाल को जिला प्रशासन की ‘समीक्षा’ करने और जिला अधिकारियों के साथ ‘चर्चा’ करने के लिए राज्य के दौरे पर निकलते देखा जाता है। संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन में, खासकर विपक्ष शासित राज्यों में, दोहरी शासन व्यवस्था अपने आप को लगातार ताकतवर बनाती जा रही है। (भाजपा शासित राज्यों के मामले में, राज्य सरकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है और आमतौर पर एक मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी ऐसा होता है जो प्रधानमंत्री की ‘आंख और कान’ होता है, जो प्रधानमंत्री के फैसलों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाता है।)
यूजीसी अधिनियम की धारा 22 में कहा गया है कि ‘डिग्री’ का अर्थ यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट कोई भी डिग्री है और इसे केवल अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। कुलपति की खोज-सह-चयन और नियुक्ति प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले नए मसविदे में ये प्रावधान प्रस्तावित हैं: यह तीन-सदस्यीय समिति के माध्यम से संपन्न होगा, जिसमें कुलपति, यूजीसी और विश्वविद्यालय के शीर्ष निकाय (विद्वत परिषद/ सीनेट/ प्रबंधन बोर्ड) में से प्रत्येक का एक नामित व्यक्ति शामिल होगा। समिति तीन से पांच नामों का एक पैनल तैयार करेगी और कुलाधिपति उनमें से एक को नियुक्त करेंगे।
अगर कोई विश्वविद्यालय इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने या यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, यूजीसी अधिनियम के तहत विश्वविद्यालयों की सूची से हटा दिया जाएगा, और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वास्तव में, वह शैक्षणिक संस्थान ‘विश्वविद्यालय’ नहीं रह जाएगा। गौरतलब है कि कुलपति के चयन और नियुक्ति में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। कुलपति यूजीसी का वायसराय बन जाएगा, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती और उन्हें हटाया भी जा सकता है।
विश्वविद्यालयों का राष्ट्रीयकरण
‘वैचारिक शुद्धता’ के लिए चुने गए दो वायसराय विश्वविद्यालय का प्रशासन संभालेंगे- एक, राज्यपाल/ कुलाधिपति और दूसरा, कुलपति। अगर यह नियम-कायदा मसविदा अधिसूचित हो जाता है, तो इससे राज्य सरकारों के उन अधिकारों का हनन होगा, जिनके तहत वे राज्य के निवासियों के लाभ के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना करते और अपने संसाधनों से उसे वित्तपोषित किया करते थे। नए नियमों के तहत दरअसल, विश्वविद्यालयों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा और ‘मसीहा’ देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआइ) पर नियंत्रण कर लेगा। यह भाजपा की ‘एक राष्ट्र, एक सरकार’ की नीति के अनुरूप तेजी से बढ़ते केंद्रीकरण का एक और उदाहरण है। यह संघवाद और राज्यों के अधिकारों पर एक जबरदस्त हमला है।
राज्यों को इस मसविदे को अस्वीकार कर देना चाहिए और भारतीय विश्वविद्यालयों के राष्ट्रीयकरण की कोशिश को परास्त करने के लिए राजनीतिक और कानूनी रूप से लड़ना चाहिए। शिक्षकों और छात्रों को विरोध करना चाहिए। सावधान रहें, अगर एक बार दोहरी शासन प्रणाली सार्वजनिक प्रशासन के सभी पक्षों में समाहित हो जाती है, तो उसके बाद केवल उस वक्त का इंतजार करना बच जाता है, जब दोहरी शासन प्रणाली, राजशाही या निरंकुश शासक के लिए रास्ता बनाना शुरू कर देती है।