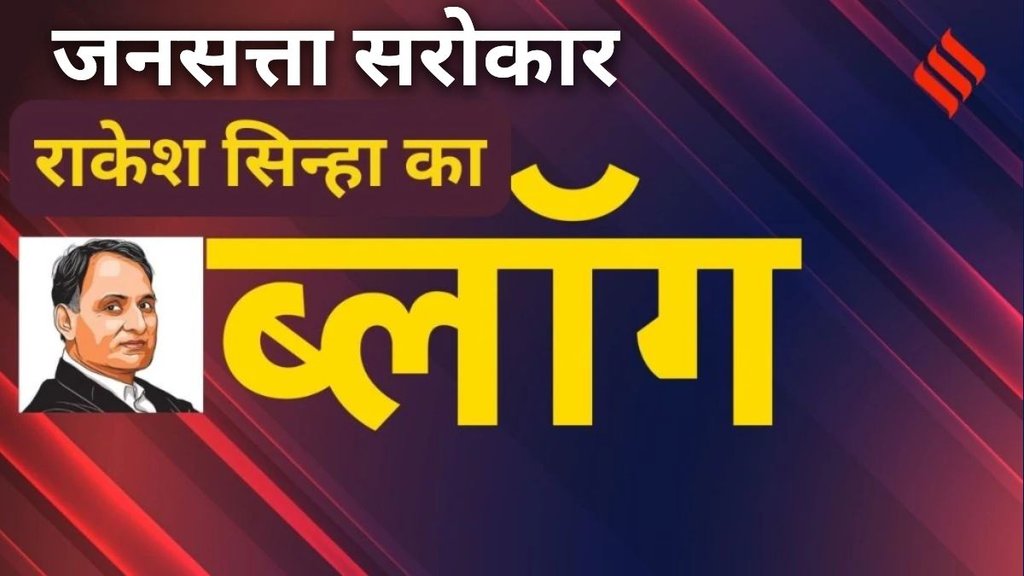संविधान की प्रस्तावना में बयालीसवें संशोधन द्वारा आरोपित ‘धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी’ शब्दों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले द्वारा राजनीतिक बहस और पुनर्विचार के सुझाव ने सियासी भूचाल ला दिया। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने संघ और भारतीय जनता पार्टी पर संविधान को ही बदलने का आरोप मढ़ दिया।
राहुल गांधी ने तो संविधान को मनुस्मृति से विस्थापित करने की साजिश तक कह दिया। यह प्रक्रिया समकालीन राजनीति की प्रकृति और गुणात्मक गिरावट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। विमर्श विपक्ष को कांटे से भी अधिक कंटीला लगने लगा है। वे विमर्श मुक्त राजनीति के पक्षधर हो गए हैं।
जनतंत्र की आत्मा मतों की भयमुक्त और स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। यही समाज की चेतना को समृद्ध करती है। इसे रोकना नदी को तालाब बना देने जैसा है। आज वही हो रहा है। जिस संविधान की राजनीतिज्ञ दुहाई देते थकते नहीं हैं, उसे या तो पढ़ा नहीं है और अगर पढ़ा है, तो उसके मर्म और संदेश को ग्रहण नहीं किया है।
संविधान सभा मत अभिव्यक्ति की एक प्रयोगशाला भी थी। इसे विमर्श का स्वर्णिम अध्याय भी कहा जा सकता है। न किसी पर कुछ थोपा गया, न ही रोका गया। अनचाही बातों को धैर्य से सुना गया। विमर्श के तीन आयाम होते हैं- तथ्य, तर्क और संयम। तीनों ही भरपूर थे। उदाहरण के लिए एचवी कामत ने संविधान में ‘ईश्वर’ शब्द जोड़ने का संशोधन रखा। उस पर शांतिपूर्ण बहस हुई और मतदान भी। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। बहस के लिए नीयत के साथ-साथ स्वध्याय, चिंतन और चेतना जरूरी होता है। इसकी गिरावट विमर्श की संस्कृति को समाप्त कर देती है।
दत्तात्रेय होसबाले ने जो कहा, उसका प्रतिबिंब संविधान सभा में विद्यमान है। केटी शाह संविधान सभा के मुखर सदस्यों में से एक थे। उन्होंने प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्द जोड़ने का संशोधन रखा था। वह खारिज हो गया। बाबा साहब आंबेडकर ने ‘समाजवादी’ शब्द की अप्रसांगिकता बताते हुए कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व में समानता, शोषण मुक्त और श्रम को सम्मान देने वाले प्रावधानों की प्रचुरता है। उन्होंने कहा था, ‘और कितना समाजवाद चाहिए?’
समाजवाद एक विशिष्ट प्रकार की विचारधारा है। एक आर्थिक विचार से पीढ़ियों को बांधा नहीं जा सकता है। समय, संदर्भ और आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक दर्शन का अन्वेषण होता है। भारतीय समाज समानता का पक्षधर है। इसलिए सामाजिक-आर्थिक न्यूनताओं के विरुद्ध व्यक्ति या संगठन को स्वाभाविक स्वीकृति मिलती रही है।
पंथनिरपेक्षता जीवंत पद्धति होती है। इसका अभिप्राय आध्यात्मिक विवेचना करने, अपनी इच्छा से तौर-तरीके को चुनने और ईश्वर से संबंध को फिर से परिभाषित करने का अधिकार होता है। इसीलिए विविधताएं डराती नहीं हैं। लड़ाई दो प्रवृतियों के बीच रहती है। एक प्रवृति है विविधता का हिस्सा बन कर चलना। दूसरी प्रवृत्ति है विविधता को किसी पुस्तक के संदेश या आध्यात्मिक गुरु के दर्शन के आधार पर एकरूपता में तब्दील कर देना।
हिंदू जीवन पद्धति जितनी ही प्रवहमान और न्यूनताओं से मुक्त रहेगी, पंथनिरपेक्षता उतनी ही प्रबल और प्रभावी होगी। वेद और उपनिषद दोनों ही हमारी इस जीवन पद्धति को ठोस आधार प्रदान करते हैं। इसीलिए दोनों शब्दों ‘धर्मनिरपेक्षता’ और ‘समाजवादी’ का संविधान की प्रस्तावना में रहना उसे पश्चात्यवादी परिभाषा का दास बना देता है।
ये शब्द मुखौटा से अधिक कुछ नहीं हैं। इन शब्दों को जोड़ने के पीछे की नीयत जनतंत्र पर लगे ग्रहण को ढकना था। इंदिरा गांधी की सरकार ने 26 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया।
देश को अभिव्यक्ति शून्य बना दिया गया जिसे कवि भवानी प्रसाद मिश्र की ये पंक्तियां जीवंतता से प्रतिबंबित करती हैं: ‘बहुत नहीं सिर्फ चार कौए थे काले,/ उन्होंने यह तय किया कि सारे उड़ने वाले/ उनके ढंग से उड़ें, रुकें, खायें और गाएं/ वे जिसको त्योहार कहें सब उसे मनाएं।’
सत्ता का केंद्रीकरण चरम पर था। व्यक्ति पूजा उससे भी आगे थी। लोकतंत्र में शक्ति का पृथक्कीकरण उसका बहुमूल्य धरोहर था। इसे समाप्त करने की प्रक्रिया का नाम ही 42वां संविधान संशोधन था। उस वक्त संसद के भाषणों में यही मुख्य धारा थी। इस संशोधन में न तो जनभागीदारी हुई और न ही लोक विमर्श हुआ।
लोकसभा में मतदान के दौरान 346 इसके पक्ष में और दो मत जिनमें जीवी मावलंकर शामिल थे, विरोध में पड़े। आखिर वे विरोध की भूमिका में रह कर वाजपेयी, देसाई, फर्नांडीज की तरह सरकार का कोपभाजन क्यों नहीं बने। इसका उत्तर रूस के एक कम्युनिस्ट तानाशाह के शब्दों में मिलता है। चुनाव में उन्हें 99.6 फीसद वोट मिले। किसी ने पूछा, शेष वोट क्यों नहीं पड़े। उत्तर था ‘आखिर जनतंत्र है।’ वही जनतंत्र 1976 में लोकसभा में था।
‘हम भारत के लोग’ का तात्पर्य एक पीढ़ी नहीं, भविष्य की पीढ़ियां भी हैं। उनके सोचने, समझने और भारत को परिभाषित करने का अधिकार किसी कालखंड की पीढ़ी की सोच-समझ और परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता है। यही भाव संविधान सभा में आंबेडकर ने एक नहीं अनेक बार व्यक्त किया था।
अमेरिका में राष्ट्रपति दो या दो से अधिक बाइबिल पर हाथ रख कर शपथ लेते हैं। ब्रिटेन के हाउस आफ लार्ड्स में चर्च आफ इंग्लैंड के 26 प्रतिनिधि मनोनीत होते हैं। यह ‘पश्चात्य पंथनिरपेक्षता का प्रतिमान है। भारत इससे आगे है। सम्राट अशोक और चोल वंश राजा राजेंद्र जैसे शासकों ने धर्मं और राजनीति के संबधों का जो प्रतिमान दिया, वह भारतीय पंथनिरपेक्षता का प्रतिमान है।
दत्तात्रेय होसबाले ने इन्हीं के बीच संघर्ष को पुनर्जीवित किया है। आरोप- प्रत्यारोप, बदजुबानी और काल्पनिकता विमर्श नहीं होता है। इन दोनों शब्दों पर विमर्श संविधान की प्रस्तावना तक सीमित रहेगा। यह भारत के यथार्थ की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकता है। विपक्ष इसे रोकना चाहता है।