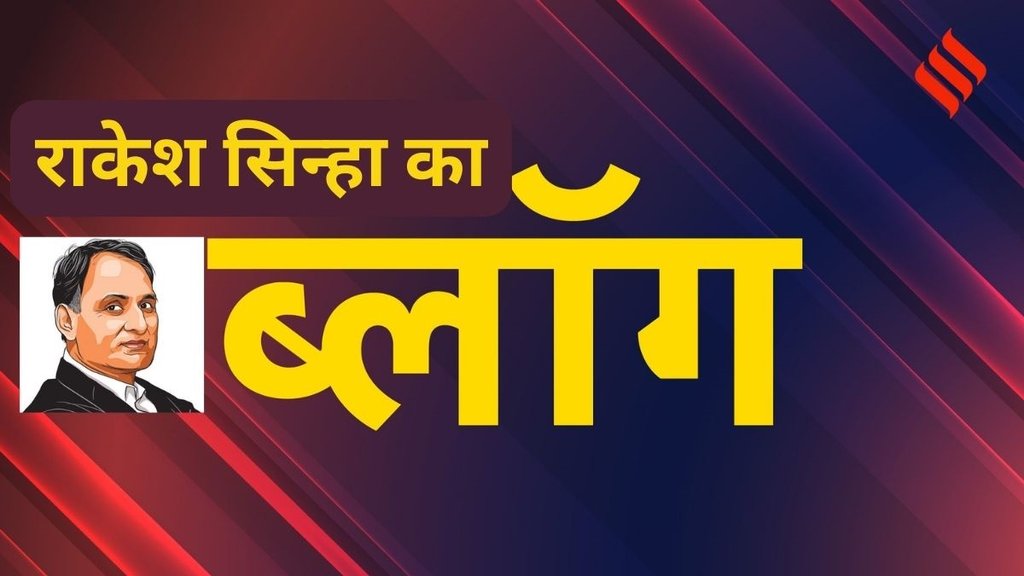कृत्रिम मेधा यानी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ के प्रति उत्सुकता और कौतूहल दोनों है। यह स्वाभाविक भी है। इसका उपयोग किस रूप में होगा, यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। समुद्र मंथन ने मानव समाज को सीख दी है। जो चीजें मानव की मौलिकता और उसकी अस्मिता को प्रबलता प्रदान करने की क्षमता रखती हैं, उन्हें ही स्वीकार करना चाहिए। 1927 में महात्मा गांधी ने इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलुरु में अपने भाषण में कहा कि शोध का लक्ष्य गरीबी मिटाना, समाज की प्रगति होना चाहिए, न कि वह लोगों पर अत्याचार का उपकरण बन जाए। यह भाषण विवादास्पद बना। कई वैज्ञानिकों ने गांधी पर आलोचनात्मक टिप्पणी की, पर इससे गांधी का दृष्टिकोण अप्रासंगिक नहीं हुआ। मनुष्य को आदर्शवादी बातों के साथ मापदंड से हटकर सोचने या बोलने का भी नैसर्गिक अधिकार है। मशीन का उपयोग मनुष्य के मस्तिष्क को शिथिल, आलसी और बाह्य तंत्र पर निर्भर बनाने के लिए होने लगेगा, तब मानव सभ्यता के बीमार होने का भय होगा। मनुष्य जीवन जिस प्रकार चलता है उसके लिए ‘माया’ शब्द का प्रयोग होता है। कबीर ने इसे ‘महाठगिनी’ कहा है। इसकी चौकीदारी मानव मन की हरित भूमि को बंजर बना देने की क्षमता रखता है। यही ‘कृत्रिम मेधा’ की सीमा तय कर देता है।
कुछ दशकों में संचार आसान हो गया है। पर उसका एकाधिकार हमारे जीवन पर अभी कुछ फीसद ही हुआ है कि साहित्य और समाजशास्त्र अरुचिकर लगने लगा है। हर जगह हम संक्षिप्त खोजते हैं। हम जितने आधुनिक हो रहे हैं, उतने ही संकीर्णता, असहिष्णुता, असंवेदनशीलता और व्यक्तिवाद जैसे दुर्गुणों से उलझते जा रहे हैं। मानव की मौलिकता उसके अपने जीवन की सबसे कीमती विशेषता है। उसे जानने और प्रकट करने की क्षमता जब विकसित हो जाती है, तब वह शक्तिशाली बन जाता है। इसी को हम ‘स्व’ कहते हैं। इसे जो जितना समृद्ध करता है, वह उतना ही प्रभावशाली प्रेरक बन जाता है। फिर वह दांडी साधु की तरह ‘विश्व विजेता’ सिकंदर को चुनौती देने का नैतिक सामर्थ्य रखता है। अन्यथा शक्ति, साक्षरता, संसाधन होते हुए भी आत्मसमर्पण की होड़ लगी रहती है। इससे कैसे बचा जाए? उसका उपाय असाध्य नहीं है। ऐसी चीजें हैं, जो हमें स्वयं का मूल्यांकन और आत्मालोचन करने की आदत डालता है। और आखिर हमारी अभिव्यक्ति को ‘तू तड़ाक’ से दूर ‘हम और आप’ की सभ्य दुनिया में रखता है।
यह डायरी और चिट्ठी लिखने की आदत और परंपरा है। हम जब कुछ लिखते हैं तो स्वयं से संघर्ष करते हैं। मन-मस्तिष्क में द्वंद्वात्मक भाव रहता है। फिर यथार्थ को श्रेष्ठतम रूप में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। यह मानव को अगली पीढ़ी से, एक संदर्भ को दूसरे संदर्भ से, एक कालखंड को दूसरे युग से जोड़ने में सहज रूप से सहायक होता है। पिछली शताब्दियों में लोगों की सोच, समकालीन संबंधों को देखने का पैमाना तब लिखी गई डायरियों और चिट्ठियों से मिलता है। पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में लोग उसे पढ़ते और संदर्भ के अनुकूल उद्धृत करते हैं। सोशल मीडिया के प्रभाव में हमारा सरोकार न तो डायरी से, न ही चिट्ठी से रह गया है। कल की पीढ़ी आज की पीढ़ी से क्या सीखेगी? विडंबना है कि आधुनिकता के साथ अंधकार का विरोधाभास साथ-साथ चल रहा है।
अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 16 अप्रैल, 1963 को बर्मिंघम जेल से इसाई पादरियों को बीस पृष्ठों का पत्र भेजा था। यह पत्र अन्याय के खिलाफ अहिंसक प्रतिकार के संकल्प का घोषणा पत्र जैसा है। वे उसमें लिखते हैं, ‘विश्वसनीय लोगों की किसी बात की सतही समझ बुरे लोगों की नासमझी से कहीं ज्यादा निराशाजनक होती है।’ उसी में वे कहते हैं, ‘मैं इस बात को महसूस करने लगा हूं कि दुर्जन लोग सज्जनों की तुलना में समय का अधिक प्रभावी तरीके से उपयोग कर लेते हैं।’ आगे लिखा कि ‘मनुष्य का अथक और निरंतर प्रयास उसे ईश्वर का सहचर बना देता है। ऐसा नहीं करने पर अच्छे कार्य का समय भी सामाजिक ठहराव का सहयोगी बन जाता है। हमें समय का रचनात्मक उपयोग करना चाहिए और यह अनुभूति करनी चाहिए कि अच्छे कार्य के लिए समय हमेशा उपयुक्त होता है।’
दस हजार बावन दिनों तक जेल में रहने वाले नेल्सन मंडेला ने जेल से सैकड़ों पत्र लिखे। एकांतवास पर चिट्ठी में उन्होंने लिखा, ‘यह आदर्श जगह है अपने आप को समझने, यथार्थवादी तरीके से खोज करने और अपने मस्तिष्क और भावनाओं को सहेजने का। 1976 में उन्होंने जेल आयुक्त को बीस पृष्ठों के पत्र में लिखा- ‘हमारे और आपके बीच में संघर्ष की पराकाष्ठा के बावजूद मैं सिद्धांतों और विचारों के आधार पर लड़ूंगा, जिसमें व्यक्तिगत नफरत का कोई स्थान नहीं होगा..! दरअसल, कायरता है उन लोगों से बदला लेना, जो स्वयं की रक्षा और प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं हैं।’ इसी तरह की चेतना गांधी के पत्रों में अभिव्यक्त होती है। 24 दिसंबर को पुणे के जेल से साम्राज्यवादियों से संघर्ष पर उन्होंने लिखा, ‘हम उन्हें बदलने के लिए न कि पराजित करने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे शासकों ने हमारी भूमि और शरीर पर भले ही नियंत्रण कर लिया है, पर आत्मा पर नहीं।’ एक दूसरे पत्र में हिटलर और मुसोलिनी को उन्होंने लिखा कि ‘आपके कार्य राक्षसी और मानव गरिमा के विपरीत हैं।’
संघर्ष से उपजे लोगों की सोच में वैश्विकता और संकल्प, दोनों होता है। यह उन्हें समान सोच का बना देता है। जब इन तीनों की चिट्ठियों के सारांश/ उद्धरणों को एक स्थान पर एकत्रित करने के बाद उनका उपयोग करते समय मैं भ्रमित हो गया कि किसका कौन उद्धरण है। उद्धरणों के उपयोग में नाम की अदला-बदली हो जाए तो भी उनके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब यथावत बना रहता है। कोई कृत्रिम बुद्धिमता इस विधा से मानव की रचनात्मक उत्पादकता को विस्थापित नहीं कर सकती है। डायरी और चिट्ठी लेखन को जीवित करना न पहाड़ तोड़ना, न समुद्र लांघना है। सिर्फ कृत्रिमता के हल्केपन को पहचानना है। और यह होगा। मंडेला ने एक पत्र में लिखा था ‘आशा एक शक्तिशाली हथियार होता है।’