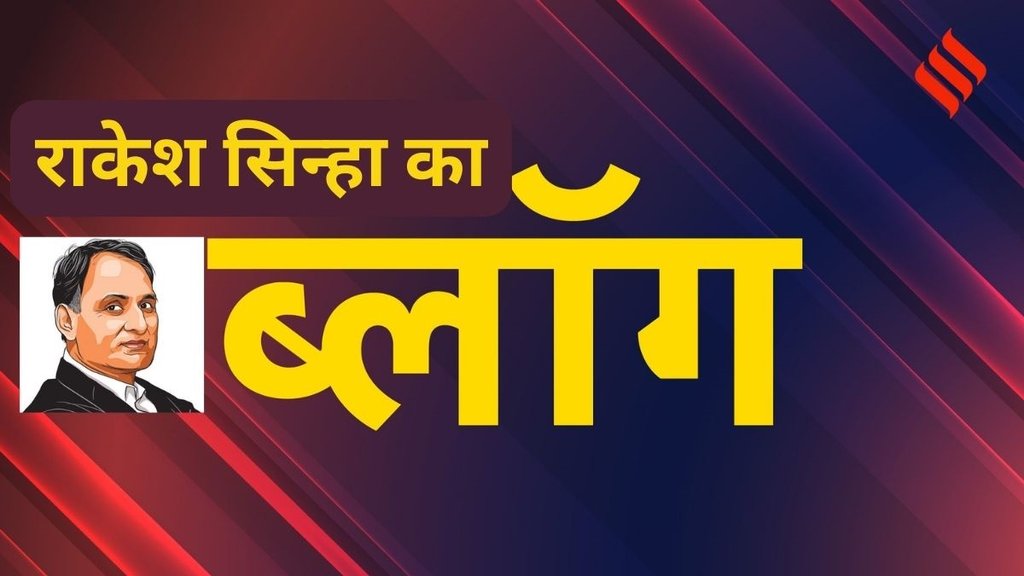जनगणना पर राजनीति ने इसकी उपयोगिता और गुणवत्ता के बारे में स्थिर मन से ठोस चिंतन करने पर ताला लगा दिया है। अब तक की पंद्रह जनगणनाओं में आठ औपनिवेशिक काल में और सात स्वतंत्रता के बाद हुई। पहली व्यवस्थित जनगणना 1872 में हुई थी। सामान्यतया जनगणना का तात्पर्य जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का तुलनात्मक आंकड़ा जमा करना होता है। पर यह पूर्ण नहीं है। स्वतंत्रता से पूर्व 1872 से 1941 तक और बाद की जनगणनाओं में 1951 से 2011 तक की जनगणनाओं के अंतर देखा जा सकता है। अंग्रेजों की नीयत चाहे जो भी हो, उस कालखंड में जनगणना का तरीका, जनगणना करने वालों का शैक्षणिक स्तर और देश के सामाजिक-सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन के अध्ययन के आयाम तब वर्तमान से बिल्कुल भिन्न थे। दुर्भाग्य से इन बातों पर गौर किया ही नहीं गया।
स्वतंत्र भारत में जनगणना को लिपिकीय काम की तरह देखा गया
स्वतंत्र भारत में जनगणना को लिपिकीय काम की तरह देखा गया। परिणामत: इसकी उपेक्षा स्वाभाविक थी। यह राज्य का रचनात्मक नहीं, रूटीन उपक्रम बनकर रह गया। राजनीतिकों की तो रुचि सिर्फ उन आंकड़ों में होती है, जो उनका राजनीतिक स्वार्थ साधता है, लेकिन चिंता का विषय तो समाजशास्त्रियों और नौकरशाही द्वारा भी इसकी उपयोगिता नहीं समझना है। अगर यह कहा जाए कि स्वतंत्र भारत में जनगणना करने वाले अधिकारी इसे बोझ की तरह देखते रहे, तो यह अतिशयोक्ति न होगी।
जनगणना तो साम्राज्यवादी शासन के दौरान भी राज्य का उपक्रम था। मगर जनगणना करने वाले इसमें रम जाते थे। साम्राज्यवादियों ने प्रशासन का उपयोग इसके लिए बेहतरीन तरीके से किया। प्रशासनिक सेवा में जो लोग आते हैं, वे पहाड़ या जंगल में शारीरिक श्रम द्वारा नहीं, बल्कि मनोयोग से अध्ययन करके आते हैं। तब उन्हें उनकी रुचि के आधार पर जनगणना में लगाया गया। मगर स्वतंत्र भारत में प्रशासनिक अधिकारियों को एक ही प्रकार से हांका जाने लगा। परिणामस्वरूप, वे फाइलों, आदेशों, सुविधाओं के दास बनकर रह गए। अपवाद भी दम तोड़ते रहे। रुचि, अध्ययन और मनोदशा के अनुसार काम बांटने की परिपाटी विकसित ही नहीं हुई।
अंग्रेजी शासन में जनगणना कार्य के लिए प्रतिभावान लोग लगाए जाते थे
औपनिवेशिक काल तक की जनगणनाओं में असाधारण प्रतिभा वाले प्रशासकों का योगदान रहा। यह जनगणना रपटों में साफ झलकता है। इसे कुछ उदाहरणों से जाना जा सकता है। 1901 में बंगाल प्रांत के जनगणना अधीक्षक इए गेट थे। वे 1911 में देश के जनगणना आयुक्त बने। लिखना-पढ़ना, सर्वे उनका प्रिय काम था। 1906 में उन्होंने ‘असम का इतिहास’ नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। उसी वर्ष देश के जनगणना आयुक्त एचएच रीजले थे, जो चार खंडों में प्रकाशित ‘ट्राइब्स एंड कास्ट आफ बंगाल’ पुस्तक के लेखक थे। वे प्रशासक होने के साथ एक एथनोग्राफर भी थे। 1931 के जनगणना आयुक्त जेजे हट्टन मानव विज्ञानी थे। नगा जनजाति पर उनकी छह पुस्तकें हैं। उनका अकादमिक झुकाव इसी बात से समझा सकता है कि 1936 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में प्राध्यापन करने लगे। सभी प्रांतों के जनगणना अधीक्षक वही अधिकारी होते थे, जिनमें विषय की समझ होती थी।
1931 में संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध के जनगणना अधीक्षक एसी टर्नर थे। उन्होंने जनगणना रपट में विस्तार से प्रकाश डाला कि ‘भारत में धर्म’ की जो अवधारणा है, वह पश्चिम के ‘रिलीजन’ की परिभाषा से मौलिक रूप से भिन्न है। 1872 में जनगणना-आयुक्त बौरडीलीयोन ने रपट में सवाल खड़ा किया था कि ‘हिंदू कौन है?’ आगे सभी जनगणनाओं में विश्लेषण चलता रहा। मेली ने लिखा कि ‘किसी खास एक व्यक्ति को हिंदू धर्म की शुरुआत करने वाला नहीं कहा जा सकता है। हट्टन ने जनगणना रपट में कहा, ‘एक ही विश्वास को साझा करना हिंदू समाज की बाध्यता नहीं है।’ सूक्ष्म परंपराओं, विवाह की पद्धतियों में अंतर, विधवाओं की संख्या का कारण, आध्यात्मिक परिपाटियों में भिन्नता आदि को ढूंढ़-ढूंढ़ कर रपट में डाला जाता था।
जनगणना का एक सभ्यताई परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। परंपराओं और लघु संस्कृतियों को समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखना जनगणना को पूर्णता देता है। राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। इसमें गुण-दोष की खोज और समाधान के रचनात्मक रास्तों के अन्वेषण के लिए जनगणना को अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। हमने पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों को भी राष्ट्रीय दृष्टि और संवैधानिक जिम्मेदारी के भाव से देखने की आदत ही नहीं डाली है। बांटकर चीजों को देखने, सतही तरीके से निपटाने और परिणाम के प्रति उदासीन रहने जैसी प्रवृत्ति जनगणना पर भारी पड़ रही है। जनगणना लिपिक कार्य नहीं, राज्य की सर्वोत्तम प्रतिभा की परीक्षा की तरह होनी चाहिए।