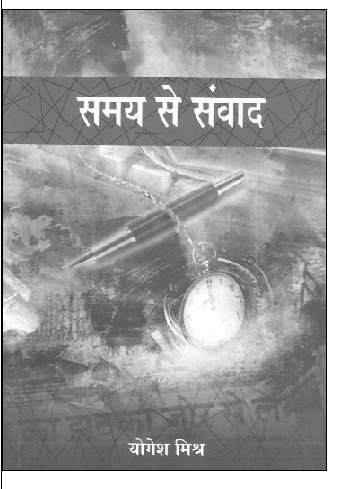समय से संवाद करने का मतलब होता है उन तमाम मसलों पर बारीक और पैनी नजर रखना, फिर बिना किसी प्रभाव में आए उसका स्पष्ट विश्लेषण करना। यह काम पेचीदा है। अपने समय में, अपने समय से बात करना ठीक वैसा ही होता है जैसे किसी व्यक्ति को खड़ा कर उसे यह बताना कि वह दरअसल कितना बुरा और कितना अच्छा है। योगेश मिश्र ऐसे ही आलोचक की भूमिका में नजर आते हैं।
अपनी पुस्तक समय से संवाद में उन्होंने अपने समय के तमाम उन मुद्दों को उठाया है, जिनसे देश को फर्क पड़ता है। चाहे वह स्त्री विमर्श और देह का मामला हो या फिर चुनाव प्रकिया का स्वरूप बदलने की बात। शिक्षा-व्यवस्था पर भी तंज किया गया है। लेखक ने एक मासूम-सा सवाल उठाया है कि आखिर हमारे बच्चे मैकाले को ही क्यों ‘फालो’ करते रहें, क्यों नहीं वे ‘ज’ से ‘जमाखोरी’ पढ़ें, क्यों ‘ज’ से जहाज पढ़ें?
योगेश मिश्र ने स्त्री विमर्श को भी कायदे से खंगाला है। वे जानना चाहते हैं कि पेज थ्री पर वे महिलाएं क्यों नहीं आ पातीं, जो सुदूर गांव में बैठ कर देश को बदलने की बात करती हैं। उन्होंने उज्जैन में बैठ कर ‘खबर लहरिया’ निकालने वाली बेहद मामूली महिला पत्रकारों का संदर्भ लेते हुए अपनी बातों को पुष्ट किया है, तो कहीं न कहीं दलितों के प्रति भी एक वाजिब जिम्मेदारी ली है।
दलित विमर्श पर उनका शोध निस्संदेह महत्त्वपूर्ण है। पुस्तक में उन्होंने भीमराव आंबेडकर का संदर्भ लेते हुए लिखा है कि मद्रास प्रेसीडेंसी के तिन्नेवली जिले की पुरादावन्नान जाति को दिन में घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं थी। कहा गया है कि सवर्ण अगर इस जाति को देख लेते थे तो उन्हें लगता था कि वे ‘अपवित्र’ हो गए हैं, इसलिए जब तक सवर्ण अपना काम-धाम करेंगे, बाहर निकलेंगे, दिनचर्या निपटाएंगे तब तक पुरादावन्नान जाति के लोग बाहर नहीं निकलेंगे। वे रात को बाहर निकलेंगे।
सवाल है कि यह तय करने का अधिकार आखिर किसी खास वर्ग के पास कहां से आया। यह आजादी किसी जाति को कहां से मिली कि वह किसी अन्य जाति या वर्ग के लोगों के जीने का तौर-तरीका तय करे। एक ही खून और एक ही हाड़-मांस का बना कोई व्यक्ति यह तय कर दे कि फलां जाति, फलां वर्ग, फलां काम नहीं करेगा तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है! लेकिन यह घटित हुआ है। इस देश के कलेजे पर काले अक्षरों में यह इतिहास हमेशा दर्ज रहेगा। लेखक के इस ज्वलंत सवाल को ढांपने का काम कौन करेगा? यह आने वाले समय में देखने वाली बात होगी।
किसी ने सही कहा है कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो… ‘समय से संवाद’ इसकी बानगी है। यह पुस्तक उन लोगों को खास तौर से पढ़नी चाहिए, जो आज भी कहीं न कहीं जातिवाद को ऊपरी माले पर रख सामाजिक न्याय तय करते हैं, जोकि केवल उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के लिए मुनासिब होता है।
ग्रामीण पत्रकारों पर कभी उस तरह निगाह नहीं गई, जिस तरह से इस पुस्तक में व्यक्त की गई है। योगेश मिश्र हमें 1947 में लेकर जाते हैं और वहां की एक घटना का जिक्र करते हैं। ‘यह सन 1947 की नजीर है। यह वह दौर था जब भारत में आजादी का आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी का सेवाग्राम यानी वर्धा आश्रम इस आंदोलन का केंद्र था। यहां भारत के सारे बड़े नेता बैठक कर रहे थे। इसी बीच नागपुर कलेक्टर का लाल पट््टे वाला चपरासी साइकिल पर सवार होकर सेवाग्राम पहुंचा, जहां उसने वहां मौजूद एक ग्रामीण पत्रकार से पूछा कि जवाहरलाल नेहरू कहां मिलेंगे? ग्रामीण पत्रकार को जिज्ञासा हुई।
उसने उल्टा सवाल दागते हुए जानना चाहा कि वजह क्या है? चपरासी बोला- कलक्टर नागपुर ने वॉयसराय की चिट््ठी भेजी है। ग्रामीण पत्रकार साइकिल से टेलीग्राफ आॅफिस जा पहुंचा और उसने एक खबर चलाई- वॉयसराय ने नेहरू को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया है। रिपोर्टर ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया। जानते हैं कि पिछली सदी की सबसे बड़ी इस खबर को एक ग्रामीण पत्रकार ने दी।’ आज बेशक ग्रामीण पत्रकार की कोई हैसियत न रह गई हो, लेकिन क्या बिना स्ट्रिंगर्स के किसी अखबार और खासकर टेलीविजन न्यूज चैनल की कल्पना की जा सकती है?
पत्रकार और पत्रकारिता से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण अध्याय इस पुस्तक में संकलित किए गए हैं, जिसमें फटाफट खबरों की दुश्वारियों से लेकर पड़ोसी मुल्क नेपाल की खबरों की पोल-पट््टी खोली गई है। नेपाल और भारत के संबंधों को लेकर एक मुकम्मल लेख इस पुस्तक में शामिल किया गया है। खासकर यह कि नेपाल को लेकर भारत की पत्रकारिता किस किस्म की है और नेपाल इस मसले पर क्या कर रहा है और करता रहा है। इसका भारत की राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर क्या असर है।
हालांकि, फटाफट खबरें और अनुवाद को लेकर किया गया लेखक का अध्ययन थोड़ी और मेहनत और समझ की दरकार अवश्य रखता है, क्योंकि जो तर्क इस पुस्तक में फटाफट खबरों और उसके अनुवाद को लेकर दिए गए हैं वह एक हद तक स्वीकार्य नहीं हो सकता।
दरअसल, न्यूज चैनलों में इस बात को तवज्जो दी जाती है कि भारत की आम जनता की भाषा क्या है। लेखक की इस बात पर आपत्ति हो सकती है कि इस देश की आम लोगों की भाषा ही हिंग्लिश है, लेकिन फिलहाल न्यूज चैनल इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि चैनलों का ‘टारगेट आॅडियंस’ यही लोग हैं।
पुस्तक में लोहिया के लोग और अगली सदी, राष्ट्रनिर्माण में युवाओं की भूमिका, व्यापक चुनाव सुधार की दरकार, राजनीति और मीडिया जैसे कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण लेखकीय दस्तावेज हैं।
अर्चना राजहंस मधुकर
समय से संवाद: योगेश मिश्र; सामयिक प्रकाशन, 3320-21, जटवाड़ा, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली; 495 रुपए।