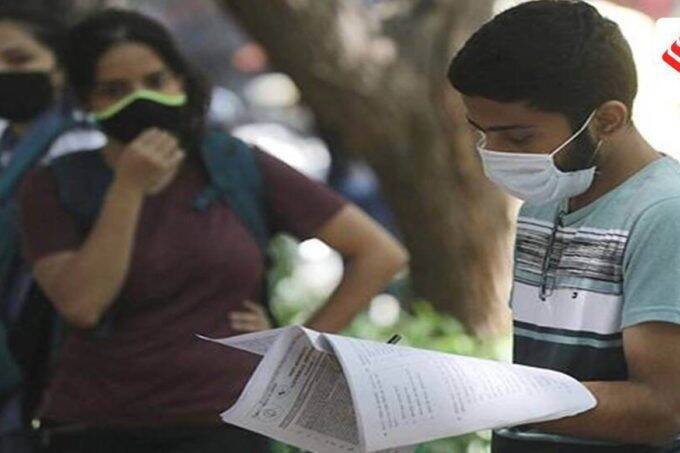केंद्र ने सरकारी मेडिकल कालेजों की सत्ताईस प्रतिशत सीटें इस सत्र से पिछड़े वर्गों के लिए और दस प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित कर दी है। कुछ लोगों का कहना है कि यह फैसला उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे महत्त्वपूर्ण राज्यों में अलगे साल होने वाले चुनावों को ध्यान में रख कर किया गया है। उनका कहना है कि यह आरक्षण पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए किया गया है। वास्तव में पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा मतदाता समूह है, जिसको हर पार्टी लुभाना चाहती है।
वोट की राजनीति से परे, यह सच है कि हमारे समाज के बड़े वर्ग को उच्च शिक्षा के अफसर उसके आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की वजह से नहीं मिल रहे हैं। आरक्षण प्राथमिक रूप में ये अफसर उनको उपलब्ध कराता है। पर किस तरह की उच्च शिक्षा, विशेषकर मेडिकल जैसे पेशेवर पाठ्यक्रमों में, आज की तारीख में उपलब्ध हैं? पहली बात तो यह है कि मेडिकल शिक्षण बहुत महंगा हो गया है। सालों साल इसकी कीमत बढ़ती गई है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी अपने बच्चे को पढ़ाना बेहद मुश्किल काम हो गया है। दूसरी तरफ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जो इतनी मोटी फीस लेते हैं कि अच्छे-खासे खाते-पीते परिवार के लिए भी अपने बच्चे का खर्चा उठा पाना एक टेढ़ी खीर है। प्राइवेट कॉलेजों में अमूमन एमबीबीएस का खर्चा एक करोड़ रुपए से ज्यादा आता है। पर सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री काफी नहीं है। विशेषज्ञता होना जरूरी है। उसका खर्चा भी लाखों में है।
प्राइवेट मेडिकल शिक्षण का एक राजस्व ढांचा है। मेडिकल कॉलेज खोलने का उद्देश्य लंबा मुनाफा कमाना है। छात्रवृत्ति लगभग न के बराबर है और फीस वसूलना साहूकार के सूद वसूलने जैसा है। साथ ही ‘कैपिटेशन फीस’ लेकर चोरी-छिपे पिछले दरवाजे से छात्र भर्ती किए जाते हैं। ये छात्र प्रवेश परीक्षा में कम नंबर आने की वजह से दाखिले से वंचित रह गए थे। मुंहमांगी कैपिटेशन फीस लेकर प्राइवेट कॉलेज धड़ल्ले से अमीर वर्गों के बच्चों को भर्ती कर लेते हैं। इन संस्थानों को सालाना कमाई चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा अर्जित हो सके। छात्र की योग्यता और सामाजिक सरोकार से इनका कोई वास्ता नहीं है।
प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे एक तजुर्बेकार अध्यापक का कहना है कि आरक्षण और ‘कैपिटेशन’ से भर्ती हुए छात्रों के चलते मेडिकल शिक्षण का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। ‘ये लोग प्रवेश तो पा जाते हैं, पर उनमें शिक्षा ग्रहण करने की योग्यता नहीं होती है। हमारे उनके बीच की खाई बहुत चौड़ी है, जिसको लांघना असंभव-सा लगता है। ऐसा नहीं है कि पिछली पीढ़ियों के सभी छात्र बहुत होशियार थे, पर कहीं न कहीं वे मेहनत करने का जज्बा रखते थे। शिक्षकों की भौं जरा-सी चढ़ी नहीं कि वे सतर्क हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है। ऐसा अक्सर होता है कि उतर पुस्तिकाएं जांचते समय मैं अपना माथा पीट लेता हूं- हाजिरी अनिवार्य होने के बावजूद वे क्लास में कुछ नहीं सीखते हैं- चेष्टा भी नहीं करते हैं सीखने की, क्योंकि जब वे भर्ती हो गए हैं, तो हमें उन्हें पास तो करना ही है। कितना ‘रिपीट’ करवाएंगे?’
शिक्षक का कहना है कि एक मेडिकल कॉलेज की उच्च स्तरीय बैठक में यह सुझाव आया था कि अगले वर्ष में जाने के लिए न्यूनतम अंकों को बढ़ा दिया जाए, जिससे छात्र पाठ्यक्रम को गंभीरता से लें। प्रस्ताव का सबसे जोरदार विरोध शिक्षकों ने किया, क्योंकि वे जानते थे कि वर्तमान में छात्र योग्यता ऐसी थी कि मुट्ठी भर छात्रों को छोड़ कर बाकी सब आजीवन पास नहीं हो पाएंगे। पैसे वाले छात्रों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। उपस्थिति कम न पड़े, इसलिए क्लास में तो आ जाते हैं, पर उनका ध्यान और चीजों में रहता है। आरक्षण से जो आते हैं, वे चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी शैक्षिक नींव बेहद कमजोर है। ऐसी स्थिति में हमारा काम यह है कि अपना लेक्चर दें और भेड़-बकरियों की तरह छात्रों को अगली कक्षा में हांक दें। पैसे के ‘टर्नओवर’ की तरह छात्रों का ‘टर्नओवर’ भी जरूरी है।
यह परेशान करने वाली स्थिति सिर्फ मेडिकल तक सीमित नहीं है। सभी प्रोफेशनल और शैक्षिक पाठ्यक्रमों का यही हाल है, क्योंकि स्कूलों से क, ख, ग की शिक्षा भी विलुप्त हो गई है। इंजीनियरिंग का छात्र हो या फिर पत्रकारिता का, अमूमन किसी को भी हिंदी या अंग्रेजी में छुट्टी का साधारण प्रार्थना-पत्र लिखना भी नहीं आता है। ऐसे में वे बी-टेक या बीए के पाठ्यक्रम से क्या लाभ उठा पाएंगे? वे सामने लिखा हुआ भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं।
पर फिर भी नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं और आइआइटी और आइआइएम कुकुरमुत्तों की तरह प्रकट हो रहे हैं। सरकार इनको खोलना अपनी बड़ी उपलब्धि मानती है। उसको इससे कोई सरोकार नहीं है कि इन उच्च शिक्षा केंद्रों में खाली काली स्लेट लिए देश का भविष्य पहुंच रहा है।