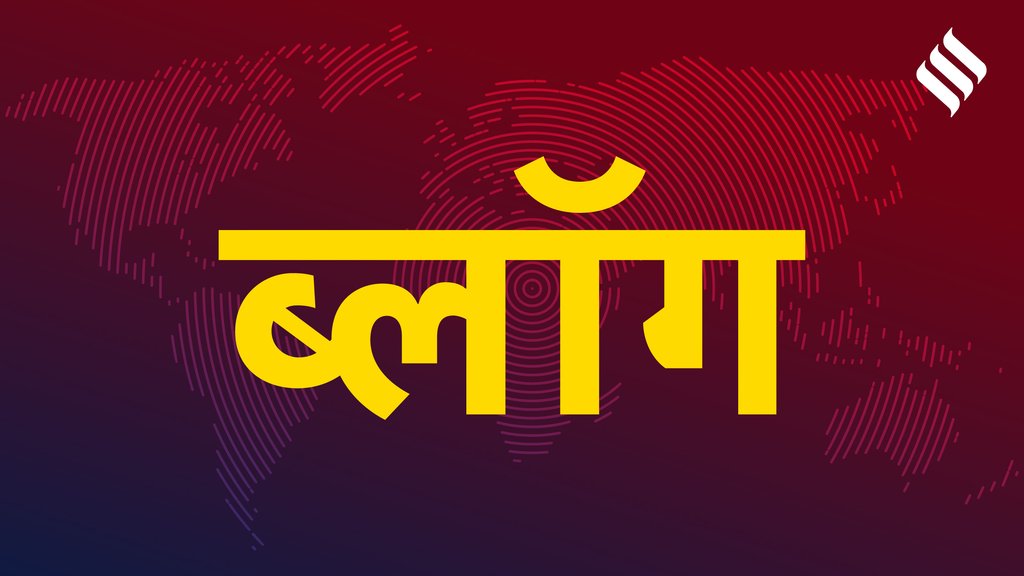भारतीय बहुभाषिकता का धरातल बहुत गहन और विस्तृत है, जो अपने लोकतांत्रिक स्वरूप में कई बार दुरूह बनकर उपस्थित होता रहा है। इसकी शुरुआत आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे के साथ हो गई थी। मगर अब यह मुखर हो चली है। एक दौर था, जब प्राय: प्रशासन में अंग्रेजी, परंपरा में संस्कृत और बाजार में हिंदी रहती थी। मगर आज भारतीय बहुभाषिकता का एक सिरा शास्त्रीय भाषाई दर्जे से जुड़ता जा रहा है, जिसमें वर्ष 2004 से तमिल के साथ शुरू हुई यह सूची 2024 तक कुल ग्यारह भाषाओं की हो गई है। इसमें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला शामिल हैं। दूसरी तरफ, आठवीं अनुसूची में भी बाईस भाषाएं हैं और इसमें विस्तार की संभावना लगातार बनी हुई है।
बांग्लादेश पहले धर्म के नाम पर फिर भाषा के नाम पर अलग हुआ
इतिहास में भाषाओं के आधार पर बनी अस्मिताएं और उनको तुष्ट करने की परंपरा रही है, जिससे इन सूचियों को कई बार शक की दृष्टि से देखा जाता है। इसमें एक ज्वलंत उदाहरण बांग्लादेश का है, जो पाकिस्तान के रूप में कभी धर्म के नाम पर अखंड भारत से विभाजित हुआ, लेकिन फिर भाषा के नाम पर पुन: अलग हुआ, लेकिन आज की स्थितियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह सब कुछ सत्ता-प्राप्ति का माध्यम भर था। आगे यह भारत में उपराष्ट्रीयताओं के संदर्भ में भी सटीक बैठता है, जिसमें तेलुगु के नाम पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, लेकिन आज उसी आंध्र प्रदेश से कट कर, तेलुगु के बावजूद, अलग राज्य तेलंगाना बन चुका है। यानी, भाषा या संस्कृति भारतीय परंपरा की थाती और सजग लोकतंत्र की बुनियाद है, जिसे महज सत्ता-प्राप्ति का साधन या गैर-जिम्मेदारी से प्रबंधित नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा सिर्फ पूंजी के आधार पर अगर देश सफल होते तो अमेरिका में उन मानसिकताओं का कोई स्थान नहीं होता, जिसमें एक व्यक्ति अचानक उठकर भरे बाजार बंदूक चलाने लगता है।
नई चुनौती डिजिटल संसार भी है, जो एक माध्यम भी है और बाजार भी
भारतीय प्रशासनिक तंत्र ने भाषाओं के आधार पर भूगोल और समाज बांटने का काम किया। यहां तक कि वर्ष 2009-10 में भारतीय भाषाओं के सर्वेक्षण के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज किया कि इससे देश की एकता को खतरा होगा। बहुभाषिकता एक प्रबंधन की चीज है और किसी लोकतंत्र में यह अधिक संवेदनशील हो जाती है, उसे महज चलताऊ ढंग से टाला नहीं जा सकता। इसमें मातृभाषा से लेकर राजभाषा तक और मनोरंजन की भाषा से लेकर ज्ञान की भाषा तक भूमिका में सरकारों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। इस क्रम में नई चुनौती डिजिटल संसार भी है, जो एक माध्यम भी है और बाजार भी। इस क्रम में उचित है कि भाषाओं को लेकर बाजार भी सक्रिय है और सरकार भी। दोनों के अपने तरीके हैं, लेकिन दोनों अपनी अभूतपूर्व भूमिका में हैं। एक तरफ कृत्रिम मेधा से लेकर गूगल सहित अनेक कंपनियां सक्रिय हैं, तो वहीं ‘भाषिनी’ नामक मशीनी अनुवाद टूल के साथ सरकार भी अपनी बहुभाषिकता को गंभीरता से देख रही है।
जनजातीय और अल्पसंख्यक भाषाओं पर खतरे की चिंता एक दशक पुरानी है। इनके संरक्षण की व्यवस्थागत पहल भी देश में जो प्रयास हुए वे अच्छे माने गए हैं, बल्कि एनसीईआरटी द्वारा जनसंख्या आंकड़ों में दर्ज सभी अल्पसंख्यक/ गैर-अनुसूचित भाषाओं, वर्णमाला की पुस्तकें तैयार की जा रहीं हैं। मगर भारतीय भाषा संस्थान के भाषा सर्वेक्षण के प्रस्ताव को तब यानी 2009-10 में मान लिया गया होता, तो आज बहुभाषिकता और बेहतर ढंग से प्रबंधित होती।
इधर भोजपुरी का जो उभार सतह पर दिख रहा है, वह अनेक भाषाओं के प्रबंधन के लिए अनुकरणीय हो सकती है। वर्ष 2012 में तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री ने जब प्रदेश, दल और विचारधारा से ऊपर उठकर संसद में सभी भोजपुरीभाषी सांसदों ने अपनी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग रखी, तो जवाब उन्होंने इसी भाषा के एक वाक्य- ‘हम रउआ सबके भावना समझतानी’ से दिया। मगर उन्होंने उस मांग पर किया कुछ नहीं।
वर्ष 2011 में जनसंख्या के आंकड़ों में भोजपुरी भाषियों की संख्या पांच करोड़ से ऊपर है, जो न सिर्फ हिंदी के अंतर्गत दर्ज किसी भी बोली/ भाषा से ऊपर है, बल्कि यह संख्या देश की अनेक उन भाषाओं से ऊपर है, जो सरकारी आंकड़ों में सम्मान पा रही हैं और इधर भोजपुरी को वांछित सम्मान नहीं मिला है। मगर इस स्थिति में बदलाव डिजिटल संसार में बड़ी तेजी से हो रहा है। सरकार ने भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने लायक नहीं समझा, लेकिन गूगल ने इसमें मशीनी अनुवाद को विकसित कर दिया है। इधर डिजिटल मीडिया को लेकर फिक्की द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि वर्ष 2023 में टीवी दर्शक के रूप में भोजपुरीभाषी न सिर्फ अंग्रेजी, बांग्ला, ओड़िया, मलयालम से कई गुना आगे हैं, बल्कि पंजाबी, तेलुगु, मराठी और तमिल के बराबर हैं। इसका संगीत, फिल्म उद्योग डिजिटल मीडिया के माध्यम से लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसमें देश के सभी भाषा-भाषियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।
इसके आगे बढ़ने का एक कारण यह भी है कि संख्या के मामले में आगे है और तमाम शास्त्रीय और संवैधानिक भाषाओं से ऊपर है, इसलिए मौजूदा सरकार से यह उम्मीद स्वाभाविक है कि दूसरी योग्य भाषाओं के साथ इसे भी आठवीं अनुसूची में स्थान दिलाए। भाषा के प्रबंधन का एक सच यह है कि किसी बहुभाषिकता में सभी भाषाओं पर समान ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन यह स्थिति जब किसी राष्ट्र के निर्माण से जुड़ी हो, तो शासन को एक स्पष्ट दृष्टि मिल जाती है। ध्यान रहे कि भाषा का मूल कर्म ही लोगों को जोड़ना होता है और इस जुड़ाव का भी उद्देश्य देश से परे नहीं है। लेकिन यह भी जरूरी है कि सभी भाषाओं के साथ एक न्यायपूर्ण व्यवहार हो और कोई भाषा या संस्कृति को अकेला न छोड़ दिया जाए।