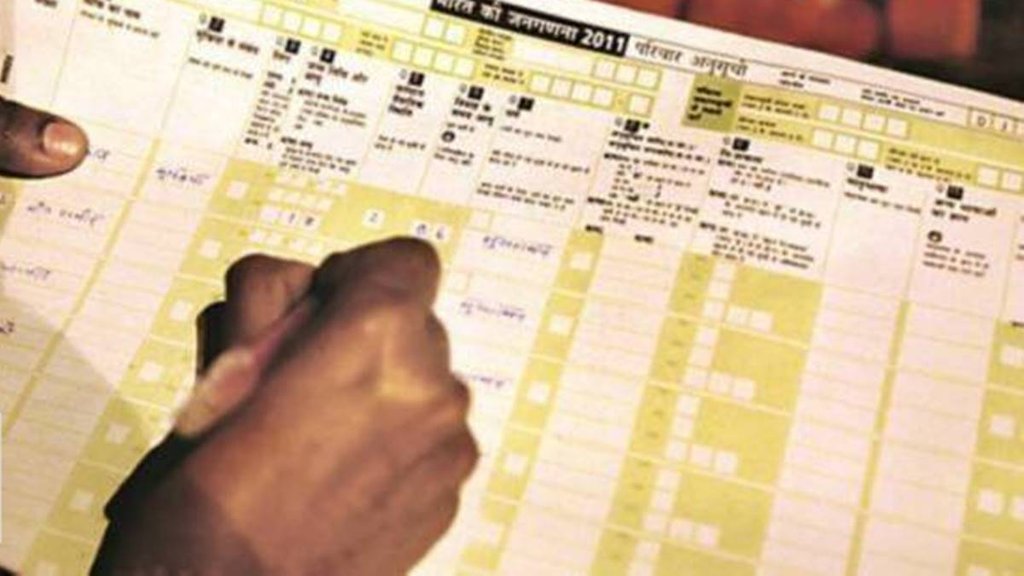राकेश सिन्हा
जाति विमर्श बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है। कुछ इस हद तक कि जातीय पहचान सार्वजनिक जीवन में अनिवार्यता की तरह हो गई है। एक समय था, जब ऐसा करना लोकतंत्र के लिए अनैतिकता की तरह था। पर अब इसमें राजनीतिक नैतिकता का बोध कराया जा रहा है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी कोने से इसका निषेध करने वाली आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। जाति-विहीन समाज की बात करने वाले गैर-राजनीतिक और अव्यावहारिक माने जाने लगे हैं।
किसी भी ऐतिहासिक समाज में, जिसका ठोस दावा बिहार के पास है, यह एक अत्यंत संकट की स्थिति है। आजादी के बाद से बिहार ने लोकतंत्र के सर्वोच्च मूल्यों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया था। ऐसा नहीं कि चुनाव में जाति का महत्त्व नहीं था, पर व्यक्ति की गुणात्मकता और विचार की ताकत ने जाति की भूमिका को असीमित, अमर्यादित और सुनामी बनने नहीं दिया था। तभी तो कर्पूरी ठाकुर जातीय सीमाओं से पार सम्मान और समर्थन हासिल करते रहे।
कई बड़े नेता बिहार से थे या बिहार उनकी कर्मभूमि बनी
दो वैचारिक दलों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ के शीर्ष नेता बंगाली थे। विजय कुमार मित्रा जनसंघ से, तो जगन्नाथ सरकार और सुनील मुखर्जी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनावों का इतिहास भी बिहार के लोगों के मूल पिंड को दर्शाता है। मधुलिमये बिहारी नहीं थे, पर वे बिहार से चार बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। दो बार मुंगेर से और दो बार बांका से। आचार्य जेबी कृपलानी सिंधी थे। वे भी दो बार बिहार से लोकसभा के लिए चुने गए थे। एक बार भागलपुर से तो दूसरी बार 1957 में सीतामढ़ी से। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। गुजरात के अशोक मेहता मुजफ्फरपुर से चुनाव जीते थे। इसी लोकसभा क्षेत्र से जार्ज फर्नांडीज पांच बार चुनाव जीते। श्यामानंद मिश्रा का संबंध नेपाल से था। शिक्षा पटना में हुई। वे भी बिहार से दो बार लोकसभा पहुंचे।
आधुनिकता के साथ लोकतंत्र का क्षरण हुआ है। जातिबोध लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संस्थाओं पर हावी हो गया। कुछ इस हद तक कि ‘समाज’ का अर्थ हर व्यक्ति के लिए उसकी जाति बन गई है। हालांकि यह बीमारी पचास के दशक में भी थी, पर इसके संक्रमण को रोकने वाली ताकतें भी मौजूद थीं। इस संदर्भ में बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह और जयप्रकाश नारायण के बीच पत्राचार उल्लेखनीय है। जेपी ने श्रीकृष्ण सिंह को आगाह किया था कि शासन-व्यवस्था किसी जाति विशेष से चिह्नित नहीं होनी चाहिए, तो श्रीकृष्ण सिंह ने जेपी पर ‘कदमकुआं ब्रेन ट्रस्ट’ द्वारा संचालित होने का आरोप लगाया था। दोनों का उद्देश्य लोकतंत्र के अवमूल्यन को रोकना था। प्रकारांतर से आलोचनात्मक विमर्श की परंपरा प्राय: मृतप्राय हो चुकी है। इसके बिना जन-प्रबोधन की कल्पना नहीं कर सकते।
आखिर यह सब कैसे और क्यों हो रहा है? इसके जवाब में वर्तमान संकट का समाधान भी छिपा हुआ है। इसका एक बड़ा और महत्त्वपूर्ण कारण प्रतिनिधित्व के प्रश्न को विचार के धरातल से उठा कर पहचान के धरातल पर ले आना है। ऐसा नहीं कि गैर-समानुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न पहले नहीं उठा है। 1930 के दशक में त्रिवेणी संघ नामक संगठन का जन्म इसी प्रश्न को लेकर हुआ। बाद में सोशलिस्ट नेता राममनोहर लोहिया ने सबलता से इसे आगे बढ़ाया। पर यह सब लोकतांत्रिक शैली और मर्यादा की परिधि में होता रहा।
राजनीति में विचारों की गिरावट ने शून्यता को जन्म दिया, जिसने जातीय कुलीनों को भरपूर अवसर दिया। अत्यंत व्यवस्थित तरीके से जनता का जातीय ध्रुवीकरण कराया जाता रहा और कल तक प्रतिरोध करने वाले भी इसी आसान रास्ते का पथिक बनने में अपना उज्ज्वल भविष्य तलाशने लगे। अपनी सर्वसमावेशी और जातिविहीन पात्रता को खोकर राजनीतिक सुधार के नायक नहीं बन सकते हैं।
जब-जब निष्कलंकित पात्रता खड़ी हुई, लोगों ने संकीर्णताओं से ऊपर उठ कर राष्ट्रीय चरित्र का परिचय दिया। इसके अनेक उदाहरण चुनावी राजनीति में देखे जा सकते हैं। जयप्रकाश नारायण की जाति ने उनकी लोकतांत्रिक उपयोगिता और उसके प्रभाव को कम नहीं होने दिया और वे 1974 के छात्र आंदोलन के नायक बने। पिछले वर्ष विनोबा भावे के पवनार आश्रम गया था।
विनोबा के अनुयायियों के मन में बिहार की श्रेष्ठ तस्वीर थी। उनमें एक चौरासी वर्षीय गौतम बजाज ने कहा, ‘बिहार का बाबा और बाबा (विनोबा) का बिहारी’। जब कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि विनोबा के भूदान यज्ञ को बिहार में अभूतपूर्व सफलता मिली थी। दूसरी तरफ बिहार को ही सर्वप्रथम जमींदारी उन्मूलन जैसे प्रगतिशील निर्णय का भी श्रेय प्राप्त है। पर सामाजिक संगठनों की आंतरिक दुर्बलता और राजनीति में हस्तक्षेप करने की क्षमता के ह्रास ने राजनीति को सामाजिक मनोविज्ञान निर्माण का एकाधिकार दे दिया है।
इस एकाधिकार को चुनौती देना कठिन नहीं है। बिहार की अपनी विरासत ही बदलाव के लिए यथेष्ट है। राजनीति लोगों का विरासत से विच्छेद नहीं कर पाई है। यही सबसे बड़ी पूंजी है। जातीय कुलीनों ने सार्वजनिक जीवन की सभी न्यूनताओं को अपयश का कारण नहीं माना है। आम जनता इस व्याधि से मुक्ति का रास्ता ढूंढ़ रही है। इसलिए जातीय राजनीति स्थायीत्व और वैधानिकता का दावा करने में पूरी तरह से अक्षम है।
लोकतंत्र सिर्फ चुनावी खेल नहीं है। इसका सांस्कृतिक पक्ष भी है। जिस समाज की सांस्कृतिक चेतना जितनी सबल होती है, लोकतंत्र उतना ही समृद्ध होता है। इसलिए विघटनकारी राजनीति सांस्कृतिक चेतना को प्रदूषित करती है। देवताओं, ऋषियों, मुनियों, स्वतंत्रता सेनानियों, साहित्यकारों को जाति-बिरादरी की शोभा बढ़ाने वाला, जातीय राजनीति को सम्मानित करने वाला उपकरण बना दिया जाता है। तात्कालिकता की यह राजनीति दीर्घकालिकता की चिंता नहीं करती है।
सांस्कृतिक चेतना को उभारने वाले सभी तत्त्वों की उपेक्षा की जाती है। बिहार स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी रहा है। पर, इतिहास की पुस्तकों में इस भूमिका के स्वर को पीढ़ियों को प्रेरित करने वाले की जगह निष्प्रभावी बना कर प्रस्तुत किया गया है। दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था। उसके साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी था। इन संस्थाओं ने भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया। पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपने स्वर्णिम योगदान की विरासत से विमुख रही है।
आर्यभट्ट से मंडन मिश्र तक और बोधगया से लेकर वैशाली तक का इतिहास विज्ञान, अध्यात्म और चेतना का इतिहास रहा है। वह सब सामान्य ज्ञान बन कर रह गया है। जो समाज अपने इतिहास को पीढ़ियों के सामने नहीं रख पाता है, वह अपनी विरासत की श्रेष्ठता का लाभ स्थांतरित भी नहीं कर पाता है।
ऐसा नहीं कि उसे संजो कर भविष्य के लिए रखने वाले नहीं हैं। इसका एक उदाहरण नवादा जिले में ‘सत्याग्रह आश्रम’ है, जो जयप्रकाश नारायण की गतिविधियों का दशकों तक केंद्र रहा है। स्थानीय लोग जाति-पंथ की सीमाओं से ऊपर उठ कर उन मूल्यों को उस आश्रम के माध्यम से इस आशा से संजोकर रखे हुए हैं कि भविष्य में यही चिंगारी नए बिहार की रचना का कारण बनेगी।
बिहार के लिच्छवी का लोकतंत्र प्राचीन ग्रीक के लोकतंत्र से पुराना है। भारत के लोकतंत्र का इतिहास इससे जुड़ा है। इसके प्राचीन इतिहास में धर्म चेतना ने सत्ता सरोकार को पीछे छोड़ दिया है। स्वयं चंद्रगुप्त जैन धर्म से प्रभावित होकर भद्रबाहु से दीक्षा लेकर दक्षिण (कर्नाटक) के चंद्रगिरि पहाड़ियों पर शेष समय व्यतीत किया, तो अशोक बौद्ध धर्म की शरण में रहा।
वर्तमान की सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रिया न तो विरासत और न ही आधुनिकता से मेल खाती है। इसने विखंडित और परस्पर कटुता आधारित सामाजिक जीवन को जन्म दिया है। जिसमें आदर्श बनने की क्षमता है, वह अपवाद बन कर रह गया है।
(लेखक भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं)