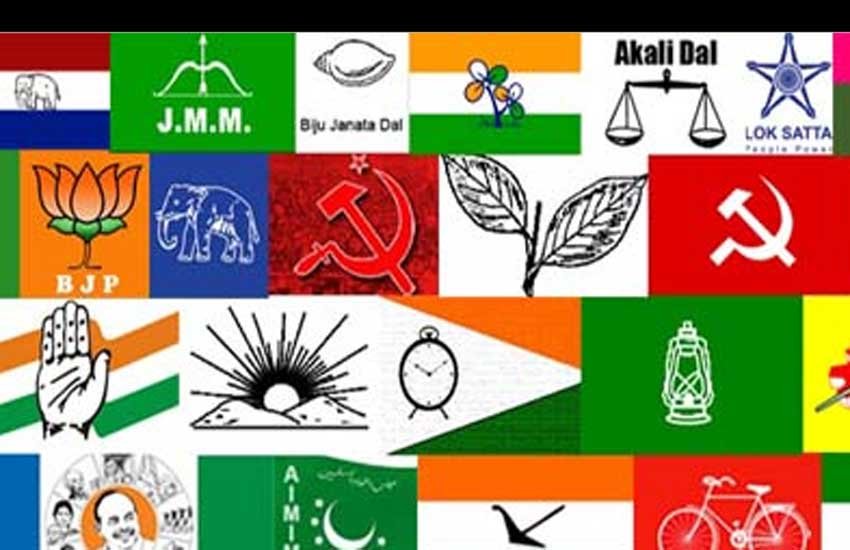चुनाव सुधार पर बरसों से चली आ रही बहस के बावजूद राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का चरित्र ज्यों का त्यों है। पांच बड़े दलों ने चुनाव आयोग में जो ताजा जानकारी दाखिल की है उसके अनुसार उन्हें मिले चंदे का 92.61 प्रतिशत पैसा चंद बड़े कॉरपोरेट-औद्योगिक घरानों, ट्रस्टों और धनी लोगों से आया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को वर्ष 2014-15 में प्राप्त चंदे की रकम से पता चलता है कि हमारे देश के अधिकतर दल उद्योगों और पैसे वाले लोगों की ‘मेहरबानी’ पर निर्भर हैं, क्योंकि उनके खजाने में आम आदमी से मिलने वाली रकम का हिस्सा महज 7.27 फीसद है।
राजनीति में काले धन के बढ़ते प्रभाव का आरोप बेमतलब नहीं लगता है। पिछले वित्तवर्ष में उक्त दलों ने 22.85 प्रतिशत चंदे का कोई विस्तृत विवरण दाखिल नहीं किया। इस मामले में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है। उसने कुल 141.46 करोड़ रुपए का चंदा दिखाया, जिसमें से 138.98 करोड़ रुपए (98 प्रतिशत) का कोई चैक या डिमांड ड्राफ्ट नंबर नहीं दिया गया। सत्तारूढ़ भाजपा ने भी बीस दानदाताओं से मिली 83.81 लाख रुपए की रकम के साथ पैन नंबर नहीं दिया है। जन प्रतिनिधित्व कानून-1951 के अनुसार हर राजनीतिक दल को बीस हजार रुपए से ज्यादा के चंदे का विस्तृत ब्योरा चुनाव आयोग के पास दाखिल करना चाहिए। ऐसा करने पर ही उन्हें आयकर विभाग शत-प्रतिशत छूट देता है। बहुजन समाज पार्टी को छोड़ शेष सभी राष्ट्रीय दल हर साल कॉरपोरेट से मिले चंदे की जानकारी देने की खानापूर्ति करते हैं।
बसपा तो यह जहमत भी नहीं उठाती। पार्टी के अनुसार पिछले दस साल में उसे एक भी चंदा बीस हजार से ऊपर का नहीं मिला है। यह दावा शायद ही किसी के गले उतरे। यह तथ्य जगजाहिर है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, सर्वाधिक चंदा उसी को मिलता है। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, सो सबसे ज्यादा चंदा भी उसे ही मिला है। पिछले वर्ष पांच बड़े दलों को कुल 622.38 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जिसमें अकेले भाजपा की हिस्सेदारी 437.35 करोड़ रुपए थी। मतलब यह कि बाकी चार पार्टियों को मिलकर जितना पैसा मिला, भाजपा ने अकेले उससे अधिक उगाहा। उसे मिले चंदे में कॉरपोरेट का हिस्सा 94 फीसद है, जो औसत (92.61 प्रतिशत) से ऊपर है।
मुंबई देश की व्यावसायिक राजधानी है, इस कारण राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने में भी वह अव्वल है। चंदे में उसका योगदान बयालीस प्रतिशत (262.5 करोड़ रुपए) रहा। दूसरा स्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहराज्य गुजरात का है, जहां से राजनीतिक दलों को चार फीसद (24.76 करोड़ रुपए) पैसा मिला। दिल्ली तीसरे नंबर पर है, वहां से दो प्रतिशत (15.34 करोड़ रुपए) चंदा आया। चंदा देने में भारती समूह का सत्य एलेक्ट्रोरल ग्रुप सबसे ऊपर है, जिसने बीते वित्तवर्ष में भाजपा को 107.25 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 18.75 करोड़ रुपए तथा राकांपा को छह करोड़ रुपए दिए।
एक और दिलचस्प बात है। जिस साल आम चुनाव या विधानसभा चुनाव होते हैं, उस साल राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में अचानक उछाल आ जाता है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के बाद छह विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। इसीलिए वर्ष 2013-14 में जहां भाजपा को मिले चंदे की रकम 170.86 करोड़ रुपए थी, वहीं वर्ष 2014-15 में यह बढ़ कर 437.35 करोड़ रुपए हो गई। एक साल में 156 फीसद इजाफा हुआ। इस अवधि में कांग्रेस को मिला चंदा 59.58 से बढ़ कर अचानक 141.46 करोड़ रुपए (137 प्रतिशित वृद्धि) तथा राकांपा का चंदा 14.02 से बढ़ कर 38.38 करोड़ रुपए (177 प्रतिशत वृद्धि) हो गया। ये आंकड़े देख कर तो साफ पता चलता है कि कॉरपोरेट के पैसे के बल पर ही हमारे देश के सारे बड़े दल चुनाव लड़ते हैं।
भारतीय राजनीति में पैसे के बढ़ते दुष्प्रभाव के कारण ही आज अच्छे और ईमानदार लोगों के लिए चुनाव लड़ना और जीतना लगभग असंभव हो गया है। वैसे तो देश का संविधान प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है लेकिन सच्चाई यह है कि आज कुछ सैकड़ा लोग और चुनिंदा राजनीतिक दल ही चुनाव लड़ने की हैसियत रखते हैं। शेष जनता केवल वोट डालने की रस्म निभाती है। लोकसभा चुनाव में अब कानूनन अधिकतम खर्च की सीमा सत्तर लाख रुपए कर दी गई है। इतना पैसा गरीब तो क्या उच्च मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी पूरी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी करने के बाद नहीं बचा पाता। ऐसे में वह चुनाव लड़ने की कल्पना कैसे कर सकता है? 1991 में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था की डगर छोड़ खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया। कोटा-परमिट राज खत्म हुआ। उद्योग-धंधे फले-फूले, भारी मात्रा में निवेश आया। इसके साथ ही राजनीति के गलियारों में कॉरपोरेट का प्रभाव बढ़ता गया।
विकास के साथ-साथ देश में आय का वितरण और असमान हो गया। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का दौर चला, जिसकी कोख से कई घोटालों का जन्म हुआ। सरकार ने निजी कंपनियों के लिए बाजार तो खोल दिया, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने के लिए न तो नियम-कायदे बनाए और न ही पारदर्शी नीतियां अपनार्इं। रातोंरात मुनाफा कमाने की नीयत से कॉरपोरेट जगत के कुछ सूरमाओं ने राजनीतिक दलों और बड़े नेताओं से नजदीकी रिश्ते बनाए। सत्ता के गलियारों में पैठ बनाने के लिए अनोखी जन-संपर्क नीति गढ़ी गई। राडिया टेप से कॉरपोरेट जगत और सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के बीच हुई दुरभिसंधियों का पर्दाफाश हुआ। तभी मौजूदा राजनीति पर पैसे की काली परछार्इं साफ देखी जा सकती है। संसद और विधानसभाओं में करोड़पति-अरबपति जनप्रतिनिधियों की संख्या में चिंताजनक स्तर तक इजाफा हो चुका है।
चुनाव में काले धन का खुल कर इस्तेमाल होता है। इसी वजह से राजनीतिक दल और नेता अपने चंदे का स्रोत बताने को राजी नहीं हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी राष्ट्रीय दलों को सूचनाधिकार कानून के तहत लाने का फैसला सुनाया था, जिस पर आज तक अमल नहीं हो पाया है। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने में अधिकतर दलों की कोई रुचि नहीं है। ज्यादातर पार्टियां और नेता काले पैसे के बूते ही चुनाव लड़ते और जीतते हैं। उन्होंने मौजूदा कानून से बचने के रास्ते भी खोज रखे हैं। सुधार के लिए सबसे पहले 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति गठित की गई थी।
इसके बाद 1993 में वोहरा समिति तथा 1998 में इंद्रजीत गुप्त समिति ने चुनाव व्यवस्था में सुधार के लिए महत्त्वपूर्ण सिफारिशें कीं। विधि आयोग और चुनाव आयोग भी समय-समय पर कारगर सुझाव देते रहे हैं। ये सभी रिपोर्टें और समस्त सुझाव बरसों से सरकारी दफ्तरों में धूल फांक रहे हैं। अदालत से सजा-प्राप्त जनप्रतिनिधियों की संसद और विधानसभा सदस्यता समाप्त करने तथा उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने का कानून भी सर्वोच्च न्यायालय की कृपा से बना है। सरकार ने तो इस कानून में फच्चर फंसाने की पूरी तैयारी कर ली थी, पर प्रबल जन-विरोध को देख कर उसे अपना कदम पीछे खींचना पड़ा।
चुनावों को काले धन के कुचक्र से बाहर निकालने के लिए चुनिंदा राजनीतिक बुद्धिजीवी, न्यायविद, शिक्षाविद और सिविल सोसायटी के लोग वर्षों से प्रयासरत हैं लेकिन सरकार के कान पर अब तक जून नहीं रेंगी है। कुछ बड़े दल और प्रभावशाली नेता इस सुझाव के प्रबल विरोधी हैं। उन्हें लगता है यदि राज्य की मदद मिलने लगी तो चुनाव लड़ने का उनका एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। जिस देश की एक चौथाई आबादी कंगाली की रेखा से नीचे हो, वहां लाखों और अधिकतर मामलों में करोड़ों रुपए खर्च कर चुनाव लड़ना संपन्न तबके का शगल ही समझा जाएगा। आज आम आदमी वोट तो दे सकता है, चुनाव में खड़े होने या जीतने का सपना नहीं देख सकता। चुनाव लड़ने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना उसकी सात पुश्तें भी नहीं कमा सकतीं। लोकतंत्र को धन से मुक्त कराने के लिए दुनिया के इकहत्तर देशों में सरकारी खर्च (स्टेट फंडिंग) व्यवस्था लागू है।
राजनीति सेवा नहीं, पैसा कमाने का जरिया बन गई है। अब हर पार्टी और बड़े नेताओं के अपने चहेते उद्योगपति और कॉरपोरेट घराने हैं जो उनके लिए चुनावों में खुले हाथ से पैसा फूंकते हैं। हवा का रुख भांप कर कुछ घराने पाला भी बदलते हैं। चंद बरस पहले तक सारा खेल परदे के पीछे होता था, अब खुल्लमखुल्ला होने लगा है। चुनावों पर कॉरपोरेट घरानों की राजनीतिक खेमेबंदी का असर दूर से ही दिखाई पड़ जाता है। अगर कोई घराना किसी एक पार्टी का साथ देता है तो दूसरा दल उसका कच्चा चिट्ठा खोल देता है। यह काम सार्वजनिक मंच से होने लगा है।
जिस हिसाब से चुनावी खर्च बढ़ रहा है उसे देख कर लगता है कि भविष्य में क्षेत्रीय और छोटी पार्टियों के लिए अपना अस्तित्व बचाना कठिन हो जाएगा। बड़ी पार्टियां अपने धन के बल पर छोटे दलों को निगल जाएंगी। हमारे यहां भी यूरोपीय देशों और अमेरिका की तरह दो-तीन दल बचेंगे। यह व्यवस्था कॉरपोरेट जगत को भाती है। चुनिंदा दलों और नेताओं को ‘मैनेज’ करना उनके लिए आसान होता है। ऐसी स्थिति में वे अपनी मर्जी से सरकार और नेताओं की अदला-बदली करते रहते हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों में पूरा कॉरपोरेट जगत और मीडिया पार्टी लाइन पर बंटा हुआ है। जिसकी पार्टी जीत जाती है उसकी पौ बारह हो जाती है। हमारे देश में भी यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।