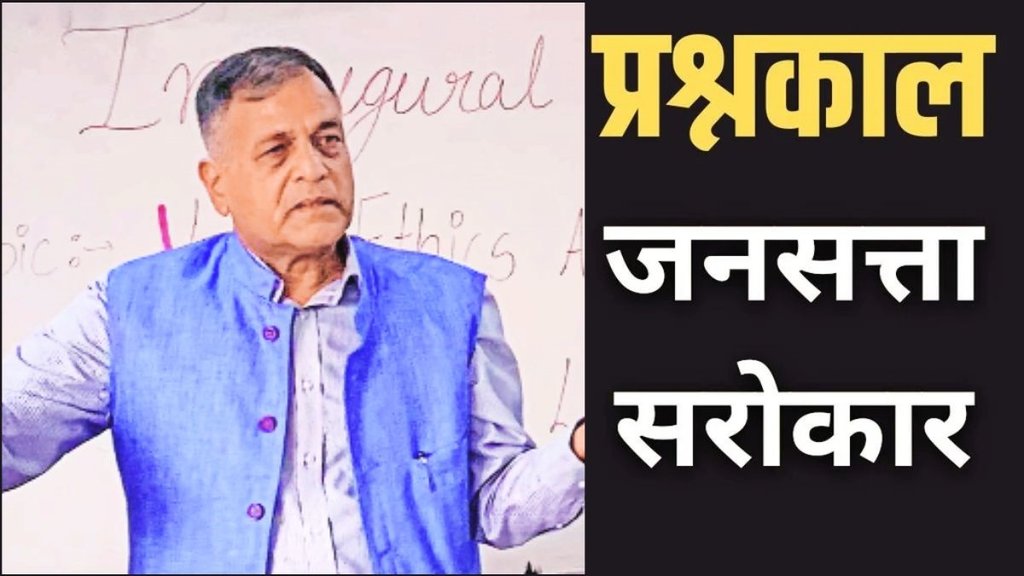पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का कहना है कि किसी भी संस्था के लिए पारदर्शिता अपने आप में कई समस्याओं का समाधान है। पारदर्शिता में कमी दिखते ही आप पर सवाल उठते हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद के दौरान चुनाव आयोग को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने कहा कि मूल समस्या की जड़ में चुनाव आयोग के द्वारा नागरिकता की अवधारणा को ले आना है। लवासा का कहना है कि एक दफ्तरी प्रक्रिया से जब किसी के संवैधानिक अधिकारों पर खतरा पैदा होता दिखा तो लोगों के बीच आशंकाओं ने जन्म लिया। बिहार में चुनाव नजदीक नहीं होते तो वहां के भी नागरिकों में इस तरह का डर पैदा नहीं होता। अशोक लवासा के साथ कार्यकारी संपादक मुकेश भारद्वाज की बातचीत के चुनिंदा अंश।
चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान के आप हिस्सा रहे हैं। बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के शुरू होते ही एक सियासी हंगामा मच गया। सबसे ज्यादा सवाल समय को लेकर हुए। विशेष गहन पुनरीक्षण के शाब्दिक अर्थ पर जोर देते हुए मेरा सवाल है कि क्या बिहार में इसके लिए पर्याप्त समय था?
अशोक लवासा: समय पर्याप्त था या नहीं, इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अगर 2003 में बिहार में हुई पिछली गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को देखें तो उसके आधिकारिक आंकड़े सार्वजनिक मंचों पर नहीं हैं। इसलिए इसकी तुलना करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछली बार साढ़े आठ महीने दिए गए थे और इस बार शायद साढ़े तीन महीने दिए गए हैं। हालांकि अलग-अलग चरणों पर गणना प्रपत्र जमा करवाने का समय उतना ही दिया गया है जो नियमों में उद्धृत है। कुल मिलाकर जो आपत्ति निवारण का समय है उसे भी देखना होगा। तयशुदा समय में आपकी आपत्तियां दूर हो सकती हैं या नहीं? यह सवाल इस संदर्भ में अहमियत रखता है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। पिछले गहन पुनरीक्षण के समय में आम चुनाव भी एक साल बाद होने वाले थे। और बिहार विधानसभा चुनाव तो दो साल बाद यानी 2005 में होने वाले थे। बाकी प्रदेशों में जहां ये लागू होने वाला है वहां इस तरह की दहशत या हंगामा नहीं है कि कोई नागरिक सोचे कि मेरे वोट का अधिकार छिन जाएगा या मैं वोट नहीं डाल पाऊंगा। चुनाव आयोग अपनी आम प्रक्रिया से भी काम कर सकता था जिसमें नाम काटे भी जा सकते हैं, नाम जोड़े भी जा सकते हैं और त्रुटियों को भी ठीक कर सकते हैं।
एक आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि बीता लोकसभा चुनाव इसी मतदाता सूची पर हुआ था। अब इसमें से 65 लाख मतदाताओं का नाम हटा दिया गया है। यानी ये किसी न किसी तरह अवैध थे। विपक्ष के सवाल उठाने के बाद आम लोगों के बीच उठी इस शंका पर क्या कहेंगे?
अशोक लवासा: देखिए, आज की तारीख में करीब 99 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 97 करोड़ मतदाता थे। उनमें से 65 या 66 फीसद के करीब लोगों ने मतदान किया। इसका मतलब यह नहीं है कि सारे 99 या 97 करोड़ लोगों ने मतदान किया। इसका मतदाता सूची से कोई सीधा संबंध नहीं है। मतदाता सूची का त्रुटिरहित होना जरूरी है। लेकिन इसके आधार पर आप कोई राष्ट्रीय खाका नहीं खींच सकते कि किसको कितने वोट मिले?
पिछले दिनों चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम मतदाता सूची साझा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो क्या ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान है जो चुनाव आयोग को अधिकार देता है सूचना की साझेदारी नहीं करने का?
अशोक लवासा: मतदाता सूची को साझा करने में कभी कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। हमेशा से प्रथा रही है कि मसविदा और अंतिम चरण दोनों में मतदाता सूची तैयार होने के बाद राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती रही है। यह वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहती है। इच्छुक व्यक्ति इसमें अपना नाम देख सकता है। बाकी जो आपने विशेष तौर पर बात कही कि चुनाव आयोग को अदालत ने कहा कि 65 लाख लोगों के नाम जाहिर करें तो आयोग ने बड़ा तकनीकी रुख लिया। आयोग ने तर्क दिया कि हम 65 लाख लोगों को ‘डिलीट’ नहीं कर रहे। नाम विलोपित करने पर हम कानूनी रूप से बाध्य हैं उन्हें सामने लाने के लिए। लेकिन हमने तो उन्हें मतदाता सूची में शामिल ही नहीं किया। मतलब 18 साल से ऊपर के जितने भी योग्य मतदाता हैं और उनका नाम सूची में नहीं है तो चुनाव आयोग यह सूची तो नहीं निकालता कि आप लोगों का नाम इसमें नहीं है। मुझे लगता है कि आयोग ने जो यह तकनीकी रुख लिया इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मतदाता सूची में किसी का नाम पहले से था और किसी वजह से आप उनका नाम सम्मिलित नहीं कर रहे हैं तो वे नाम और कारण बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने तो अंतत: यही कहा कि कारण सहित हटाए गए नामों की सूची वेबसाइट पर डालें और सार्वजनिक जगहों पर लगाएं ताकि प्रभावित लोगों की पहुंच उस तक हो पाए।
आरोप है कि बिहार का एसआइआर एक मतदाता के लिए कम, एक नागरिक के लिए ज्यादा है। क्या यह सूची भारत के नागरिक होने का प्रमाणपत्र तय कर रही है? क्या यह चुनाव आयोग के दायरे में है?
अशोक लवासा: संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि 18 साल से ऊपर का भारत का नागरिक जो किसी अन्य कारण से अयोग्य घोषित नहीं हुआ हो वह मतदाता बन सकता है। अब चुनाव आयोग कहेगा कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि भारत के नागरिक को ही मताधिकार दूं। पिछले 74 वर्षों से चुनाव आयोग ने यही प्रक्रिया बनाई कि आप एक फार्म पर भारत के नागरिक होने का शपथपत्र देकर मतदाता सूची में जोड़े जाने के लिए आवेदन देते हैं। उसके बाद आयोग दस्तावेजों के आधार पर तसल्ली करता है कि आपकी सारी योग्यताएं सही हैं। यह पहली बार है कि नागरिकता वाली बात उल्लेखनीय हो गई। सारे विवाद की जड़ में 24 जून 2025 को आया चुनाव आयोग का सूचनापत्र है। इसमें आयोग ने मतदाताओं को दो हिस्सों में बांट दिया, 2003 से पहले और उसके बाद वाले। 2003 के पहले वालों के बारे में पहली बार चुनाव आयोग ने ‘पात्रता का प्रमाणात्मक साक्ष्य व नागरिकता की धारणा’ शब्द का इस्तेमाल किया। इसका अर्थ यह निकला कि जो 2003 वाले मतदाता हैं वे तो नागरिक हैं लेकिन 2003 के बाद वाले जब तक तय दस्तावेजों के साथ फार्म नहीं भरेंगे, हम उनको नागरिक नहीं मानेंगे। चुनाव आयोग ने ये जो दायरा अख्तियार किया यह थोड़ी मुसीबत वाला साबित हुआ। चुनाव आयोग समझता रहा है कि भारत के नागरिकों को वोट दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसके लिए आयोग की मशीनरी घर-घर जाकर लोगों के वोट बनाती रही है। आयोग इंतजार नहीं करता कि आप सूची में जुड़ने के लिए दरख्वास्त देंगे। इसी वजह से भारत में मतदाता बनाम जनसंख्या का अनुपात 99 फीसद है। लेकिन इस बार आयोग ने सारा भार मतदाता के ऊपर डाल दिया। अब किसी को भी मतदाता सूची से निकालना बहुत आसान हो गया। एक उदाहरण देखिए। जब पहली मतदाता सूची बनी अगर तब आप उसमें थे और 2003 में भी थे व 24 जून 2005 तक भी हैं तो आपकी उम्र 95 साल हो गई। यानी 74 वर्षों से आपका नाम मतदाता सूची में है। अब अगर आप गणना प्रपत्र पर दस्तखत करके उसे वापस नहीं देंगे तो आपको सूची से निकाल दिया जाएगा। मैं नहीं समझ सकता कि एक दफ्तरी प्रक्रिया आपके संवैधानिक अधिकार को इतनी आसानी से कैसे खत्म कर देगी?
इसी आधार पर राजनीतिक दल घुसपैठियों का भी मुद्दा ले आए कि यह कवायद इन्हें बाहर निकालने के लिए है।
अशोक लवासा: कोई भी इस बात का पक्ष नहीं ले सकता कि जो भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाए। जिन दस-ग्यारह लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी या जो सार्वजनिक मंचों पर इसकी मुखालफत कर रहे हैं वे भी यह नहीं कह रहे कि आप हर एक को बिना सोचे-समझे आंखें बंद करके मताधिकार दे दीजिए। चुनाव आयोग भी यह नहीं मानता कि हमारे यहां बहुत से बाहरी लोग घुसे हुए हैं। चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है कि उसे किसी विधानसभा या संसदीय क्षेत्र में भारी मात्रा में घुसपैठियों की जानकारी के साथ गहन पुनरीक्षण के लिए कहा जाए तो वह कर सकता है। अभी जिनके नाम मतदाता सूची में आए हैं, या जिन 65 लाख लोगों के नाम नहीं आए, इसमें ये नहीं पता चला कि गैर नागरिक कितने हैं?
क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे चुनाव आयोग गैर नागरिकों के बारे में पता लगा सके?
अशोक लवासा: इसका तरीका यही है कि किसी ‘अ’ ने शिकायत की कि फलां आदमी भारत का नागरिक नहीं है या उसने फ्रांस की नागरिकता ले रखी है। शिकायतकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो कोई ऐसा दस्तावेज पेश करे जिससे चुनाव अधिकारियों के मन में शक पैदा हो। फिर आयोग अपनी तसल्ली करके आरोपित को नोटिस देगा कि आपके खिलाफ यह शिकायत आई है। अगर उसे आरोपित पर शक होता है तो वह गृह मंत्रालय के पास मामला भेज देगा कि आप तहकीकात करें। क्योंकि यह दायरा उसका नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो शपथपत्र दाखिल किया है उसमें कहा है कि किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भारत का नागरिक नहीं है। यह मसला छेड़ना ही एक समस्या बन गया।
वीडियो फुटेज को लेकर भी विवाद और गहरा गया जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने उसे मां-बहन-बेटी की इज्जत का सवाल बना दिया। इसे आप कैसे देखते हैं।
अशोक लवासा: इस तरह के भाव का इस्तेमाल क्यों किया गया पता नहीं। मतदाता की निजता का प्रश्न हर किसी पर लागू होगा, किसी वर्ग विशेष पर नहीं। वीडियो फुटेज मामले के कई पहलू हैं। यह कोर्ट के एक आदेश के कारण विवादास्पद हुआ क्योंकि आदेश का पालन नहीं किया गया। लाखों मिनटों के फुटेज आयोग के पास होते हैं और वे किसी विवाद के समाधान में काम आ जाएं ऐसा जरूरी भी नहीं है। इसलिए अभी तक वीडियो फुटेज की मांग होती भी नहीं थी। यह तो चुनाव आयोग अपने आंतरिक प्रबंधन के लिए करता है कि अगर कोई वेब प्रसारण हुआ या कोई विवाद हुआ। इसका उपयोग कितना हो सकता है यह मुझे नहीं पता। विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि लोगों ने देखा कि जो चुनाव आयोग हमेशा पारदर्शिता की वकालत करता है, वो खुद ऐसे फैसले क्यों कर रहा है?
चुनाव आयोग इतने व्यापक विवाद की जद में आज तक नहीं आया। इसके पहले विवाद होते भी थे तो चुनावों के समय में। लेकिन इस बार तो चुनाव भी सामने नहीं थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने रविवार को, राहुल गांधी की बिहार में रैली के दिन और लगभग उसी समय में प्रेस कांफ्रेंस की। इसने विवादों के आरोपों को और मजबूत कर दिया। क्या आपको लगता है कि इससे चुनाव आयोग की स्वायत्तता की साख पर असर पड़ा?
अशोक लवासा: इस मुद्दे पर मेरा दृष्टिकोण थोड़ा पारंपरिक है कि किसी एक-दो चीजों से किसी संस्था के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। चुनाव आयोग का सात दशक का इतिहास रहा है। बीच में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जब विवाद बढ़ जाते हैं। मैंने उस प्रेस कांफ्रेंस का सीधा प्रसारण नहीं देखा, लेकिन इंटरनेट के माध्यमों पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आईं उससे लगा कि कई लोगों को अपने सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले। कई लोगों के दिमाग में उलझनें बरकरार रहीं तो कई की बढ़ गईं। यह तो है कि अभी तक के इतिहास में चुनाव आयोग की किसी प्रेस कांफ्रेंस के बारे में इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई थी।
शास्त्रीय साहित्य की तरह मेरा मानना है कि चुनाव आयोग को सीजर की पत्नी की तरह संदेह के परे होना चाहिए। अब आयोग पर गंभीर आरोप लग रहा है कि वह ‘वोट चोरी’ कर सत्ताधारी पार्टी की ओर स्थानांतरित कर रहा है।
अशोक लवासा: राजनीतिक दल उत्तेजित होकर जिन लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं तो यह उनका दायरा है। जहां तक विश्वास का सवाल है तो हाल ही में सीएसडीएस का एक सर्वेक्षण आया था कि चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा पहले से कम हो गया है। हमने विदेशों में भी कहते सुना है कि भारत की निर्वाचन प्रणाली लोकतांत्रिक मानकों पर खरी उतरती है। अगर आप किसी खेल के रेफरी हैं तो लोगों को दिखना चाहिए कि आप निष्पक्ष हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप दोनों पक्षों को प्रतियोगिता का समान मैदान दीजिए। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आपने इसकी भी गलती नजरअंदाज कर दी और उसकी भी गलती नजरअंदाज कर दी। आपको वह करना है जो कानून की दृष्टि से सही है। यही कानून आप पर भी लागू होता है। आप किसी कक्षा के मानीटर हैं और कक्षा में अनुशासन मानने वाले कम हो जाएंगे तो मुश्किल होगी।
पिछले दिनों उठे विवाद के बाद आम धारणा यह बन रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। अभी यह बहुत कुछ सत्ता के पक्ष में चला जाता है।
अशोक लवासा: कोई भी प्रणाली ऐसी नहीं है जो ऐसे नतीजे की गारंटी दे जैसा आप चाहते हैं। एक वाक्य में कहूं तो सबसे अहम यह है कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति हुई है वह कैसे काम करता है।
जिस तरह का माहौल है तो क्या देश को कोई दूसरा टीएन शेषन मिल पाएगा?
अशोक लवासा: जरूरत होगी तो जरूर मिलेगा।
जब चुनाव आयोग पर उठे सवालों का जवाब सत्ताधारी दल के प्रवक्ता देने लगते हैं तो लाजिम तौर पर जनता पूछती है कि पारदर्शिता कहां है?
अशोक लवासा: बिल्कुल ठीक बात है। पारदर्शिता अपने आप में कई समस्याओं का समाधान है।
क्या इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़खानी की जा सकती है?
अशोक लवासा: भारत में पिछले दो दशक से ईवीएम से हजारों चुनाव हुए हैं और 40-45 अदालती मामले हुए हैं। किसी में भी यह साबित नहीं हुआ कि ईवीएम में छेड़खानी हुई है। अगर आपका सवाल यह है कि क्या ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई है तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। इसके कई तकनीकी पहलू हैं। ईवीएम कई स्तरों पर जांच और सुरक्षा के दायरे में रहती है।
प्रस्तुति : मृणाल वल्लरी