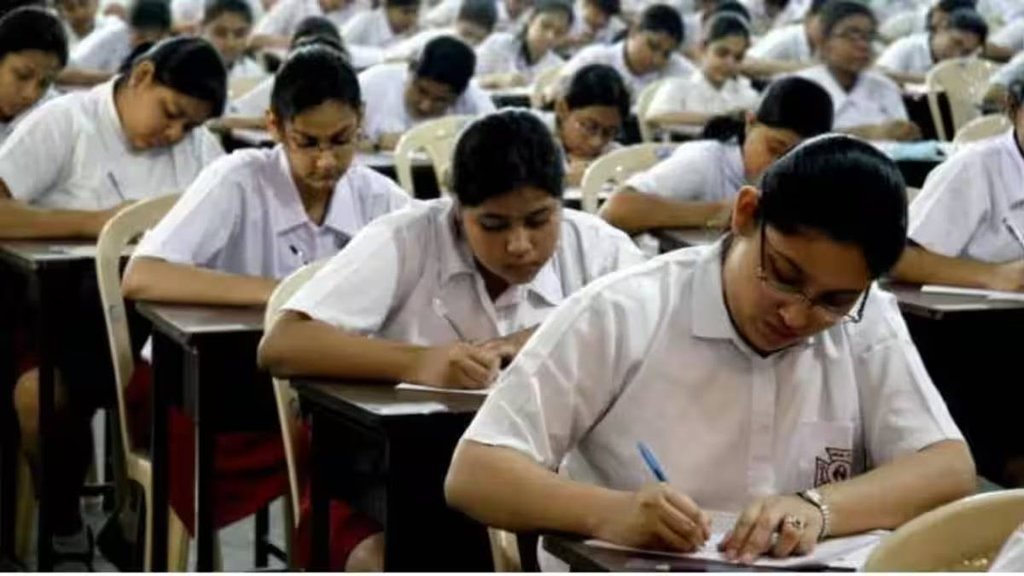सुशील कुमार सिंह
शिक्षा समाज का वह आईना है, जिसमें सूरत और सीरत दोनों को खूबसूरत बनाया जा सकता है। इसी सिद्धांत को व्यापकता देते हुए 2020 में नई शिक्षा नीति बनी, जिसमें कई सकारात्मक उद्देश्य शामिल किए गए। इसका एक बड़ा उद्देश्य 2030 तक प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक सौ फीसद सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद से ही इसे लागू करने की प्रक्रिया देश भर में शुरू हो गई थी। इस क्रम में कर्नाटक देश का पहला राज्य है, जहां नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। मध्यप्रदेश दूसरा राज्य है, जहां अगस्त 2021 में विद्यालयी और उच्च शिक्षा में इसे लागू करने की बात कही थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान और असम समेत तमाम राज्य इसे लेकर तैयारी में जुट गए। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में भी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से इसकी शुरुआत की गई।
चौंतीस साल बाद देश में एक नया शिक्षा प्रारूप अमल में लाया गया
हालांकि अब नई शिक्षा नीति के आलोक में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप यानी एनसीएफ की घोषणा भी कर दी गई है, मगर तीन साल बाद भी नई शिक्षा नीति सभी राज्यों में लागू नहीं हो पाई है। इसे लेकर राज्यों के अपने दृष्टिकोण हैं, मगर इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि नई शिक्षा नीति तत्कालीन परिस्थितियों में एक नई व्यवस्था का प्रारूप पेश करती है, जो देश की जरूरत है। गौरतलब है कि इसके पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी, जिसमें 1992 में संशोधन किया गया था, और तब से वही व्यवस्था अनवरत चली आ रही है। चौंतीस साल बाद देश में एक नया शिक्षा प्रारूप अमल में लाया गया, जिसका मसविदा पूर्व इसरो प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने तैयार किया था। नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई परिवर्तन किए गए हैं।
पहले तीन साल बच्चे आंगनबाड़ी में विद्यालय पूर्व की पढ़ाई करेंगे
नई शिक्षा नीति में कई नए आयाम हैं। भाषा के स्तर पर इसमें उदारता और पाठ्यक्रम की दृष्टि से कहीं अधिक लोचशीलता है। चरणबद्ध प्रक्रिया में देखें तो अब भारत में शिक्षा की शुरुआत आधार स्तर से शुरू होगी, जिसमें पहले तीन साल बच्चे आंगनबाड़ी में विद्यालय पूर्व की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद अगले दो वर्ष यानी कक्षा एक और दो के लिए स्कूल जाएंगे, जो नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत होगा। यह क्रियाकलाप आधारित शिक्षण होगा। यह पढ़ाई का पहले पांच साल का चरण है। दूसरा चरण तीन वर्षीय ‘प्रीप्रेटरी स्टेज’ का है, जिसमें कक्षा तीन से पांच और ग्यारह वर्ष की आयु के विद्यार्थियों के बच्चों के लिए होगा। जबकि माध्यमिक स्तर की पढ़ाई कक्षा छह से आठ और उम्र ग्यारह से चौदह वर्ष की है।
नई शिक्षा नीति में भाषा थोपने की स्थिति नहीं है
इसके बाद अगला चरण कक्षा नौ से बारहवीं तक का है, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी रुचि का विषय चुनने की आजादी दी गई है। इसमें खास बात यह है कि पांचवीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने का प्रावधान है। विदेशी भाषा की पढ़ाई माध्यमिक स्तर पर करने का प्रावधान है, जिसे कक्षा आठ या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यानी नई शिक्षा नीति में भाषा थोपने की स्थिति नहीं है।
प्रतिभा पलायन पर भी विराम लग सकता है।
उच्च शिक्षा स्तर पर भी कई बदलाव किए गए हैं। डिग्री कार्यक्रम में कई संदर्भ निहित हैं। मसलन, जो छात्र शोध में जाना चाहता है, उसे चार साल का स्नातक और एक साल का परास्नातक करना होगा। जो नौकरी में जाना चाहता है, उसके लिए यही कार्यक्रम तीन वर्ष का होगा। रिसर्च यानी पीएचडी में सीधे प्रवेश होगा, यहां एमफिल की जरूरत खत्म कर दी गई है। यानी उच्च शिक्षा भी लोचशील है और इसमें पढ़ाई छोड़ने और फिर उससे जुड़ने के अलावा भी कई सुविधाएं हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भी दरवाजे खुल चुके हैं। मगर यह बदलाव जमीन पर कितनी जल्दी उतर पाएगा, कहना मुश्किल है। हालांकि भारत में शीर्ष दो सौ विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए द्वार खुलने से यहां की उच्च शिक्षा का स्तर भी बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही प्रतिभा पलायन पर भी विराम लग सकता है।
नई शिक्षा नीति में अधिकतम फीस की सीमा भी तय करने की बात
यूपीए सरकार के समय विदेशी शिक्षण संस्थाओं के लिए लाए गए ‘रेगुलेशन आफ एंट्री ऐंड आपरेशन बिल 2010’ को लेकर भाजपा विरोध में थी। मगर अब उसी ने इसे लागू कर दिया है। हालांकि यह सही कदम है, क्योंकि हर साल साढ़े सात लाख से अधिक भारतीय छह अरब डालर खर्च करके विदेश में पढ़ते हैं, जिसका आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस दृष्टि से इस पर न केवल विराम लगेगा, बल्कि आर्थिक मुनाफा भी देश को होगा। हालांकि सवाल यह भी है कि भारत के शैक्षणिक वातावरण को देख कर क्या विदेशी विश्वविद्यालय यहां काम करने का रुख करेंगे। ऐसे में तब जब नई शिक्षा नीति में अधिकतम फीस की सीमा भी तय करने की बात कही गई है।
खास बात यह भी है कि उच्च शिक्षा में 2035 तक पचास फीसद सकल नामांकन अनुपात पहुंचाने का लक्ष्य है, जो साल 2018 के आंकड़े छब्बीस फीसद से लगभग दोगुना है। फिलहाल उच्च शिक्षा में करोड़ों नई सीटें जोड़ने की बात भी है।
भारत की नई शिक्षा नीति कई ऐसे सवालों का बेहतर जवाब हो सकती है, बशर्ते इसे सही ढंग से जमीन पर उतारा जाए। इसे शीघ्रता और सकारात्मकता के साथ प्रचलन में लाया जाए, तो इसके नतीजे भी बड़े होंगे। वैसे दुनिया में कई देश शिक्षा की स्थिति और प्रगति को लेकर नए प्रयोग करते रहे हैं। अमेरिका में स्कूल व्यावहारिक समझ और अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों पर अधिक जोर देते हैं। यहां प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय की श्रेणी रखी गई है।
चीन की शिक्षा प्रणाली में भी चार चरण हैं। पहले प्राथमिक शिक्षा, फिर पेशेवर शिक्षा और उसके बाद उच्च शिक्षा और अंतत: वयस्क शिक्षा शामिल है। खास बात यह है कि यहां छह से पंद्रह वर्ष के चीनी बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी और मुफ्त है। यहां औसतन एक कक्षा में पैंतीस विद्यार्थी रखने का नियम है। वहां दाखिले में किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है। वहां छह साल की उम्र से बच्चों का दाखिला स्कूल में होता है।
स्विटजरलैंड की शिक्षा पद्धति अपने आप में एक अलग तरह की जिंदगी है। यह प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। यूरोप के कई देश मसलन, स्विटजरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली समेत कई देश शिक्षा के मामले में काफी ताकत बना चुके हैं। नीदरलैंड की शिक्षा को काफी किफायती माना जाता है। शिक्षा के साथ कई देशों में अंशकालिक नौकरी करने की भी छूट मिलती है। इसके अलावा भी कई सुविधाएं हैं।
नई शिक्षा नीति से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधारों और योजनाओं की संभावना है, जिससे भावी पीढ़ी को लक्ष्य के अनुसार मानसिक और बौद्धिक रूप से तैयार किया जा सकेगा। वैसे आजादी के बाद से शिक्षा को लेकर कई आयोग और समितियों का गठन हुआ। स्वतंत्रता से पहले की शिक्षा पद्धति में व्यापक परिवर्तन भी होते रहे हैं।
नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा यह संदर्भ उजागर करती है कि 1954 की लार्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा का दौर आगे उस पैमाने पर नहीं रहेगा। 1964, 1966 और 1968 तथा 1975 में शिक्षा संबंधी आयोगों का गठन हुआ। मगर नई शिक्षा नीति में बुनियादी स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक में बदलाव की पहल की गई है। मगर अब भी अपेक्षा बनी हुई है कि इस नीति को व्यावहारिक रूप में जमीन पर जल्दी उतारा जाए।