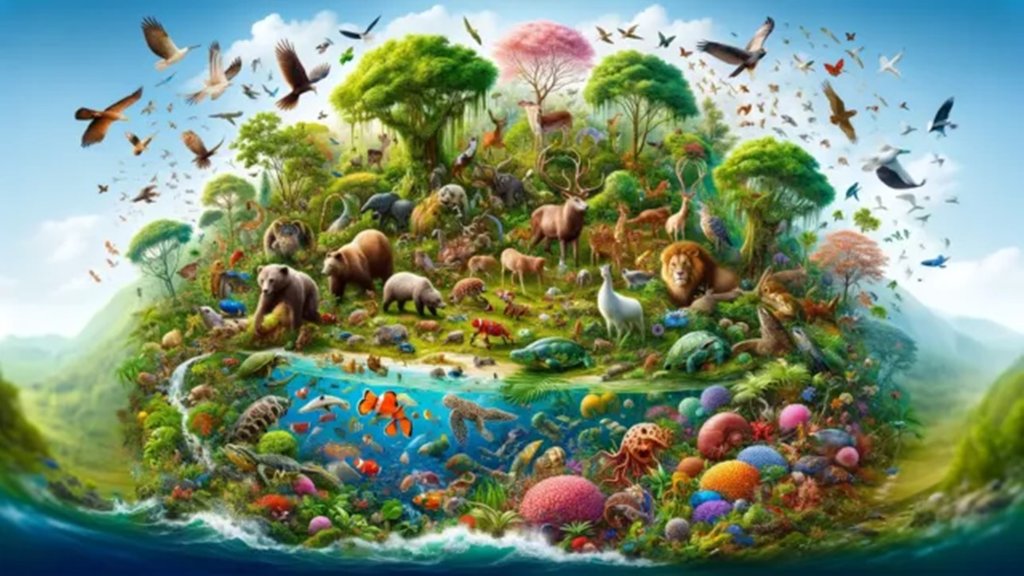भारत जैव विविधता से समृद्ध देश है। विश्व के चौंतीस जैव विविधता क्षेत्रों में से चार भारत में हैं। इसी प्रकार विश्व के सत्रह ‘मेगा-डायवर्सिटी’ देशों में भारत शामिल है। इस प्रकार जैव विविधता न केवल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार निर्मित करता, बल्कि देश में आजीविका को भी आधार प्रदान करता है। भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कई उपाय किए गए हैं जैसे कि 103 राष्ट्रीय उद्यानों, 510 वन्य जीव अभ्यारण्यों, 50 टाइगर रिजर्व, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, तीन कंजर्वेशन रिजर्व तथा 2 सामुदायिक रिजर्व की स्थापना। जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता कार्रवाई योजना तैयार की गई है, जो वैश्विक जैव विविधता रणनीतिक योजना 2011-20 के अनुकूल है। इसे 2010 में ‘कन्वेंशन आन बायोलाजिकल डायवर्सिटी’ की बैठक में स्वीकार किया गया था।
भारत में जैव विविधता और इससे संबंधित ज्ञान के संरक्षण के लिए 2002 में जैव विविधता अधिनियम तैयार किया गया। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए त्रि-स्तरीय संस्थागत ढांचे का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 8 के तहत सर्वोच्च स्तर पर वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। यह एक वैधानिक निकाय है, जिसकी मुख्य भूमिका विनियामक और परामर्शदाता की है। राज्यों में राज्य जैव विविधता प्राधिकरण की भी स्थापना की गई है। स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंध समितियों (बीएमसी) का गठन किया गया है।
एनबीए के डेटा के अनुसार, देश के 26 राज्यों ने राज्य जैव विविधता प्राधिकरण एवं जैव विविधता प्रबंध समितियों का गठन किया है। अकेले महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में 43,743 बीएमसी का गठन किया गया है। इन समितियों का उद्देश्य देश की जैव विविधता और संबंधित ज्ञान का संरक्षण, इसके सतत उपयोग में मदद तथा यह सुनिश्चित करना कि जैविक संसाधनों के उपयोग से जनित लाभों को उन सबसे उचित और समान रूप से साझा किया जाए, जो इसके संरक्षण, उपयोग एवं प्रबंधन में शामिल हैं।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्रवाई योजना का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण है। इसके सफल क्रियान्वयन में लोगों की भागीदारी की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। केरल के वायनाड जिले में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का सामुदायिक कृषि जैव विविधता केंद्र इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करके स्थानीय विकास योजनाओं में जैव विविधता संरक्षण को समन्वित किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की मदद से ग्रामीणों की आजीविका में बेहतरी के नए मानदंड स्थापित किए हैं।
जैव विविधता पर सम्मेलन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए व्यापक कानूनी और संस्थागत प्रणाली स्थापित करने में भारत काफी आगे रहा है। आनुवांशिक संसाधनों को लोगों के लिए उपलब्ध कराना और लाभ के निष्पक्ष, समान बंटवारे के सम्मेलन के तीसरे उद्देश्य को जैव विविधता अधिनियम 2002 और नियम 2004 के तहत लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की पहुंच बढ़ाने और लाभ साझाकरण प्रावधानों के संचालन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के जैव विविधता रजिस्टर और जैव विविधता प्रबंधन समितियों का संजाल तैयार किया जाता है।
2002 के अधिनियम के आधार पर बनी जैव विविधता प्रबंधन समितियां स्थानीय स्तर की वैधानिक निकाय हैं, जिनमें लोकतांत्रिक चयन प्रक्रिया के तहत कम से कम दो महिला सदस्यों की भागीदारी जरूरी होती है। ये समितियां शोधकर्ताओं, निजी कंपनियों, सरकारों जैसे प्रस्तावित उपयोगकर्ताओं की जैव संसाधनों तक पहुंच संभव बनाने और सहमति बनाने में मदद करती हैं। इससे जैव विविधता रजिस्टरों और जैविक संसाधनों के संरक्षण तथा टिकाऊ उपयोग के फैसलों के जरिए उपलब्ध संसाधनों का स्थायी उपयोग और संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है।
इस परियोजना का उद्देश्य जैविक संसाधनों तक बेहतर पहुंच बनाना, उनके आर्थिक मूल्य का आकलन करना और स्थानीय लोगों के बीच उनके लाभों को बेहतर ढंग से साझा करना है।
इसे देश के दस राज्यों- आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, ओड़ीशा, तेलंगाना और त्रिपुरा में चलाया जा रहा है। भारत में जैव विविधता के कई आकर्षक वैश्विक केंद्र हैं। मसलन, सिक्किम में पक्षियों की 422 प्रजातियां और तितलियों की 697, फूलों के पौधों की साढ़े चार हजार, पौधों की 362 प्रजातियां और सुंदर आर्किड फूलों की समृद्ध विविधता है।
जंतुओं और वनस्पतियों की अनगिनत प्रजातियां ही हिमालय को जैव विविधता का अनमोल भंडार बनाती हैं। यहां मौजूद हजारों छोटे-बड़े ग्लेशियर, बहुमूल्य जंगल, नदियां और झरने इसके लिए उपयुक्त जमीन तैयार करते हैं। मध्य हिमालय में बसे उत्तराखंड में ही वनस्पतियों की 7000 और जंतुओं की 500 महत्त्वपूर्ण प्रजातियां मौजूद हैं। आज हिमालयी क्षेत्र में जैव विविधता को कई खतरे भी हैं। इसकी मुख्य वजहें जलवायु परिवर्तन से लेकर जंगलों की कटान, वहां बार-बार लगने वाली अनियंत्रित आग, जल धाराओं का सूखना, खराब वन प्रबंधन और लोगों में जागरूकता की कमी आदि हैं। इस वजह से कई प्रजातियों के सामने अस्तित्व का संकट है। ऐसी ही एक वनस्पति प्रजाति है आर्किड, जिसे बचाने के लिए उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों से कोशिश हो रही है।
आर्किड पादप संसार की सबसे प्राचीन वनस्पतियों में है, जो अपने खूबसूरत फूलों और पर्यावरण में अनमोल योगदान के लिए जानी जाती है। उत्तराखंड में आर्किड की लगभग ढाई सौ प्रजातियां पहचानी गई हैं, लेकिन ज्यादातर अपना वजूद खोने की कगार पर हैं। जीव वैज्ञानिकों का कहना है कि कम से कम 5 या 6 प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। खुद जमीन या फिर बांज या तून जैसे पेड़ों पर उगने वाला आर्किड कई वनस्पतियों में परागण को संभव और सुगम बनाता है। पिछले दो वर्ष से उत्तराखंड वन विभाग के शोधकर्ताओं ने कुमाऊं की गोरी घाटी और गढ़वाल मंडल के इलाकों में आर्किड की करीब सौ से अधिक प्रजातियों को संरक्षित किया है।
संयुक्त राष्ट्र ने 2021-30 को पारिस्थितिकी संरक्षण का दशक घोषित किया है। इसलिए यह विश्वव्यापी चिंताओं का भी समय है, जब दुनिया के लोगों के सामने अपनी उस कुदरती पारिस्थितिकी का पुनरुद्धार करने की चुनौती है, जो विभिन्न कारणों से नष्ट हो रही है। जाहिर है, इस व्यापक चिंता से भारत के लोग भी अलग नहीं रह सकते। तेज आर्थिक वृद्धि और विकास नियोजन में पर्यावरणीय चिंताओं को समाहित न कर पाने की सीमाओं, कमजोरियों या दूरदर्शिता के अभाव के चलते भारत की जैव विविधता पर भी अनावश्यक और अतिरिक्त दबाव पड़ रहे हैं।
ऐसे में संरक्षण की हर स्तर की पहल स्वागत योग्य है। खासकर यह ध्यान रखते हुए कि जैव संपदा और मनुष्य अस्तित्व के बीच सीधा और गहरा नाता है। जैव विविधता के इस केंद्र में भारत की वह करीब पचास फीसद आबादी भी आती है, जो गरीबी रेखा से नीचे बसर करती है, जंगल जिनका घर है और जंगल से जिनका रिश्ता अटूट है। यही लोग जैव विविधता के नैसर्गिक पहरेदार हैं।