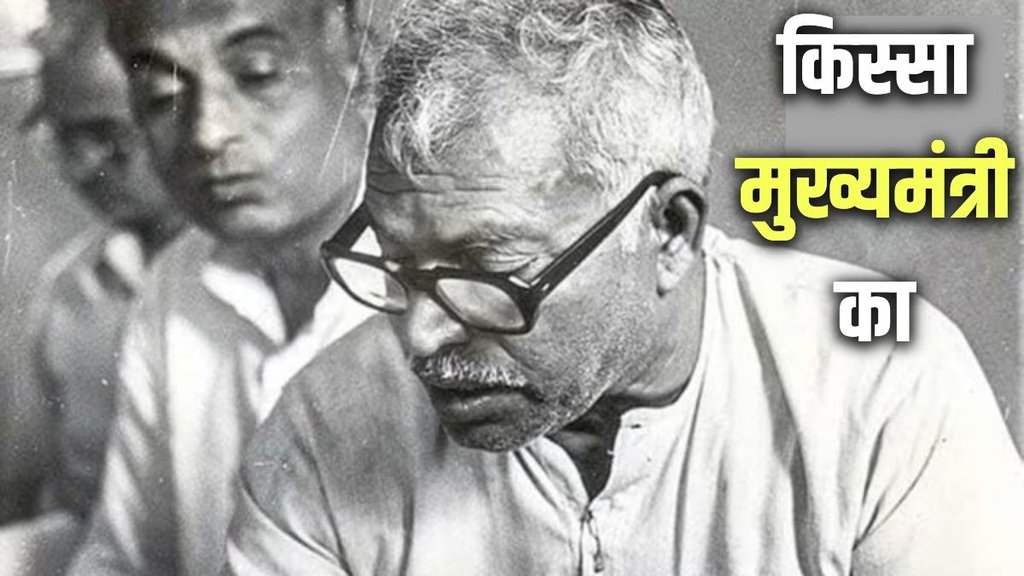बिहार की राजनीति हमेशा से उतनी ही दिलचस्प रही है जितनी पेचीदा। यहां सत्ता की हर करवट के साथ एक नई कहानी जन्म लेती है — कभी विद्रोह की, कभी वैचारिक टकराव की, तो कभी सामाजिक न्याय की। इन्हीं कहानियों में एक नाम है कर्पूरी ठाकुर का — एक नाई परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे वह नेता, जिसने राजनीति में सिद्धांतों को ताक़त दी और सत्ता को साधन नहीं, ज़िम्मेदारी माना। वह नेता, जिसने सत्ता के अस्थिर दौर में भी ऐसी नीतियां बनाईं, जिन्होंने आने वाले दशकों की राजनीति को दिशा दी। यह कहानी है उस जननायक की, जिसने जातिगत जटिलताओं के बीच समानता की नई परिभाषा गढ़ी — और बिहार से निकलकर पूरे देश में सामाजिक न्याय का अध्याय लिखा।
बिहार के 11वें मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर दो बार इस पद पर रहे — एक बार लगभग छह महीने के लिए और दूसरी बार दो साल से भी कम समय के लिए। उनके कार्यकाल की अवधि उनके द्वारा छोड़ी गई वैचारिक और नीतिगत विरासत की गहराई को पूरी तरह नहीं दर्शाती। अपने जीवनकाल में ठाकुर ने अपने मार्गदर्शक नेताओं के उभार के कारण अपने कद को घटते देखा, लेकिन हाल के दशकों में उन्हें सभी राजनीतिक गलियारों में व्यापक सम्मान और प्रतिष्ठा मिली है। समाजवादी नेताओं की श्रेणी में वे डॉ. राम मनोहर लोहिया के बाद आने वाले प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। पिछले वर्ष नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया।
उथल-पुथल के बीच सत्ता में आए
फरवरी 1969 में गठित और जनवरी 1972 में भंग हुई पांचवीं बिहार विधानसभा उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक थी। इस अवधि में पांच मुख्यमंत्रियों — हरिहर सिंह, भोला पासवान शास्त्री (दो बार), दरोगा प्रसाद राय और कर्पूरी ठाकुर — ने शपथ ली, और इस दौरान राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ। इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच ठाकुर परिवर्तनकारी नीतियों के बीज बोने में सफल रहे।
जब दिसंबर 1970 में दरोगा प्रसाद राय के कांग्रेस-नेतृत्व वाले गठबंधन ने इस्तीफा दिया, तो तुरंत ही विरोधी दावे सामने आने लगे। गठबंधन उस समय बेहद कमज़ोर थे; जातिगत निष्ठाओं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और वैचारिक मतभेदों के कारण दलबदल का खतरा हमेशा बना रहता था। भोला पासवान शास्त्री, जो पहले दो बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, ने फिर से दावा किया, लेकिन राज्यपाल ने 169 विधायकों के समर्थन के आधार पर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (एसएसपी) के नेता कर्पूरी ठाकुर को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया।
22 दिसंबर 1970 को ठाकुर ने शपथ ली और 1967 के बाद (राष्ट्रपति शासन को छोड़कर) आठवीं सरकार का नेतृत्व किया। उनके गठबंधन में एसएसपी, कांग्रेस (ओ), भारतीय क्रांति दल (बीकेडी), भारतीय जनसंघ (बीजेएस), स्वतंत्र पार्टी, शोषित दल का एक गुट और अन्य शामिल थे — एक ऐसा मिश्रित गठबंधन जो वैचारिक एकजुटता की तुलना में कांग्रेस-विरोधी भावना से अधिक जुड़ा हुआ था।
साझेदारों को समायोजित करने के लिए ठाकुर के मंत्रिमंडल का आकार लगातार बढ़ता गया। फरवरी 1971 में उन्होंने लगातार तीन दिनों तक मंत्रिमंडल का विस्तार किया और अंततः 53 मंत्रियों तक पहुंचे। अपने कई पूर्ववर्तियों की तरह, उनकी अधिकांश ऊर्जा अलग-अलग समूहों, व्यक्तित्व संघर्षों और जातिगत अहंकारों के बीच संतुलन बनाए रखने में खर्च होती रही।
मार्च 1971 के लोकसभा मध्यावधि चुनावों ने तनाव को और गहरा दिया। इंदिरा गांधी की कांग्रेस (आर) ने बिहार में 39 सीटें जीतीं (1967 में अविभाजित कांग्रेस की 34 सीटों से अधिक), जिससे राज्य की राजनीतिक दिशा बदल गई। दलबदल तेज हो गए; शोषित दल और बीकेडी के गुट अस्थिर रुख अपनाने लगे, जबकि एसएसपी और बीजेएस के कुछ विधायक पार्टी छोड़कर चले गए।
1 जून 1971 को अविश्वास प्रस्ताव की संभावना बन रही थी। विधानसभा शुरू होने से कुछ घंटे पहले ठाकुर ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि, उसी सुबह उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की स्थिति का अध्ययन करने और उनके उत्थान के उपाय सुझाने के लिए 20 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। यह साहसिक कदम भोला पासवान शास्त्री की उत्तराधिकारी सरकार ने रद्द कर दिया।
विपक्षी नेता और संसदीय कार्यकाल ठाकुर एक स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्र भारत में उनका राजनीतिक जीवन 1952 में शुरू हुआ, जब उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर ताजपुर से विधानसभा सीट जीती। उन्होंने 1957 और 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (पीएसपी) के टिकट पर, और 1967 व 1969 में एसएसपी के टिकट पर यह सीट बरकरार रखी। 1972 में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी से पुनः यह सीट जीती और लगभग दो वर्षों तक विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे।
इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर उथल-पुथल का दौर शुरू हुआ — इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल, उसका हटाया जाना, और 1977 में लोकसभा में जनता पार्टी की जीत। ठाकुर जनता पार्टी के टिकट पर समस्तीपुर से संसद पहुंचे। मोरारजी देसाई सरकार ने अप्रैल 1977 में बिहार सहित कांग्रेस की राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया।
1971 की जनगणना के बाद परिसीमन के परिणामस्वरूप बिहार विधानसभा की सीटें 318 से बढ़कर 324 हो गईं। इसके बाद के चुनावों में कांग्रेस घटकर 57 सीटों तक सिमट गई, जबकि जनता पार्टी ने चार प्रमुख और छोटे दलों के विलय से 214 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त किया। सांसद होने के बावजूद ठाकुर जनता विधायक दल के नेता चुने गए।
फिर से मुख्यमंत्री बने
लोकसभा से इस्तीफा देकर कर्पूरी ठाकुर 24 जून 1977 को 22 महीने के कार्यकाल के लिए पुनः मुख्यमंत्री बने। विधानसभा पहुंचने के लिए उन्होंने फुलपरास सीट से उपचुनाव जीता।
नाई (नाई) जाति में जन्मे ठाकुर, जो एक गैर-कृषक अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) से थे, सामाजिक समानता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। उनका 1971 का आयोग रद्द कर दिया गया था, लेकिन उसकी जगह दिसंबर 1971 में शास्त्री जी द्वारा गठित मुंगेरी लाल आयोग ने ले ली, जिसकी अध्यक्षता स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व विधायक मुंगेरी लाल ने की थी। 1976 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी के उत्थान की सिफारिश की।
पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद ठाकुर ने श्रेणीबद्ध आरक्षण सूत्र लागू किया — अति पिछड़ी जातियों के लिए 12 प्रतिशत, पिछड़े वर्गों (मुख्यतः यादव, कुर्मी, कोइरी जैसी कृषक पिछड़ी जातियों) के लिए 8 प्रतिशत, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 3 प्रतिशत। इस उप-वर्गीकरण ने कारीगरों और सेवा-आधारित जातियों को कृषक जातियों से अलग कर दिया, जिससे ओबीसी के भीतर की असमानताओं का समाधान हुआ।
हालांकि, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव ने अगस्त 1977 में ओबीसी के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था, लेकिन बिहार की तरह वहाँ इसे उप-वर्गीकृत नहीं किया गया था।
ठाकुर की सकारात्मक कार्रवाई की नीति ने तीव्र राजनीतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न की। जनता पार्टी के उच्च-जाति के कई सदस्यों ने इसका विरोध किया। उनके कई कैबिनेट सहयोगियों ने इस्तीफा दे दिया, और कुछ समय के लिए जनता पार्टी दो हिस्सों में बंटी दिखाई दी — ओबीसी आरक्षण के समर्थक और विरोधी। अंततः आंतरिक विद्रोह के कारण अप्रैल 1979 में ठाकुर को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह अनुसूचित जाति के नेता राम सुंदर दास को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया।
ठाकुर ने अपने कार्यकाल में शराब पर प्रतिबंध लगाया था — यह कदम बाद में दास सरकार ने रद्द कर दिया, लेकिन दशकों बाद नीतीश कुमार ने इसे फिर से लागू किया।
1980 में ठाकुर ने जनता पार्टी (सेक्युलर) — चरण सिंह गुट — के टिकट पर समस्तीपुर विधानसभा सीट जीती। 1980 में कांग्रेस ने बिहार में पुनः सत्ता हासिल की, और ठाकुर विपक्ष के नेता बने रहे। उन्होंने 1985 में लोकदल के उम्मीदवार के रूप में सोनबरसा से चुनाव जीता और 12 फरवरी 1988 तक विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई। एक सप्ताह बाद उनका निधन हो गया।
भारत छोड़ो आंदोलन के एक अनुभवी नेता, जिन्होंने आपातकाल सहित कई बार जेल की सज़ा भुगती, ठाकुर ने सिद्धांतवादी समाजवाद को अपने जीवन में मूर्त रूप दिया।
उनके आरक्षण मॉडल ने आगे की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। जैसे-जैसे ओबीसी एकीकरण मजबूत हुआ — यादव, कुर्मी, कोइरी, लोध और सैनी राजनीति पर हावी हुए — पार्टियों ने गैर-यादव/ईबीसी समूहों के साथ नए गठबंधन बनाने शुरू किए, जिससे ठाकुर का मॉडल पुनः प्रासंगिक हो उठा। मोदी सरकार ने 2017 में ओबीसी उप-वर्गीकरण के लिए जी. रोहिणी आयोग का गठन किया, जिसने 31 जुलाई 2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
दलबदल और अस्थिरता के दौर में ठाकुर ने उप-वर्गीकृत आरक्षण की शुरुआत कर जातिगत जटिलताओं के बीच समानता को बढ़ावा दिया। उनकी दूरदर्शिता ने बिहार के सामाजिक न्याय विमर्श को आकार दिया, राष्ट्रीय नीतियों को प्रेरित किया, और उन्हें “जननायक” की उपाधि से विभूषित किया।ठाकुर के पुत्र, रामनाथ ठाकुर, जनता दल (यूनाइटेड) से राज्यसभा सांसद हैं और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं।