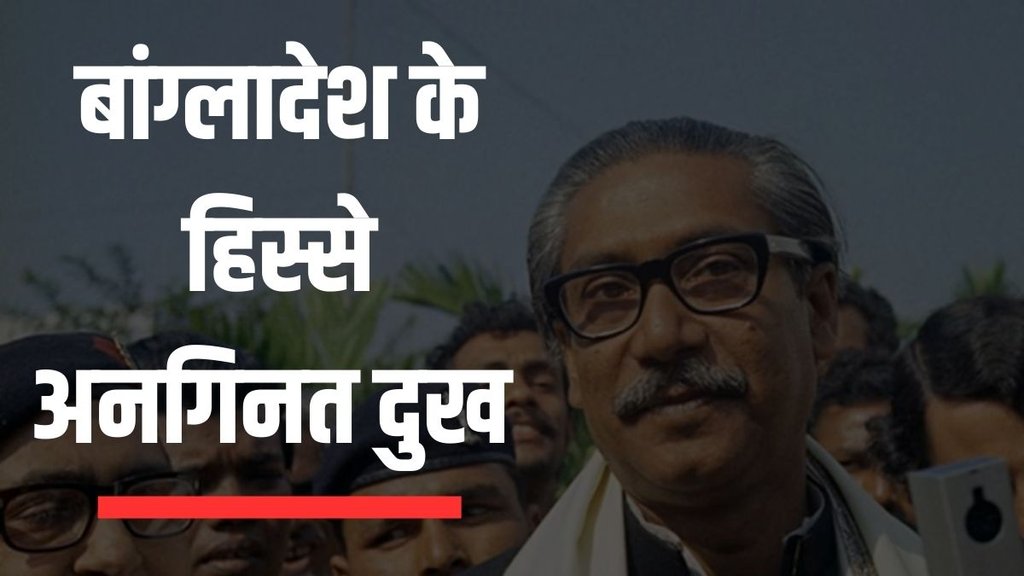बांग्लादेश में शेख हसीना का दौर खत्म हुआ। सेना के अध्यक्ष वकार-उज-जमान मीडिया के सामने आए तो सभी की नज़रें उनपर थी।
‘वह पद छोड़कर चली गई हैं। अब हम अंतरिम सरकार बनाने वाले हैं।’ यह उनके शब्द थे।
14 करोड़ की तादाद वाला एक मुल्क अचानक थम गया। एक गुस्सा जो कभी छिपा, कभी निकला, देश को ऐतिहासिक मोड़ पर लाकर थम गया। अब सेना ही प्रधानमंत्री थी, सेना ही संसद थी, सेना ही सबकुछ थी। लेकिन ‘अंतरिम सरकार’ शब्द में एक रास्ता छिपा था। आंदोलन से जुड़े छात्रों ने राय दी कि नोबल विजेता मुहम्मद यूनुस को बुलाया जाए। वह देश की सियासत की कमान संभालें। वह आ गए हैं। लेकिन अब बांग्लादेश की सियासत में सेना की दखलअंदाजी फिरसे कितनी होने वाली है, यह बहुत बड़ा सवाल है।
बांग्लादेश : सेना ही सबकुछ?
अमेरिका ने जो कुछ बांग्लादेश में हुआ उसे लेकर सबसे पहले टिप्पणी की, इसमें सबसे खास पहलू बांग्लादेश की आर्मी की तारीफ थी। बांग्लादेश की सेना जिस तरह से सामने आई, इसे पिक्चर का सेंटर कहा गया। हर तरफ वकार-उज-जमान की चर्चा होने लगी। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन के दौरान जब हालात नहीं संभले तो हसीना सरकार ने सेना की मदद ली। सरकार के मददगार के तौर पर तब सेना लोगों को कंट्रोल करने का रोल निभा रही थी। लेकिन जैसी ही हालात सरकार के काबू से बाहर हुए, सबकुछ बदल गया। सेना अब भी पिक्चर में थी, लेकिन अलग ढंग से।
सेना ने हालात को काबू करने का हर तरीके से प्रयास किया। बीबीसी की एक रिपोर्ट में लिखा गया कि बांग्लादेश की सेना के अधिकारी हमेशा इस बात के खिलाफ रहे कि आम लोगों पर गोलियां चलाई जाएं। सड़कों पर मौजूद छात्र आंदोलन के इस अंतिम पड़ाव में किसी भी स्थिति के लिए तैयार थे। इसलिए सेना अगर अपना रवैया नरम नहीं रखती तो हालात कुछ और होते और मौतों का आंकड़ा ज़्यादा हो सकता था। पिछले कई दशकों में बांग्लादेश में सेना की भूमिका रही है। इसपर एक नज़र डालते हैं।
1971 का युद्ध
बांग्लादेश बनने से पहले पाकिस्तान में 1970 के आम चुनावों में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में 162 में से 160 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत दर्ज किया। जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपीपी ने पश्चिमी पाकिस्तान में 138 में से 81 सीटें जीतीं।
अवामी लीग की जीत के बावजूद पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल याह्या खान (जो उस समय मार्शल लॉ के ज़रिए देश पर शासन कर रहे थे) ने मुजीबुर रहमान को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। इससे पूर्वी पाकिस्तान में हालात खराब हुए। जहां बंगाली सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रेरित और उर्दू थोपे जाने के खिलाफ़ आंदोलन पहले से ही चल रहा था।
7 मार्च, 1971 को मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों से आह्वान किया कि वह बांग्लादेश की आज़ादी के लिए उठ खड़े हों। जवाब में पाकिस्तानी सेना ने अपना ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। जिसके तहत बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई। यहीं से बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई (मुक्ति वाहिनी) शुरू हुई और बांग्लादेश एक देश बन गया।
बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद मुक्ति वाहिनी के सदस्य बांग्लादेश सेना का हिस्सा बन गए। हालांकि स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में सेना के भीतर उन बंगाली सैनिकों के खिलाफ भेदभाव के कारण तनाव उभरने लगा, जिन्होंने मुक्ति युद्ध की अगुवाई में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था।
पहला सैन्य तख्तापलट
15 अगस्त 1975 को हालात खराब होने लगे। जब मुट्ठी भर युवा सैनिकों ने मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी और उनके परिवार के भी कई सदस्यों को मार दिया। यह पहली बार था जब बांग्लादेश ने सैन्य तख्तापलट देखा। जिसका नेतृत्व मेजर सैयद फारुक रहमान, मेजर खांडेकर अब्दुर रशीद और राजनीतिज्ञ खोंडेकर मुस्ताक अहमद ने किया। एक नई सरकार स्थापित हुई – मुस्ताक अहमद राष्ट्रपति बने और मेजर जनरल जियाउर रहमान को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया।
कुछ महीने बाद दूसरा तख्तापलट हुआ। 3 नवंबर को ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ, जिन्हें मुजीब का समर्थक माना जाता था, ने एक और तख्तापलट किया और खुद को नया सेना प्रमुख नियुक्त कर लिया। मुशर्रफ ने जियाउर रहमान को नजरबंद कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि बंगबंधु की हत्या के पीछे जियाउर रहमान का हाथ था।
तीसरा तख्तापलट: 7 नवंबर को तीसरा तख्तापलट हुआ। यह वामपंथी सैन्यकर्मियों द्वारा जातीय समाजवादी दल के वामपंथी राजनेताओं के साथ मिलकर किया गया था। मुशर्रफ की हत्या कर दी गई और जियाउर रहमान राष्ट्रपति बन गए। हालांकि 1991 में बांग्लादेश में संसदीय लोकतंत्र की वापसी हुई, लेकिन सेना का हस्तक्षेप नहीं रुका। 2006 में बीएनपी-जमात-ए-इस्लामी सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गई। नए चुनाव होने से पहले आवश्यक कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व करने के लिए उम्मीदवार चुनने को लेकर बीएनपी और अवामी लीग में ठन गई। उस वर्ष अक्टूबर में राष्ट्रपति इयाजुद्दीन अहमद ने स्वयं को कार्यवाहक सरकार का नेता घोषित किया और घोषणा की कि अगले वर्ष जनवरी में चुनाव होंगे।
हालांकि, 11 जनवरी 2007 को सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोईन अहमद ने सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व किया, जिससे सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार बनी। अर्थशास्त्री फखरुद्दीन अहमद को सरकार का मुखिया नियुक्त किया गया, जबकि राष्ट्रपति इयाजुद्दीन अहमद को अपना राष्ट्रपति पद बरकरार रखने के लिए मजबूर होना पड़ा।
मोईन ने सेना प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल एक साल और कार्यवाहक सरकार का शासन दो साल के लिए बढ़ा दिया। दिसंबर में राष्ट्रीय चुनाव होने के बाद 2008 में सैन्य शासन समाप्त हो गया और शेख हसीना सत्ता में आईं।