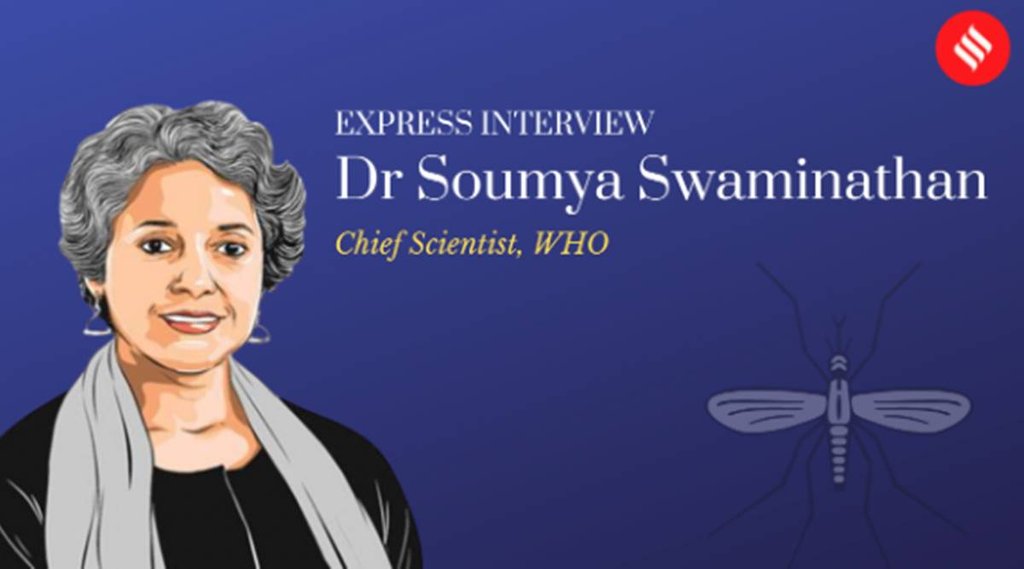विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ‘वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021’ के मुताबिक भारत मलेरिया के बोझ को कम करने में काफी हद तक सफल रहा है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में मलेरिया से होने वाली कुल मौतों में 82 परसेंट मौतें भारत से हैं, जो चिंता का विषय है। मलेरिया की पहचान, रोकथाम और खात्मे के रास्ते में आखिर क्या चुनौतियां हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है? इसी मसले पर डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने द इंडियन एक्सप्रेस समूह के ई. कुमार शर्मा से बातचीत की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश…
विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम ‘मलेरिया के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें’ ( Harness innovation to reduce the malaria disease burden and save lives) रखी गई है। मलेरिया की रोकथाम के लिए तमाम नई तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर आपका क्या विचार है?
कुछ देश काफी हद तक मलेरिया से लड़ने में सफल रहे हैं, लेकिन मलेरिया के पूरी तरह खात्मे से अभी हम बहुत पीछे हैं। साल 2020 में दुनिया भर में मलेरिया के करीब 241 मिलियन मरीज सामने आए और 6,27,000 मौतें दर्ज की गईं। सब-सहारन अफ्रीका में मलेरिया के सर्वाधिक मामले आए। कुल केसेज में से 95% मामले और कुल मौतों में से 96 फीसद वहीं से आए। मलेरिया से लड़ने के लिए तमाम नई पहल की जा रही है। मसलन- मच्छरों से लड़ने के लिए खास तरह की जाल आदि तो डिवेलप किए ही गए हैं, नई एंटीमैलेरियल दवाइयां भी आ गई हैं। साथ ही मलेरिया की नई वैक्सीन भी काफी कारगर है।
डॉ. सौम्या, मच्छरों में जेनेटिक मोडिफिकेशन विकल्प पर काम करने के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को इस विकल्प पर काम करना चाहिए
देखिये, अभी जीन-ड्राइव लार्ज स्केल पर लैब में ही टेस्ट हो रही है। फील्ड ट्रायल अभी कई साल दूर है। लैब टेस्ट के नतीजों पर ही तमाम चीजें निर्भर करती हैं। इन नतीजों के आधार पर ही डब्लूएचओ मलेरिया की रोकथाम के लिए जेनेटिक मॉडिफाइड विकल्प का सुझाव देगा।
आपके अनुसार भारत को मलेरिया पर प्रभावी रोकथाम के लिए कौन से 3 कदम उठाने चाहिए?
मेरा मानना है कि भारत मलेरिया की रोकथाम के लिए जो कदम उठा रहा है, उसमें और तेजी लाना चाहिए। सबसे पहला काम तो ह्यूमन रिसोर्स को और मजबूत करना चाहिए। केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर तमाम महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं, इनको भरना चाहिए। दूसरा- सर्विलांस सिस्टम को और मजबूत करना चाहिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नए टूल्स के रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश की भी जरूरत है। इससे न सिर्फ भारत को बल्कि दूसरे देशों को भी लाभ मिलेगा।
प्रवासी कामगारों के मोर्चे पर किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है?
देखें, प्रवासी कामगार खासकर ऐसे प्रवासी जो मलेरिया जनित गांव से शहरों की तरफ पलायन करते हैं, वे मलेरिया फैलाने के सबसे बड़े कारणों में से एक हैं। यही वजह है कि भारत के कई शहरों में मलेरिया अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इससे निपटने के लिए मजबूत सर्विलांस और रिस्पांस सिस्टम की जरूरत है।
इस बात पर अभी भी बहस होती है कि भारत में मलेरिया की समस्या सिर्फ कुछ इलाकों, खासकर ट्राइबल इलाकों में है। आपके अनुसार मलेरिया की रोकथाम में कौन सी चीजें बाधा बन रही हैं और क्या कदम उठाए जाने चाहिए?
देखिये, भारत ने मलेरिया की रोकथाम के लिए तमाम कदम उठाए हैं और काफी प्रगति की है। लेकिन अभी भी तमाम ट्राईबल कम्युनिटीज में मलेरिया का ज्यादा खतरा है और वहां तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। हालांकि सरकार ने आशा वगैरह को ट्रेनिंग दी है। इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। इन इलाकों में मलेरिया से निपटने के लिए ट्राइबल हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ-साथ एजुकेशन और फारेस्ट डिपार्टमेंट को भी साथ आना चाहिए।
क्या मलेरिया की पूरी तरह रोकथाम में के लिए क्रॉस बॉर्डर हेल्थ फ्रेमवर्क पर काम करना चाहिए?
भारत समेत साउथ ईस्ट एशिया रीजन के तमाम देशों में साल 2030 तक मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन तब तक अफ्रीका के तमाम देशों में मलेरिया पूरी तरह खत्म नहीं होगा। ऐसे में भारत में मलेरिया के दोबारा फैलने के काफी चांस हैं। जहां तक रही क्रॉस बॉर्डर फ्रेमवर्क की बात तो यह अभी भी है। भारत, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के बीच। हां…इस पर और बारीकी से काम करने की आवश्यकता है।
कोविड-19 महामारी ने मलेरिया की रोकथाम की दिशा में भी नकारात्मक असर डाला। आपके मुताबिक कोरोना वायरस महामारी से हमें क्या सबक लेना चाहिए?
मलेरिया की पहचान और उसके रोकथाम में कोरोना वायरस महामारी ने असर डाला है। इससे तमाम सबक भी लिया जा सकता है। भारत की बात करें तो से पहले हेल्थ सिस्टम, सर्विलांस, बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी तैयारी, सप्लाई चेन, केंद्र, राज्य और जिलों के बीच समन्वय बेहद जरूरी है। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी और मल्टी सेक्टर रिस्पांस पर भी काम करने की जरूरत है।
तमाम रिसर्च ऐसा इशारा करती हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ इलाकों में मलेरिया के केस बढ़ सकते हैं…
आज की तारीख में हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो इस तरफ इशारा करता हो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मलेरिया के रोकथाम पर असर पड़ेगा। इस पहलू पर बारीकी से नजर रखी जा रही है।