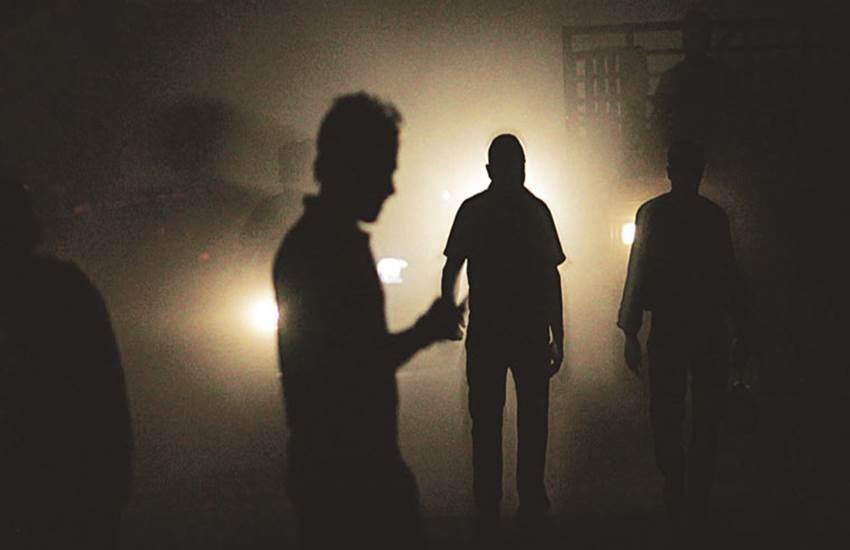एक बार फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर के सबसे प्रदूषित शहरों की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के आते ही भारत में प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सरकारी एजेंसियों ने राहत की सांस ली है। यह तसल्ली खासकर दिल्ली को लेकर है। दो साल पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसी तरह की अपनी रिपोर्ट में दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर करार दिया था। इसके बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण घटाने की कोशिशों में तेजी आई और हाइकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया तो इसके पीछे डब्ल्यूएचओ के अध्ययन का भी असर रहा होगा। पर अब डब्ल्यूएचओ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर होने का कलंक दिल्ली के माथे से मिट गया है। यही नहीं, दुनिया के सर्वाधिक दस प्रदूषित शहरों में भी उसका नाम नहीं है। फिर भी भारत को चिंतित करने वाली बहुत-सी बातें हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर अब भी सामान्य के दोगुने से अधिक है। फिर, बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है।
बीस सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाले शहरों में आधी हिस्सेदारी अकेले भारत की है। अलबत्ता इसमें भी भारत ने सुधार किया है। दो साल पहले आई रिपोर्ट में बीस शहरों की इस तरह की सूची में भारत के तेरह शहरों के नाम थे। उनमें से आगरा, अमृतसर और अमदाबाद ने अपना रिकार्ड सुधारा है। भारत के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर उत्तर भारत के हैं। सवाल है कि रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों की रोशनी में हमें क्या निष्कर्ष हासिल होते हैं और क्या दिशा मिलती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट आते ही आप सरकार श्रेय लेने में जुट गई है। शायद वह जताना चाहती है कि दिल्ली की हवा में आया थोड़ा-सा सुधार सम-विषम जैसे उसके प्रयासों की देन है। पर असल में पंद्रह दिनों के दो बार के इस प्रयोग से ज्यादा दूसरे कारक प्रभावी रहे। सीएनजी के इस्तेमाल का बढ़ता दायरा, बाहरी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर पर्यावरण शुल्क, अन्य राज्यों को जाने वाले ट्रकों के दिल्ली से होकर गुजरने पर रोक, कई कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का बंद होना आदि अनेक कदम दिल्ली में वायु प्रदूषण घटाने में मददगार साबित हुए। पर ताजा रिपोर्ट सिर्फ तुलनात्मक रूप से राहत की तस्वीर कही जा सकती है।
अगर इंसानी सेहत के पैमाने से देखें तो हालत अब भी काफी चिंताजनक है और बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। स्थिति की भयावहता का अंदाजा विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस निष्कर्ष से लगाया जा सकता है कि वायु प्रदूषण अकाल मौतों की पांचवीं सबसे बड़ी वजह है। जो लोग मौत की चपेट में नहीं आते, पर प्रदूषित हवा में जीने को विवश हैं, वे तरह-तरह की बीमारियों को न्योता देते रहते हैं। यों हमारे संविधान के अनुच्छेद इक्कीस में गरिमापूर्ण ढंग से जीने की गारंटी दी हुई है। फिर, संयुक्त राष्ट्र मानता है कि स्वस्थ जीवन हरेक इंसान का बुनियादी हक है। पर ऐसी घोषणाओं का क्या मतलब, अगर जीने की परिस्थितियां गरिमापूर्ण और स्वास्थ्यप्रद न हों? विडंबना यह है कि प्रदूषण के मसले को स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के नजरिए से आमतौर पर देखा ही नहीं जाता। पर अब जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि जन-स्वास्थ्य के सार्वजनिक लक्ष्य के लिहाज से इस पर सोचना जरूरी हो गया है। इससे हमारे नीति नियंताओं व क्रियान्वयन-कर्ताओं पर कुछ कारगर कदम उठाने का दबाव पड़ेगा, जो कि पर्यावरणीय संकट के इस दौर में एक बहुत अहम तकाजा है।