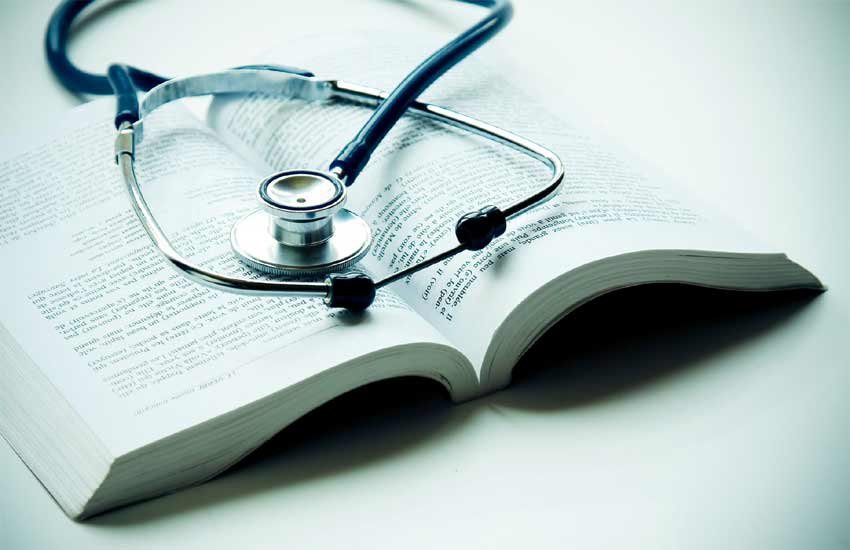जब हम किसी व्यक्ति, समुदाय, समाज, राज्य या विश्व की चिंताओं के बारे में सोचते हैं तो प्रमुख समस्या के रूप में आज भी रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा की समस्या सामने उभरती है। गौण बातों में हम सम्मिलित करते हैं- शिक्षा और स्वास्थ्य। इसके बाद असंख्य बातें और भी होती हैं, जिनको लक्ष्य बना कर समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। विख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने दो मसलों शिक्षा और स्वास्थ्य को जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने में बहुत ही जरूरी माना है और यह समझाने का प्रयास किया है कि उपरोक्त दोनों में यथोचित परिवर्तन करके जीवन के स्तर में पर्याप्त और सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। देखा जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य मात्र चुनावी नारा नहीं हैं और न ही सरकारी नीतियों और अनुदानों पर निर्भर हैं। किसी भी लोकतांत्रिक या लोक-कल्याणकारी राज्य का यह प्रथम दायित्व है कि वह नागरिकों की इन आधारभूत जरूरतों को पूरा करे। पर यहां एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या लोगों की अपनी भूमिका नहीं है? क्या सरकार को अनिवार्य रूप से लोगों की उन जरूरतों को पूरा करना चाहिए?
रोटी, कपड़ा और मकान की बहुत ही जरूरी और आधारभूत समस्याओं के साथ-साथ स्वास्थ्य के प्रश्न को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए और ये सारी जरूरतें कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ती भी हैं। व्यक्ति और समूचे समाज का जीवन, उसका वर्तमान और भविष्य उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। स्वस्थ रहने के लिए उचित दृष्टिकोण, स्थानीय संसाधन, उपचार और प्रकृति के साथ लयात्मक संबंध बहुत ही जरूरी हैं। यहां उचित दृष्टिकोण से तात्पर्य है- एक संतुलित दृष्टि या वैज्ञानिक दृष्टि।
स्वास्थ्य के समूचे मसले को हम मूलत: दो नजरिए से देखते हैं। पहला, उपचारात्मक और दूसरा, सुरक्षात्मक। पूंजीवाद और वैश्वीकरण के चलते हमारा पूरा स्वाथ्य-चिंतन उपचारात्मक उपायों के इर्द-गिर्द ही घूम रहा है और सुरक्षात्मक उपाय लगभग नगण्य हो चले हैं। वैश्विक-आर्थिक संस्थाएं, राज्य की मशीनरी और डॉक्टर व चिकित्सा अधिकारी तंत्र उपचारात्मक तरीकों पर ही बल देते हैं क्योंकि इससे उनके आर्थिक हितों की पूर्ति होती है। उनकी चिंता स्वास्थ्य को बनाए रखने की जगह रोक की चिकित्सा को लेकर रहती है। इसमें बाजार तंत्र और अर्थतंत्र की जबर्दस्त सांठगांठ है जिसे आम आदमी अक्सर समझ नहीं पाता और चिकित्सा-बाजार के इस चंगुल में फंसता चला जाता है। इस दुश्चक्र से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसमें बैंक, जीवन बीमा कंपनियां और सरकारें सभी सम्मिलित हैं। स्वास्थ्य के प्रश्न पर इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखना होगा।
उपचारात्मक स्वास्थ्य-दृष्टि के चलते हमारी निर्भरता दवाइयों पर बढ़ती जाती है। इससे जहां अकल्पनीय आर्थिक नुकसान होता है वहीं हम शरीर के अन्य हिस्सों पर इन दवाइयों के पड़ने वाले दुष्प्रभावों से भी नही बच सकते। इसकी वजह से हमारे पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन का अधिकांश समय स्वास्थ्य संबंधी उलझनों में ही फंसा रहता है। खराब स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव जहां जीवन पर पड़ता है वहीं पारिवारिक विकास, समृद्धि, रोजगार और संपत्ति भी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। सच ही कहा गया है कि ‘जान है तो जहान है’।
अब चर्चा कर सकते हैं कि सुरक्षात्मक स्वास्थ्य क्या है? इसे कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? इसके फायदे क्या हो सकते हैं? व्यक्तिगत, सामाजिक और वैश्विक विकास में इसका क्या योगदान है? क्या यह काल्पनिक और आदर्शात्मक है, या व्यावहारिक और अनुकरणीय? क्या इसे विश्वास या श्रद्धा के साथ जोड़ कर देखा जा सकता है? या फिर इसे विवेक, अनुभव और ज्ञान के आधार पर देखा जाए?
एक और भी चौंकाने वाली स्थिति यह है कि स्वास्थ्य की समस्या स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। इसमें बहुत ही जबर्दस्त पेच है जिसे हम भाग्य या भगवान का खेल या फिर सामान्य दिनचर्या मान कर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया में इतनी षड्यंत्रकारी और नकारात्मक ताकतें संलग्न हैं कि स्वास्थ्य स्वतंत्र चिंतन का विषय ही नहीं बन पा रहा है। इस पर एक तरफ तो डॉक्टरों, सरकारी तंत्र, देशी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा है तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य की ठेकेदारी पर बाबा, मौलवी, पादरी, ओझा, तथाकथित आध्यात्मिक गुरु, चमत्कारी पुरुष तथा उनके दलालों का भी बड़ा दबदबा है।
अधिकतर लोग इनके चक्कर इसलिए नहीं लगाते कि उन्हें किसी प्रकार की आध्यात्मिक शांति या दिव्य ज्ञान की जरूरत होती है, बल्कि वहां खराब स्वास्थ्य ही उनकी भागदौड़ के केंद्र में होता है। स्वास्थ्य से जुड़ी और भी उलझनें हैं जैसे नपुंसकता की समस्या, बच्चा न होने की समस्या, कामोत्तेजना की कमी, पुत्र-प्राप्ति की लालसा, सुंदरता और चिर-युवा बने रहने की इच्छा आदि। देखा जाए तो उचित जानकारी के अभाव में या पूर्वाग्रहों के कारण या गलत-सलत धार्मिक मान्यताओं के असर में बहुत-से लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं या ऐसे व्यक्तियों की शरण में जाते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य तबाही के कगार पर पहुंच जाता है। जब हालात काबू से बाहर हो जाते हैं तो यही लोग बाबाओं, फकीरों, पादरियों के यहां झाड़-फूंक के लिए चक्कर लगाते रहते हैं। इससे उनकी कोई समस्या हल होने का तो सवाल ही नहीं उठता, बल्कि जिन समस्याओं में वे पहले से फंसे होते हैं वे और गहरी होती जाती हैं और अंतत: उनका जीवन दुश्चक्र बन जाता है।
सुरक्षात्मक स्वास्थ्य से तात्पर्य है कि शरीर को इस योग्य बनाया जाए कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके और दवाइयों की जरूरत कम से कम पड़े। इसके लिए सबसे महत्त्वपूर्ण है स्वास्थ्य-जागरूकता, स्वास्थ्य के प्रति चेतना और स्वास्थ्य केंद्रित सरकारी योजनाएं आदि। पर यहां एक यह भी बात सामने आती है कि सक्षम व्यक्ति तो व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उपरोक्त सुविधाओं का लाभ उठा सकता है, पर जो समर्थ नहीं हैं उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उनके लिए सरकार को आगे आना होगा। पर जहां स्वास्थ्य की जिम्मेदारी व्यक्तिगत होती है वहां इसका उत्तरदायित्व सामाजिक संगठनों और अंतत: राज्य और वैश्विक समाज को लेना होगा। इसमें भी कार्यक्षेत्र को दो भागों में बांटना होगा- व्यक्तिगत स्वास्थ्य का क्षेत्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य का क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र की पूरी जिम्मेवारी सरकारों को लेनी होगी, क्योंकि सार्वजनिक स्तर पर स्वास्थ्य की समस्याएं अंतत: व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों को प्रभावित करती हैं।
वैश्वीकरण के युग में विकास मुख्य चुनौती के रूप मे उभरा है। इसी के मद्देनजर सितंबर 2000 में न्यूयार्क में 189 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वावधान में ‘सहस्राब्दी विकास लक्ष्य’ स्वीकार किया, जिसके तहत कुपोषण मिटाने और मातृ और शिशु मृत्यु दर पर काबू पाने सहित अनेक लक्ष्य तय किए गए। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को अंगीकार करने वाले तमाम देशों में भारत भी शामिल है। पर इसे स्वीकार किए जाने के डेढ़ दशक बाद भी हालत यह है कि भारत के चालीस फीसद से पैंतालीस फीसद बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। संयुक्त राष्ट्र की ताजा मानव विकास रिपोर्ट बताती है कि भारत के वैश्विक औसत से नीचे बने रहने के पीछे शिक्षा और स्वास्थ्य, इन मोर्चों पर उसका पिछड़ना है। जिस देश का स्वास्थ्य-सूचकांक अच्छा है उस देश का मानव विकास सूचकांक, सामाजिक प्रगति सूचकांक, लैंगिक समानता सूचकांक, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक बेहतर हैं।
स्वास्थ्य के न केवल शारीरिक या चिकित्सीय आयाम हैं बल्कि उसके सामाजिक पहलू भी होते हैं। अत: स्वस्थ होने या रहने के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। जबकि बाजारीकरण के इस दौर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव के कारण स्वास्थ्य को मात्र रोग न होने की स्थिति के रूप में प्रचारित किया जाता है। कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य या स्वास्थ्य संबंधी चिंतन, कार्यक्रम और प्रयास एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। जब तक लोग होंगे, समाज होगा और समाज का संचालन के लिए राज्य या अनेक राज्य होंगे, स्वास्थ्य का मुद््दा सदैव जीवंत और जरूरी बना रहेगा। स्वस्थ मानव जीवन किसी भी समाज, राज्य या राष्ट्र के लिए अवसर प्रदान करता है। इससे कुशल और दक्ष मानव-संसाधन तैयार किए जाते हैं। इससे निश्चित ही सामाजिक विषमता कम होगी, गरीबी-बेरोजगारी आदि को पूरी तरह तो नहीं मगर बहुत हद तक कम तो किया ही जा सकता है। यह हमें सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर भी अग्रसर करेगा। वैश्विक स्तर पर भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। सुरक्षात्मक स्वास्थ्य के लिए सरकारों को ऐसे उपाय और नीतियां बनानी होंगी जिससे व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्तर पर भी बीमारियों और संक्रामक रोगों की आशंकाएं कम की जा सकें। इसके लिए वैश्विक स्तर पर एक आपसी समझ उत्पन्न करनी होगी ताकि विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के अनुपालन का एक वैज्ञानिक आधार बन सके।
भारत की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जहां स्वास्थ्य के मद में सरकारी खर्च बहुत कम होता है। चीन और ब्राजील में यह जीडीपी के तीन फीसद के करीब है, जबकि भारत में एक फीसद के आसपास। इस एक फीसद का भी पूरी तरह सदुपयोग नहीं होता। आबंटित रकम का एक खासा हिस्सा बदइंतजामी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इसका सबसे ज्यादा खमियाजा समाज के कमजोर तबकों को भुगतना पड़ता है, जो निजी अस्पतालों का खर्च नहीं उठा सकते और सार्वजनिक चिकित्सा व्यवस्था पर पूरी तरह आश्रित हैं। यों सबको चिकित्सा सेवाओं के दायरे में लाने की बात जब-तब होती है, पर वास्तव में नीतियों की दिशा इससे उलट है।