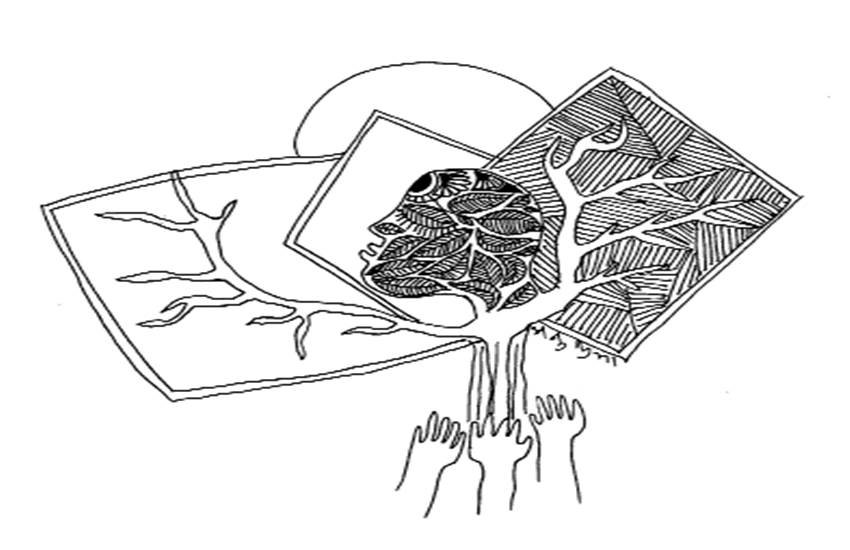पिछले दस-बारह सालों में, दो-तीन साल को छोड़ कर, विकास दर के लिहाज से भारत की उपलब्धि शानदार रही है। लेकिन आम लोगों की हालत की कसौटी पर देखें तो यह कामयाबी प्रतिबिंबित नहीं होती। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से हर साल आने वाली मानव विकास रिपोर्ट बता देती है कि आम लोगों के रहन-सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मानकों पर हम दुनिया के सबसे पिछड़े व बदहाल मुल्कों के बीच खड़े हैं। खुद राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जैसे सरकारी अध्ययन भी विकास के दावों और हकीकत के बीच की गहरी खाई की ओर ही इशारा करते हैं।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने एक बार फिर भारत के जन-स्वास्थ्य की निराशाजनक तस्वीर पेश की है। यह सर्वेक्षण तेरह राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों में किया गया। जिन राज्यों को शामिल किया गया उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और दो केंद्रशासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और पुदुच्चेरी शामिल हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ताजा दौर के बाकी देश के आंकड़े इस साल के अंत तक जारी होने की संभावना है। पर जारी हुई रिपोर्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी राज्यों की हालत कोई अलग नहीं होगी। रिपोर्ट ने बड़े पैमाने पर बच्चों के कुपोषण का शिकार होने की कड़वी सच्चाई स्वीकार की है।
रिपोर्ट के मुताबिक चालीस फीसद से ज्यादा बच्चे अल्प-विकसित हैं। अल्प-विकास का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि इसका मतलब मानसिक क्षमता या सीखने की क्षमता का विकास न हो पाने और भविष्य में उत्पादकता की कसौटी पर खरे न उतरने से भी है। आज विश्व भर के अल्प-विकसित बच्चों की संख्या का तैंतीस फीसद भारत में है। वहीं यूनिसेफ के मुताबिक भारत में पांच साल से कम उम्र के अड़तालीस फीसद बच्चे अल्प-विकसित हैं। कुपोषण की चपेट में बड़े होने वाले बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता का अभाव रहता है और वे बीमारियों के जल्दी शिकार होते हैं।
एक तरफ हम कौशल विकास और ज्ञान आधारित समाज बनाने की बातें करते रहते हैं और दूसरी तरफ देश के हर दूसरे बच्चे का अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है। चमकते नारों और विकास के बड़बोले दावों के बरक्स, वास्तव में भारत का कैसा भविष्य बन रहा है! विभिन्न रिपोर्टों के आकलन में थोड़ा-बहुत हेर-फेर हो सकता है, मगर ये सारी रिपोर्टें भारत में कुपोषण की व्यापकता ही बयान करती हैं। कहने को एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम और मिड-डे मील जैसी योजनाएं कुपोषण निवारण के लिए ही चलाई जाती हैं, पर वे निहायत अपर्याप्त आबंटन और लचर कार्यान्वयन की शिकार हैं।
लड़कों की बनिस्बत लड़कियां ज्यादा कुपोषित हैं। सत्तर फीसद किशोरियां अनीमिया यानी खून की कमी की शिकार हैं। आगे चल कर जब वे मां बनती हैं तो इसका असर भ्रूण और शिशु पर भी पड़ता है। इसलिए कुपोषण निवारण की नीति और कार्यक्रम को हर हाल में बालिका स्वास्थ्य और माताओं के स्वास्थ्य से जोड़ना होगा। कुपोषण का एक पहलू गरीबी और वंचना से ताल्लुक रखता है तो दूसरा आहार संबंधी खराब आदतों और अस्वास्थ्यकर जीवनशैली से।
परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट जहां अभाव-जनित कुपोषण की व्यापकता को बयान करती है, वहीं यह भी बताती है कि सर्वेक्षण में शामिल किए गए राज्यों में दस में से तीन महिलाएं मोटापे की शिकार हैं। जाहिर है, अब भारत कुपोषण के दोहरे खतरे से जूझ रहा है। अगर स्वस्थ भारत के सपने को साकार करना है तो इस खतरे को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए।