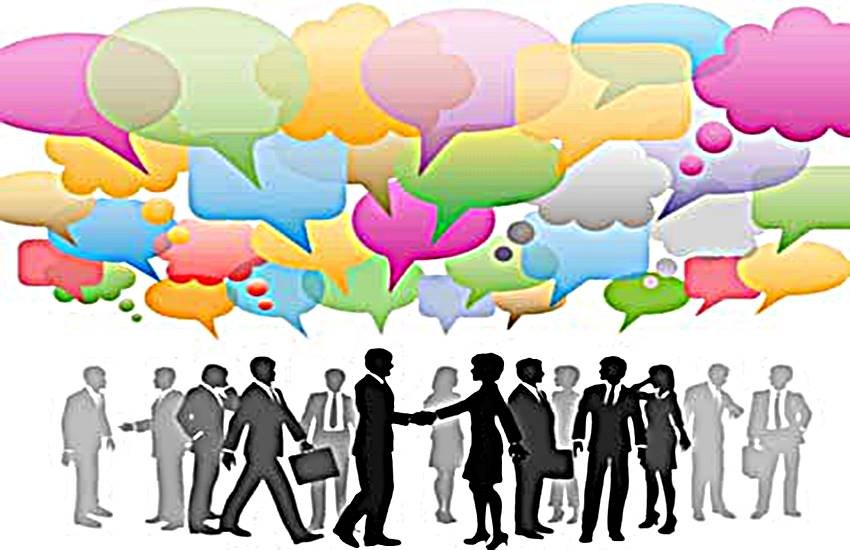एक लंबे अरसे से भारतीय समाज में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो सभी चेतनशील नागरिक को असहज बनाता है। सड़क दुर्घटना होने पर देख कर भी आगे बढ़ जाने, लड़ाई-झगड़े में चुप रह कर अपनी असहायता दर्शा देने और रिश्तेदार या पड़ोसी होने के बावजूद हिंसा की घटना के बाद तुरंत कुछ करने के बजाय संबधित व्यक्ति को मरने देने के वाकये आम हैं। ये कुछ ऐसे पक्ष हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि ये हमारे आम चरित्र के परिचायक हैं। कुछ समय पहले दिल्ली के विकासपुरी में एक डॉक्टर की हत्या, तमिलनाडु में कथित सम्मान के नाम पर एक दलित युवक की हत्या और उसकी पत्नी को बुरी तरह घायल कर देना या फिर छोटे-मोटे अपराधों को लेकर बच्चों की पिटाई और उन्हें निर्वस्त्र करके गांव में घुमाना ऐसी घटनाएं हैं जो हमें सोचने को मजबूर करती हैं कि क्या हमें हिंसक और आक्रामक होने की शिक्षा जन्म से दी जाती है!
ऐसी घटनाओं के बाद महात्मा गांधी की याद आना स्वाभाविक है, जिन्होंने अहिंसा को एक जीवन मूल्य के रूप में अपने व्यक्तित्व का न केवल हिस्सा बनाया, बल्कि उसे स्वाधीनता संघर्ष में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। कहीं सांप्रदायिक दंगे जैसी घटना होने पर हिंसक लोगों के बीच अकेले खड़े हो जाना गांधी को शक्तिशाली बनाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। क्या इसके पीछे हमारी अपनी सुरक्षा की भावना इतने गहरे बैठी हुई है? दिल्ली के विकासपुरी में सारे पड़ोसी अपने मकान से पंकज नारंग को पिटते और मारे जाते हुए देखते रहे। किसी गांव में भाईचारे की चर्चा करने वाले लोगों ने महज खानपान की अफवाह के आधार पर अपने पड़ोसी की जान ले ली। यह दर्शाता है कि हमारे भीतर मानवीय मूल्यों की कितनी कमी होती जा रही है।
हालांकि हमारी संस्कृति मानवीय होने का सदियों से दावा करती रही है। असल में हिंसा कायरता का दूसरा रूप है, जिसका परिचय लोग हमेशा ही देते रहे हैं। दिल्ली में डॉ पंकज नारंग का केवल इतना ही दोष था कि गेंद लगने के बाद मोटरसाइकिल से गुजरते लड़कों के कुछ कहने पर कोई जवाब दे दिया। वही उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। ऐसे अवसरों पर पुलिस-प्रशासन की भूमिका और राजनीतिक हस्तक्षेप अनेक सवाल पैदा करते हैं। ऐसा लगता है कि हम सब कई बार लोगों को बिना तथ्यों के जाने-समझे लांछित कर देते हैं या फिर उसे पीट-पीट कर बेहाल कर देते हैं या मार डालते हैं। लेकिन क्या इससे लांछन भी मर जाता है?
समाज विज्ञान में एक सूत्र है- अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। इस तर्क को हर स्तर पर इसलिए स्थापित किया जाता है कि अपराध सामाजिक विसंगतियों की उत्पत्ति है। अपराधी तो केवल व्यक्ति भर है। इसलिए सुधारवादी दंड एक महत्त्वपूर्ण जनतांत्रिक विशेषता बना। पर हम इसे धार्मिक, नस्लीय, जातीय और लैंगिक अस्मिताओं के कारण सामाजिक जीवन में स्वीकार नहीं कर सके। डॉ नारंग की हत्या की तरह की अन्य घटनाएं इस अस्वीकृति को दर्शाती हैं। ऐसे मामलों में शायद कानून का शासन लोगों को स्वीकार नहीं हो पाता है, क्योंकि दंड देने और निर्णय लेने का अधिकार हमें हमारे धार्मिक, नस्लीय, जातीय और लैंगिक समूहों ने प्रदान किया है। नतीजतन, लोकतांत्रिक मूल्यों में हमारी प्रतिबद्धता महज एक छलावा नजर आती है।
मुख्य रूप से यह शिक्षा और जनमत की पराजय है। हम शायद यह सोच पाने में असमर्थ हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली बिना न्याय, समानता और स्वतंत्रता के चल नहीं सकती। कानून हमारी जीवन शैली का एक ऐसा हिस्सा है जो अनेक अवसरों पर पीड़ित होने के बावजूद हमें सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है और हम कहते हैं कि ‘कानून को अपना काम स्वतंत्रता से करने दीजिए।’ यह वाक्य हालांकि अनेक अवसरों पर विषयपरक और पूर्वग्रही भी हो जाता है। खासतौर पर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कानून के सम्मुख सबकी समानता का मूल्य पूरी तरह से लागू नहीं होता जो कि मानवाधिकारों के हनन से जुड़ जाता है।
यहां एक सवाल और महत्त्वपूर्ण है। क्या इस तरह की घटनाएं सोची-समझी होती हैं या फिर भावावेश में हो जाती हैं? अपराध तो अपराध ही है, लेकिन अगर भावावेश में किया जाता है तो फिर यह समाजीकरण का दोष है। और अगर सोचा-समझा हुआ है तो फिर यह आक्रामकता और हिंसा की संस्कृति के हमारी जीवन-शैली का हिस्सा होने का परिचायक है। कारण चाहे कोई भी हो, पर ऐसी घटनाओं और तात्कालिक आवेग की आक्रामकता से कोई हंसता-खेलता परिवार तो बिखर कर रह जाता है। हमारे सामने यह सवाल है कि क्या हम एकजुटता के साथ हिंसा और आक्रामकता का मुकाबला नहीं कर सकते? हो सकता है कि अभी हम इन सवालों को स्थगित कर दें, लेकिन भविष्य में कभी न कभी इन सवालों के जवाब तो खोजने ही होंगे, क्योंकि बिल्ली के आंखें बंद करने का मतलब यह नहीं है कि खतरा टल गया है।
ज्योति सिडाना