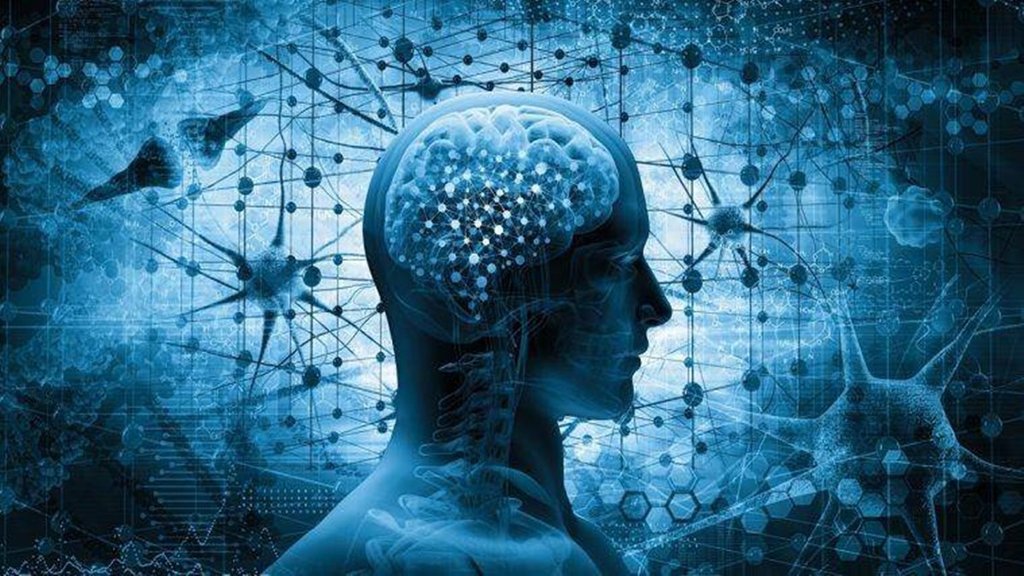रीना स्वामी
लेकिन पिछले कुछ समय से खबरों पर नजर दौड़ाते हुए आनंद पर वेदना के काले बादल मंडराने लगे हैं। वजह यह है कि अमूमन हर रोज आत्महत्या की घटनाएं दहलाने लगी हैं। दिमाग में लगातार अनुत्तरित सवाल गोते लगाने लगते हैं कि आखिर आत्महत्या का यह सिलसिला कब रुकेगा! कब मनुष्य जीवन को गले लगाएगा? कब वह इस मानव जीवन की खूबसूरती को समझ पाएगा? क्या वाकई मानव का जीवन इतना सस्ता हो गया है? भारतीय दर्शन तो जीवन को एक उत्सव मानता आया है! सुख-दुख, हर्ष-विषाद, अमीरी-गरीबी, प्रेम-धोखा, सम्मान-तिरस्कार, सुखमय जीवन हो या कलहपूर्ण, बीमारी हो या निरोगी काया, इनमें से किसी भी परिस्थिति से मनुष्य क्यों न गुजर रहा हो, लेकिन जीवन का अंत करने का अधिकार उसे नहीं है।
इस विश्वव्यापी समस्या का समाधान ढूंढ़ना है तो हमें भारतीय जीवन दर्शन और साहित्य में झांकना पडेÞगा। भारतीय जीवन दर्शन और साहित्य मनुष्य को जीवन में प्रवृत्त होने का संदेश देते हैं, न कि निवृत्त होने का। मध्यकालीन भक्त कवयित्रियों का जीवन और साहित्य इसका बेहतरीन उदाहरण है। इनमें अंडाल, अक्कमहादेवी, ललद्यद, मीरा और ताज प्रमुख हैं। इन्होंने जीवन में जितने कष्ट, पीड़ा, निंदा और तिरस्कार सहन किया, उतना किसी के लिए भी सहना कठिन है। उनका रास्ता आसान नहीं था।
मध्यकाल में समाज की कमजोर जातियों-तबकों के सामने कैसी दुश्वार स्थितियां थीं, यह छिपा नहीं रहा है। स्त्री भक्तों को परिवार और समाज के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे वे टूटकर बिखरी नहीं, बल्कि इससे उन्हें एक आंतरिक शक्ति प्राप्त हुई। कश्मीरी कवयित्री ललद्यद को ससुराल में सास की कटु आलोचनाओं और यंत्रणाओं का सामना करना पडा। मां न बन पाने के कारण समाज के ताने भी उन्हें सुनने पड़े।
उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए लिखा है- ‘मैं उसी उमंग और चाव के साथ इस संसार में खिली थी, जिस उमंग और चाव के साथ कपास के डंठल पर फूल खिलता है। पर बेलने की रगड़ और पिंजयारे की धुनकी ने मेरी खूब गत बनाई… बारीक बनाते-बनाते मेरा कण-कण उखाड़ लिया।’ योग और सांख्य में कितनी शक्ति है, यह दर्शन जीवन संघर्ष में मनुष्य की कितनी बड़ी सहायता कर सकता है, यह ललद्यद के काव्य में देखा जा सकता है। वे इस सत्य से परिचित थीं कि संसार परिवर्तनशील है, अनित्य है, पर शून्य नहीं है। संसार वास्तविक है और कुछ समय के लिए है। अगर इसमें रहना है तो विरोध का सामना तो करना ही होगा। ये भक्त कवयित्रियां निंदा और स्तुति की चिंता न करके धैर्य से जीवन बिताना चाहती हैं।
राजस्थान की प्रसिद्ध कवयित्री मीरा का जीवन तो उस विशाल समुद्र की भांति था, जिसमें निंदा, तिरस्कार, लांछन और वेदना के विशाल भंवर और ज्वार प्रतिदिन उठते रहते थे, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। मीरा को समाज ने ‘कुलटा’, ‘बिगड़ी’, ‘कुलनाशी’ नामों से संबोधित किया, जिसकी सेज सूली पर थी, जिसके लिए पीने को जहर था और आभूषण की जगह सर्प। समाज की परवाह मीरा को नहीं थी। मीरा अपने शर्तों पर जीवन जीती रहीं। प्रतिकूल परिस्थिति में मीरा की इच्छा अपनी इहलीला समाप्त करने की नहीं होती, बल्कि स्त्री जीवन को एक उत्सव मानकर उसे आनंदित होकर जीने की होती है।
बेशक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कई बार समाज का डर ही मनुष्य को अपना जीवन नष्ट करने को बाध्य कर देता है। असफलता, गरीबी, प्रेम संबंधों का उद्घाटन अपराध का प्रकटीकरण आदि कारणों से जो लोग आत्महत्या करते हैं, उसके पीछे समाज का डर ही होता है। मनुष्य को समझना होगा कि जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है, समाज भी नहीं ।
भूमंडलीकरण और बाजारवाद ने मनुष्य में संग्रह और देखादेखी की प्रवृत्ति को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। इसके कारण मनुष्य अधिक धन कमाने के चक्कर में मानसिक अवसाद का शिकार होकर अपने बहुमूल्य जीवन गंवा रहा है। आर्थिक संकट के दौर में भी मनुष्य अपनी आवश्यकता को सीमित कर जीवन जी सकता है। प्रसिद्ध कन्नड़ कवयित्री अक्कमहादेवी के वचन इसकी प्रेरणा देते हैं। अक्कमहादेवी कहती हैं- ‘भूख लगने पर भीख मिल सकती है/ प्यास लगने पर तालाब, नदी और कुएं हैं/ सोने के लिए पुराने देवालय हैं/ हे मल्लिकार्जुन, मेरे साथ रहने के लिए तू है’।
एकाकीपन आज के महानगरीय जीवन की गंभीर समस्या है। इसके चलते मनुष्य को कभी-कभी अपना जीवन व्यर्थ, रूखा और बोझिल लगता है और अपने जीवन को समाप्त करना इसका एकमात्र समाधान। आत्महत्या एक ऐसी विश्वव्यापी समस्या है, जिसका संबंध मन से है, मनोदशा से है। इस समस्या के निराकरण में न तो सरकार कुछ कर सकती है न ही समाज या परिवार। सकारात्मक सोच, मजबूत मन और प्रतिकूल परिस्थितियों को डटकर सामना करने की इच्छाशक्ति ही इस समस्या का समाधान कर सकती है।