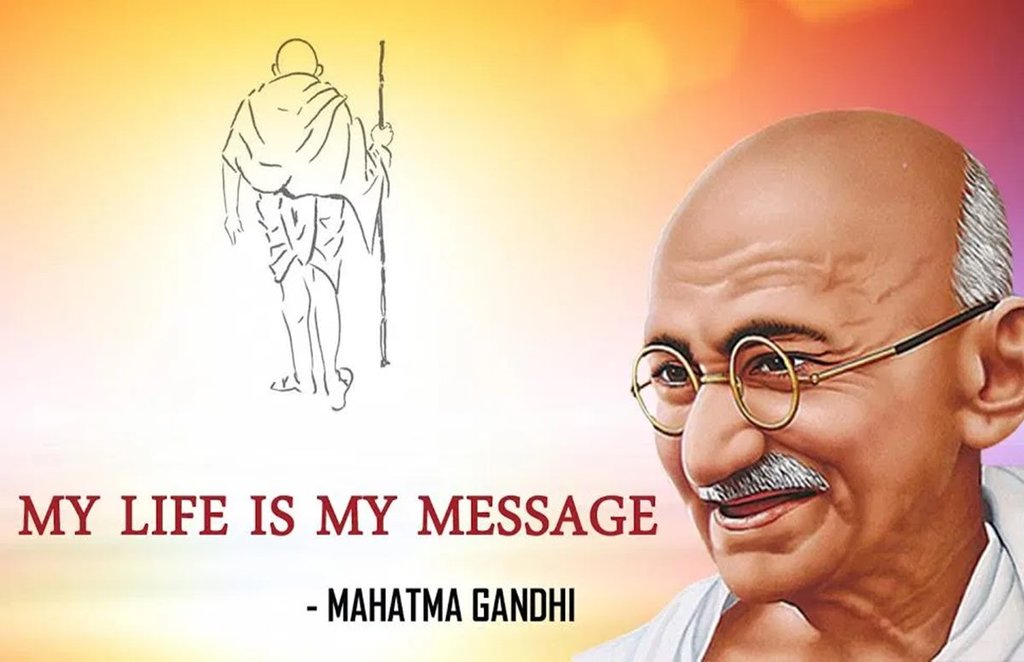नंदितेश निलय
वे लोग कुछ खास होते हैं जो अपना भी हिसाब-किताब रखते हैं। उस दिन सोमवार था यानी, महात्मा गांधी के मौन का दिन। संध्या के समय ही यह मौन समाप्त होता था। गांधी अपनी डायरी के पन्नों को पलट रहे थे। अचानक उन्होंने बगल में बैठे अपने शिष्य की ओर देखा। उस शाम जब ट्रेन पटना स्टेशन पहुंचने वाली थी तो महात्मा गांधी ने अपने एक शिष्य से उस चिट्ठी के बारे में पूछा, जिसे पटना में किसी को देना था।
उन्होंने वह चिट्ठी वायसराय को लिखी थी। हुआ यह था कि वह चिट्ठी टाइप ही नहीं हुई थी। बगल के डिब्बे में बैठे एक पत्रकार से टाइपराइटर लेकर चिट्ठी रेलगाड़ी में ही टाइप की गई और पटना स्टेशन पर दे भी दी गई। गांधी किसी काम को अधूरा छोड़ने में भरोसा नहीं करते थे। उनकी डायरी मानो वह आईना रही जो उनका चेहरा नहीं, बल्कि मन की छवि दिखाती थी।
दरअसल, गांधी समय से कुछ आगे चलते थे और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को ढूंढ़ते थे। सुबह चार बजे उठना, प्रतिदिन लिखना-पढ़ना, पांच किलोमीटर की सैर करना, कम खाना, आश्रम के काम में हाथ बंटाना, लोगों को सुनना और उन खतों का जवाब देना और साथ-साथ उस बकरी को समय देना।
ये कुछ ऐसी आदतें थीं जो उन्हें निराश नहीं होने देती थी और यों कहें कि उत्साह से लबरेज रखती थीं। इस दौर में हमें भी आदतों की डायरी को पलटने की जरूरत है। महात्मा गांधी अंत तक कबीर की उक्ति को चरितार्थ करते रहे कि ‘जस की तस धरी दीनी चदरिया!’ मुश्किल की घड़ी अच्छी आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
एक इंसान के रूप में हमारे दिन भर के सकारात्मक कर्म हमें कभी भी उदास नहीं होने देते। वह भी ऐसे वक्त, जब मृत्यु बस मास्क से कुछ दूरी पर खड़ी नजर सभी को आती हो। ऐसे स्थिति में यह जरूरी है कि महात्मा गांधी की उन आदतों को ऐसे मुश्किल दौर में अपनाया जाए। खासकर उनकी सादगी, संवेदशीलता को संभालने की जरूरत है।
अगर हम दो गज की दूरी बना कर रखते हैं और साथ-साथ मास्क भी पहने रहते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि हम सभी के लिए जी रहे हैं। जितना हमारा जीवन कीमती है, उतना हम सभी का जीवन कीमती मानते हैं। यह दौर सिर्फ कर्म का ही नहीं है बल्कि प्रार्थना का भी है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए किया जाए, गांधी की तरह।
महात्मा गांधी यह मानते रहे कि संसार की उथल-पुथल और झंझावत में रहते हुए भी जो मनुष्य अपनी मानसिक शांति को कायम रख सके, वही सच्चा इंसान है। जब हम इस महामारी के बीच अपने जीवन को और अनुशासन से जीने की कोशिश करते हैं तो मन की उद्विग्नता भी कम होती है। पर उस काम से अनुराग होना चाहिए। तभी अनुशासन के साथ हम जिएंगे।
अगर कुछ पढ़ा- लिखा जाए और अपनी गलतियों को माना जाए, सुधारा जाए तो यह दौर आत्मावलोकन के दौर से कम नहीं होगा। कई बार हम सकारात्मक बनने के चक्कर में अपने शब्दों के अर्थ को खो बैठते हैं या अपने परिवार या बच्चों के लिए भाषण से ज्यादा कुछ भी नहीं रहते। जिस दौर में हर पल जीवन असुरक्षित नजर आता हो तो संप्रेषण में नकारात्मकता यों ही आ जाती है। महात्मा गांधी हमें सतर्क करते हैं और वापस हमें अपने विचारों की ओर फिर से परखने को कहते हैं और उन्हें शुद्ध करने को भी। ये विचार शुद्ध होते हैं प्रार्थना, मदद, मौन और अनवरत कर्म से।
‘रोमा रोलां का भारत’ पुस्तक में इस घटना का जिक्र भी है कि जब गांधीजी के एक सहयोगी पियर्सन से रोमा रोलां ने पूछा कि महात्मा गांधी की धीमी आवाज भीड़ सुन कैसे पाती है तो पियर्सन कहते हैं कि भीड़ की नजर गांधी के होठों पर होती थी और वह समझ जाती थी कि गांधी कहना क्या चाहते हैं।
क्या बुरा दौर हमारी परीक्षा ले रहा है और कहीं यह हमें और रचनात्मक होने की प्रेरणा तो नहीं दे रहा है? महान संगीतज्ञ रविशंकर से 1948 में गांधीजी की मृत्यु के समय एक ऐसी दुखभरी धुन बनाने को कहा गया, जिसमें पीड़ा हो और पुकार भी। यह रविशंकर के लिए आसान नहीं था। पर कोई भी कठिन दौर उनके लिए वरदान बन जाता है जो इंसानियत के धुनों में जीते हैं। हुआ यह कि ‘गांधी’ नाम पर ही अचानक रविशंकर का सितार टिक गया। सरगम का तीसरा, छठा, सातवां सुर क्रमश: गा, धा, नी थे जो गांधी नाम में ही शामिल थे। बस क्या था, दुख और पीड़ा के बीच जन्म हुआ एक नए राग ‘मोहनकौस’ का।
यह संभव है कि हम सभी के अंदर एक नई आदत, नया विचार, ऐसी अच्छाई का जन्म हो जो हमें फिर पढ़ने-लिखने, मदद करने और साहस और आदर के अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करे। महात्मा गांधी रस्किन की ‘अन टू दिस लास्ट’ को पढ़ते हुए यह समझ बैठे थे कि धन जीवन नहीं होता, बल्कि जीवन ही धन होता है। चलिए हम भी इस दौर में जीवन को ही अपनी डायरी के पन्नों में प्रतिदिन ढूंढ़ते हैं और बजाते हैं उस ‘मोहनकौस’ को जो हर किसी को जीवन जीने और कुछ ज्यादा संवेदनशील और सहृदय बनने की प्रेरणा देगा।