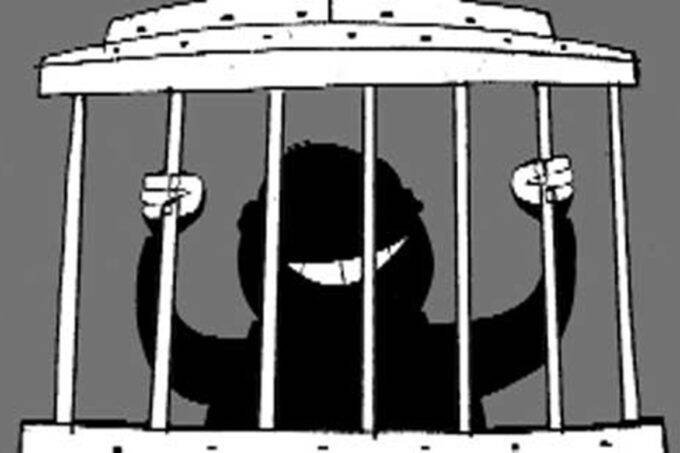हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के संदर्भ में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के खिलाफ एक याचिका की सुनवाई करते हुए राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर चिंता जाहिर की। शीर्ष अदालत ने कड़े शब्दों में कहा कि विधायिका राजनीति में दागी नेताओं को रोकने में असफल रही है। यों भी आंकड़ों पर नजर डालें तो यह अपने आप में ही परेशान कर देने वाले हैं। एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक संसद में तैंतालीस फीसद सांसदों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में नौ फीसद आपराधिक मामलों में लिप्त सांसदों की संख्या में वृद्धि हुई है। 301 सांसदों में बीजेपी के 116 सांसदों पर और कांग्रेस के 51 सांसदों में से 29 पर, डीएमके के 23 में से 10, तृणमूल कांग्रेस के 22 में से 9, जदयू के 16 में से 13 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
सवाल है कि क्या भारतीय राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है या फिर अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है। यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खोखला कर देगा, क्योंकि जिन जनप्रतिनिधियों को समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वही जनप्रतिनिधि अपराध की दुनिया से आते हों तो हम कैसे एक आदर्श लोकतंत्र स्थापित कर पाएंगे।
भारतीय राजनीति में दागी नेताओं का बढ़ते प्रभाव के कुछ प्रमुख कारण हैं। जब-जब भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास हुआ, तब अधिकतर राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। एक कारण है राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की अवहेलना। विधायिका द्वारा लाभकारी कानूनी संशोधन कर अपनी स्थिरता बनाए रखना और राजनीतिक अपराधों के मामले से निपटने के लिए त्वरित अदालतों की कमी होना भी अहम वजहें हैं। कुछ नेताओं के मामले दशकों से लंबित पड़े हुए हैं जो हमारी चुनावी सुधारों पर सवाल तो उठाता ही है, साथ ही यह न्यायपालिका को भी कठघरे में खड़ा करता है।
इसके अलावा, पूर्व में निर्मित कानूनों का बेहतर ढंग से उपयोग नहीं हो पाने की वजह से आज भी भारतीय राजनीति में बाहुबल और धनबल का बोलबाला है। यह बेवजह नहीं है कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद होता है, वह वहां से बैठे हुए भी चुनाव जीत जाता है। यह हमारी लोकतंत्र व्यवस्था पर प्रश्न चिह्न लगाता है, वहीं यह भारतीय मतदाताओं में जागरूकता की कमी को भी दर्शाता है। इसलिए अब समय की मांग है कि सरकारों, निर्वाचन आयोग और न्यायपालिका को इस खराब चलन को को बदलने के लिए तत्काल प्रभाव से कुछ सकारात्मक और ठोस पहल करनी होगी।
’सौरव बुंदेला, भोपाल, मप्र
समावेशी विकास
भारत में सरकारी आकड़ों में जनसंख्या को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग। सामान्य वर्ग के अंतर्गत वे जातियां शामिल हैं, जो सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक रूप से अग्रणी हैं। पिछड़े वर्ग के अंतर्गत वे जातियां हैं जो न तो बहुत जागरूक हैं, न ही सामाजिक व राजनीतिक रूप से सक्षम हैं। वहीं अनुसूचित जाति व जनजाति के अंतर्गत लोग हैं तो समाज में हाशिये पर रहे हैं। इन वर्गों या जातियों की संख्या का पता लगाने के लिए ब्रिटिश काल मे जनगणना के प्रावधान था। लेकिन आजादी के बाद 1951 की जनगणना में अनुसूचित जाति व जनजाति को छोड़ कर अन्य जातियों की जनगणना को बंद कर दिया गया। नतीजतन, जो जाति अपने वर्ग में हाशिये पर थी, वह आज भी वही हैं। ऐसी स्थिति में जातिवार जनगणना कर यह स्पष्ट करने की आवयश्कता है कि किस जाति की संख्या कितनी है। तभी स्पष्ट होगा कि सरकारी कार्यक्रमों में आरक्षण का लाभ किस जाति को कितना मिला रहा है और कौन अब भी वंचित है।
इससे नीति निर्धारण में भी सहायता मिलेगी। यह केवल सामाजिक न्याय से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि संविधान में प्रदत अधिकारों और मानवाधिकार से भी जुड़ा है। अगर जाति को खत्म करना है तो सबसे पहले हमें इनकी संख्या के सही आंकड़ों को इकट्ठा करना होगा। यह ठीक वैसे ही है, जिस प्रकार डॉक्टर बीमार मरीज के इलाज से पहले मरीज की जांच कर बीमारी की सही स्थिति का पता लगाता है और फिर उसके अनुसार दवा देता है।
’अनूप सिंह कुशवाहा, प्रयागराज, उप्र