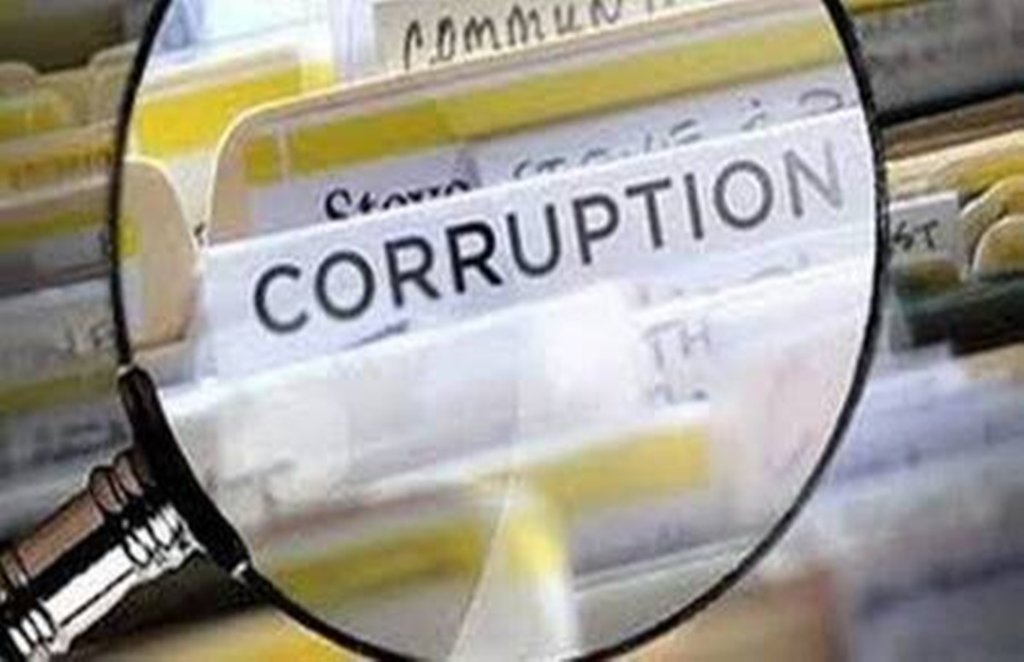भारत में भ्रष्टाचार का रोग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा, जहां भ्रष्टाचार ने अपने पंजे न गड़ाए हों। देश की सबसे छोटी इकाई पंचायत से लेकर शीर्ष स्तर के कार्यालयों और क्लर्क से लेकर बड़े अफसर तक आमतौर पर घूस के काम नहीं करना चाहते। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक-2019 के अनुसार भारत भ्रष्टाचार के मामले में एक सौ अस्सी देशों की सूची में अस्सीवें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2018 में भारत इस सूचकांक में अठहत्तरवें स्थान पर था।
लगभग हर दिन अखबारों, टीवी और रेडियो में एक खबर सबसे अधिक सुनने-देखने को मिलती रहती है, वह है भ्रष्टाचार की। हर दिन भ्रष्टाचार के काले करनामे उजागर हो रहे हैं। देश में भ्रष्टाचार को मिटाकर सभी नागरिकों को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना सरकार का काम ही नहीं, बल्कि राजनीतिक धर्म भी होता है। लेकिन आजादी से लेकर अब तक देश की सरकारें भ्रष्टाचार को मिटाने के दावे तो करती हैं, लेकिन इसमें विफल रही हैं।
दरअसल, जब तक भ्रष्टाचार की राजनीतिक बुनियाद पर चोट नहीं की जाती, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी मुहिम तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच सकती। चुनाव कितने खर्चीले हैं, चुनावों में कितना बेहिसाब धन बहाया जाता है, हर कोई जानता है। लेकिन यह कितने लोग जानते हैं कि यह सारा धन किन जगहों से, किन स्रोतों से जुटाया जाता है? चुनावों में खर्च होने वाले धन का अधिकांश स्रोत अज्ञात रहता है। जब तक चुनाव पूरी तरह पारदर्शी और सादगीपूर्ण नहीं होंगे, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पाएगा।
x7xy6cuभ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में जितना महत्त्व निगरानी तंत्र, संस्थाओं और कानूनों का है, उससे भी कहीं अधिक आवश्यकता इससे निपटने में लोगों की भागीदारी बढ़ाने की है। जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी, भ्रष्ट गतिविधियों का विरोध नहीं करेगी, तब तक केवल कानूनों के माध्यम से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। एक सुदृढ़ और सतर्क सिविल समाज ही भ्रष्टाचार पर प्रभावी निगरानी रख सकता है और तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को और अधिक जवाबदेह बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे बेहतर उदाहरण जापान है, जहां भ्रष्ट अधिकारियों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है।
जब तक आम जनमानस में यह धारणा पुष्ट नहीं की जाएगी कि भ्रष्ट व्यवस्था को बनाए रखने के मुकाबले इसे उखाड़ने वाले प्रोत्साहन अधिक हैं, तब तक इस समस्या से लड़ाई भी स्पष्ट नहीं हो सकेगी। महत्त्वपूर्ण सरकारी संस्थानों और कार्यालयों में नैतिकता का आकलन और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया में नागरिकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। सेवा स्तर का निर्धारण करके नागरिकों के चार्टर को भी और अधिक असरदार बनाया जा सकता है।
’गौतम एसआर, भोपाल, मप्र