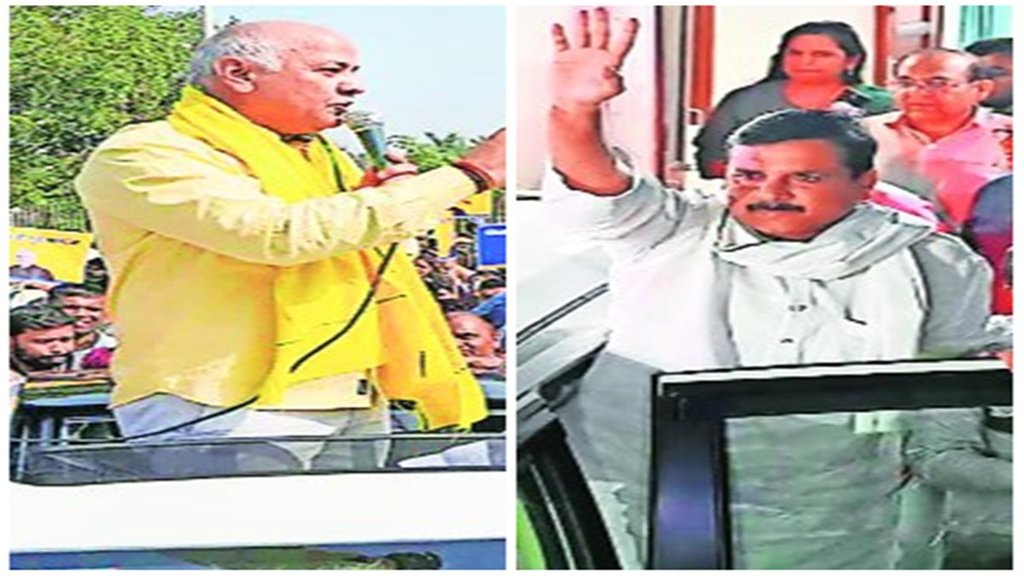पिछले लंबे समय से चल रहे विपक्ष बनाम जांच एजंसियों के विवाद में एक सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर अपराध का पैसा एक राजनीतिक दल को मिला है तो वह आरोपी क्यों नहीं है? फिर क्या था… जांच एजंसियों ने सवाल को हाथों-हाथ लिया और कहा कि वे इस पर विचार कर रही हैं। सुनवाई के इस मंथन से जो नया निष्कर्ष सामने आया है, वह राजनीतिक भ्रष्टाचार के विमर्श की पूरी भाषा बदल सकता है।
अदालत के सवाल से ज्ञान चक्षु खुलने के बाद अब सरकारी एजंसियों को यह मुफीद लग रहा है कि एक व्यक्ति को क्यों आरोपी बनाएं, जबकि इसका फायदा पूरा राजनीतिक दल उठाता है। यह विचार कितनी दूर तक आगे जाएगा, हम अभी आकलन नहीं कर सकते, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के खतरे को राजनीतिक दल भांप सकते हैं। आज इस पक्ष का पकड़ा जाएगा तो कल उस पक्ष की भी बारी आनी है। फिर अभी की तरह हर आरोपी ‘सत्ता शरणम्’ होना चाहेगा। राजनीतिक दलों के आपदाकाल की घोषणा करती टिप्पणी की विवेचना प्रस्तुत करता बेबाक बोल।
संगठित अपराध को बर्दाश्त करना ‘सब गंदा है, पर धंधा है’ जैसे सस्ते दर्शन को बढ़ावा देना है।- राबर्ट कैनेडी
भारतीय राजनीति में चुनावी दलों, गठबंधनों के बीच जो कर्ता सबसे ज्यादा क्रिया करता दिख रहा है, वे सीबीआइ और ईडी जैसी जांच एजंसियां हैं। प्रचंड बहुमत की सरकारें इससे पहले भी आई हैं, लेकिन इतना परेशानहाल विपक्ष पहले कभी नहीं दिखा था। विपक्ष ‘भूतो न भविष्यति’ जैसी इस स्थिति को लेकर अदालत तक पहुंच गया है कि हम ही क्यों!
विपक्षी दलों के त्राहिमाम के बीच दिल्ली शराब घोटाले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजंसियों से पूछा कि अगर आपके हिसाब से अपराध की रकम एक राजनीतिक दल को मिली तो उसे क्यों पक्षकार नहीं बनाया गया? अब हाल ही में हुई सुनवाई में जांच एजंसियों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि शराब घोटाले में वे राजनीतिक दल को पक्षकार बनाने पर विचार कर रही हैं। हालांकि सरकारी पक्ष की यह बात कोई रूप ले पाती है या नहीं, यह भविष्य के गर्भ में है।
जांच एजंसियों की दलील पर गौर किया जाए तो हमारे सामने कुछ कानून आते हैं। इनमें से एक है मकोका यानी ‘महाराष्ट्र कंट्रोल आफ आर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट।’ इसे 1999 में महाराष्ट्र में संगठित अपराध खत्म करने के मकसद से लागू किया गया था। फिर इसे दिल्ली में 2002 में लागू किया गया। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में दोषियों को ‘मकोका’ के तहत सजा सुनाई गई।
एक और कानून है जो कई राज्यों में लागू किया जा चुका है। वह है गैंगस्टर एक्ट। यह कानून किसी व्यक्ति नहीं, बल्कि अपराधियों के पूरे गिरोह के खिलाफ है। यह कानून संगठित अपराध की रोकथाम के लिए है, जिसमें निचले पायदान के गुर्गे से लेकर ऊपर बैठा डान तक है। माफिया डान दाऊद इब्राहिम का उदाहरण हमारे सामने है कि किस तरह मुंबई पर गुंडाराज-सा कायम था। देश के अन्य राज्य भी इस स्थिति से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं।
राजनीति में आर्थिक भ्रष्टाचार ऐसा अपराध है जो संगठित तरीके से ही किया जाता है। सभी मुख्यधारा के दलों पर इसमें शामिल होने के आरोप लगे हैं। जिस तरह कभी मुंबई में और बहुत हद तक अभी भी उत्तर प्रदेश में गैंगवार को सामान्य मान लिया गया था, उसी तरह देश की जनता के बीच राजनीतिक भ्रष्टाचार है। बोफोर्स को लेकर या यूपीए के भ्रष्टाचार को देख कर जनता सरकार तो बदलती है, लेकिन उसे भ्रष्टाचार से छुटकारा नहीं मिलता है।
कोर्ट के सवाल के बाद जांच एजंसी ने भ्रष्टाचार के आरोप में जिस तरह राजनीतिक दलों को आरोपी बनाने का मुद्दा उठाया है, वह कुछ-कुछ गैंगस्टर एक्ट जैसा ही है। इस नजरिये से हम 75 साल के हालात पर नजर डालें तो राजनीतिक दलों और गिरोहों के बीच समानता गौर करने लायक है। पहली यह है कि गिरोह संगठित होते हैं। इसी तरह राजनीतिक दलों का भी एक संगठित ढांचा होता है। जैसे राजनीतिक दलों में वरीयता क्रम होता है, वैसे गिरोह में भी। ऊपर आदेश देने से लेकर नीचे वसूली करने तक सबके काम बंटे होते हैं।
दूसरी समानता, सारे गिरोहों का एक सरगना होता है। इसे डान, बास, भाई आदि कई तरह के नाम दिए जाते हैं। राजनीतिक दलों का अगुआ भी ऐसा ही ‘अहं ब्रह्मास्मि’ वाला चेहरा रखने लगा है। पार्टी अध्यक्ष की जगह उसे सुप्रीमो या दीदी, दादा, भाई जैसा कुछ कहलवाना पसंद होता है। जिसकी छवि ‘मेरा वचन ही शासन है’ जैसी बन गई, वह उतना ही बड़ा ‘बाहुबली’ मान लिया जाता है। सभी के अनुशासन की जगह एक का शासन ही इन सुप्रीमो का लक्ष्य होता है।
तीसरी समानता, हर गिरोह का अपना इलाका होता है। अपने इलाके से बाहर जाकर अपराध करना माफिया कानून के खिलाफ है, जिसे जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। किसी ने दूसरे इलाके में थोड़े-बहुत पांव जमा भी लिए तो वह तब तक बाहरी ही माना जाता है जब कि उसे पूरी तरह बाहर नहीं कर दिया जाता है। राजनीतिक दलों का भी यही हाल है।
क्षेत्रीय क्षत्रप किसी चुनाव में अन्य राज्यों में कुछ फीसद सीटें जीत कर थोड़े समय के लिए राष्ट्रीय दल का दर्जा पा जाते हैं। लेकिन जल्दी ही बाहर से बहिष्कृत होकर अपने गृह-प्रदेश तक महदूद हो जाते हैं। एक पार्टी ने तो राष्ट्रीय बनने के लिए अपने नाम के आगे राज्य (तेलंगाना) का नाम हटा कर देश (भारत) का नाम जोड़ लिया। लेकिन नाम बदल देने से इलाका नहीं बदल जाता है। माफिया का यह नियम क्षेत्रीय क्षत्रप नहीं बदल पाए हैं।
चौथी अहम समानता है-संख्या बल। आज राजनीतिक दल इस बात की दुहाई देकर खुद को बड़ा साबित करते हैं कि हमारे दस करोड़ हैं, तुम्हारे दो करोड़ भी नहीं। संख्या बल दोनों के लिए अहम है। सारे आदर्श की बातें एक तरफ और बाहुबलियों का सुरक्षित टिकट एक तरफ। बाहुबलियों का अघोषित आरक्षण है। यह किसी भी जाति, धर्म और जेंडर का हो सकता है, बस आपको अपने भय से अपनी पकड़ बनाए रखनी है।
हालांकि संख्या बल में माफिया ज्यादा शुद्धतावादी हैं। अगर आप उनकी आपराधिक प्रवृत्ति से सहमत नहीं हैं तो आपको सदस्य बनाना तो दूर, वे आपको अपना दुश्मन मानेंगे। लेकिन राजनीतिक दल तो ‘मिस्ड काल’ से ही सदस्य बना लेंगे। नया खाता खोलने से पहले ‘जीमेल’ भी पूछता है कि आप प्रमाणित करें कि इंसान हैं या रोबोट। लेकिन राजनीतिक दलों को इससे मतलब नहीं है कि ‘मिस्ड काल’ देने वाला इंसान है या रोबोट, संख्या बढ़नी चाहिए। नेताओं को यह मतलब नहीं है कि ‘एक्स’ पर उनके कितने ‘फालोवर’ असली हैं। उन्हें सिर्फ ‘मिलियन’ में गणना चाहिए।
सबसे अहम पांचवीं समानता कि किसके खजाने में कितना पैसा है। खजाना ही तय करता है कि कौन कितना बड़ा है। जैसे-जैसे माफिया का प्रभाव बढ़ता है, उसका खजाना बढ़ता है। जब हमारे यहां देवताओं की भी ‘रैंकिंग’ कर दी जाती है कि कौन कितना धनवान है तो नेता तो धरती के ही हैं। हमारे कानों से यह शेखी टकराती रहती है कि हमारे पास इतने हजार करोड़।
जैसे कि हमने एक अंतर बताते हुए कहा कि सदस्यता को लेकर माफिया ज्यादा ईमानदार हैं, उसी तरह कमाई की बात भी है। माफिया गिरोह इस मामले में ईमानदार हैं। उनकी बुराई की कमाई की सबको पहचान है। वे किसी की जान बचाने के लिए ‘रखवाली शुल्क’ लेते हैं तो किसी से ‘अपने क्षेत्र’ में काम करने देने का कर वसूलते हैं। सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों के पास जीएसटी है तो गिरोह के पास जेजेबी (जाकी जैसी भावना)!
राजनीतिक दल अपनी काली कमाई को छिपाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गैर आपराधिक छवि बनानी है। इसके लिए चुनावी बांड जैसी धुलाई मशीन ले आई गई। चुनावी बांड की मशीन में जाते ही आपसे कोई हिसाब नहीं मांगेगा। राजनीतिक दलों के अलावा कोई और ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां आपको अपने पैसे का हिसाब नहीं देना पड़े। मंदिर एक ऐसी जगह थी, जहां दान गुप्त होता था और हिसाब से बाहर होता था, लेकिन सरकार को यह भी मंजूर नहीं था।
सरकार ने बहुत सारे मंदिरों का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। अब चढ़ावों में हेरफेर के मामले भी सामने आने लगे। भगवान के सामने सब एक हैं, के सिद्धांत को सरकार ने नकार दिया। वहां पर अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रभावियों को प्रथम बताया गया। आपकी साख इतनी मजबूत है तो आपका रास्ता अलग होगा। मंदिर परिसर में ‘प्रोटोकाल दफ्तर’ सरकारी धौंस का नमूना हैं।
एक अंतर और। गिरोह से जुड़े हर सदस्य की बांह पर ‘मैं चोर हूं’ का टैटू अलिखित में भी पढ़ लिया जाएगा। लेकिन राजनीतिक दलों के मामले में एक वैश्विक कहावत सटीक है- ‘जो पकड़ा गया वही चोर है’। गैंगस्टर एक्ट के तहत एक के पकड़े जाने के बाद सारे गिरोह की धर-पकड़ शुरू हो जाती है और वह अपनी अंतिम सांसें लेने लगता है। लेकिन राजनीति में एक के पकड़े जाने के बाद पूरे दल का शुद्धीकरण हो जाता है।
तो क्या राजनीति के भ्रष्टाचार में गिरोह सरीखा इंसाफ लाने का वक्त आ गया है? पहले-पहल तो हो सकता है कि एक पकड़ा गया, क्यों और कैसे पकड़ा गया! इसी में एक संदेश है- ‘सब दिन होत न एक समान’। तो एक दिन ऐसा आएगा कि दूसरे तरफ के भी पकड़े जाएंगे। फिर वही होगा जो आज हो रहा है। बचने के लिए आपको सत्तारूढ़ की शरण लेनी होगी। जेल से बच कर जैसे-तैसे आगे का राजनीतिक जीवन काट लेना होगा। वह सत्ता पक्ष में बाहरी की पहचान के साथ इसी सुकून के साथ रह लेगा कि जेल से तो बाहर है।
एक कदम आगे बढ़कर यह सवाल भी कि राजनीतिक दलों को अयोग्य साबित करेगा कौन? चुनाव आयोग जो एक लुंज-पुंज संस्था के रूप में अपनी साख खो रहा है? जो यह आंकड़े देता है कि फलां चुनाव में इतने हजार लीटर शराब पकड़ी? लेकिन उस पर कार्रवाई क्या होती है? सरकारी मालखाने में चूहे शराब पी जाते हैं और शराब आपूर्ति करने वाले राजनीतिक दल अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं।
चुनाव आयोग प्रस्ताव दे रहा है कि उम्मीदवारों को अखबारों में अपने अपराध के बारे में विज्ञापन देना होगा। यह कह कर चुनाव आयोग अपनी छवि अच्छी कर रहा, लेकिन उन आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों का होगा क्या? चुनाव जीत गए तो धुल गए! अभी कम से कम जनता के पास दिल बहलाने के लिए मतदान केंद्र जाने का जज्बा तो है।
अपराधी ही अपराधी वाला विज्ञापन दिखा कर आयोग जनता का मनोबल क्यों तोड़ना चाहता है, जबकि नेताओं के बाहुबल पर उसका कोई जोर नहीं। जो काला धन चुनाव आयोग ने पकड़ा, राजनीतिक दल उसे बिना फायदे वाला निवेश मान भूल गए। चुनाव आयोग ने आज तक कितने राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द की?
आयोग को राजनीति को अपराध से मुक्त करना है तो चुनावी बांड का स्रोत बताने के लिए क्यों नहीं कहता? अगर स्रोत पता चल भी जाता है तो कार्रवाई क्यों नहीं करता? इस शून्य कार्रवाई की वजह भ्रष्टाचार में ‘हम सब भाई-भाई है’ं वाला भाव है। आज इनके पकड़े जाएंगे तो कल हमारे पकड़े जाएंगे। देखते हैं भ्रष्टाचार में राजनीतिक दलों को आरोपी बनाने वाली फुसफुसाहट शोर में बदलती है या नहीं। यहां एक कहावत थोड़े बदलाव के साथ- ‘जब सारे चोर तो कोई न मचाए शोर।’