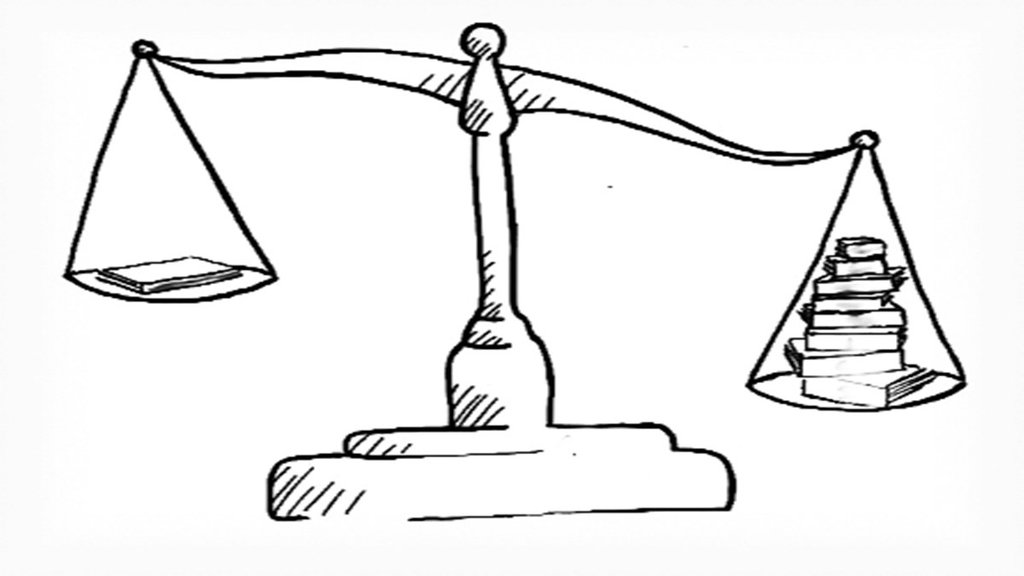एक समय था जब फिल्में दर्शकों को बांधने के लिए मनोरंजन का सहारा लेती थीं। तब साहित्य नैतिक मूल्यों के शीर्ष पर होता था। आज हालत यह है कि साहित्यिक मंच विज्ञापन लाने के नाम पर फिल्में और सस्ते मनोरंजन का सहारा ले रहे हैं। अब जब फिल्में यथार्थवादी बन रही हैं तो साहित्य के प्रतिनिधि ‘दर्शक-दीर्घा’ में भीड़ जुटाने के लिए द्विअर्थी गीतों के गायकों को साहित्य का मंच प्रदान करना न्यायोचित ठहराते हैं। सोशल मीडिया के खाते पर फिल्मी सितारों के साथ वाले कार्यक्रम में अपना आमंत्रण गर्व से दिखाते, साहित्यकार। किसी ने इसकी आलोचना कर दी तो कह दिया जाएगा-आपके लिए अंगूर खट्टे हैं। साहित्यकारों ने अभिव्यक्ति की सारी लड़ाई उन पत्रकारों के जिम्मे कर दी है जो जांच एजंसियों के सामने तारीख पर तारीख का सामना कर रहे हैं। ऐसे चमाचम समारोहों के इतर किसी और मंच पर ‘गोदी मीडिया’ की आलोचना कर बेचारा आलोचक अपनी इज्जत बचा लेता है कि देखिए मैंने ‘आलोचना’ की है। अभिव्यक्ति की लड़ाई में मेरा अहम योगदान है। साहित्य के ऐसे आ हत समय पर प्रस्तुत है बेबाक बोल।
रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलजुग आएगा किताब लिखने से पहले आलोचक विधि बताएगा
साहित्य की सबसे गंभीर विधा पर इस व्यंग्यात्मक लहजे में बात करने के लिए चारों दिशाओं, दिग-दिगंत से क्षमा। साहित्य के संदर्भ में बीसवीं सदी को आलोचकों की सदी भी कहा जा सकता है। साहित्य में आलोचक का स्थान आराध्य जैसा माना गया है। लेखक गीता में कृष्णोपदेश को ध्यान में रख कर रचना करता था कि कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो
यानी, तुम्हारे लिखे को आराध्य आलोचक किस तरह परखेंगे इसकी चिंता में पड़ गए तो कभी नव-सृजन नहीं कर पाओगे। लिखो और उसे आलोचकों के हवाले कर दो। हां, बीसवीं सदी वह सदी थी जहां पाठक से ज्यादा आलोचक अहम थे। क्योंकि तब आलोचना का मतलब निंदा नहीं होता था, समीक्षा का मतलब सिर्फ तारीफ नहीं होती थी। आलोचना का भाव उतना ही व्यापक होता था, जितना किसी भाषा और उससे जुड़े साहित्य का।
आज आलोचक नए अवतार में आ गए हैं। आलोचना का अकादमिक अध्ययन किया हो या न किया हो आप लेखन कैसे करें इसका फतवा देना शुरू कर देते हैं। आलोचक अपने सीमा क्षेत्र को लांघ कर लेखकों के क्षेत्र का जो अतिक्रमण कर रहे हैं वह बहुत खतरनाक है। बहुत से लेखकों पर यह खतरा हमला कर चुका है। पर, वे लहूलुहान होकर भी चुप हैं कि साहित्य की, कलम की इज्जत बची रहे। पाठकों को वे वैसी कठपुतली न दिखें जिसकी डोर मंच के लिए लेखक तैयार करने वाले आलोचक के हाथ में है।
किसी के सोचने-समझने की प्रक्रिया का प्रायोगिक परीक्षण होता है, लेखन। स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में भाषा के शिक्षण के बाद विद्यार्थियों को मौलिक लेखन के लिए प्रेरित किया जाता है। उनसे अपने परिवार, आस-पास, पालतू जानवरों के बारे में लिखने कहा जाता है। शिक्षकों की कोशिश रहती है कि लिखते वक्त बच्चे मौलिक रहें किसी वरिष्ठ या परिजनों का सहारा नहीं लें। बच्चे मौलिक नहीं रहेंगे तो उनके सोचने-समझने की क्षमता का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा।
अगर बच्चे लेखन में दूसरे की नकल करते हैं तो कुछ हास्यास्पद हादसे भी हो जाते हैं। जैसे कि दो बच्चों के पालतू जानवरों के नाम और हरकतें एक जैसी हो जाती हैं और शिक्षक के दरियाफ्त करने पर पता चलता है कि एक के घर में कुत्ता है तो दूसरे के घर में बिल्ली। कहने का आशय यह है कि स्कूल में प्राथमिक कक्षाओं का प्रशिक्षण मौलिक लेखन का होता है। शिक्षक उसकी वर्तनी और व्याकरण ही ठीक करते हैं, उन्हें यह आदेश नहीं देते कि तुम्हें अपने पालतू कुत्ते के बारे में वैसे ही लिखना चाहिए जैसे मैं कहता हूं।
स्कूल में स्थापित इस बुनियादी नियम की सीमा को आज के आलोचकों ने मानने से इनकार कर दिया है। अब लेखक अपनी पांडुलिपी के छापेखाने से आने के बाद प्रथम प्रति उन्हें समर्पित करने नहीं जाता। अब वे खुद गाहे-बगाहे वैसे लोगों को फोन कर लेते हैं जो अपनी सोच-समझ के साथ लिख रहे हैं। आलोचक इन लेखकों को बताते हैं कि आप फलां पद पर हैं तो आपको इस तरह की किताब, कविता या उपन्यास लिखना चाहिए।
फिर आप हर मंच पर होंगे। आप फलां पद पर हैं तो आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए। लेखक के शील धर्म को तुला पर रख कर उसके पदनाम के हिसाब से ‘श्लीलता’ का भी पैमाना तय किया जाएगा कि आप सत्तर के दशक के सिनेमा की तर्ज पर फूल से फूल टकराते हुए जैसा ही दृश्य लिखें या आज के ‘ओटीटी’ मंचों के सिनेमा की तरह खुले दृश्य। लब्बोलुआब यह कि लेखक को आलोचक के सुझाए गए विषयों के इतर दाएं-बाएं सोचना भी नहीं चाहिए। तभी आपको खास मंच पर जाने का मौका दिया जाएगा। तभी आप आज के साहित्यकार होंगे।
आलोचक का सर्वप्रथम ‘धर्म’ होता है कि वह किसी रचना की समालोचना भाषा-विज्ञान, इतिहास बोध और समय बोध पर करे। लेखक युग-बोध में कितना आगे बढ़ा और कितना पीछे छूटा व समकालीनों में क्या खासियत रखता है। क्या उसके लेखन में समाज के लिए कोई वृहत्तर संदेश है? याद रखिए, लिखा गया हर किस्सा अपने समय का हिस्सा होता है। सभ्यता के विकास में इंसान ने सबसे पहले किस्सागोई ही सीखी है। लेखन की हर विधा मूल रूप में किस्सा ही है।
अगर आलोचक इस किस्सागोई में हस्तक्षेप करेगा तो सबसे पहला नुकसान खास समय और उसके संदर्भों को होगा। खास सत्ता में खास आलोचकों की विधि से तैयार साहित्य समाज की एकरंगी तस्वीर ही प्रस्तुत करेगा। एक जैसा पढ़ते-समझते और एक जैसा लिखते लोग। लेखन कारखाने का वैसा कथ्य यानी उत्पाद हो जाएगा, जिसकी गुणवत्ता वहां का ‘मैनेजर’ तय करेगा।
किसी भाषा और उसके साहित्य का स्तर उसके आलोचकों के स्तर से तय होता है। बात करें हिंदी साहित्य की। पूरी दुनिया की तरह भारत भी राजनीतिक व सामाजिक विसंगतियों से गुजर रहा है, क्योंकि मूल मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का किसी के पास कोई समाधान नहीं है। लेकिन, हिंदी साहित्य के उत्सवमयी माहौल को देखें तो बाहरी भाषा और संस्कृति का कोई व्यक्ति अंदाजा नहीं लगा जा सकता कि यह देश अभी किस हाल से गुजर रहा है। जांच एजंसी के दफ्तरों से लेकर अदालतों में पत्रकार हाजिर हो रहे हैं। उनके लैपटाप, फोन जब्त कर लिए गए हैं।
दूसरी ओर, हिंदी पट्टी के एक छोर से दूसरे छोर तक महोत्सव ही महोत्सव है। इतना महोत्सव और उसकी इतनी तस्वीरें कि आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएं। महोत्सव कोने-कोने पर हो रहा, लेकिन लेखक और आलोचक चुनिंदा हैं। आलोचकों को तो अपने लिए एक सहायक रखने की जरूरत महसूस हो रही होगी इस बात का हिसाब-किताब रखने के लिए कि इन महोत्सवों में उन्होंने कितने लेखकों और उनकी रचनाओं को कालजयी घोषित किया होगा। प्रकाशन समूह भी धन्य-धन्य हो कर पोस्टर जारी कर रहे कि ‘हमारे’ लेखक इस मंच पर जा रहे हैं।
आलोचक एक बात में भारतीय धर्म परंपरा के वाहक हैं। वे गणेश को आदर्श मानते हैं जो मां-बाप की परिक्रमा कर पूरी दुनिया की परिक्रमा करने का दावा कर गए। आलोचकों की भी यही सदिच्छा है कि लेखक उनके आस-पास घूर्णन करते रहें। ऐसा करने वाले लेखकों को आलोचक वैश्विक छवि का घोषित कर देते हैं। महोत्सव के मंच पर से उनकी नजर सीधे कुर्सियों पर होती है कि कितने लेखकों ने उनके लिए ताली बजाई, और कार्यक्रम खत्म होने के बहुत देर पहले ‘एक सफल कार्यक्रम’ के कैप्शन के साथ तस्वीर सोशल मीडिया के खाते पर लगाई।
हिंदी साहित्य के आलोचकों ने वस्तुनिष्ठता का बोझ पत्रकारिता की पीठ पर लाद दिया है। वे और उनसे जुड़े लेखक पत्रकारिता का आकलन कर उन्हें गोदी व अ-गोदी मीडिया का खिताब बांटते रहते हैं। वहीं, आलोचकों की गोदी में बैठे लेखकों के छवि प्रबंधन का पूरा ध्यान रखा जाता है कि वे जनसरोकारी दिखाए जाते रहें।
आलोचना साहित्य की शीर्ष संस्था है। सारी संस्थाओं की तरह आलोचना भी ढह चुकी है। आज आलोचक सिर्फ निंदक व प्रशंसक की भूमिका में हैं। आज के दौर में कबीर भी प्रासंगिक नहीं रह गए कि निंदक नियरे राखिए। कबीर ने यह दोहा स्वमूल्यांकन के लिए कहा था कि आप अहंकार में न आ जाएं। लेकिन ये निंदक बने आलोचक तो हर बात पर पूछने आ जाते हैं कि बता तू क्या है? ये आप में इतनी हीन भावना डाल देंगे कि अहंकार आपको अपमानित कर चला जाएगा। इसलिए, खुद को बचाए रखने के लिए कबीर को दरकिनार कर हम गालिब की तरह पलटवार करेंगे-ये अंदाज ए गुफ्तगू क्या है?